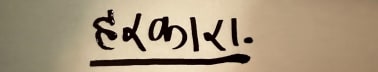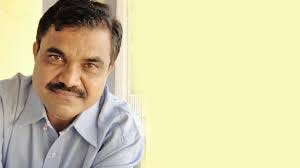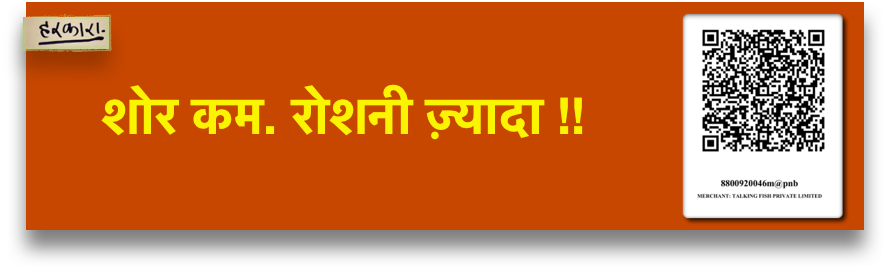02/11/2025 : ममदानी पर श्रवण गर्ग | स्मार्ट सिटी पर आकार पटेल | जातीय जनगणना पर आनंद तेलतुंबडे | नर्मदा पर राकेश दीवान
‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.
निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फ़लक अफ़शां
आज इतवार के दिन कुछ महत्वपूर्ण लगने वाले लेखों , टिप्पणियों का दिन.
श्रवण गर्ग : ज़ोहरान ममदानी जिससे ट्रंप से लेकर मोदी समर्थक तक परेशान हैं?
न्यूयॉर्क शहर में मेयर का चुनाव हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज दुनिया के सबसे शक्तिशाली गलियारों से लेकर दिल्ली और तेल अवीव की राजधानियों तक साफ़ सुनाई दे रही है. इस वैश्विक हलचल के केंद्र में हैं 34 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी, गुजराती मुस्लिम मूल के एक उम्मीदवार, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो गुजरात में होते तो शायद सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ पाते. आज वही ज़ोहरान दुनिया के सबसे अहम शहर का नेतृत्व करने की दौड़ में हैं और उनके सामने कोई एक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप, इज़राइल की ताक़तवर लॉबी, अमेरिका का कॉर्पोरेट जगत और भारत की दक्षिणपंथी ताक़तें एक साथ खड़ी हैं.
ज़ोहरान ममदानी, मशहूर फ़िल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं और उनके पिता युगांडा से विस्थापित हुए एक गुजराती शिया मुस्लिम विद्वान हैं. ज़ोहरान की पहचान सिर्फ़ उनके परिवार तक सीमित नहीं है. वह न्यूयॉर्क की राजनीति में एक ऐसी ताक़त बनकर उभरे हैं, जो स्थापित व्यवस्था को सीधे चुनौती दे रही है. उनकी लड़ाई एक बहुआयामी मोर्चे पर है:
डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी: ट्रंप ने ज़ोहरान को हराने के लिए अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है. उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ज़ोहरान जीते तो वह उन्हें गिरफ़्तार करवा देंगे.
कॉरपोरेट जगत और अमीर तबका: ज़ोहरान के मुद्दे सीधे तौर पर न्यूयॉर्क के आम और ग़रीब लोगों से जुड़े हैं, जो अमेरिका के अरबपति और कॉर्पोरेट वर्ग को डरा रहे हैं.
इज़राइल लॉबी: ज़ोहरान ने इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुलेआम “युद्ध अपराधी” (War Criminal) कहा है और फ़िलिस्तीन राष्ट्र के समर्थन में आवाज़ उठाई है.
भारत का दक्षिणपंथ: ज़ोहरान ने गुजरात दंगों का ज़िक्र करते हुए नरेंद्र मोदी की तुलना नेतन्याहू से की थी और बाबरी विध्वंस की भी निंदा की. इसके बाद भारत में एक वर्ग ने उन्हें “हिंदू विरोधी” और “पाकिस्तानी” प्रचारित करना शुरू कर दिया.
ख़ुद की पार्टी का एक धड़ा: हैरानी की बात यह है कि ज़ोहरान अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी के कॉर्पोरेट समर्थक नेताओं से भी लड़ रहे हैं, जिन्होंने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया है.
ज़ोहरान के मुद्दे: क्यों डरा है अमेरिका का अमीर तबका?
ज़ोहरान की लोकप्रियता का राज़ संविधान या लोकतंत्र बचाने जैसे बड़े नारों में नहीं, बल्कि उन बुनियादी मुद्दों में छिपा है जो न्यूयॉर्क के 80 लाख लोगों की ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं. उनके प्रमुख वादे हैं:
नफ़रती अपराधों के ख़िलाफ़ बजट में 800% की वृद्धि.
शहर में सभी के लिए मुफ़्त और तेज़ बस सेवा.
अपार्टमेंट के किराए पर चार साल की रोक, ताकि ग़रीबों को घर से न निकाला जा सके.
बच्चों की देखभाल के लिए मुफ़्त यूनिवर्सल चाइल्ड केयर प्रोग्राम.
अवैध प्रवासियों की सुरक्षा का वादा और ट्रंप प्रशासन को न्यूयॉर्क में घुसने से रोकने की चेतावनी.
यह एजेंडा साफ़ तौर पर दिखाता है कि ज़ोहरान की राजनीति का केंद्र जनता है, न कि कॉर्पोरेट मुनाफ़ा.
ज़ोहरान ममदानी का उभार भारतीय राजनीति के लिए भी कई दिलचस्प तुलनाएं और सवाल खड़े करता है. 34 साल के ज़ोहरान और 36 साल के तेजस्वी यादव में एक समानता दिखती है. दोनों युवा हैं और अपने-अपने देश की सबसे शक्तिशाली सत्ता को चुनौती दे रहे हैं.
लेकिन सबसे बड़ा सवाल 55 वर्षीय राहुल गांधी के लिए उठता है. ज़ोहरान 34 साल की उम्र में जो साहस दिखा रहे हैं, वह राहुल गांधी अपने लंबे राजनीतिक करियर में क्यों नहीं दिखा पाए? ज़ोहरान अमेरिका जैसे गन-कल्चर वाले देश में अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया के सबसे ताक़तवर नेताओं को सीधे चुनौती दे रहे हैं. जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी से ज़ोहरान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “ज़ोहरान जैसे मित्र हों तो भारत को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है. वह पाकिस्तान की ज़ुबान बोलते हैं.” यह दिखाता है कि ज़ोहरान की राजनीति ने भारत की मुख्यधारा की पार्टियों को भी असहज कर दिया है.
ज़ोहरान ममदानी का चुनाव सिर्फ़ न्यूयॉर्क का मेयर चुनने तक सीमित नहीं है. यह इस बात का प्रतीक बन गया है कि क्या एक युवा नेता बिना कॉर्पोरेट चंदे के, सिर्फ़ जनता के मुद्दों के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी ताक़तों को हरा सकता है. अमेरिका में कोई चुनाव आयोग नहीं है और न ही वोट चोरी का वैसा डर, जैसा कई अन्य देशों में होता है. इसलिए नतीजा जो भी हो, यह चुनाव दुनिया भर में तानाशाही प्रवृत्तियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है.
यह चुनाव दिखाता है कि जब राजनीति जन-पक्षधर होती है और अपने बुनियादी मूल्यों की ओर लौटती है, तो जनता की ताक़त के आगे बड़े-बड़े साम्राज्य भी हिल जाते हैं. ज़ोहरान की जीत या हार, दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी और दुनिया भर के विपक्षी दलों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि राजनीति का असली मक़सद क्या है – अरबपतियों के हितों की रक्षा करना या कामगारों और आम नागरिकों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना.
आकार पटेल: हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मलबे पर खड़े हैं
मैं घर से निकलकर सड़क पर आता हूँ और चारों तरफ़ देखता हूँ. 10 साल पहले के मुक़ाबले कुछ ख़ास नहीं बदला है, सिवाय इसके कि ट्रैफ़िक और बढ़ गया है.
कुछ दिन पहले की एक हेडलाइन थी, ‘करोड़ों ख़र्च हुए, स्मार्ट सिटीज़ मिशन अपने पीछे और बिल, और सतही बुनियादी ढाँचा छोड़ गया’. रिपोर्ट वही बात कहती है जो उन लोगों के लिए साफ़ है जो अपने आस-पास की चीज़ों पर ग़ौर करते हैं: कि इस साल ख़त्म हुए 10 साल के एक प्रोग्राम का कोई असर नहीं हुआ है. अब जबकि ये ख़त्म हो चुका है और दफ़्न हो गया है, और इस पर आगे कोई वादे नहीं किए जाएँगे, तो हम इसके बचे-खुचे हिस्सों को खंगाल सकते हैं.
स्मार्ट सिटीज़ मिशन को एक कॉन्सेप्ट नोट के साथ शुरू किया गया था जिसमें कहा गया था कि इसका मक़सद ऐसे शहर बनाना है जो ‘हर निवासी को जीने के ठीक-ठाक विकल्प’ देंगे. शहरी मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज़ पर कॉन्सेप्ट नोट के मुताबिक़, ये शहर ‘किसी भी विकसित यूरोपीय शहर के बराबर बहुत ऊँची गुणवत्ता वाला जीवन’ प्रदान करेंगे. सरकार ने कहा था कि ऐसा 2020 तक हो जाएगा. अरुण जेटली ने 2014 में संसद को बताया था कि इन स्मार्ट सिटीज़ की ज़रूरत उस मिडिल क्लास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थी, जिसका मोदी की आर्थिक नीतियों से बहुत विस्तार होने वाला था. अगले साल, 2015 में, भाषा को थोड़ा बदल दिया गया ताकि लक्ष्य को और मामूली बनाया जा सके, और किसी यूरोपीय शहर की नक़ल करने के बजाय, हमें बताया गया कि भारत का स्मार्ट सिटी नागरिकों को पर्याप्त पानी, पक्की बिजली सप्लाई, सफ़ाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग़रीबों के लिए सस्ते घर, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा मुहैया कराएगा. ये, ज़ाहिर है, उससे अलग नहीं था जिस पर सभी शहरों की नगरपालिकाएँ वैसे भी ध्यान दे ही रही थीं. समस्या सख़्त गवर्नेंस की थी, न कि सिर्फ़ लोगो और नाम बदलने की. शायद यही वजह है कि मोदी सरकार की इसमें दिलचस्पी लगभग तुरंत ही कम हो गई. 2021 में ख़बर आई कि ‘स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट उड़ान भरने में नाकाम रहा, और इसका आधा फंड ख़र्च ही नहीं हुआ’. रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रोजेक्ट को ‘2020 तक तो अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए था’, लेकिन हक़ीक़त यह थी कि 2019 तक, 2015-19 के बीच ‘स्वीकृत’ किए गए कुल 48,000 करोड़ रुपये में से सिर्फ़ आधा ही असल में आवंटित किया गया था. इस आधे में से भी, सिर्फ़ तीन-चौथाई ही असल में जारी किया गया, और जो जारी हुआ उसमें से महज़ 36 प्रतिशत का ही इस्तेमाल हुआ. जहाँ 48,000 करोड़ रुपये ‘स्वीकृत’ किए गए थे, वहीं ख़र्च सिर्फ़ 6,160 करोड़ रुपये हुए.
शहरी विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि वह ‘मिशन के तहत ज़मीनी स्तर पर अब तक हुई असल प्रगति को लेकर हैरान’ है और उसने ‘एक एजेंसी द्वारा दूसरी एजेंसी के काम को बिगाड़ने के कई मामले’ भी देखे. 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, 26 ने जारी किए गए फंड का 20 प्रतिशत से भी कम इस्तेमाल किया था. भारत से जुड़ी आम समस्याएँ भी सामने आईं. स्थायी समिति ने कहा कि वह यह देखकर ‘हैरान है कि उपलब्ध तंत्र होने के बावजूद, मिशन के तहत ख़राब काम की शिकायतें अभी भी समिति के सामने आ रही हैं’. समिति ने सिफ़ारिश की कि ‘स्थानीय सांसदों की तरफ़ से स्मार्ट सिटीज़ के तहत किए गए काम के दावों पर सवाल उठाने वाले सभी मामलों की तेज़ी से जाँच की जाए और दोषियों को सज़ा दी जाए’.
जो मीडिया संस्थान इस मुद्दे में अब भी दिलचस्पी ले रहे थे, उनकी ख़बरों ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन की कुछ मुख्य ख़ामियों को उजागर किया. इसने हाई-एंड इंफ़्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर आधारित निगरानी पर तो ज़ोर दिया, लेकिन पानी, स्कूल, सरकारी अस्पताल, और घर जैसी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया. अपने एरिया-आधारित विकास के साथ, इसका ज़्यादातर ध्यान शहर के बीच के उन छोटे-छोटे हिस्सों पर पैसा ख़र्च करने पर था जो पहले से ही विकसित थे. मिसाल के तौर पर, बेंगलुरु में, स्मार्ट सिटीज़ का पैसा चर्च स्ट्रीट को विकसित करने पर इस्तेमाल किया गया - जो शहर के बाक़ी ज़्यादातर हिस्सों से पहले ही ज़्यादा विकसित थी - और इंफ़ेंट्री रोड, कामराज रोड, टाटा लेन, वुड स्ट्रीट, कैसल स्ट्रीट, डिकेंसन रोड, केंसिंग्टन रोड, सेंट जॉन्स रोड, रेज़िडेंसी रोड, कस्तूरबा रोड, बोरिंग हॉस्पिटल रोड, मिलर्स रोड, लैवेल रोड, मैक्ग्राथ रोड, कॉन्वेंट रोड, क्वींस रोड, हेस रोड, राजा राम मोहन रॉय रोड और रेस कोर्स रोड जैसे पॉश इलाक़ों पर ख़र्च हुआ.
दिल्ली में, यह नई दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाला इलाक़ा था, जो पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सबसे विकसित हिस्सा है. यह मिशन एक ख़ास तबके, यानी अपर क्लास, पर केंद्रित था, जो आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, न कि किसी नए-नवेले मिडिल क्लास पर, जिसे मोदी की आर्थिक नीतियों ने वैसे भी पैदा नहीं किया. यह अभिजात्य वर्ग वाला रवैया दूसरी जगहों पर भी दिखा, जैसे कि पुणे, दिल्ली, भोपाल और कोयंबटूर सहित कई शहरों में लागू की गई पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग परियोजना में. कंपनी की वेबसाइट पर साइकिल किराए पर लेने के निर्देश सिर्फ़ अंग्रेज़ी में थे और यह सिर्फ़ ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार करती थी. स्मार्ट सिटीज़ भारत के शहरी ग़रीबों को और भी हाशिए पर धकेल रहे थे. 2019 में ‘आवंटन’ 2018 के बराबर ही रहा. और, 2021 के बजट में, ‘स्मार्ट सिटीज़’ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया. शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवार ने इसकी वजह बताई: ‘इन स्मार्ट सिटीज़ को देश के दूसरे शहरों के लिए लाइटहाउस यानी रोशनी दिखाने वाला बनना था. बजट इस पर पूरी तरह से चुप है क्योंकि यह मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी में से एक बन गया है.’
शायद इसीलिए आपको पता भी नहीं चला होगा कि (एक आकर्षक नाम होने के अलावा) इस प्रोग्राम का मक़सद क्या था, इसने असल में क्या बदलाव लाया, या यह कि यह प्रोग्राम अब ख़त्म कर दिया गया है, और इसका ज़िक्र फिर कभी नहीं किया जाएगा.
आनंद तेलतुंबडे: ‘लोग सरकार के सामने नंगे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए परदे के पीछे’
विद्वान और कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे ने भीमा कोरेगांव मामले में एक विचाराधीन कैदी के तौर पर 31 महीने तालोजा सेंट्रल जेल में बिताए. उन्हें नवंबर 2022 में ज़मानत पर रिहा किया गया था. अपनी नई किताब ‘द सेल एंड द सोल: ए प्रिज़न मेमॉयर’ में, उन्होंने जेल में बिताए अपने समय, महामारी, जेल की व्यवस्थागत विफलताओं और वहां मिले लोगों के बारे में विस्तार से लिखा है. एक और नई किताब, ‘द कास्ट कॉन सेंसस’ में, उन्होंने जाति जनगणना की मांग के पीछे के विचारों और इसके संभावित परिणामों का मूल्यांकन किया है. द कैरेवन के सहायक संपादक, अजीत महाले ने तेलतुंबडे से उनकी हालिया किताबों, जाति जनगणना के विचारों, जेल के समय की यादों, असहमति के अपराधीकरण और अन्य मुद्दों पर बात की.
अपनी रिहाई के बाद के जीवन के बारे में तेलतुंबडे ने कहा, “मेरा पूरा जीवन अस्त-व्यस्त और विस्थापित हो गया है. मैंने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बिग डेटा में एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया था. लेकिन 2018 में मुझे इस मामले में फंसा दिया गया, जिसके कारण अप्रैल 2020 में मेरी गिरफ्तारी हुई. मेरी विदेश में रहने या पढ़ाने की योजना थी, लेकिन अब मैं भारत के भीतर भी यात्रा नहीं कर सकता.”
जेल में अपने सबसे बुरे दिनों को याद करते हुए, उन्होंने स्टेन स्वामी की मृत्यु और एक पुलिस मुठभेड़ में अपने भाई के मारे जाने का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, “ये वास्तव में विनाशकारी घटनाएं थीं. स्टेन का गुजरना—वास्तव में हम में से किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी. स्टेन पार्किंसंस के अलावा काफी स्वस्थ थे. अगर उन्हें भी समय पर बाहरी अस्पताल ले जाया गया होता, तो वे भी बच जाते. दूसरी घटना, मेरे भाई की हत्या, एक सुन्न कर देने वाला सदमा था.”
जाति जनगणना पर अपनी नई किताब ‘द कास्ट कॉन सेंसस’ लिखने के पीछे की वजह बताते हुए तेलतुंबडे ने कहा कि यह एक लेख से शुरू हुई. उन्होंने बताया, “जब इस जनगणना ने लोगों का ध्यान खींचा, तो फ्रंटलाइन ने मुझे एक लेख लिखने के लिए कहा. उस लेख पर अच्छी चर्चा हुई, जिसके बाद नवयाना प्रकाशन ने मुझसे इसे एक किताब में विकसित करने के लिए संपर्क किया.”
तेलतुंबडे का तर्क है कि अगर समानता लक्ष्य है, तो जाति जनगणना इसे कभी पूरा नहीं कर सकती. वे कहते हैं, “जाति जनगणना दृश्यता का एक उपकरण है. लेकिन उसके आगे क्या? समानता लाने के लिए, संरचनात्मक फेरबदल की आवश्यकता है. यह काम सिर्फ जनगणना नहीं कर सकती. यह एक राजनीतिक इच्छाशक्ति है जो तय करती है कि जाति-जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कैसे किया जाए.” उन्होंने अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि जाति एक ‘धारणा’ है, कोई भौतिक चीज़ नहीं, जिसे सटीक रूप से मापा जा सके. उन्होंने इसे समाज की एक ‘सेल्फी’ बताया, जो जातिगत पहचान को और गहरा कर सकती है और जिसका फायदा केवल राजनेता उठा सकते हैं.
राजनीतिक दलों की भूमिका पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है. राहुल गांधी ने कांशीराम के नारे ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ के साथ इसे उठाया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि हिस्सेदारी किस चीज़ में होगी. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा के अनुसार जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ़ है, लेकिन अब उसने अपना रुख बदल लिया है. तेलतुंबडे का अनुमान है कि बीजेपी जाति जनगणना का इस्तेमाल लंबे समय में जाति-आधारित आरक्षण को खत्म करने और इसे आर्थिक आधार पर लाने के लिए कर सकती है. उन्होंने कहा, “बीजेपी की विचारधारा समरसता—यानी सद्भाव—की वकालत करती है, समता यानी समानता की नहीं.”
देश में हाल की जातिगत घटनाओं पर, तेलतुंबडे ने कहा कि ये घटनाएं इसलिए खबर बनीं क्योंकि वे उच्च-पदस्थ लोगों से जुड़ी थीं, लेकिन दलितों के खिलाफ़ अत्याचार और अपमान एक सामान्य बात है. उन्होंने कहा कि 2014 से जातिगत अपराधों के लिए एक स्पष्ट दंडमुक्ति का माहौल बना है.
असहमति को ‘शहरी नक्सल’ (Urban Naxal) के रूप में ब्रांड करने की प्रवृत्ति पर, उन्होंने कहा, “उन्होंने एक विरोधाभास, ‘अर्बन नक्सल’ का आविष्कार किया, ताकि हर उस व्यक्ति को इसमें शामिल किया जा सके जिसे राज्य या पुलिस पसंद नहीं करती. एक बार जब आप पर ‘नक्सल’ या ‘शहरी नक्सल’ का लेबल लग जाता है, तो आप अपनी जाति खो देते हैं. यह लोगों को चुप कराने के लिए एक रणनीतिक उपकरण बन गया है.”
सरकार द्वारा डेटा के उपयोग पर उन्होंने एक गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा, “सरकार के पास लोगों के बारे में हर तरह का डेटा है. लेकिन जब लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा की बात आती है, तो सरकार ने इसे या तो मुश्किल बना दिया है या अनुपलब्ध. विषमता यह है कि लोग सरकार के सामने नग्न हैं, लेकिन सरकार, जिसे इस देश के वास्तविक संप्रभु यानी लोगों के प्रति पारदर्शी होना चाहिए, वह उनके लिए अपारदर्शी है.”
‘चरमपंथियों के साथ जातिगत हितों को जोड़ना अमेरिका में काम नहीं आया’: 2025 वाइकोम पुरस्कार विजेता
अमेरिका के सबसे बड़े दलित नागरिक अधिकार संगठनों में से एक, ‘इक्वलिटी लैब्स’ की सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, थेनमोझी सुंदरराजन को तमिलनाडु सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के लिए वाइकोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आर्टिकल-14 को दिए एक साक्षात्कार में, उन्होंने अमेरिका में जाति-विरोधी आंदोलन, जाति के आघात (trauma) और वैश्विक राजनीति पर अपने विचार साझा किए.
सुंदरराजन ने कहा कि अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच जातिवाद को फिर से स्थापित होते देखना भयावह है. उन्होंने अपनी किताब ‘द ट्रॉमा ऑफ़ कास्ट’ का हवाला देते हुए कहा कि जाति का घाव एक “आत्मा का घाव” है, जिससे न केवल उत्पीड़ित, बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को भी उबरने की ज़रूरत है. उन्होंने तर्क दिया कि प्रमुख जाति के लोगों की तंत्रिका प्रणाली (nervous systems) जाति-उत्पीड़ित लोगों के साथ समानता को बर्दाश्त नहीं कर पाती है.
सुंदरराजन ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के उदय और भारत में हिंदुत्व की राजनीति के बीच समानताएं बताईं. उन्होंने कहा, “कई प्रमुख जाति के भारतीय हिंदुओं ने इस विचार के साथ ट्रंप को वोट दिया कि वह उनके हितों का ध्यान रखेंगे. लेकिन अब वे इसके भयानक परिणाम देख रहे हैं, क्योंकि इससे नफ़रती भाषण, घृणा अपराध और वीज़ा तथा स्टेटस के नुक़सान में वृद्धि हुई है. विशेषाधिकार आपको राष्ट्रवाद और उग्रवाद से नहीं बचाता.” उन्होंने कहा कि चरमपंथी और राष्ट्रवादी हितों के साथ जातिगत हितों को जोड़ने की उनकी शर्त अमेरिका में काम नहीं आई.
अमेरिका में लोकतंत्र के पतन पर चिंता व्यक्त करते हुए, सुंदरराजन ने कहा कि नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए यह एक विनाशकारी क्षण है. उन्होंने कहा, “हम लोकतंत्र के बाइडेन-युग के संस्करण में वापस नहीं जा रहे हैं. इस पहले साल में हुए नुक़सान ने दशकों के नागरिक अधिकार कार्यों को पहले ही समाप्त कर दिया है.” उन्होंने कहा कि अब लोगों को केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय भविष्य के वास्तुकार बनने की दिशा में काम करना होगा.
उन्होंने उत्पीड़ित लोगों के बीच वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और कहा कि दलित नारीवादियों ने दुनिया भर के अन्य नारीवादी आंदोलनों के साथ भौतिक एकजुटता बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि दुख और पीड़ा लोगों को आत्म-चिंतन के लिए प्रेरित कर सकती है और शायद सुलह और सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है.
राकेश दीवान | नर्मदा बचाओ आंदोलन
इतिहास के पन्नों से गुम होती एक नदी की आत्मा
जब हम नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम लेते हैं, तो कुछ चेहरे हमारी आँखों के सामने कौंध जाते हैं. मेधा पाटकर, आलोक अग्रवाल और कुछ दूसरे बड़े नाम. हम उनकी कुर्बानियों, उनके भाषणों और उनके संघर्ष को याद करते हैं. लेकिन क्या आंदोलन सिर्फ़ इन चंद नामों का संग्रह है. या इसकी जड़ें उन हज़ारों लोगों में हैं, जिनकी ज़मीनें डूबीं, घर डूबे, और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस लड़ाई को दे दी.
वरिष्ठ पत्रकार और नर्मदा के किनारे पले-बढ़े राकेश दीवान जब यह सवाल उठाते हैं, तो यह सिर्फ़ एक सवाल नहीं रहता, बल्कि एक गहरा दर्द बनकर उभरता है. एक ऐसा दर्द, जो आंदोलन की सबसे बड़ी ताक़त और सबसे बड़ी चूक, दोनों को एक साथ उजागर करता है.
राकेश दीवान की चिंता बहुत बुनियादी है. वो पूछते हैं कि जब आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें कौन होगा. क्या सिर्फ़ राकेश दीवान, मेधा पाटकर, नंदिनी ओझा जैसे पढ़े-लिखे, शहरी कार्यकर्ताओं के नाम होंगे. उन हज़ारों लोगों का क्या, जो असल में आंदोलन की नींव हैं, जो ख़ुद ही आंदोलन हैं. दीवान कहते हैं, “हमारा योगदान उनके सामने कुछ भी नहीं है.”
यह एहसास उन्हें भोपाल में हुए एक अनशन के दौरान हुआ. 27-30 दिन चले उस अनशन में मेधा पाटकर के साथ लुवारिया, सीताराम काका और कम्मुजी भी बैठे थे. लेकिन अख़बारों और टीवी चैनलों पर सिर्फ़ मेधा की कहानियाँ थीं. बाक़ी तीन चेहरे अदृश्य थे. राकेश ने महसूस किया कि ये लोग सिर्फ़ आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, वे अपने आप में एक पूरी कहानी हैं. वे इस लड़ाई में कैसे आए, उनके सपने क्या थे, उनकी उम्मीदें क्या थीं.
इसी सोच ने उन्हें इन गुमनाम नायकों की कहानियों को दस्तावेज़ बनाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने अपनी एक दोस्त जयश्री से कहकर उन तीनों अनशनकारियों के जीवन-चित्र लिखवाए, जो इंदौर के ‘नई दुनिया’ अख़बार में सम्मान के साथ छपे. यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने एक बड़े सवाल को जन्म दिया.
राकेश दीवान उन मार्मिक पलों को याद करते हैं, जब अनशन के बाद निमाड़ लौटने पर कम्मुजी पर फूल बरसाए गए, तो वह फूट-फूटकर रो पड़ीं. उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि समाज में बिना किसी हैसियत वाली उन जैसी महिला को आंदोलन की वजह से ऐसा सम्मान मिलेगा. यह सम्मान सिर्फ़ कम्मुजी का नहीं था, यह उस हर आम इंसान की आवाज़ थी, जिसे आंदोलन ने एक पहचान दी थी.
दीवान ने इन कहानियों को सहेजने की कोशिश भी की. दिल्ली से एक ख़ास टेप रिकॉर्डर लाए, जो धीमी गति से रिकॉर्डिंग चला सकता था, ताकि उसे सुनकर लिखा जा सके. उन्होंने रहमत जैसे युवाओं को यह ज़िम्मेदारी दी. लोगों से कहा कि वे अपने अनुभव एक-दो पन्नों पर लिखकर दें. कुछ लोगों ने लिखा भी, लेकिन यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि आंदोलन की दूसरी गतिविधियों में वे इतना उलझे थे कि इस काम को पूरा समय नहीं दे पाए.
वह गुमान नाम के एक पोलियो ग्रस्त लड़के की कहानी सुनाते हैं, जो अपनी ट्राइसाइकिल पर एक यात्रा के पीछे-पीछे चल पड़ा और फिर आंदोलन के दफ़्तर की जान बन गया. उसका जुनून ऐसा था कि कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे पोस्टर चिपकाने के लिए होशंगाबाद पहुँच गया. रहमत और आशीष जैसे स्कूली बच्चों की कहानी, जो नारे लिखते-लिखते आंदोलन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक बन गए. दीवान पूछते हैं, “इनकी कहानियाँ कौन लिखेगा.”
उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि यह काम संस्थागत रूप से नहीं हो सका. उन्होंने छात्रों को पीएचडी के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही. उन्होंने अपने दोस्तों को नर्मदा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए बुलाया, लेकिन उन्हें आंदोलन के भीतर से कोई मदद नहीं मिली.
राकेश दीवान का मानना है कि लोगों की कहानियों का दस्तावेज़ीकरण करना किसी बड़े मंच से भाषण देने से ज़्यादा ज़रूरी था. अगर यह काम हुआ होता, तो आज निमाड़ और मालवा में एक ज़्यादा बड़ी और जागरूक राजनीतिक शक्ति खड़ी होती, जो अपने इतिहास और समाज को अपनी नज़रों से देखती.
आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि सियाराम काका जैसे दार्शनिक और पूंजीयाभाई जैसे अनगिनत लोग अपनी कहानियों के साथ इस दुनिया से चले गए. एक पूरा खज़ाना लुट गया. दीवान का यह अफ़सोस हर उस शख़्स का अफ़सोस है, जो मानता है कि आंदोलनों का इतिहास शासकों की तरह नहीं, बल्कि लोगों की ज़ुबानी लिखा जाना चाहिए.
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.