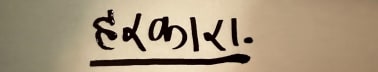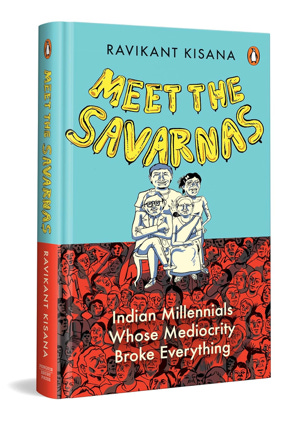06/07/2025: चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फरियाद | ठाकरे बंधु साथ | आय की असमानता ब्रिटिश राज से भी बुरी | गडकरी तक चिंतित | गोयल फिर बोले | सवर्णों को आईना | डिंडी यात्रा में संविधान
‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.
निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल
आज की सुर्खियां :
3 करोड़ से अधिक मतदाता हो सकते हैं बाहर, एनजीओ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयोग के इस कदम से बिहार के 75-80% मतदाता हो जाएंगे बेदखल : छोकर
आय और संपत्ति की असमानता ब्रिटिश राज से भी बदतर, 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति पर काबिज
नितिन गडकरी के मुताबिक भी गरीबों की आबादी बढ़ रही है और धन अमीर के हाथों में जा रहा है
पटना में भाजपा नेता गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, 6 साल पहले बेटे को भी मारा था
पीयूष गोयल फिर बोले, अबकी अमेरिका को घुड़की, दावों का हमने किया रियलिटी चैक
उद्धव और राज 20 साल बाद साथ आए
स्टैन स्वामी को किसने मारा?
आरएसएस को संविधान वाला भारत नहीं, मनुस्मृति वाला भारत चाहिए: भंवर मेघवंशी
सवर्णों की खोज ख़बर: जाति पर जहां सबसे ज़्यादा सन्नाटा है, वहीं सबसे ज्यादा क्रूर उत्पीड़न भी
संजय हेगड़े: दो लोकतंत्रों में तानाशाही की प्रतिध्वनि
वारी के दौरान संविधान की बात
बिहार
3 करोड़ से अधिक मतदाता हो सकते हैं बाहर, एनजीओ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
'द हिन्दू' की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने के फैसले को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) नामक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन ने इस प्रक्रिया को संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और वकील नेहा राठी ने चुनाव आयोग की 24 जून की अधिसूचना को चुनौती दी है और मांग की है कि इस आदेश को असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और लोकतंत्र के लिए घातक घोषित किया जाए. क्या है एडीआर की आपत्ति?
एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया ने वोटर सूची में नाम जोड़ने की जिम्मेदारी राज्य से हटाकर आम नागरिकों पर डाल दी है, जो असंवैधानिक है।
जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, उनमें आधार और राशन कार्ड को वैध प्रमाण नहीं माना गया है, जिससे गरीब, दलित, आदिवासी और प्रवासी श्रमिकों के मताधिकार पर खतरा मंडरा रहा है.
अनुमानित 3 करोड़ मतदाता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिये के समुदायों से, इस प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं.
याचिका में बताया गया है कि “विशेष गहन पुनरीक्षण आदेश के तहत न केवल नागरिक को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है, बल्कि माता-पिता की भी नागरिकता के प्रमाण देने होंगे. जिनके पास ये दस्तावेज़ नहीं हैं, उनका नाम या तो ड्राफ्ट रोल में जोड़ा ही नहीं जाएगा या पूर्ववत हटा दिया जाएगा.”
अव्यवहारिक समयसीमा और चुनावी दबाव
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक हुए नियमित विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) के बाद दोहराई जा रही है, जिसे ADR ने “चुनावी दबाव में किया गया अनुचित फैसला” बताया है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि बिहार एक गरीब, पिछड़ा और उच्च पलायन दर वाला राज्य है, जहां लाखों नागरिकों के पास जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या माता-पिता की नागरिकता से जुड़ा कोई वैध कागज़ नहीं है.
इतने कम समय में दस्तावेज़ जुटाना "असंभव" है और इस तरह की शर्तें लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा कदम हैं.
योगेन्द्र यादव ने भी उठाई आवाज़ : चुनावी सुधारों के लिए जाने जाने वाले कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट में अलग याचिका दायर कर विशेष गहन पुनरीक्षण को “मतदाता सूची का पुनर्लेखन” करार दिया है. उन्होंने कहा कि - “विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में पूरी मतदाता सूची दोबारा तैयार की जा रही है, जो गरीबी, अशिक्षा और दस्तावेज़ों की कमी से जूझ रहे लाखों मतदाताओं के लिए वोट का अधिकार छीन लेने जैसा है.” बिहार में नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. यदि विशेष गहन पुनरीक्षण की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहती है, तो कई विपक्षी दलों की आशंका है कि इससे चुनाव परिणामों में गड़बड़ी, मतदाता सहभागिता में गिरावट और जनप्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं.
चुनाव आयोग के इस कदम से बिहार के 75-80% मतदाता हो जाएंगे बेदखल : छोकर
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के संस्थापक सदस्य प्रो. जगदीप छोकर ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना की है. “द वायर” में करण थापर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह न केवल गलत है, बल्कि हास्यास्पद और अनावश्यक भी है. उनका मानना है कि इस प्रक्रिया के कारण बिहार के 75-80% मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं. इससे 18 वर्ष से अधिक आयु के वे बिहारी, जो संशोधित सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें भारत का नागरिक न मानकर 'गैर-नागरिक' घोषित किया जा सकता है.
चुनाव से ठीक चार महीने पहले, जब बिहार में मानसून और बाढ़ का समय है, यह प्रक्रिया शुरू करना अव्यवहारिक है. बहुत से लोग मजदूरी या काम के लिए बिहार से बाहर होते हैं, ऐसे में वे दस्तावेज़ कैसे देंगे? जिनका जन्म जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें जन्म प्रमाणपत्र या 11 अन्य दस्तावेज़ों में से कोई देना होगा. बिहार में 2000 तक केवल 3.7% जन्म ही पंजीकृत थे, 2007 तक भी यह संख्या 25% ही थी. सबसे आम दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, और वोटर आईडी को मान्य दस्तावेज़ों की सूची में नहीं रखा गया है. पीएसयू आईडी, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट आदि बहुत कम लोगों के पास हैं. 80,000 बूथ लेवल अधिकारियों को 3 दिन में प्रशिक्षित करना अव्यवहारिक है. इतने कम समय में हर घर तक पहुंचना और दस्तावेज़ इकट्ठा करना असंभव है.
गरीब, पिछड़े, दलित, मुस्लिम और आदिवासी सबसे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेज़ नहीं हैं. इससे बड़ी संख्या में लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे.
कानूनी और प्रशासनिक खामियां : प्रो. छोकर के अनुसार, कानून चुनाव आयोग को पुनरीक्षण का अधिकार देता है, लेकिन प्रक्रिया और दस्तावेज़ तय करने में पारदर्शिता और व्यावहारिकता का अभाव है. आयोग ने राजनीतिक दलों या नागरिक समाज से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया.
प्रो. छोकर का कहना है कि चुनाव आयोग का असली काम नागरिकों को वोट देने में मदद करना है, न कि उन्हें बाहर करना. इस तरह की प्रक्रिया से लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को गंभीर खतरा है. उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को प्रक्रिया को सरल और समावेशी बनाना चाहिए.
आय और संपत्ति की असमानता ब्रिटिश राज से भी बदतर, 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति पर काबिज
वित्तीय विश्लेषक हार्दिक जोशी का कहना है कि आज भारत में आय और संपत्ति की असमानता उस स्तर से भी अधिक हो गई है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान थी. उनके अनुसार, भारत की कुल संपत्ति के 40.1% हिस्से पर 1% सबसे अमीर लोग काबिज़ हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 6.4% संपत्ति है. इसी तरह, शीर्ष 10% लोग देश की 57.7% राष्ट्रीय आय कमाते हैं.
जोशी के मुताबिक, यह असमानता कोई संयोग नहीं, बल्कि नीतिगत परिणाम है. उन्होंने लिखा, "आधी आबादी बचे-खुचे संसाधनों के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि एक छोटा सा वर्ग अकल्पनीय ऐशो-आराम में जी रहा है."
आय और संपत्ति की असमानता के कारण:
अमीरों के पक्ष में टैक्स नीति
मज़दूरों के लिए कमज़ोर सुरक्षा
कंपनियों का बढ़ता एकाधिकार
रियल एस्टेट और शेयर बाज़ार से होने वाले लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं, जिनके पास पहले से पूंजी है
अमीरों द्वारा चुनावी चंदा, मीडिया को प्रभावित करना, और पुनर्वितरण के विरोध में लॉबिंग
जोशी का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था असमानता को दूर करने के बजाय उसे और मज़बूत करती है. “इकोनॉमिक टाइम्स” में प्रकाशित लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि "असमानता से जिनके पास ताकत है, उन्हें नुकसान नहीं होता — बल्कि फायदा होता है. वे चुनावों को फंड करते हैं, मीडिया की दिशा तय करते हैं, और पुनर्वितरण के खिलाफ लॉबी करते हैं."
समाधान के लिए सुझाव: जोशी ने सरकार से संपत्ति पर टैक्स लगाने, मज़दूरों की सुरक्षा बढ़ाने, और स्वास्थ्य व शिक्षा में निवेश बढ़ाने की अपील की है. वे लिखते हैं, "जब तक असली राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं होगी, यह समस्या और बढ़ती जाएगी." उन्होंने असमानता को 'प्राकृतिक' मानने की धारणा पर सवाल उठाया है और कहा है कि "यह सिस्टम टूटा नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसा बनाया गया है. अब समय आ गया है कि हम यह पूछें कि यह व्यवस्था आखिर किसके हित में है?”
भारत में गरीबी रेखा की सच्चाई, 3 डॉलर 62 रुपये होता है, 255 रुपये नहीं : हाल के महीनों में भारत की गरीबी दर को लेकर कई खबरें आई हैं. 25 अप्रैल को भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज़ में दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं. यह दावा वर्ल्ड बैंक के “गरीबी और समानता के सार-पत्र” (पीईबी) के आधार पर किया गया. इसके बाद, वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा की नई पद्धति और स्तर जारी किए. इसके अनुसार, अब केवल 5.75% भारतीय अत्यधिक गरीबी में हैं, जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा 27% था. लेकिन, “द इंडियन एक्सप्रेस” के डिप्टी एसोसिएट एडिटर उदित मिश्रा ने अपने लेख में भारत में गरीबी की सच्चाई बताई है. उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा के लिए आय का जो नया स्तर तय किया है, उससे ताज़ा आंकड़ों पर सवाल खड़ा होता है.
वर्ल्ड बैंक के ताजा आंकड़ों से क्या पता चलता है?
पहला : नए अनुमानों के अनुसार, भारत में पहले की तुलना में गरीबी दर कम थी. उदाहरण के लिए, 1977-78 में गरीबी दर 64% नहीं, बल्कि 47% थी.
दूसरा : वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा को अब $3 प्रतिदिन कर दिया है. इस नए आय स्तर के हिसाब से 2011-12 में 27% (करीब 34.44 करोड़) लोग अत्यधिक गरीबी में थे, जो 2022-23 में घटकर करीब 6% (7.5 करोड़) रह गए.
क्या $3 प्रतिदिन का मतलब 255 रुपये प्रतिदिन है? ऐसा नहीं है. 3 डॉलर की गणना ‘क्रय शक्ति समानता’ (पीपीपी) के आधार पर होती है, न कि सीधे डॉलर-रुपये विनिमय दर से. 2025 में पीपीपी के अनुसार 3 डॉलर प्रतिदिन 62 रुपये के बराबर है, न कि 255 रुपये.
भारत में गरीबी रेखा कैसे तय होती है? भारत ने 2011-12 में अंतिम बार आधिकारिक गरीबी रेखा तय की थी, जो 2009 में प्रो. सुरेश तेंडुलकर समिति की सिफारिश पर आधारित थी. इसके बाद 2014 में रंगराजन समिति ने नई पद्धति सुझाई, लेकिन उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया. अब भारत या तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक या वर्ल्ड बैंक की गरीबी रेखा का उपयोग करता है.
वर्ल्ड बैंक की गरीबी रेखा कैसे बनती है? वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले 1990 में प्रतिदिन 1 डॉलर की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा तय की थी, जो पीपीपी के आधार पर थी. समय के साथ महंगाई बढ़ने पर इसे बढ़ाकर अब 3 डॉलर प्रतिदिन कर दिया गया है. भारत के लिए 2025 में यह 62 रुपये प्रतिदिन है.
भारत में घरेलू गरीबी रेखा (पिछले वर्षों में) :
2009: शहरी क्षेत्र में 17 रुपये/दिन, ग्रामीण में 12 रुपये/दिन
तेंडुलकर समिति (2009) : शहरी 29 रुपये/दिन, ग्रामीण 22 रुपये/दिन
2011-12: शहरी 36 रुपये/दिन, ग्रामीण 30 रुपये/दिन
रंगराजन समिति (2014): शहरी 47 रुपये/दिन, ग्रामीण 33 रुपये/दिन
भारत में गरीबी के आंकड़ों पर विवाद क्यों? कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि अद्यतन घरेलू गरीबी रेखा और मजबूत डेटा की कमी के कारण भारत में गरीबी के आंकड़े काफी भिन्न हो सकते हैं. गरीबी दर 2% से 82% तक हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन-सी गरीबी रेखा और पद्धति अपनाई जाती है. भारत में गरीबी की वास्तविकता, आंकड़ों और पद्धतियों के चयन पर निर्भर करती है. वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जहां 5.75% लोग अत्यधिक गरीबी में हैं, वहीं 83% भारतीय प्रतिदिन 171 रुपये या उससे कम पर जीवनयापन कर रहे हैं.
नितिन गडकरी के मुताबिक भी गरीबों की आबादी बढ़ रही है और धन अमीर के हाथों में जा रहा है
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को गरीबों की "बढ़ती" संख्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है. नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि धन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, जहां उन्होंने कृषि, विनिर्माण, कराधान और बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित कई मुद्दों पर बात की. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, "धीरे-धीरे गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए". उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से बढ़ना चाहिए कि रोजगार पैदा हों और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो. उन्होंने कहा, "हम एक ऐसे आर्थिक विकल्प पर विचार कर रहे हैं जो रोजगार पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा. धन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है, और उस दिशा में कई बदलाव हुए हैं". वरिष्ठ भाजपा नेता ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को उदार आर्थिक नीतियों को अपनाने का श्रेय भी दिया, लेकिन अनियंत्रित केंद्रीकरण के खिलाफ आगाह किया. उन्होंने कहा, "हमें इसके बारे में चिंतित होना होगा". भारत की आर्थिक संरचना का उल्लेख करते हुए, उन्होंने जीडीपी में क्षेत्रीय योगदान में असंतुलन की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, "विनिर्माण का योगदान 22-24 प्रतिशत, सेवाओं का 52-54 प्रतिशत है, जबकि कृषि, 65-70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को संलग्न करने के बावजूद, केवल लगभग 12 प्रतिशत का योगदान करती है". स्वामी विवेकानंद का आह्वान करते हुए, गडकरी ने कहा, "जिसका पेट खाली हो, उसे दर्शन नहीं सिखाया जा सकता".
पटना में भाजपा नेता गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, 6 साल पहले बेटे को भी मारा था
बिहार के प्रमुख व्यवसायी और भाजपा नेता गोपाल खेमका की शुक्रवार देर रात पटना के गांधी मैदान इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात 'पनाश' होटल के पास घटी, जब खेमका अपने 'ट्विन टॉवर' आवास लौट रहे थे. हमलावर ने करीब 11 बजे रात को उन पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। खेमका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. 2018 में खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की भी इसी तरह हत्या कर दी गई थी.
हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है. गोपाल खेमका पटना के जाने-माने व्यवसायी और मगध अस्पताल के मालिक थे. उनकी हत्या से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है. विपक्ष ने इस हत्याकांड के बाद राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. पुलिस पर यह आरोप भी लगे कि घटना की सूचना मिलने के बाद भी टीम मौके पर देर से पहुंची.
पीयूष गोयल फिर बोले, अबकी अमेरिका को घुड़की, दावों का हमने किया रियलिटी चैक
'द हिंन्दू' की रिपोर्ट है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत किसी डेडलाइन के दबाव में वार्ता नहीं करता, बल्कि वह राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए ताकत की स्थिति से वार्ता करता है. बेंगलुरु में IIT मद्रास और IIT मद्रास एलुमनाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित ‘संगम 2025’ सम्मेलन में बोलते हुए गोयल ने कहा— “भारत आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो दुनिया में किसी से भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है. यह वह कमजोर भारत नहीं है जो कांग्रेस और यूपीए के शासन में था, जहाँ राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हुए समझौते किए जाते थे.” यह बयान उस समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई 2025 की समयसीमा से पहले एक मिनी-ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है.
गोयल ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने ऐसे समझौते किए जो देश के हित में नहीं थे, जबकि मोदी सरकार के तहत भारत ने कई महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं— जैसे कि मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ. भारत-UK FTA हाल ही में हुआ है. अमेरिका, यूरोपीय संघ, ओमान, पेरू और चिली जैसे देशों से बातचीत जारी है. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय टेक पेशेवरों को H-1B वीज़ा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज “वर्क फ्रॉम होम” के ज़रिए भारत में रहते हुए ही दुनिया के लिए काम किया जा सकता है. गोयल ने कहा कि भारत को वैश्विक मंदी के असर से बाहर निकालने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना और नवाचार ज़रूरी है.
नई योजनाओं की घोषणा
₹10,000 करोड़ के डीप टेक फंड की दूसरी किश्त की घोषणा
कैबिनेट द्वारा ₹1 लाख करोड़ का RDI (अनुसंधान, विकास और नवाचार) स्कीम पास—जो निजी क्षेत्र को 50 साल के लिए ब्याजमुक्त फंडिंग देगा
पीयूष गोयल का बयान लोकलुभावन और आत्मविश्वास से भरा जरूर है, लेकिन ज़मीनी हालात अलग हैं. आप अमेरिकी दबाव और भारत की तैयारी पर नज़र डालते हैं, तब कई विरोधाभास साफ़ नज़र आते हैं.
यहां हरकारा के पाठकों के लिए हमने पीयूष गोयल के हर प्वाइंट पर हकीकत की परत चढ़ाने की कोशिश की है...
हकीकत: ताकत की स्थिति या मजबूरी में समझौता?
अमेरिका और भारत जुलाई 9 की तय डेडलाइन पर “मिनी ट्रेड डील” को अंतिम रूप देने की हड़बड़ी में हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 12 देशों को टैरिफ चेतावनी भेजने की तारीख (7 जुलाई) घोषित कर दी है. मतलब भारत पर सीधा दबाव है.
हकीकत: "यूपीए ने राष्ट्रीय हितों के ख़िलाफ़ समझौते किए, हम नहीं करते"
WTO में भारत ने फूड सब्सिडी को लेकर कई बार झुकाव दिखाया — जिसे खेती-किसानों के लिए बड़ा खतरा बताया गया था.
कई क्षेत्रों में (जैसे कि कृषि और ऑटोमोबाइल) भारत को अपने टैरिफ खोलने पड़ रहे हैं, जबकि विकसित देश अपने नॉन-टैरिफ बैरियर्स को बनाए रखे हैं.
हकीकत: "H-1B वीजा की ज़रूरत नहीं, काम यहीं से करो"
कई टेक कंपनियां अभी भी हायरिंग में H-1B पर निर्भर हैं.
भारत में रिमोट वर्क की सुविधा मेट्रो सिटी तक सीमित है ग्रामीण या छोटे शहरों में इंटरनेट और पावर कट जैसे बुनियादी मुद्दे अब भी हैं.
दुनिया में "वर्चुअल गिग इकोनॉमी" के नाम पर कम वेतन, बिना सुरक्षा वाले अस्थायी जॉब्स बढ़ रहे हैं — क्या यही है आत्मनिर्भरता?
हकीकत: "₹1 लाख करोड़ का RDI फंड और ₹10,000 करोड़ का डीप टेक फंड"
कौन सी कंपनियों को मिलेगा यह पैसा? अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इसका क्रियान्वयन ढांचा क्या होगा.
पहले भी कई स्कीमें बनीं, लेकिन नतीजे कागज़ी रहे (जैसे: स्टार्टअप इंडिया फंड, स्किल इंडिया).
क्या यह पैसा कॉरपोरेट्स को ब्याजमुक्त फायदा देने के लिए है या सचमुच R&D के लिए?
उद्धव और राज 20 साल बाद साथ आए
‘हां, हम गुंडे हैं... थप्पड़ मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ’
करीब दो दशकों बाद एक मंच पर आए चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार के उस विवादित फैसले को पलटने का जश्न मनाया, जिसमें राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की योजना थी. मराठी अस्मिता की रक्षा के नाम पर हुई इस पुनर्मिलन रैली में उद्धव ठाकरे ने दृढ़ता के साथ कहा, “हां, हम गुंडे हैं; अगर न्याय पाने के लिए हमें गुंडा बनना पड़े, तो हम गुंडागर्दी करेंगे."
'थप्पड़ मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ' : राज ठाकरे ने उद्धव से पहले भाषण दिया. उन्होंने मराठी में कहा, "चाहे यहां कोई गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे मारने की जरूरत नहीं है. हां, अगर कोई नाटक करे, तो उसे कान के नीचे मारो. लेकिन, अगर किसी को मारो, तो उसका वीडियो मत बनाओ. जिसे मारा गया है, वही बताएगा कि उसे मारा गया है; आपको सबको बताने की जरूरत नहीं. " राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को श्रेय दिया कि उन्होंने वह कर दिखाया जो हजारों लोग नहीं कर सके. कहा-"उद्धव और मैं 20 साल बाद साथ आ रहे हैं... जो बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, वह देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया."
बीजेपी और सहयोगियों पर हमला : राज ठाकरे ने बीजेपी और उसके सहयोगियों से कहा, "आपकी ताकत विधानसभा में है, हमारी ताकत सड़क पर है." आरोप लगाया कि अगर हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता, तो अगला कदम मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश होती. उन्होंने अन्य राज्यों से हो रहे प्रवास का भी जिक्र किया और कहा कि हिंदी भाषी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए लोग गैर-हिंदी राज्यों में जा रहे हैं. "अगर हिंदी इतनी मददगार होती, तो ये राज्य पिछड़े क्यों रहते?"
‘सत्ता में साथ आएंगे’ उद्धव ठाकरे ने कहा, "भाषाई पहचान के सवाल पर, राज, मैं और यहां मौजूद सभी लोग एकजुट हैं. हम साथ आए हैं और साथ रहेंगे. हम मुंबई महानगरपालिका और महाराष्ट्र में सत्ता में आएंगे." उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ का एजेंडा देश पर थोप रही है. हमें हिंदू, हिंदुस्तान से कोई दिक्कत नहीं है. हम हिंदुत्व की विचारधारा की रक्षा करेंगे, लेकिन मराठी भाषा में.
स्टैन स्वामी को किसने मारा?
“मैंने अपनी आँखों से देखा कि कैसे संवेदनहीन जेल अधिकारियों और उनकी लापरवाही ने स्टैन स्वामी की जान ले ली. तलोजा जेल में 84 वर्षीय स्टैन की हालत का बिगड़ना साफ दिख रहा था. मेडिकल स्टाफ यह सब देखता रहा”
फादर स्टैन स्वामी और अरुण फरेरा नागरिक समाज के उन 16 सदस्यों में से थे - वकील, प्रोफेसर, कवि - जिन्हें 2018 में पुणे के पास भीमा कोरेगांव गांव में हुई जातिगत हिंसा से जुड़े एक मामले में आतंकवाद-विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था. स्क्रोल ने अरुण फरेरा का लेख प्रकाशित किया है. इसे एल्गार परिषद मामले के नाम से भी जाना जाता है - यह 1818 में एक लड़ाई में दलित सैनिकों की भूमिका की याद में आयोजित एक बैठक का नाम था, जिसमें उन्होंने पेशवा की सेना को हराया था, जिनकी प्रतिष्ठा जातिवादी होने की थी.
सरकार का दावा है कि गिरफ्तार किए गए 16 लोगों ने देश भर में हिंसा और आतंक के अन्य कृत्यों को भड़काने की साजिश रची थी. लेकिन तब से, स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने तकनीकी रिपोर्ट पेश की हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ जुटाए जा रहे सबूत हैकर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्लांट किए गए थे. फरेरा को स्वामी के साथ जेल अस्पताल में कैद किया गया था. उन्हें अब जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन शर्तों में से एक यह है कि वह मीडिया में इस मामले के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते. "यह एक स्वाभाविक मौत नहीं है, बल्कि एक कोमल आत्मा की संस्थागत हत्या है," 5 जुलाई, 2021 को फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु के तुरंत बाद जारी किए गए एल्गार परिषद मामले में आरोपी लोगों के परिवार के सदस्यों के बयान में लिखा है. कुछ लोग इन शब्दों को स्टैन की उम्र (वह 84 वर्ष के थे) और स्वास्थ्य (उन्हें पार्किंसंस रोग था) को देखते हुए थोड़ा कठोर मान सकते हैं. हालाँकि, तलोजा जेल में स्टैन के साथ किए गए संवेदनहीन व्यवहार को देखते और अनुभव करते हुए, मैं उनके दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए इच्छुक हूँ. 5 दिसंबर, 2020 को, स्टैन के अनुरोध पर, अधिकारियों ने मुझे जेल अस्पताल में उनकी कोठरी में रहने की अनुमति दी. वह चाहते थे कि उन्हें उनके सह-आरोपियों में से किसी एक के साथ रखा जाए ताकि कुछ सार्थक बातचीत हो सके. वह कोविड का समय था: किसी भी आरोपी को अदालत नहीं ले जाया जा रहा था, परिवार या दोस्तों के साथ कोई शारीरिक मुलाकात की अनुमति नहीं थी, कोई अखबार नहीं आने दिया जाता था और जेल में सभी कैदियों की आवाजाही पर प्रतिबंध था. स्टैन के लिए, हम बाकी लोगों की तरह, अपने सह-आरोपियों के संपर्क में रहना और बातचीत करना ही सब कुछ था.
जिस समय स्टैन ने मुंबई के बाहर तलोजा जेल में प्रवेश किया, जेल अस्पताल में चिकित्सा देखभाल की निगरानी BAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) की डिग्री वाले तीन लोगों और एक फार्मासिस्ट द्वारा की जाती थी. यह स्थिति कोविड से पहले और उसके दौरान थी. इन मुट्ठी भर कर्मचारियों के अलावा, दवाइयाँ देने, अंतःशिरा इंजेक्शन लगाने, पैरा-मेडिकल सहायता और वार्डों में मदद जैसे अन्य सभी कार्य कैदियों द्वारा किए जाते थे जिनका श्रम बिना वेतन के होता था क्योंकि रिकॉर्ड पर कहीं भी उनकी सहायता का उल्लेख करना अनुचित होता. मनोरोग में विशेषज्ञता वाला एक डॉक्टर सप्ताह में एक बार जेल का दौरा करता था. उसने स्टैन की चिकित्सा देखभाल की निगरानी की, लेकिन केवल वही दवाएं जारी रखीं जो उन्हें गिरफ्तार होने से पहले दी गई थीं. जेल अधिकारियों ने स्टैन को उनके पार्किंसन के साफ दिख रहे कंपन और कमजोर हड्डियों के बावजूद सिटी सिविल अस्पताल में भेजने का कोई प्रयास नहीं किया.
अधिकारियों के लिए ऐसी चिकित्सा स्थितियों को ध्यान देने योग्य न समझना कोई असामान्य बात नहीं है. अक्टूबर 2020 में जेल जाने के बाद स्टैन का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया. इससे पहले, वह बिना किसी सहायता के काम चला लेते थे, लेकिन बाद में वह दूसरों की मदद पर निर्भर हो गए. अंततः, उन्हें व्हीलचेयर पर आना पड़ा. मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि स्टैन के कारावास के शुरुआती दिनों में एक दिन, जब उन्हें ऐसी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, जेल अधीक्षक ने जोर देकर कहा कि वह सात या आठ प्लास्टिक सिपर, एक छड़ी, एक वॉकर, एक चारपाई, एक व्हीलचेयर और एक पश्चिमी कमोड कुर्सी के साथ एक तस्वीर खिंचवाएं. स्टैन को एक सिपर की अनुमति के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता पड़ी थी, जिसके बिना वह अपने कंपन के कारण खुद पानी नहीं पी सकते थे. स्टैन ने हठपूर्वक इसका विरोध किया, लेकिन अधीक्षक यह दिखाने के लिए सबूत चाहते थे कि उन्होंने किसी भी संभावित चिकित्सा आपात स्थिति, वर्तमान या भविष्य के लिए सुविधाएं प्रदान की थीं. पीछे मुड़कर देखें, तो जेलर शायद जानता था कि जेल की परिस्थितियाँ अंततः स्टैन को व्हीलचेयर तक ले आएंगी. मई 2021 में गिरावट तेजी से बढ़ी. कोविड मामलों के दूसरे दौर की आशंका में, जेल प्रशासन ने कोविड रोगियों और क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए जगह बनाने के लिए जेल अस्पताल के भूतल की सभी कोठरियों को खाली करने का फैसला किया. इसका मतलब था कि स्टैन, मैं और हमारे सेलमेट चाचा को पहली मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा. इस बारे में हमारी मिली-जुली भावनाएँ थीं.
पहली मंजिल पर जाने से हमें अपने एक सह-आरोपी, आनंद तेलतुंबडे, जो उस मंजिल पर थे, के साथ अधिक निकटता से बातचीत करने का मौका मिलता. लेकिन स्टैन अस्पताल के आंगन में अपनी दैनिक शाम की सैर को याद करते. हालांकि, कैदियों के ऐसे सभी प्रशासनिक तबादलों की तरह, चुनाव कभी हमारा नहीं होता. 10 मई को, हमें अस्पताल की पहली मंजिल पर एक कोठरी में स्थानांतरित कर दिया गया. आनंद अब हमसे हर दिन बात कर सकते थे. हमें एक और सह-आरोपी, हैनी बाबू से भी संक्षिप्त रूप से मिलने का मौका मिला, इससे पहले कि उन्हें अपनी आंख के संक्रमण का इलाज कराने के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन स्टैन के लिए, चीजें बदतर हो गई थीं. उन्हें तुरंत गंभीर खांसी हो गई. ड्यूटी पर मौजूद आयुर्वेदिक चिकित्सक ने फैसला किया कि इसका इलाज एक मजबूत एंटीबायोटिक से किया जाना चाहिए और तीन दिन का एज़िथ्रोमाइसिन का कोर्स निर्धारित किया. खांसी थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर स्टैन को दस्त हो गए. जेल-चिकित्सा-प्रथा के अनुसार, यह तर्कसंगत था कि इसका भी एंटीबायोटिक्स के एक और कोर्स से इलाज किया जाना चाहिए. इसलिए स्टैन को मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन की खुराक भी दी गई. इस सबने स्टैन को बेहद कमजोर बना दिया.
अब उन्हें गलियारे में वॉकर का उपयोग करने की आवश्यकता थी. जेल अधीक्षक और वरिष्ठतम आयुर्वेदिक चिकित्सक के अगले साप्ताहिक दौर तक, स्टैन की कमजोरी को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो गया था. वह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. जिस डॉक्टर ने पहले स्टैन के लिए उबले अंडे और दूध का मेडिकल आहार निर्धारित किया था, अब उसने उन्हें दस्त के कारण इनसे बचने की सलाह दी. रिकॉर्ड पर, जेल स्टैन को "उच्च प्रोटीन आहार" प्रदान कर रहा था, लेकिन हकीकत में यह सच नहीं था. स्टैन के पास अपने दस्त को नियंत्रित करने के साधन के रूप में कम खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. उन्हें यह भी लगा कि अधिक पानी का उपयोग करना उचित नहीं होगा क्योंकि अस्पताल के छोटे कैदियों को हमारी कोठरी में भंडारण ड्रम भरने के लिए लगभग आधा किलोमीटर दूर से बाल्टी भर पानी लाना पड़ता था. इस भारी गिरावट को देखते हुए, आनंद और मैंने डॉक्टर से जोर देकर कहा कि स्टैन को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है. वास्तव में, ऑक्सीमीटर प्रतिदिन लगभग 75% के ऑक्सीजन (SPO2) स्तर का संकेत दे रहा था.
आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दावा किया कि या तो ऑक्सीमीटर खराब था या रीडिंग गलत थी क्योंकि स्टैन की उंगलियां झुर्रीदार थीं. लेकिन उनके ऑक्सीमीटर बदलने या कई उंगलियों पर प्रयास करने के बावजूद, रीडिंग नहीं बदली. अंततः, जब स्टैन को ऑक्सीजन पर रखा गया, तो डॉक्टरों को एहसास हुआ कि अस्पताल में एकमात्र ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग खाली था. हालांकि अभी भी कमजोर और स्पष्ट रूप से बीमार, 18 मई, 2021 को, स्टैन को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई. उसी दिन, उन्हें दक्षिण मुंबई के सिटी सिविल अस्पताल ले जाया गया. हम एक ही दिन में दोनों काम करने की तात्कालिकता को समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में महसूस किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अगले दिन उच्च न्यायालय में चिकित्सीय आधार पर स्टैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. जेल अधिकारियों को यह दिखाना था कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है.
उस शाम बाद में, जब स्टैन हमारी कोठरी में लौटे, तो वे न केवल स्पष्ट रूप से थके हुए थे, बल्कि गुस्से में भी थे. जेल अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल के गलत विभाग में भेज दिया था. उन्हें न्यूरोलॉजी विभाग में ले जाने के बजाय, उन्हें मनोरोग विभाग में ले जाया गया, जहाँ प्रशिक्षु डॉक्टर उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते रहे. अगले दिन, 19 मई को, उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत की सुनवाई के दौरान, जेल अधिकारियों की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया गया. अन्य बातों के अलावा, इसमें कहा गया था कि स्टैन को "दैनिक आधार पर उच्च प्रोटीन आहार प्रदान किया जा रहा है; दैनिक स्नान के लिए गर्म पानी; उन्हें गिरने से बचाने के लिए उनकी सेहत और आवश्यक देखभाल के लिए अपनी इच्छा से दो परिचारक (कैदी) प्रदान किए गए हैं; उन्हें गद्दा, चादर, तकिया, व्हील चेयर, वॉकर, चलने की छड़ी, स्ट्रॉ, सिपर मग, सिपर बोतल, कमोड कुर्सी और उनके श्रवण यंत्र के लिए बैटरी सेल भी प्रदान किए गए हैं" और कि "नियमित अंतराल पर मनोरोग चिकित्सक द्वारा उनकी जांच और इलाज भी किया जाता है". पीठ ने जेल अधिकारियों को अगले दिन मुंबई के सिटी सिविल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया, ताकि न्यूरो फिजिशियन, ईएनटी विशेषज्ञ, आर्थोपेडिक सर्जन और जनरल सर्जन जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा उनकी चिकित्सा जांच हो सके.
स्टैन इस उम्मीद में अस्पताल गए कि उन्हें भर्ती कर लिया जाएगा और आराम करने दिया जाएगा. लेकिन इस बार भी, विभिन्न विभागों में जाकर कई परीक्षणों से गुजरने से वे शारीरिक रूप से थक गए. वह शाम को पूरी तरह से थके हुए और निराश होकर अपनी कोठरी में लौट आए. इसी संदर्भ में स्टैन को लगा कि बाहर के अस्पताल जाना व्यर्थ है. अगर अपनों के साथ रहने की उनकी कानूनी दलील खारिज कर दी गई तो वह जेल में मरना पसंद करेंगे. उन्होंने यह बात अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय की पीठ के सामने ऑनलाइन व्यक्त की थी. फिर भी, अगली तारीख, 28 मई को, पीठ ने स्टैन को एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी. निजी अस्पताल पहुंचने पर, जेल विभाग की विफलता उजागर हो गई. स्टैन को कोविड पॉजिटिव पाया गया. स्पष्टीकरण तुरंत दिए गए. जेल अधीक्षक और डॉक्टर ने मुझे बताया कि स्टैन ने जेल के गेट से निकलने के बाद और निजी अस्पताल में प्रवेश करने से पहले वायरस पकड़ा था. यह जेल विभाग और उसकी पर्यवेक्षी संस्थाओं की संवेदनहीनता और लापरवाही है जो फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं. अन्य संस्थाएं भी समान रूप से दोषी हैं और उनकी मृत्यु में भागीदार हैं.
आरएसएस को संविधान वाला भारत नहीं, मनुस्मृति वाला भारत चाहिए: भंवर मेघवंशी
हरकारा डीपडाइव के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आरएसएस सदस्य भंवर मेघवंशी के साथ निधीश त्यागी ने लंबी बातचीत की है, जो आरएसएस और भाजपा की भारतीय संविधान के प्रति विचारधारा पर केंद्रित है. चर्चा की शुरुआत हाल ही में आपातकाल की बरसी पर संघ और भाजपा के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से होती है, जिसमें सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को हटाने की वकालत की थी. मेघवंशी का तर्क है कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह संघ के मूल चरित्र का हिस्सा है, जिसका संविधान के साथ रिश्ता हमेशा से टकराव का रहा है. इसके लिए उन्होंने अपने चार-चरणों वाले विश्लेषण को प्रस्तुत किया: तिरस्कार, बहिष्कार, परिष्कार और अंत में, जय-जयकार. उनके अनुसार, संघ का मौजूदा संविधान-प्रेम केवल एक "केंचुली" बदलने जैसा है, जिसमें ज़हर बरकरार रहता है, और उनका अंतिम लक्ष्य भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए वर्तमान संविधान को हटाना आवश्यक है. भंवर मेघवंशी ने इन बयानों के बाद फॉरवर्ड प्रेस में लिखा था, जिसे हरकारा ने भी छापा था. यह बातचीत उनके इस लेख पर आधारित है.
बातचीत का केंद्रीय बिंदु मनुस्मृति और संविधान के बीच का बुनियादी वैचारिक संघर्ष है. मेघवंशी बताते हैं कि यह लड़ाई संसाधनों और सत्ता पर नियंत्रण की है. मनुस्मृति एक ऐसी व्यवस्था बनाती है जो जन्म के आधार पर कुछ चुनिंदा वर्गों को सभी अधिकार और विशेषाधिकार देती है, जबकि महिलाओं और शूद्रों (बहुसंख्यक आबादी) को केवल सेवा करने का कर्तव्य सौंपती है और उन्हें शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से भी वंचित करती है. इसके विपरीत, भारत का संविधान सभी नागरिकों को, विशेषकर हाशिये पर खड़े अंतिम व्यक्ति को, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय गरिमा प्रदान करता है. यही समानता का सिद्धांत संघ की विचारधारा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह उनके जन्म-आधारित पदानुक्रम को तोड़ता है.
इस बातचीत में इस विरोधाभास पर भी चर्चा की गई है कि जो दल बहुसंख्यक दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों का वैचारिक रूप से विरोध करता है, वह उन्हीं का वोट हासिल करने में कैसे सफल हो जाता है. मेघवंशी इसके पीछे कई कारण बताते हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ डर का माहौल बनाना, लोक देवताओं और कबीर जैसी क्रांतिकारी हस्तियों की परंपराओं का ब्राह्मणीकरण और सांस्कृतिक विनियोजन करना, और दलित-ओबीसी समाज में अपने को 'बेहतर हिंदू' साबित करने के लिए कट्टर धार्मिक प्रथाओं को अपनाने की प्रवृत्ति शामिल है. यह एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां उत्पीड़ित समुदाय ही अपनी संवैधानिक सुरक्षा के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को मजबूत करता है. अंत में, इस समस्या के समाधान पर बात करते हुए मेघवंशी कहते हैं कि रास्ता नफरत के जवाब में नफरत से नहीं, बल्कि भारत की अपनी श्रमणिक और बहुजन परंपरा (चार्वाक, बुद्ध, कबीर, फुले, अंबेडकर) को मजबूत करने से निकलेगा. उनके अनुसार, अंतिम रास्ता संविधान के मूल्यों को थामे रहने में ही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व ही भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक साथ जोड़ सकते हैं. उनका मानना है कि असहमत लोगों से भी संवाद की गुंजाइश बनाए रखनी चाहिए और बिना डरे लगातार काम करते रहना चाहिए.
किताब
सवर्णों की खोज ख़बर: जाति पर जहां सबसे ज़्यादा सन्नाटा है, वहीं सबसे ज्यादा क्रूर उत्पीड़न भी
स्क्रोल के लिए शोएब दानियाल ने लेखक रविकांत के साथ उनकी किताब "मीट द सवर्णाज़" पर एक विस्तृत बातचीत की है. रविकांत इस चर्चा की शुरुआत अपनी किताब के मूल उद्देश्य को समझाते हुए करते हैं. उनका लक्ष्य उस सवर्ण समाज पर एक विश्लेषणात्मक दृष्टि डालना है, जो आमतौर पर दूसरों का अध्ययन करता है लेकिन खुद कभी अध्ययन का विषय नहीं बनता. यह किताब उस संस्कृति को समझने और उसकी आलोचना करने का एक प्रयास है, जो भारत में मुख्यधारा को परिभाषित करती है और जिससे रविकांत जैसे गैर-सवर्ण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए संस्कृति का मतलब तय होता है.
बातचीत के एक महत्वपूर्ण हिस्से में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (डीडीएलजे) फिल्म का विश्लेषण किया गया है, जिसे रविकांत सवर्ण मिलेनियल्स के लिए रोमांस का आधार स्तंभ मानते हैं. उनके अनुसार, इस फिल्म में कोई खलनायक नहीं है और असल में कोई संकट भी नहीं है. फिल्म का केंद्रीय संघर्ष यह है कि आधुनिकता की तमाम संभावनाओं के बावजूद, व्यक्तिगत पसंद को परिवार के पुरुष मुखिया (पिता) की स्वीकृति की आवश्यकता होती है. यह विद्रोह करने के बजाय व्यवस्था के भीतर ही समायोजन करने की मानसिकता को दर्शाता है. यह फिल्म इस बात का आश्वासन देती है कि सांस्कृतिक सत्ता का हस्तांतरण अंततः पितृसत्ता की मंजूरी से ही होगा, और यही फॉर्मूला बाद की कई फिल्मों में भी दोहराया गया.
रविकांत "प्रगतिशील" सवर्णों की भी गहन आलोचना करते हैं, जो लैंगिक समानता या सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर तो प्रगतिशील हो सकते हैं, लेकिन जाति के सवाल पर उनकी प्रगति रुक जाती है. वह बताते हैं कि ये लोग अपने पारिवारिक और सामाजिक नेटवर्क से मिलने वाले विशेषाधिकारों (जैसे इंटर्नशिप, सिफारिशें) को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए वे जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए वास्तविक कदम उठाने से बचते हैं. बंगाल के जातिवाद का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि "भद्रलोक" की सांस्कृतिक महानता के नैरेटिव के नीचे गहरा जातिवाद छिपा हुआ है. उनके अनुसार, जिन समाजों में जाति पर सबसे ज़्यादा सन्नाटा है, वहीं सबसे क्रूर उत्पीड़न होता है.
चर्चा में गैर-सवर्ण मर्दानगी के हिंसक दमन का भी ज़िक्र है, जहाँ मूंछ रखने, घोड़ी पर चढ़ने या अच्छे कपड़े पहनने जैसे आत्म-सम्मान के प्रतीकों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता और इसे "जुर्रत" मानकर कुचल दिया जाता है. रविकांत यह भी बताते हैं कि कैसे सवर्ण महिलाएं, जो स्वयं पितृसत्ता की शिकार हैं, धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं को बनाए रखकर जाति व्यवस्था को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. बातचीत में अंग्रेजी भाषा को एक "पासपोर्ट" के रूप में देखा गया है, जो अभिजात्य वर्ग में प्रवेश के लिए एक आवश्यक फ़िल्टर का काम करती है.
अंत में, रविकांत "बहुजन" शब्द का उपयोग करने से बचने का कारण बताते हैं. उनका मानना है कि इस आंदोलन को दलित बुद्धिजीवियों ने आगे बढ़ाया, लेकिन प्रभावशाली ओबीसी जातियों से उन्हें अपेक्षित समर्थन और पारस्परिकता नहीं मिली. वह स्पष्ट करते हैं कि उनकी किताब कड़वाहट या गुस्से से नहीं, बल्कि एक आलोचनात्मक स्नेह के साथ लिखी गई है. इसका उद्देश्य सवर्णों को अपनी संस्कृति पर एक बाहरी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना है ताकि एक सार्थक संवाद शुरू हो सके. उनका अंतिम संदेश संघर्ष के बजाय शिक्षा और करियर के माध्यम से अपने समुदाय को सशक्त बनाने पर केंद्रित है.
किताब का लिंक यहां है.
विश्लेषण
संजय हेगड़े: दो लोकतंत्रों में तानाशाही की प्रतिध्वनि
'द हिन्दू' में संजय हेगड़े ने लिखा है कि अमेरिकियों को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा: वही ताकतें, जिन्होंने भारत में आपातकाल को संभव बनाया, अब अमेरिका के गणराज्य को भी खतरे में डाल रही हैं. 4 जुलाई को अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस मनाया. लगभग ढाई सौ साल पहले, अमेरिकी लोगों ने यह संकल्प लिया था कि वे किसी राजा के अधीन नहीं, बल्कि कानून के अधीन रहेंगे. लेकिन अब, अमेरिका के ही एक वरिष्ठ न्यायाधीश जे. माइकल लुटिग ने आगाह किया है. 1776 की लोकतांत्रिक मूल्य अपने आप नहीं टिकते, उन्हें हर दिन बचाना होता है. तानाशाही अब बाहरी खतरा नहीं, बल्कि भीतर से उभरती चुनौती है.
भारत की लोकतांत्रिक गिरावट; इतिहास से सबक :भारत में 1975 में लगाए गए आपातकाल की चर्चा करते हुए हेगड़े बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने कानून का सहारा लेकर लोकतंत्र को कुचल दिया — संविधान का उल्लंघन नहीं, उसका दोहन किया गया.
25 जून 1975 को आपातकाल घोषित हुआ और प्रेस पर सेंसरशिप लगी. 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी, संसद और न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया. एकमात्र न्यायाधीश एच.आर. खन्ना ने विरोध में फैसला दिया और उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया. इतिहासकार ज्ञान प्रकाश लिखते हैं — लोकतांत्रिक संस्थाएं अक्सर गोली या टैंक से नहीं, बल्कि "सहमति" से मरती हैं.
संस्थाएं कैसे ढहती हैं? हेगड़े लिखते हैं — “वास्तविक त्रासदी यह नहीं थी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, बल्कि यह थी कि उन्होंने कितनी आसानी से किया. न्यायाधीश, मंत्री, अफसर, पत्रकार सबने कानून के बजाय वफादारी चुनी.” एच.वी. कामथ ने 1949 में चेतावनी दी थी कि संविधान में आपातकाल की धाराएं जर्मनी की वही गलती दोहरा रही हैं, जिसका फायदा हिटलर ने उठाया था.
अब वही दोहराव अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में आपातकाल घोषित नहीं किया — क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है. संसद में बहुमत, सुप्रीम कोर्ट में 6-3, रूढ़िवादी बहुमत, विरोधियों पर मुकदमे, आव्रजन कानूनों को हथियार बनाना और संविधान के हिस्सों को "समाप्त" करने की धमकी. हेगड़े कहते हैं — यह सुधार नहीं, राजशाही का नया नाम है.
रोकने वाले संस्थान कैसे विफल हुए जैसे भारत में:
संसद चुप रही
विपक्ष झुका
न्यायपालिका ने देरी की
मीडिया ने तर्क गढ़े
जनता ने इंतज़ार किया कि कोई और बोले
“संवैधानिक रक्षक खुद अंदर से सड़ने लगे तो तानाशाही बाहर से नहीं आती — घर में ही जन्म लेती है।”
इतिहास का व्यंग्य: संविधान अब हथियार बन गया है : जहाँ एक समय इंदिरा गांधी ने संविधान को दबाया, वहीं आज राहुल गांधी उसी संविधान की प्रति लेकर तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं. संविधान जो कभी चुप्पी का प्रतीक था, अब प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है. लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, संयम और जवाबदेही की संस्कृति है. थॉमस पेन ने कहा था: “Let the law be king” — राजा नहीं, कानून राजा हो.
अंतिम चेतावनी: तानाशाही हमेशा विदेशी नहीं होती : “तानाशाही जब आती है, तो वह कभी बाहरी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि अंदरूनी व्यवस्था की चूक से आती है — क़ानूनी, स्वीकार्य और आत्मीय रूप में.” भारत और अमेरिका दोनों आज रूप से लोकतंत्र हैं — पर मूल्य और आत्मा से लोकतंत्र बचा रहेगा या नहीं, यह नागरिकों की चेतना और संस्थाओं की रीढ़ पर निर्भर करता है. "भारत 1975 में इस परीक्षा में फेल हुआ था. हम दोबारा नहीं हो सकते." "कानून को अपने सिर का ताज समझिए — वरना कोई और पहनेगा, और फिर वह ताज नहीं उतरेगा."
वारी के दौरान संविधान की बात
पंढरपुर वारी महाराष्ट्र में एक तीर्थयात्रा है, जिसमें लाखों वारकरी हर साल विट्ठल-रुक्मिणी मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं. संविधान समता दिंडी इसी तीर्थयात्रा के भीतर होती है, जो पैदल चलने, कीर्तन (भक्ति गीत), और चर्चा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करती है. इसका आयोजन सामाजिक समूहों द्वारा किया जाता है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों के प्रतिभागी शामिल होते हैं. श्रीगोंडा के शेख मुहम्मद और नागपुर के हजरत बाबा ताजुद्दीन सहित मुस्लिम सूफी संतों की पालखियां भी वारी का हिस्सा हैं. आर्टिकल 14 के लिए विशाल विमल ने इस पर वीडियो रिपोर्ट बनाई है.
पाठकों से अपील :
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.