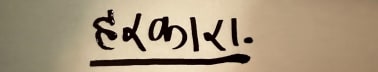10/09/2025: जलता काठमांडू, पीएम दुबई भागा | ट्रम्प दबाव बढ़ाएंगे? | विकास नहीं सोशल मीडिया करो, मोदी के सांसदों को जीत के नुस्खे| मोदी की विश्व छवि पर श्रवण गर्ग | संविधान और अदालतों पर मुरलीधर
‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.
निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फ़लक अफ़शां
आज की सुर्खियां
पीएम की सांसदों को नसीहत: सड़कों-स्कूलों से नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट से जीतेंगे चुनाव...
संघ से टकराव: मोदी के बाद कौन होगा उत्तराधिकारी, बीजेपी अध्यक्ष के चयन पर टकराव...
बिहार SIR: सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिलों से सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए,
वेतन में असमानता: काशी विश्वनाथ के पुजारियों को 90 हजार और अग्निवीर को 25 हजार!...
रूस पर नए प्रतिबंधों के लिए ट्रंप तैयार, भारत समेत तेल ख़रीदने वाले देशों पर बढ़ सकता है दबाव...
टैरिफ की मार से भदोही का कालीन उद्योग बर्बादी की कगार पर, 6,000 करोड़ का स्टॉक फँसा...
सामान्य स्थिति के दावों के बावजूद पूर्वी लद्दाख में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, तनाव बरकरार...
गाजा में युद्ध के बीच भारत और इज़राइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए...
कुकी शिविर के स्थानांतरण पर नगा समूहों का कड़ा विरोध, "रक्तपात" की चेतावनी दी...
रूस से और S-400 सिस्टम खरीदने पर भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों का ख़तरा बढ़ा...
भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में संविदाकर्मियों की हिस्सेदारी 27 साल के उच्चतम स्तर पर...
बीएलओ को लेकर चुनाव आयोग और ममता में संघर्ष
मोतिहारी का मुसहर समाज: सामाजिक भेदभाव, भूखमरी और गरीबी के अंधेरे में जीने को मजबूर...
नए उपराष्ट्रपति: एनडीए के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित...
नेपाल में अराजकता: पीएम ओली का इस्तीफा, देश छोड़कर भागे; प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट को फूंका...
मालेगांव विस्फोट: एनआईए ने फैसले को चुनौती नहीं दी, मृतकों के परिजन हाईकोर्ट पहुँचे...
वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने कहा- लोकतंत्र से खिसककर मोदी तानाशाहों की तरफ बढ़ रहे...
'प्रशासन में बैठे लोग मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, तो संविधान बेमानी हो जाएगा' एस मुरलीधर...
सड़कों और स्कूलों से नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट से जीतेंगे चुनाव: पीएम मोदी की सांसदों को नसीहत
एक अपनी तरह के अनूठे क़दम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को एक स्पष्ट संदेश दिया है: सड़कें और स्कूल बनाने से आपको वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ पोस्ट करने से शायद मिल जाएँ. पार्टी सूत्रों का कहना है कि संसद की लाइब्रेरी में आयोजित एक कार्यशाला में सांसदों को "फटकार" लगाई गई, जहाँ उनके फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब पर उनकी गतिविधि का मूल्यांकन करने वाला तीन पन्नों का एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया.
यह घटना 21वीं सदी की भारतीय राजनीति में आ रहे एक बड़े बदलाव को रेखांकित करती है, जहाँ ज़मीनी काम और पारंपरिक विकास के मुद्दों पर डिजिटल प्रचार और ऑनलाइन छवि-निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है. यह दर्शाता है कि राजनीतिक दलों के लिए अब मतदाताओं तक पहुँचने का माध्यम सोशल मीडिया बन गया है, और सांसदों का मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जा रहा है. यह मूल्यांकन प्रणाली एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड की तरह रंग-कोडित है: निष्क्रिय सांसदों के लिए लाल, बमुश्किल सक्रिय के लिए पीला, और विपुल पोस्टर के लिए हरा. एक महीने में फ़ेसबुक पर शून्य पोस्ट वाले सांसदों को 'लाल' श्रेणी में रखा गया, जबकि 60 से अधिक पोस्ट करने वालों को 'हरा' मिला. संक्षेप में, देश पर शासन करने से ज़्यादा ज़रूरी इंस्टाग्राम फ़ीड को संवारना हो गया है. डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी ने लोगों के साथ जुड़ाव पर ज़ोर दिया - हालाँकि, अब "लोग" का मतलब वास्तविक मतदाताओं के बजाय स्क्रॉल करने वाले फ़ॉलोअर्स हो गया है.
यह निर्देश स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पार्टी का नेतृत्व मानता है कि धारणा (perception) ही हक़ीक़त है. लगातार ऑनलाइन उपस्थिति और प्रचार के माध्यम से एक सकारात्मक कहानी गढ़ना, ज़मीनी स्तर पर वास्तविक विकास कार्यों की तुलना में चुनावी रूप से अधिक फायदेमंद माना जा रहा है. संदेश साफ़ था: 21वीं सदी की भारतीय राजनीति में, राजमार्गों पर हैशटैग भारी पड़ रहे हैं. इस 'वेक-अप कॉल' के बाद, भाजपा सांसदों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी गतिविधि बढ़ाने की उम्मीद है. हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट, रील और लाइव सत्रों में भारी वृद्धि देख सकते हैं, जहाँ वे सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, भले ही उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ज़मीनी काम की स्थिति कुछ भी हो.
मोदी के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, इसी को लेकर संघ से टकराव
“द प्रिंट” में डी.के. सिंह लिखते हैं कि मोदी-शाह और आरएसएस के बीच भाजपा अध्यक्ष के चयन को लेकर वास्तव में टकराव का असली कारण यह है कि 2029 और उसके बाद भी अगर भाजपा संसद पर अपना दबदबा बनाए रखती है, तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के बाद किसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, यही दांव पर है. एक सशक्त भाजपा अध्यक्ष संभावित उत्तराधिकारियों की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने या रोकने की सबसे अच्छी स्थिति में होता है, क्योंकि उसके पास राज्य स्तर पर नेताओं के चयन का नियंत्रण होता है – और यही चयन शीर्ष पद के दावेदारों के लिए प्राथमिक आधार तैयार करता है.
बिहार एसआईआर
सीमांचल के दो ज़िलों से सबसे ज्यादा नाम हटाए गए, यहां एनडीए का असर कम हुआ था
बिहार में ‘एसआईआर’ के दावों और आपत्तियों के चरण के समाप्त होने के साथ ही मतदान केंद्रवार आंकड़ों से पता चलता है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र के चार जिलों में से दो जिलों में मतदाता हटाने की दर सबसे अधिक रही है.
बिहार के 38 जिलों में कुल 65 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया, जो कुल 7.9 करोड़ मतदाता संख्या का 8.31% है. जिलावार देखें तो गोपालगंज (जो उत्तर प्रदेश से सटा है) में हटाने की सबसे अधिक दर 15.1% रही. इसके बाद सीमांचल क्षेत्र के पुर्णिया और किशनगंज जिले में यह क्रमशः 12.08% और 11.82% रही, जो पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा पर हैं.
सीमांचल के बाकी दो जिलों कटिहार और अररिया में हटाने की दर राज्य औसत से कम, क्रमशः 8.27% और 7.59%, रही. दस प्रतिशत से ऊपर हटाने की दर सिर्फ मधुबनी (नेपाल सीमा पर) 10.44% और भागलपुर (झारखंड सीमा पर) 10.19% जिलों में ही थी.
2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार के सभी जिलों में सीमांचल के चार जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है. किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.89% है, इसके बाद कटिहार 44.47%, अररिया 42.95%, और पुर्णिया 38.46% है. सीमांचल के अलावा 11 अन्य जिलों में भी मुस्लिम आबादी 15% से ऊपर है. कुल मिलाकर, बिहार की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 16.87% है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने “द इंडियन एक्सप्रेस” को बताया कि एसआईआर के लिए आवश्यक 11 मान्य पहचान दस्तावेजों में से एक, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए सीमांचल में आवेदन बढ़े हैं. इससे पता चलता है कि कई आवेदक अन्य देशों से आए अप्रवासी हैं.
सीमांचल में मतदाता हटाने का सबसे आम कारण "स्थायी रूप से स्थानांतरित" होना था, जो चार जिलों में कुल हटाए गए मतदाताओं में 2.97 लाख (39.29%) थे. इसके बाद "स्वर्गीय" मतदाता 2.54 लाख (33.57%), "अनुपस्थित" या "अज्ञात" मतदाता 1.38 लाख (18.25%), और "पहले से नामांकित" या "डुप्लिकेट" मतदाता 67,191 (8.89%) थे.
कुल हटाने के अनुपात में, सीमांचल में "अनुपस्थित" मतदाताओं को हटाने की दर राज्य औसत 14.82% से काफी अधिक रही. "स्थायी रूप से स्थानांतरित" और "स्वर्गीय" मतदाताओं की दर राज्य औसत के करीब है. "डुप्लिकेट" मतदाताओं की हटाने की दर सीमांचल में राज्य औसत 10.69% से कम रही.
पुर्णिया (39.8%), किशनगंज (40.87%) और कटिहार (43.31%) में "स्थायी रूप से स्थानांतरित" सबसे अधिक कारण था, जबकि अररिया में "स्वर्गीय" सबसे अधिक रहा (45.4%), इसके बाद "स्थायी रूप से स्थानांतरित" (32.32%) था. बाकी तीन जिलों में "स्वर्गीय" दूसरे सबसे आम कारण थे.
पिछले तीन विधानसभा चुनावों में, सीमांचल में बीजेपी-नेतृत्व वाली एनडीए की पकड़ कमजोर हुई है. 2010 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने क्षेत्र के 24 में से 17 सीटें जीती थीं. 2015 में जद(यू), आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में थे, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 8 सीटें जीतीं. 2020 में क्षेत्र में एआईएमआईएम की उपस्थिति बढ़ी, जिसने पांच सीटें जीतीं, हालांकि बाद में उसके चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए. इस चुनाव में बीजेपी ने आठ, जद(यू) ने चार, कांग्रेस ने पांच सीटें हासिल कीं.
पुर्णिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50,000 मतदाता हटाए गए हैं, जहां बीजेपी विधायक विजय कुमार खेमका का कहना है कि हटाए गए नाम सही थे और चुनावों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सर्वेक्षण पारदर्शी तरीके से किया है.
कटिहार के प्रणपुर क्षेत्र से कांग्रेस के तौकीर आलम ने कहा कि अभी हटाने के प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगी, उनका ध्यान अंतिम मतदाता सूची में सही मतदाताओं को शामिल कराने पर है.
किशनगंज के कांग्रेस विधायक इजाहरुल हुसैन ने कहा कि हटाए गए नाम किसी विशेष समुदाय या जाति के नहीं हैं. अब जब चुनाव आयोग आधार स्वीकार भी कर रहा है, तो लोग दस्तावेज जमा कर रहे हैं. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा की है.
अररिया जिले के रानीगंज से जद (यू) विधायक अच्मित ऋषिदेव ने भी कहा कि हटाना उचित था. वे आरजेडी के अविनाश मंगलम को हरा चुके हैं, जो मानते हैं कि यह हटाने का फैसला विपक्षी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा. हटाए गए नाम ज्यादातर यादव, मुस्लिम और दलितों के हैं.
पटना सहित अधिक शहरी क्षेत्रों में हटाए गए नाम ज्यादातर वे थे, जो किराए के मकानों में रहते थे और आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे. विकास के नाम पर कई झुग्गी-झोपड़ी ध्वस्त कर दिए गए थे, जिससे वोटर वहां से चले गए और सर्वेक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए. ये लोग गरीब और वंचित वर्गों से संबंध रखते हैं और महागठबंधन के समर्थक माने जाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार की जमानत के मामले में नोटिस दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा को प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने की उनकी अर्जी पर ईडी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. “द इंडियन एक्सप्रेस” की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत ने एक जिज्ञासापूर्ण सवाल उठाया कि लांगा किस तरह के पत्रकार हैं. अदालत में उन्होंने कहा—“वह किस तरह के पत्रकार हैं? बहुत से वास्तविक पत्रकार होते हैं. लेकिन कुछ लोग वाहन या स्कूटर पर घूमते हैं और कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, और वे क्या करते हैं, यह सबको पता है.” लांगा के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जिन दो एफआईआर पर ईडी ने यह मामला बनाया है, उनमें लांगा को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है.
पुजारियों को 90 हजार और अग्निवीर को 25 हजार!
बिस्वजीत बनर्जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को उत्तरप्रदेश सरकार 1983 से वेतन दे रही है, यानी जब से राज्य सरकार ने मंदिर का प्रशासन अपने हाथ में लिया. अब पुजारियों का वेतन तीन गुना बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है और उन्हें राज्यकर्मियों के समान दर्जा और सुविधाएं मिलेंगी. इसके विपरीत, अग्निवीर – यानी भारतीय सेना में अनुबंध पर भर्ती होने वाले सैनिक – की शुरुआती तनख्वाह करीब 25,000 रुपये है और उनमें से अधिकांश को दो या तीन साल बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी.
रूस पर नए प्रतिबंधों के लिए ट्रम्प तैयार, भारत समेत तेल ख़रीदने वाले देशों पर बढ़ सकता है दबाव
एक ऐसे घटनाक्रम में जिसका भारत पर असर पड़ सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि वह यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर नए दौर के प्रतिबंधों के लिए तैयार हैं. व्हाइट हाउस में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हाँ, मैं तैयार हूँ". यह बयान अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के उन दावों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने टैरिफ़ से अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं को नुक़सान होने की बात को कम महत्व दिया था. बेसेंट ने रूसी तेल का आयात करने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर संयुक्त रूप से अमेरिका-यूरोपीय संघ द्वारा टैरिफ़ लगाने पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, "अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल ख़रीदने वाले देशों पर अधिक प्रतिबंध और सेकेंडरी टैरिफ़ लगा सकते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी".
यह ख़बर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रूसी तेल के सबसे बड़े ख़रीददारों में से एक है.अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए किसी भी नए या सेकेंडरी प्रतिबंध का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. अमेरिका पहले ही रूसी तेल की ख़रीद को लेकर भारत पर 50% का टैरिफ़ लगा चुका है.
वाशिंगटन और ब्रुसेल्स द्वारा प्रतिबंधों को और कड़ा करने के संकेतों के बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर अमेरिकी टैरिफ़ का समर्थन किया है. एबीसी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने, भारत का नाम लिए बिना, कहा, "मुझे लगता है कि जो देश रूस के साथ सौदे करना जारी रखे हुए हैं, उन पर टैरिफ़ लगाने का विचार सही है". दूसरी ओर, ट्रम्प के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने ब्रिक्स गठबंधन की तीखी आलोचना करते हुए सदस्य देशों को "वैम्पायर" बताया है, जिनके "अनुचित व्यापार व्यवहार" अमेरिका का शोषण कर रहे हैं. नवारो ने यह भी दावा किया कि ब्रिक्स देश अमेरिका को अपना माल बेचे बिना जीवित नहीं रह सकते.
विश्लेषकों का कहना है कि भारत ब्रिक्स में अमेरिका और चीन-रूस के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. जहाँ अन्य सदस्य देशों ने वाशिंगटन के टैरिफ़ उपायों की आलोचना के लिए मंच का इस्तेमाल किया, वहीं भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया. इस बीच, ट्रम्प की टीम, नवारो के नेतृत्व में, भारत को MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) राजनीति के लिए एक नया युद्धक्षेत्र बना रही है. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बयानों से संकेत मिलता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ मिलकर रूस पर दबाव बढ़ा सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो भारत को अपनी ऊर्जा ख़रीद और व्यापार नीतियों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम किया जा सके. भारत को अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों और रूस के साथ अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना होगा.
टैरिफ की मार
भदोही का कालीन उद्योग बर्बादी की कगार पर, 6,000 करोड़ रुपये का स्टॉक फँसा
भदोही और वाराणसी का प्रसिद्ध कालीन उद्योग 6,000 करोड़ रुपये की बिना बिकी इन्वेंट्री में फँसकर बर्बादी का सामना कर रहा है. अमेरिकी टैरिफ़ और लापरवाह व्यापार प्रथाओं ने इस संकट को और गहरा कर दिया है. यह संकट भारत के सबसे बड़े कालीन बाज़ार में उसकी प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुँचाने के साथ-साथ हज़ारों बुनकरों के रोज़गार को ख़तरे में डाल रहा है. भदोही और उसके आसपास के इलाक़ों में लगभग 20 लाख लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं.
अनुभवी निर्माता इस संकट के लिए युवा निर्यातकों की एक नई पीढ़ी को दोषी ठहराते हैं, जिन्होंने भरोसेमंद थोक विक्रेताओं को दरकिनार कर छोटे अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं के साथ क़रार कर लिया, जो देरी से भुगतान करने के लिए जाने जाते हैं. एक व्यापारी ने अफ़सोस जताते हुए कहा, "वे तभी भुगतान करते हैं जब कालीन बिक जाते हैं, जिससे हमारी कार्यशील पूँजी फँस जाती है और बाज़ार को चलाने वाली शृंखला टूट जाती है". अमेरिका को भारत के कुल हस्तनिर्मित कालीन निर्यात का 60% हिस्सा जाता है. ट्रम्प-युग के टैरिफ़ के तहत अमेरिकी माँग में गिरावट और निर्यातकों के जोखिम भरे प्रयोगों के विफल होने से, हज़ारों बुनकर अब अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. यह संकट केवल टैरिफ़ का परिणाम नहीं है, बल्कि उद्योग के भीतर की अदूरदर्शी व्यापारिक प्रथाओं का भी नतीजा है. मुनाफ़े के लिए जल्दबाज़ी में युवा निर्यातकों द्वारा अपनाए गए नए व्यापार मॉडल ने पारंपरिक और स्थिर आपूर्ति शृंखला को नुक़सान पहुँचाया है.
निर्माता बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुक़सान को रोकने और भारत के सबसे बड़े कालीन बाज़ार में देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तत्काल बेलआउट पैकेज की माँग कर रहे हैं. यदि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, तो यह 450 साल पुराना विरासत उद्योग ढह सकता है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी.
इंजीनियरिंग निर्यातकों को 7.5 अरब डॉलर के नुक़सान का डर, बड़े पैमाने पर छँटनी की आशंका
पिछले महीने अगस्त से भारतीय सामानों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के चौंकाने वाले टैरिफ़ ने देश के इंजीनियरिंग निर्यातकों को संकट में डाल दिया है. इससे वित्त वर्ष 26 में लगभग 7.5 बिलियन डॉलर के नुक़सान का ख़तरा है और बड़े पैमाने पर छँटनी की आशंका पैदा हो गई है. इंजीनियरिंग सामान भारत के कुल वस्तु निर्यात में एक चौथाई से अधिक का योगदान देता है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाज़ार है. इस टैरिफ़ का असर बहुत गंभीर हो सकता है, जिससे न केवल राजस्व का नुक़सान होगा बल्कि लाखों नौकरियाँ भी जा सकती हैं. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) के अध्यक्ष पंकज चड्ढा ने मिंट के साथ एक साक्षात्कार में चेतावनी दी कि अचानक शुल्क वृद्धि, जो पहले से ही कम मार्जिन पर चल रहे कारखानों को पंगु बना सकती है. उन्होंने कहा, "इसका प्रभाव इतना गंभीर होगा कि इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से नौकरियाँ जाएँगी, क्योंकि इतने बड़े मूल्य के निर्यात के लिए घरेलू विविधीकरण संभव नहीं है". निर्यातक वाशिंगटन पर राजनीतिक मक़सद के लिए व्यापार को हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं. यह टैरिफ़ भारत की रूसी कच्चे तेल की ख़रीद से जुड़ा है. यह दिखाता है कि कैसे भू-राजनीतिक तनाव सीधे तौर पर आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और भारतीय उद्योगों को नुक़सान पहुँचा रहे हैं जो सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं हैं.
उद्योग जगत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और नुक़सान की भरपाई के लिए उपायों के एक पैकेज की माँग कर रहा है. यदि नई दिल्ली की प्रतिक्रिया धीमी रहती है, तो यह टैरिफ़ का झटका एक बड़े रोज़गार संकट में बदल सकता है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ेगा.
पूर्वी लद्दाख में तनाव बरकरार, सामान्य स्थिति के दावों के बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं
मोदी सरकार भले ही सामान्य स्थिति और प्रगति का दावा करे, लेकिन पूर्वी लद्दाख में ज़मीनी हक़ीक़त एक अलग कहानी बयां करती है. बीजिंग के साथ संबंधों में हालिया नरमी के बावजूद, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारतीय सेना की सैन्य मुद्रा अपरिवर्तित बनी हुई है. यह ख़बर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है. यह सरकार के सार्वजनिक बयानों और वास्तविक सीमा स्थिति के बीच एक अंतर को उजागर करती है, जो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या जनता को पूरी जानकारी दी जा रही है.
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय गश्ती दल अभी भी बफ़र ज़ोन में प्रवेश करने से वंचित हैं और उन्हें केवल विघटन वाले क्षेत्रों में सहमत मार्गों तक ही सीमित रखा गया है, जबकि चीन डी-एस्केलेशन (तनाव कम करने) के विचार पर भी विचार करने से इनकार कर रहा है. फिर भी, जनता को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल हो गई है - यह एक ऐसा दावा है जो हक़ीक़त से बहुत दूर है. यह स्थिति चीन के साथ बातचीत में भारत की सीमित सफलता को दर्शाती है. चीन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है, जबकि भारत एक रक्षात्मक मुद्रा में है. सामान्य स्थिति का सार्वजनिक आख्यान चीन पर और अधिक दबाव डालने के लिए सरकार की अनिच्छा का संकेत दे सकता है. जब तक चीन डी-एस्केलेशन के लिए सहमत नहीं होता, तब तक एलएसी पर सैन्य तनाव बना रहेगा. भारत को अपनी सैन्य तैयारी बनाए रखनी होगी और साथ ही चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए राजनयिक रास्ते तलाशने होंगे.
गाजा में युद्ध के बीच भारत और इज़राइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए
अति-दक्षिणपंथी इज़राइली वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच की भारत यात्रा के दौरान इज़राइल और भारत ने आपसी व्यापार का विस्तार करने के लिए एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता नई दिल्ली में स्मोट्रिच और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हस्ताक्षरित किया गया. यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब गाजा पर इज़राइल के युद्ध के कारण वैश्विक आक्रोश है, जिसमें अक्टूबर 2023 से अब तक 64,000 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. स्मोट्रिच, जिन पर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों से संबंधों के लिए कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, के साथ यह सौदा भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है.
समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना है. सीतारमण ने "साइबर सुरक्षा, रक्षा, नवाचार और उच्च-प्रौद्योगिकी" में अधिक सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. स्मोट्रिच ने इस सौदे को "हमारे संयुक्त दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क़दम" बताया. यह समझौता मोदी के नेतृत्व में इज़राइल के साथ भारत के गहरे होते संबंधों को दर्शाता है. भारत की विदेश नीति आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देती दिख रही है, भले ही इसके लिए मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं की अनदेखी करनी पड़े. रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है. इस समझौते से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, रक्षा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है. हालाँकि, यह सौदा भारत को उन देशों के साथ खड़ा कर सकता है जो इज़राइल की कार्रवाइयों की आलोचना कर रहे हैं, जिससे इसके राजनयिक संबंधों में जटिलताएँ आ सकती हैं.
कुकी शिविर के स्थानांतरण पर नगा समूहों का कड़ा विरोध, "रक्तपात" की चेतावनी
मणिपुर में इंफाल घाटी के किनारे रहने वाले नगाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था, फ़ुटहिल्स नगा कोऑर्डिनेशन कमेटी (FNCC) ने पुनर्निधारित सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशंस (SoO) समझौते के तहत एक कुकी उग्रवादी शिविर को अपनी पैतृक नगा भूमि में स्थानांतरित करने की निंदा की है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि यह क़दम आगे बढ़ता है तो "अपरिहार्य रक्तपात" होगा.यह चेतावनी मणिपुर के पहले से ही अस्थिर जातीय समीकरणों को और बिगाड़ सकती है. नगा और कुकी समुदायों के बीच किसी भी तरह का टकराव राज्य में हिंसा का एक नया दौर शुरू कर सकता है.
एफएनसीसी ने सरकार पर नगाओं के अधिकारों को कमज़ोर करने और उग्रवादियों को "सुरक्षित पनाहगाह" प्रदान करने का आरोप लगाया. इस बीच, यूनाइटेड नगा काउंसिल (UNC) ने कहा है कि वह म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के विरोध में मणिपुर के मुख्य रूप से नगा क्षेत्रों में अपनी 'व्यापार नाकेबंदी' के साथ आगे बढ़ेगी. इस नाकेबंदी से इंफाल को नागालैंड से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर मालवाहक ट्रकों की आवाजाही बाधित होने की संभावना है. यह घटनाक्रम क्षेत्र में भूमि, पहचान और संसाधनों पर विभिन्न जातीय समूहों के बीच गहरे अविश्वास और प्रतिस्पर्धी दावों को रेखांकित करता है. केंद्र सरकार के निर्णय, जैसे कि सीमा पर बाड़ लगाना और उग्रवादी शिविरों का स्थानांतरण, अक्सर स्थानीय समुदायों से परामर्श के बिना लिए जाते हैं, जिससे नाराज़गी और संघर्ष होता है. यदि सरकार नगा समूहों की चिंताओं का समाधान नहीं करती है, तो स्थिति और बिगड़ सकती है. 'व्यापार नाकेबंदी' से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है, और कुकी शिविर का स्थानांतरण हिंसक टकराव को जन्म दे सकता है.
रूस से और S-400 सिस्टम खरीदने पर भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों का ख़तरा
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के अच्छे प्रदर्शन के बाद, नई दिल्ली ने हाल के हफ्तों में कथित तौर पर अतिरिक्त S-400 की खरीद के लिए रूस के साथ बातचीत शुरू कर दी है और निकट भविष्य में उच्च-क्षमता वाली S-500 प्रणालियों को खरीदने पर भी विचार कर रही है. सैन्य और रक्षा उद्योग के सूत्रों का हवाला देते हुए राहुल बेदी की रिपोर्ट के अनुसार, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से अमेरिका के 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन्स एक्ट' (CAATSA) के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम है.
यह ख़बर भारत की रक्षा ख़रीद और इसकी स्वतंत्र विदेश नीति के सामने एक बड़ी दुविधा को उजागर करती है. भारत को अपनी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने और अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना होगा. सूत्रों का कहना है कि ट्रम्प और मोदी के बीच हालिया मेल-मिलाप के बावजूद यह जोखिम कम होने की संभावना नहीं है, और हाल ही में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की भारत की आलोचनात्मक बयानबाज़ी को देखते हुए यह निश्चित रूप से 'जीवित' है. बेदी यह भी याद दिलाते हैं कि यह ट्रम्प नहीं बल्कि जो बाइडेन थे, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में वाशिंगटन की इंडो-पैसिफिक रणनीति के आलोक में S-400 खरीदने के लिए भारत को CAATSA प्रतिबंधों से छूट दी थी.
यह स्थिति अमेरिका और रूस के बीच शक्ति संतुलन में भारत की नाजुक स्थिति को दर्शाती है. जहाँ रूस एक पारंपरिक रक्षा भागीदार बना हुआ है, वहीं अमेरिका इंडो-पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है. S-400 की खरीद इस जटिल समीकरण का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है. यदि भारत अतिरिक्त S-400/S-500 सिस्टम की खरीद के साथ आगे बढ़ता है, तो उसे CAATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा. यह भारत-अमेरिका रक्षा और व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकता है. नई दिल्ली को सावधानी से अपने विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा.
42% भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में संविदाकर्मियों की हिस्सेदारी 27 साल के उच्चतम स्तर पर
भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी 42% है, जो कम से कम 27 वर्षों में सबसे अधिक है. यह आँकड़ा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) से लिया गया है. यह आँकड़ा भारत में रोज़गार की गुणवत्ता में गिरावट का संकेत देता है. संविदा पर काम करने वाले श्रमिकों को अक्सर स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और उन्हें कम सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं. पिछले दशक में इस हिस्सेदारी में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 1990 के दशक के अंत के बाद से इसमें केवल 2013-14 में कमी आई थी. TISS के प्रोफेसर बिनो पॉल के हवाले से मम्पट्टा कहते हैं: "जब तक भारतीय विनिर्माण सस्ते श्रम के तुलनात्मक लाभों से हटकर नवाचार और उत्पादकता की वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं की ओर नहीं बढ़ता, तब तक संविदा श्रम बल का विस्तार जारी रहेगा". यह प्रवृत्ति कंपनियों द्वारा श्रम क़ानूनों की कठोरता से बचने और लागत कम करने की कोशिश को दर्शाती है. हालाँकि यह कंपनियों के लिए लचीलापन प्रदान कर सकता है, लेकिन यह श्रमिकों के लिए नौकरी की असुरक्षा और कम आय का कारण बनता है, जिससे व्यापक आर्थिक असमानता बढ़ती है.
बीएलओ को लेकर ईसीआई और ममता में संघर्ष, बिहार जैसा एसआईआर बंगाल में हो पाएगा?
“स्क्रॉल” में अनंत गुप्ता ने लिखा है कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में बिहार जैसा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने में दिक्कत आ सकती है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच इस बात पर संघर्ष जारी है कि अधिकारी पूरी तरह किसके नियंत्रण में होंगे. बिहार में चुनावी तैयारी के दौरान ब्लॉक लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की भूमिका और उनकी तैनाती को लेकर जो विवाद सामने आया था, वह पश्चिम बंगाल में एक अलग चुनौती पेश कर रहा है.
पश्चिम बंगाल में बीएलओ की नियुक्ति और नियंत्रण को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर मतभेद हैं, जो चुनाव आयोग के लिए एसआईआर को बिहार के जैसा सफलतापूर्वक लागू करने में बाधा बन सकते हैं.
चुनाव आयोग बीएलओ को एक महत्वपूर्ण कड़ी मानता है, जो मतदाता सूची की सटीकता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है. लेकिन बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों और स्थानीय प्रशासन में ममता सरकार के प्रभाव के कारण बीएलओ को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चुनौतिपूर्ण हो सकता है.
नीतीश को अब “कुर्सी कुमार” और “पलटू चाचा” कहा जाता है
“गल्फ न्यूज़” में स्वाति चतुर्वेदी की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के सबसे मजबूत नेता और मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, जिन्हें कभी "सुशासन बाबू" कहा जाता था, अब उन्हें तंज़ में "कुर्सी कुमार" और "पलटू चाचा" कहा जाता है. राजनीतिक फेरबदल और सत्ता के प्रति उनकी भूख को लेकर अब ये उनके “उपनाम” बने हैं.
74 वर्षीय नीतीश कुमार, जो बिहार के "जंगल राज" से सुशासन की ओर बदलाव के लिए प्रशंसा के पात्र थे, अब बिहार की राजनीति में कमजोर पड़ते दिख रहे हैं. उनके शासन को सबसे कमजोर प्रशासन माना जा रहा है, जिसमें वे केवल चार वरिष्ठ अधिकारियों पर भरोसा करते हैं. वे अपनी पार्टी और राजनीतिक माहौल से कटे हुए हैं और उनके पुत्र निशांत कुमार लगातार उनके साथ नजर आते हैं.
हर गली-मोहल्ले में उनकी “क्षणिक विस्मृति” को लेकर चर्चा होती है, जिसमें लोग उनके बूढ़े होने को समझदारी के साथ देखते हैं. बिहार में विपक्षी ‘इंडिया ब्लॉक’ ने एकजुटता दिखाई है और तेजस्वी यादव को अपने नेता के तौर पर आगे लाया है, जिससे सरकार और भाजपा चिंतित हैं.
नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों बिहार के लंबे समय तक राज करने वाले नेता रहे हैं. उनके बीच दोस्ती से दुश्मनी और फिर से साथ काम करने का फिल्मी इतिहास साफ दिखता है. लेकिन, नीतीश के प्रधानमंत्री बनने के सपने मोदी के उदय और राजनीति के कठोर यथार्थ के कारण अब धुंधले पड़ गए हैं.
इस बार, जदयू ने भाजपा से एक सीट ज्यादा मांग कर यह दिखाने की कोशिश की है कि गठबंधन में उसका नेतृत्व मजबूत है. लोग भी अब भाजपा और जदयू के बीच की इस कड़ी राजनीति को देख रहे हैं.
चिराग पासवान ने भी 40 सीटों की मांग से राजनीतिक समीकरणों को जटिल बना दिया है, जबकि भाजपा और जदयू दोनों ही इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. पासवान मुख्यमंत्री पद के अपने इरादे खोलकर रख चुके हैं.
प्रशांत किशोर, जो कभी नीतीश के करीबी थे और उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे, अब सत्ता के लिए नीतीश के सामने विरोधी बन गए हैं. किशोर का राजनीतिक खेल जटिल है, क्योंकि वे मोदी और शाह पर कभी हमला नहीं करते, बल्कि इंडिया गठबंधन और जदयू दोनों पर वार करते हैं.
नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा उन्हें एक छोटे नेता में बदल चुकी है, जो केवल सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए संघर्ष करते रहे हैं. क्या बिहार उन्हें फिर से वह मौका देगा? ये सवाल खुला हुआ है.
वैकल्पिक मीडिया
मोतिहारी का मुसहर समाज: सामाजिक भेदभाव, भूखमरी और गरीबी के अंधेरे में
बिहार इन दिनों अपने चुनावी रणनीतियों और प्रधानमंत्री की माँ के लिए इस्तेमाल हुए अपशब्द, पिंडदान जैसे मोज़ू की वजह से ज़ेर ए बहस है. इन सब इन्तेख़ाबी शोर और दावे के दरमियान मुसहर जाती के लोग आज भी रोटी, रोज़ी से दूर और सामाजिक रुस्वाई का सामना कर रहे हैं. बिहार के मोतिहारी जिले के रुलही गाँव की महादलित मुसहर बस्ती के लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक जैसे लफ्ज़ का बोझ नहीं उठाते. इनके पेट आज भी दो वक़्त की रोटी से खाली, हाथ मज़दूरी से सने और कंधे रोज़ रोज़ के जातीय असमानता से झुक गया है.
द मूकनायक की एक रिपोर्ट के अनुसार रुलही में करीब 50 मुसहर परिवार रहते हैं. पुरुष मज़दूरी के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पलायन कर गए हैं. महिलाएँ खेतों में 8-9 घंटे काम करती हैं और केवल 50-60 रुपये कमाती हैं. संपति देवी कहती हैं, "भूख से बड़ी कोई चीज़ नहीं. पेट भरने के लिए दिनभर झुके रहना पड़ता है, लेकिन इतने में बच्चों का पेट भी नहीं भरता."
सरकारी योजनाएँ भी बस्ती में काम नहीं आतीं. राशन दुकानदार घोटाला करते हैं. पूनम देवी बताती हैं कि पाँच किलो अनाज की जगह केवल तीन-किलो ही मिलता है. पीने के पानी, पोषण योजना और स्वरोज़गार के साधन भी नहीं हैं. मनरेगा का दावा साल में 100 दिन काम दिलाने का है, लेकिन गाँव में मज़दूरों को मुश्किल से 30-40 दिन काम मिलता है. बुजुर्ग मानिक कहते हैं, "सरकार कहती है 200 दिन काम मिलेगा, लेकिन साल भर में सिर्फ़ 20-25 दिन ही मिलता है."
जातिगत भेदभाव और तिरस्कार इनकी ज़िन्दगी की वह हकीकत है जिसे न आज़ादी बदल पाई और न संविधान. सरपंच जब बस्ती में आता है तो मुसहरों से दूरी बनाता है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो वोट मांगने ज़रूर आता है.
बिहार में मुसहर जाति महादलित है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में यह समाज के सबसे पिछड़े और कमज़ोर वर्ग में आते हैं. योजनाएँ केवल कागज़ों तक सीमित हैं. भूख और बेबसी की लड़ाई यहाँ हर घर की दीवारों से चीख बन कर निकलती है, जिसकी आवाज़ को सरकारी दफ़्तरों और सामाजिक पदक्रम दबा देता है.
चुनावों में नेताओं के भाषणों में मुसहर समाज को गरीब और वंचित का प्रतीक बनाकर कई वादे किये जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई उनकी ज़िन्दगी की समस्याओं को हल करने के लिए वापस उनकी बस्ती में लौटकर नहीं आता.
गेमिंग के पीछे छिपी परतें
चमकदार ऐप्स और जैकपॉट्स के पीछे खाता-खोलने वालों (म्यूल अकाउंट्स), पे-आउट्स और पेमेंट के जटिल तरीकों का जाल है, जो स्क्रीन के परे हजारों करोड़ रुपये इधर-उधर कर देता है. “द हेड एंड टेल” की आरती सिंह ने गेमिंग की इन छिपी परतों को खंगाला और दिखाया कि किस तरह यह सेक्टर पैसे घुमाने की मशीन बन गया है. सख्त सज़ाओं के बावजूद, उनके परीक्षण बताते हैं – “खेल अब भी जारी है.”
सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित
एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले और वे भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए. विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए. “द इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, कुल 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया, जो कुल संख्या का 98.2 प्रतिशत है. इनमें से 752 वोट वैध माने गए और 15 अमान्य घोषित हुए. जीत का कोटा या बहुमत-सीमा 377 थी. इस प्रकार जीत का अंतर 152 वोटों का रहा.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने “एक्स” पर कहा कि विपक्षी सांसदों ने 100 प्रतिशत मतदान किया. जबकि बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने स्थानीय मुद्दों को सामने रखा और राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी गठबंधन से दूरी बनाई. हालांकि, लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने दावा किया कि राधाकृष्णन ने 452 वोटों से विजय हासिल की, क्योंकि उन्हें कुछ विपक्षी सांसदों का भी समर्थन मिला. उन्होंने कहा, “विपक्ष के करीब 40 सांसदों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर राधाकृष्णन का समर्थन किया.” इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा कि- “आपका इस गरिमामय पद पर पहुंचना प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है.” “आपके नेतृत्व में यह गरिमामय पद अवश्य ही और अधिक सम्मान एवं गौरव प्राप्त करेगा”, उन्होंने कहा.
अडानी समूह के आरोप झूठे, निराधार और अपमानजनक : परंजॉय
वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने कहा है कि अडानी समूह द्वारा उन पर लगाए गए आरोप झूठे, निराधार और अपमानजनक हैं, और उन्हें जवाब देने का अधिकार दिए बिना लगाए गए हैं. उन्होंने कहा, “मैं अपनी रिपोर्टिंग पर अडिग हूं, जो सत्यापित, तथ्यात्मक, निष्पक्ष, संतुलित और बिना किसी भय या पक्षपात के की गई है.”
एक बयान में ठाकुरता ने बताया कि शनिवार 6 सितंबर 2025 को नई दिल्ली की रोहिणी अदालत ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मेरे खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की. ‘एकपक्षीय’ का अर्थ है कि अदालती आदेश घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में मेरा पक्ष सुने बिना ही पारित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से अडानी समूह की कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा मेरे खिलाफ दायर किया गया यह सातवां मानहानि का मुकदमा है. उन्होंने कहा कि मैं लगभग 50 वर्षों से पत्रकार हूं. मुझे भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा लिखे गए सभी लेख और मेरे द्वारा दिए गए सभी बयान न केवल सत्य और सटीक हैं, बल्कि हमेशा जनहित में हैं.
नेपाल में अराजकता, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया, सरकारी इमारतों को आग लगाई, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री आवास, संसद, सुप्रीम कोर्ट को भी फूंका
पीएम ओली का इस्तीफा, नेपाल छोड़कर भागे
भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार को अराजकता फैल गई. भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन-जी के विरोध प्रदर्शन ने दूसरे दिन तो हिंसक रूप ले लिया. लिहाजा नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जला दिया. उनके घर में आग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह जल गईं. उनको गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउबा तथा उनकी पत्नी और मौजूदा विदेश मंत्री आरज़ू राणा देउबा के आवास पर हमला किया गया और दोनों की पिटाई की गई. प्रदर्शनकारियों ने बांकट स्थित पीएम ओली के आवास, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सोमवार को गृहमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ के घरों को भी आग लगा दी. वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया. उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर आग लगा दी. सुरक्षा बलों के हथियार लूट लिये. मंगलवार को प्रधानमंत्री ओली ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत, ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों को भी आग लगा दी.
इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री ओली सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर चले गए. एक वीडियो में ऐसा दिखाया गया. वे संभवतः दुबई गए हैं. भारत के पड़ोस में बांग्लादेश की शेख हसीना के बाद ओली दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है. इस्तीफे की घोषणा करते हुए ओली ने कहा कि उन्होंने "समस्या के समाधान को सुगम बनाने और इसे राजनीतिक रूप से हल करने में मदद के लिए" यह निर्णय लिया है. नेपाली सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने एक दुर्लभ संयुक्त अपील जारी की, जिसमें संयम बरतने और शांति बहाली के लिए संवाद को ही एकमात्र रास्ता बताया गया. सुरक्षा परिस्थितियों और गंभीर हालात का हवाला देते हुए काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.
An aerial view of smoke rising from the Federal Parliament of Nepal premises in Kathmandu on September 9, 2025. Photo: PTI/Abhishek Maharjan.
भारतीयों को सलाह : इधर, विदेश मंत्रालय ने नेपाल में तेजी से बदलते घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई है, जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए. नेपाल में वर्तमान में मौजूद भारतीय नागरिकों को अपने मौजूदा निवास स्थानों पर ही रुकने, सड़क पर बाहर निकलने से बचने और पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
“द न्यूयॉर्क टाइम्स” के अनुसार, नेपाल की राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा तब हुई, के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया था और सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए थे. यह हालिया वर्षों में इस दक्षिण एशियाई देश में सबसे गंभीर सामाजिक अशांति मानी जा रही है. काठमांडू में सत्ताधारी तबके को सीधे निशाना बनाया गया. सोशल मीडिया पर साझा वीडियोज़ में दिखा कि मंत्रियों को सरकार की मुख्य प्रशासनिक इमारत से हेलिकॉप्टरों द्वारा निकाला गया.
प्रतिबंध हटना : नेपाल में सोशल मीडिया बेहद अहम है, क्योंकि बड़ी संख्या में नागरिक विदेशों में काम करते हैं और घर पैसे भेजते हैं. पिछले हफ्ते सरकार ने 26 सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था, जिनमें वीचैट, यूट्यूब और लिंक्डइन शामिल थे, लेकिन मंगलवार सुबह सभी सेवाएं, फिर से बहाल कर दी गईं.
दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य : यह संकट क्षेत्र के अन्य देशों की अशांति से मेल खाता है. एक साल पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी इसी तरह के दृश्य देखे गए थे, जहां प्रधानमंत्री को सड़क पर हुए प्रदर्शनों के बाद पद छोड़ना पड़ा. करीब तीन साल पहले, ऐसा ही श्रीलंका में भी हुआ था.
युवा और लोकतंत्र : नेपाल में प्रदर्शनकारी ज्यादातर किशोर और युवा वयस्क थे, जिन्हें अब "जेनरेशन जी प्रोटेस्ट" कहा जा रहा है. नेपाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत क़द्र की गई है, जबकि दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों में यह अधिकार सीमित होते जा रहे हैं.
आर्थिक संकट : आम जनता में आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार के बड़े मामलों पर ढीला रवैया अपनाने को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है. देश का सबसे बड़ा संकट नौकरियों की कमी है.
इस्तीफ़े : ओली 2024 में पांचवी बार नेपाल के शीर्ष पद पर निर्वाचित हुए थे. अब यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी जगह कौन लेगा. कुल मिलाकर, चार मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया है, जिनमें नेपाली कांग्रेस के तीन मंत्री भी शामिल हैं.
‘मुझे तभी जाने दिया जब मैंने सरकार के खिलाफ नारा लगाया’
“काठमांडू की सड़कों पर आज रात हालात बेहद खतरनाक हैं. कुछ प्रदर्शनकारियों ने मेरी मोटरसाइकिल को घेर लिया और जब उन्हें पता चला कि मैं पत्रकार हूं, तो वे उस पर टूट पड़े. उन्होंने मुझे तभी जाने दिया जब मैंने सरकार के खिलाफ नारा लगाया. शहर में सुरक्षा बल बहुत कम हैं, और हथियार सिर्फ उनके पास ही नहीं हैं. कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत में जिंदा ग्रेनेड फेंके. दूसरों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वे असॉल्ट राइफल लिए हुए दिख रहे हैं,” भद्र शर्मा ने काठमांडू से लिखा है.
मालेगांव बम विस्फोट; एनएआई ने चुनौती नहीं दी, मृतकों के परिजनों ने हाईकोर्ट का रुख किया
चूंकि सरकारी जांच एजेंसी ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती नहीं दी है, लिहाजा 2008 मालेगांव बम विस्फोट के छह मृतकों के परिजनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने 31 जुलाई के विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया था. याचिका में एनआईए अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत के 31 जुलाई के निर्णय को निरस्त करने और आरोपियों को दोषी ठहराने की मांग की गई है. “द इंडियन एक्सप्रेस” के मुताबिक, मामले की जांच करने वाली एनआईए ने दरअसल, अब तक इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी है.
हरकारा डीपडाइव
श्रवण गर्ग: लोकतंत्र से खिसककर मोदी तानाशाहों की तरफ
वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने वैश्विक राजनीति, भारत की भूमिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं. गर्ग ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता ने दुनिया को मोदी की नज़र से देखना शुरू किया और दुनिया ने मोदी को भारतीयों की नज़र से समझना शुरू किया. असल में मोदी की छवि विदेशी ज़मीन में गढ़ी गई और भारत में उसे तरतीब दी गई. अब पहली बार भारतीय नागरिकों को मौका मिल रहा है कि वे मोदी को भारतीय दृष्टि से देखें.
उन्होंने कहा कि आज पश्चिमी देश मोदी को अर्ध-तानाशाह के रूप में देखते हैं. वह एक ऐसे नेता के तौर पर उभर के आए हैं जो लोकतांत्रिक देशों की नज़रों में बने रहना चाहते हैं लेकिन भीतर से तानाशाही रुझान रखते हैं. उन्होंने बताया कि मोदी की छवि पर जो परतें चढ़ाई गईं, वे अब खुलने लगी हैं और भारत के लोग उनके "मूल स्वरूप" को देख रहे हैं.
गर्ग ने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि इमरजेंसी के बावजूद विदेशी मीडिया ने उन्हें तानाशाह नहीं कहा, लेकिन मोदी को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर "सेमी-ऑटोक्रेट" कहा जा रहा है. मोदी की छवि मंचीय करिश्मे से आगे अब सामान्य और साधारण दिखाई देने लगी है.
गर्ग ने कहा कि जब ट्रंप ने लोकतांत्रिक देशों, जैसे यूरोप पर टैरिफ लगाया तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और ट्रंप को पीठ दिखाने की जगह संतुलित रखा. लेकिन मोदी ने अलग राह ली, भारत पर टैरिफ लगने पर ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती वाले समीकरण को संतुलित रखने के बजाय वह रूस और चीन की ओर झुकने लगे. इससे पश्चिमी देशों की नज़र में भारत की विश्वसनीयता और भी कमज़ोर हुई. मोदी चीन और रूस के साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे क्योंकि भारत के पास उनकी तरह सैन्य शक्ति नहीं है. भारत की ताकत लोकतंत्र में है.
उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि भारत अब लोकतांत्रिक ताक़तों का सहारा नहीं ले रहा, बल्कि तानाशाही ताक़तों का सहारा ले रहा है. मोदी की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वे पुतिन की तरह आजीवन सत्ता बनाए रखने का रास्ता तलाश रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर अनजाने में BRICS को मजबूत किया. इससे चीन, रूस, भारत और ब्राज़ील आपस में और करीब आए और उनके रिश्ते मजबूत हुए. इस तरह BRICS एक ऐसा cocktail बन गया जिसमें लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का मिश्रण है.
श्रवण गर्ग ने बिहार में मतदाता सूची विवाद पर मोदी की तनक़ीद करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जितना वे असुरक्षित और भयभीत होते हैं, उतना ही उनकी नीतियां भारत और भारतीयों के खिलाफ और कठोर व क्रूर हो जाती हैं.
विश्लेषण | धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका
‘प्रशासन में बैठे लोग मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, तो संविधान आम आदमी के लिए बेमानी हो जाएगा’
वकील और हाईकोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस एस मुरलीधर ने एजी नूरानी मेमोरियल व्याख्यान में 'धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका: एक असहज संबंध' विषय पर एक गहन और विचारोत्तेजक भाषण दिया. अपने व्याख्यान में, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका के जटिल संबंधों, बाबरी मस्जिद मामले में न्यायपालिका की भूमिका, पूजा स्थल अधिनियम, सामासिक संस्कृति, हिजाब मामले, संवैधानिक नैतिकता और न्यायाधीशों के निजी व सार्वजनिक जीवन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. यह लेख न्यायमूर्ति मुरलीधर के व्याख्यान के प्रमुख तथ्यों, तर्कों और निष्कर्षों को व्यापक रूप से प्रस्तुत करता है.
भारत की विविधता और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संस्करण
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने अपने व्याख्यान की शुरुआत भारत की अद्वितीय विविधता को रेखांकित करते हुए की. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के अधिकांश हिंदुओं, जैनियों और सिखों का घर होने के साथ-साथ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में से एक और लाखों ईसाइयों तथा बौद्धों का भी घर है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत कभी भी एक संस्कृति, एक भाषा या एक धर्म का राष्ट्र नहीं था और न ही हो सकता है. हमारी विविधता और बहुलता ही हमारी पहचान और गौरव है.
उन्होंने प्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. जी.एन. देवी द्वारा संपादित 2023 की पुस्तक "इंडियंस, हिस्ट्रीज ऑफ ए सिविलाइजेशन" का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे औपनिवेशिक काल के लेखन ने भारत को हिंदुओं की भूमि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जबकि मुसलमानों को आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया गया. इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण ने वैदिक संस्कृति, ब्राह्मणवाद और संस्कृत को भारत से जोड़ा, जबकि मुसलमानों, अरबी और फारसी को विदेशी माना.
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने बताया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से अलग है, जो चर्च और राज्य के बीच सख्त अलगाव की बात करता है. भारत में धर्मनिरपेक्षता को "सर्व धर्म समभाव" या सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के रूप में समझा जाता है, जहां राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है. उन्होंने बताया कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया था.
बाबरी मस्जिद मामला: न्यायपालिका की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने बाबरी मस्जिद मामले को भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया. उन्होंने इस मामले के कानूनी इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसमें 1885 में फैजाबाद के एक सिविल जज द्वारा मंदिर बनाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने से लेकर 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक की घटनाओं का जिक्र था.
उन्होंने 1885 के जज के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अगर मंदिर का निर्माण होता है तो शंख और घंटियों की आवाज से अशांति फैल सकती है और हजारों लोग मारे जा सकते हैं. यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी न्यायपालिका शांति और सद्भाव बनाए रखने के प्रति कितनी सचेत थी.
उन्होंने 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद में मूर्तियों को रखे जाने की घटना और उसके बाद की न्यायिक प्रक्रिया का भी उल्लेख किया, जिसके कारण यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए. उन्होंने बताया कि कैसे न्यायिक हस्तक्षेपों ने इस मुद्दे को दशकों तक जीवित रखा.
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे शाहबानो मामले के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल बदला और बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से गरमा गया. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो मामले में संसद के माध्यम से कानून बनाकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के ताले खोलकर हिंदुओं को भी साधने का प्रयास किया गया, जिसने स्थिति को और जटिल बना दिया.
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस को उन्होंने भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास का एक काला अध्याय बताया. उन्होंने इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में सही ठहराया और धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना के रूप में फिर से स्थापित किया.
उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक कार्यवाही की धीमी गति और अंततः सभी आरोपियों के बरी हो जाने पर निराशा व्यक्त की. उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अदालत की अवमानना के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मात्र एक दिन की सांकेतिक सजा क्यों दी गई. उन्होंने कहा कि यह न्याय का मजाक था और इसने कानून के शासन में लोगों के विश्वास को कमजोर किया.
अयोध्या फैसला: एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने 9 नवंबर 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के अयोध्या फैसले का भी आलोचनात्मक विश्लेषण किया. उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि अदालत ने अपने फैसले में यह स्वीकार किया कि मुसलमानों को गलत तरीके से मस्जिद से वंचित किया गया था, लेकिन फिर भी विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी.
उन्होंने इस तथ्य पर भी ध्यान दिलाया कि अदालत ने अपने फैसले में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के महत्व को रेखांकित किया था, जिसका उद्देश्य 15 अगस्त 1947 को मौजूद पूजा स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना था, लेकिन अयोध्या फैसले ने इस कानून के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद देश भर में कई अन्य पूजा स्थलों को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं.
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि अदालत ने मध्यस्थता के विकल्प को पूरी तरह से नहीं खोजा. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता पैनल ने एक समझौते पर पहुंचने की सूचना दी थी, लेकिन अदालत ने उस पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह फैसला सिर्फ इसलिए जल्दबाजी में दिया गया क्योंकि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले थे.
पूजा स्थल अधिनियम, सामासिक संस्कृति और हिजाब मामला
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह कानून देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है. उन्होंने सरकार और न्यायपालिका से इस कानून की भावना को बनाए रखने का आग्रह किया.
उन्होंने भारत की "सामासिक संस्कृति" की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं. उन्होंने तमिलनाडु के नागपट्टिनम शहर का उदाहरण दिया, जहां एक चर्च, एक दरगाह और एक मंदिर एक-दूसरे के करीब स्थित हैं और सभी धर्मों के लोग इन तीनों पवित्र स्थानों पर जाते हैं. उन्होंने कहा कि यही भारत की असली ताकत है, जिसे हमें हर कीमत पर बचाए रखना चाहिए.
हिजाब मामले पर, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के विपरीत विचारों का उल्लेख किया. एक न्यायाधीश ने जहां स्कूल में एकरूपता पर जोर दिया, वहीं दूसरे न्यायाधीश ने एक छात्रा की निजता, गरिमा और पसंद के अधिकार का समर्थन किया. न्यायमूर्ति मुरलीधर ने दूसरे न्यायाधीश के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि हमें अपनी विविधता का जश्न मनाना चाहिए, न कि उसे दबाने की कोशिश करनी चाहिए.
संवैधानिक नैतिकता और न्यायाधीशों का निजी व सार्वजनिक जीवन
न्यायमूर्ति मुरलीधर ने संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है कि प्रशासन में बैठे लोग संविधान के मूल्यों, जैसे समानता, गैर-भेदभाव और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन में बैठे लोग इन मूल्यों का पालन नहीं करेंगे, तो संविधान आम आदमी के लिए निरर्थक हो जाएगा.
उन्होंने न्यायाधीशों के निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच के अंतर पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को अपने निजी विश्वासों को अपने न्यायिक कार्यों पर हावी नहीं होने देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब न्यायाधीश सार्वजनिक रूप से धार्मिक समारोहों में भाग लेते हैं या धार्मिक प्रतीक पहनते हैं, तो इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं. उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को अपने आचरण के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, ताकि न्याय न केवल हो, बल्कि होता हुआ भी दिखे.
अंत में, न्यायमूर्ति मुरलीधर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को संवैधानिक मूल्यों के बारे में शिक्षित करना होगा, ताकि वे एक सुरक्षित और समावेशी भारत में रह सकें. उन्होंने न्यायपालिका से आत्मनिरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वह धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों को बनाए रखे.
चीनी फ़ायरवॉल का इस्तेमाल कर अपने लाखों लोगों की जासूसी कर रहा पाकिस्तान
पाकिस्तान अपने नागरिकों पर जासूसी करने के लिए फोन-टैपिंग सिस्टम और चीन द्वारा बनाए गए इंटरनेट फ़ायरवॉल का इस्तेमाल कर रहा है, जो सोशल मीडिया को सेंसर करता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि यह चीन के बाहर राज्य निगरानी (स्टेट सर्विलांस) के सबसे व्यापक उदाहरणों में से एक है.
मानवाधिकार निगरानी संगठन ने एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान का बढ़ता निगरानी नेटवर्क चीनी और पश्चिमी तकनीक दोनों की सहायता से बनाया गया है और इसका इस्तेमाल असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर व्यापक दमन के लिए किया जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में पहले से ही सीमित राजनीतिक और मीडिया स्वतंत्रताओं पर हाल के वर्षों में और अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, खासकर तब से जब सेना ने 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से नाता तोड़ लिया. बाद में उन्हें जेल भेजा गया और उनकी पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.
‘रॉयटर्स’ की खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अपने "लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम" (एलआईएमएस) के जरिये एक समय में कम से कम 40 लाख मोबाइल फोन की निगरानी कर सकती हैं, जबकि "डब्ल्यूएमएस2.0" नामक फ़ायरवॉल, जो इंटरनेट ट्रैफ़िक की जांच करता है, एक समय में 20 लाख सक्रिय सत्रों को ब्लॉक कर सकता है.
चलते चलते
पारसी समुदाय की आवाज़ 'पारसियाना' पत्रिका छह दशकों के बाद बंद होगी
भारत की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित पारसी पत्रिकाओं में से एक, 'पारसियाना', पारसी समुदाय का छह दशकों तक इतिहास लिखने के बाद इस अक्टूबर में अपना प्रकाशन बंद कर देगी. इसके अगस्त के संपादकीय में की गई इस घोषणा ने पाठकों को एक ऐसे प्रकाशन के खोने का शोक मनाने पर मजबूर कर दिया है, जिसने घटती आबादी के लिए एक आईने और एक पुल दोनों के रूप में काम किया. 'पारसियाना' का बंद होना सिर्फ़ एक पत्रिका का अंत नहीं है, बल्कि यह पारसी समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दस्तावेज़ का नुक़सान है. यह पत्रिका समुदाय के भीतर संवाद, बहस और आत्म-चिंतन का एक महत्वपूर्ण मंच थी. इसका बंद होना समुदाय की घटती संख्या और उसकी विरासत को संरक्षित करने की चुनौतियों का भी प्रतीक है. 1964 में एक डॉक्टर और चंदन के व्यापारी पेस्टनजी वार्डन द्वारा स्थापित, 'पारसियाना' की शुरुआत एक मासिक पत्रिका के रूप में हुई जिसमें निबंध और चिकित्सा लेख शामिल थे. 1973 में जहांगीर पटेल द्वारा इसे एक पाक्षिक पत्रिका में बदल दिया गया, जिन्होंने इसे एक रुपये में ख़रीदा और इसे एक पूर्ण पत्रकारिता उद्यम में बदल दिया. बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में पटेल ने समुदाय की उच्च तलाक़ दर पर अपनी पहली कहानी को याद करते हुए कहा, "किसी ने भी पारसियाना में ऐसा कुछ पढ़ने की उम्मीद नहीं की थी". यह पत्रिका सिर्फ़ समुदाय की ख़बरें ही नहीं छापती थी, बल्कि इसने समुदाय के भीतर के विवादास्पद मुद्दों जैसे तलाक़, अंतर-धार्मिक विवाह और घटती जनसंख्या पर भी साहसिक रिपोर्टिंग की. इसने पारसी समुदाय को ख़ुद को और बाहरी दुनिया को समझने में मदद की. इसका बंद होना स्वतंत्र और समुदाय-केंद्रित पत्रकारिता के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को भी उजागर करता है.
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.