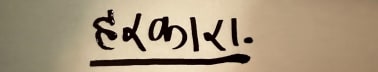16/07/2025: बिहार को लेकर भाजपा में भी धुकधुक | तेलुगु देशम चिंतित | ‘झटका और प्रताड़ना’ नीति | पायलटों ने रिपोर्ट का बुरा माना | खाद की किल्लत | दिल्ली दंगों पर बेमेल दलीलें | कांवड़ियों पर नोटिस
‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.
निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल
आज की सुर्खियां :
सिर्फ़ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी भी चिंतित
बिहार में 35 लाख से ज़्यादा वोटर लिस्ट से बाहर, चुनाव आयोग के दावों पर सवाल
एसआईआर पर भाजपा चुप पर तेलुगु देशम चिंतित
अजाज़ अशरफ़: ‘झटका और प्रताड़ना’ सरकार की स्थापित नीति है
बोइंग विमानों की सुरक्षा 'भगवान भरोसे,' रिकॉर्ड में 65 इंजन फेल और 11 ‘मेडे कॉल’
जमानत पर झूठी कड़ी: सॉलिसिटर जनरल ने अनुमान के आधार पर जोड़ा इमाम को ट्रम्प से
चीन ने घटाई सप्लाई, भारत में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान
चीन से संबंधों पर जयशंकर के बयान पर कांग्रेस ने की संसद में बहस की मांग
ओडिशा: यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर छात्रा ने दी जान
मुंबई के खराब टॉयलेट्स पर रिपोर्ट देने वाले एनजीओ की होगी जांच, मंत्री ने पूछे मंशा पर सवाल
ट्रम्प का 22वीं बार दावा, मैंने भारत-पाकिस्तान का परमाणु युद्ध रुकवाया
मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए बनाए थे सरकारी अस्पताल, पर अब बेचे जा रहे
सैर पर निकले फौजा सिंह की कार टक्कर में मौत
महाराष्ट्र भाषा विवादः हिंदुत्ववादी राजनीति का हथियार है हिंदी
भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली
अरुणाचल में मेगा डैम का विरोध जारी, ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को लिखा पत्र
पुलिस को मॉब लिंचिंग का केस दर्ज करना था, लेकिन सामान्य हत्या की धारा लगाई, जांच रोकी
कांवड़ यात्रा मार्ग पर क्यूआर कोड, सुप्रीम कोर्ट का यूपी और उत्तराखंड सरकारों को नोटिस
लद्दाख में बढ़ते हुए हिम तेंदुए
बिहार
सिर्फ़ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी भी चिंतित
'द इंडियन एक्सप्रेस' के लिए संतोष सिंह की रिपोर्ट है कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष संवीक्षण अभियान को लेकर जारी भ्रम और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अब भाजपा भी दबाव में है. सूत्रों के अनुसार, ज़मीन से मिल रही नकारात्मक रिपोर्टों के बाद, बीजेपी के संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया ने सोमवार को पार्टी के 26 प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि वे राज्यभर में फैलकर मतदाताओं से मिलें, उनकी शंकाओं को दूर करें और पार्टी समर्थकों को नामांकन प्रक्रिया में मदद करें. पार्टी को यह चिंता भी है कि उसने SIR को लेकर उठे सवालों पर विपक्ष को नैरेटिव सेट करने दिया, जो लगातार "बड़े पैमाने पर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने" की चेतावनी दे रहा है और चुनाव आयोग की "जल्दबाज़ी" पर सवाल उठा रहा है. विपक्षी INDIA गठबंधन (राजद, कांग्रेस और वाम दल) ने बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) की संख्या बढ़ाने में भी भाजपा से तेज़ी दिखाई है.
बीते सप्ताहांत भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी. एल. संतोष बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने राजगीर व मुज़फ्फरपुर में शीर्ष स्तर की बैठकें कीं. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने चुनावी तैयारियों के साथ-साथ यह भी जाना कि लोग SIR को लेकर क्या सोच रहे हैं. दलसानिया की बैठक में भाजपा नेताओं को निर्देश दिया गया कि पार्टी के बीएलए राज्य के अधिकतम बूथों तक पहुंचे. 19 जुलाई से भाजपा विधानसभा क्षेत्रवार बैठकें शुरू करेगी, ताकि उन्हें इस प्रक्रिया पर स्वतःस्फूर्त फीडबैक मिल सके. ये बैठकें 31 जुलाई तक चलेंगी यानी पहले ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन से एक दिन पहले तक.
बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' से कहा — "हमने लोगों की चिंताओं पर चर्चा की, खासतौर पर इस बात पर कि आयोग कितनी जल्दबाज़ी में यह प्रक्रिया चला रहा है. यहां तक कि नामांकन फॉर्म जमा करने पर लोगों को रसीद (दूसरा एन्युमरेशन फॉर्म) नहीं दी जा रही है और अधिकतर लोगों का कहना है कि उनसे कोई फॉर्म भरवाने भी नहीं आया है." हालांकि भाजपा के पास अभी भी सभी दलों में सबसे ज़्यादा, 52,000 से अधिक बीएलए हैं, पर पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये संख्या अभी 73,000 से अधिक बूथों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है. एक नेता ने कहा, "हम विपक्ष के मुकाबले सुस्त और संतुष्ट नज़र आ रहे हैं."
भाजपा की आंतरिक फील्ड रिपोर्ट के अनुसार, अब तक जिन लोगों ने नामांकन फॉर्म भरे हैं, उनमें से केवल 30% ने ही आवश्यक दस्तावेज़ जमा किए हैं. "70-80% लोग फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 में से कोई दस्तावेज़ साथ नहीं दे रहे," उन्होंने कहा.
1 अगस्त के बाद वह चरण शुरू होगा जिसमें वोटर नामांकन के लिए दस्तावेज़ अपलोड किए जाएंगे. यह अवधि भाजपा के लिए और भी निर्णायक मानी जा रही है. पार्टी अब चाहती है कि उसके दोनों प्रकार के बीएलए — BLA-1 (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक) और BLA-2 (प्रत्येक बूथ पर तैनात) इस प्रक्रिया के अंत तक सक्रिय रूप से शामिल रहें. भाजपा कार्यकर्ता अब दोनों के साथ मैदान में उतरेंगे.
बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा — "हमें SIR प्रक्रिया पर भरोसा है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं. हम इस बात को लेकर सहयोग कर रहे हैं कि सभी वैध मतदाता सूची में बने रहें, लेकिन ऐसे भी हालात हैं जहां काम के सिलसिले में बाहर गए लोग छूट सकते हैं. हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग का ऑनलाइन ऐप इस स्थिति से निपटने में मदद करेगा."
SIR अभियान की शुरुआत 25 जून को हुई थी. इसके बाद 2 जुलाई तक राज्य में विभिन्न दलों के बीएलए की संख्या में 13% की वृद्धि हुई है.
विपक्षी INDIA गठबंधन (राजद, कांग्रेस, वाम दल) ने 17.51% की वृद्धि दर्ज की — उनकी बीएलए संख्या 56,038 से बढ़कर 65,853 हो गई.
कांग्रेस ने सबसे अधिक वृद्धि (92.17%) दर्ज की — 8,586 से बढ़कर 16,500 तक.
वहीं एनडीए गठबंधन (भाजपा-जदयू) ने 10.86% की वृद्धि के साथ बीएलए संख्या 80,083 से बढ़ाकर 88,781 की.
भाजपा की वृद्धि मात्र 1.39% रही — 51,964 से 52,689.
जदयू ने 24.13% की बढ़ोतरी की — 27,931 से 34,669.
कुल मिलाकर इस समय पूरे बिहार में मतदाता सूची को लेकर ज़ोरदार खींचतान जारी है और अब सत्तारूढ़ दल भाजपा भी मैदान में पूरी ताकत से उतरने को मजबूर हो गई है.
बिहार में 35 लाख से ज़्यादा वोटर लिस्ट से बाहर, चुनाव आयोग के दावों पर सवाल
बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में एक 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान चला रहा है. लेकिन इसके तीसरे दौर के शुरू होने से पहले ही, चुनाव आयोग के अपने आंकड़े बताते हैं कि 35.6 लाख मतदाता सूची से बाहर होने वाले हैं. आयोग के अनुसार, उसके अधिकारियों ने घर-घर जाकर दो राउंड का सर्वे पूरा कर लिया है. अब तक बिहार के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से केवल 88.18% तक ही पहुंचा जा सका है. इनमें से भी सिर्फ 6.6 करोड़ (83.66%) मतदाताओं ने ही अपने फॉर्म जमा किए हैं. इसका मतलब है कि एक बड़ी आबादी इस प्रक्रिया से अब तक दूर है. अब जाकर चुनाव आयोग ने अखबारों में विज्ञापन देना शुरू किया है ताकि बिहार से बाहर काम कर रहे प्रवासी मज़दूरों तक पहुंचा जा सके. हिंदुस्तान टाइम्स ने इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की है.
बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर क्यों गहराया अविश्वास? | जेएनयू में राजनीति विज्ञान के शिक्षक डॉ. मणिंद्र ठाकुर क्यों कह रहे हैं कि बिहार में चल रही गहन मतदाता पुनरीक्षण सूची की कवायद सरकार के प्रति नागरिकों में गहरे अविश्वास को जन्म दे रही है! हरकारा 'डीप डाइव' के इस एपिसोड में निधीश त्यागी ने बिहार से उठ रहे ऐसे ही कई जमीनी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है.
एसआईआर पर भाजपा चुप पर तेलुगु देशम चिंतित
‘द वायर’ के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट सुधार अभियान पर गंभीर चिंता जताई है. टीडीपी ने कहा है कि चुनाव आयोग को यह साफ करना चाहिए कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' का मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को ठीक करना है, न कि नागरिकों की नागरिकता की जांच करना. पार्टी का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया से भ्रम और डर का माहौल बन सकता है. टीडीपी ने अपनी चिट्ठी में यह भी मांग की है कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उनके खिलाफ कोई ठोस और पुख्ता कारण न हो.
पार्टी ने इस अभियान के लिए दिए गए समय को भी बहुत कम बताया है. बिहार से एक बड़ी आबादी दूसरे राज्यों में मज़दूरी करने जाती है. इन प्रवासी मज़दूरों का नाम लिस्ट से न कट जाए, इसके लिए टीडीपी ने 'मोबाइल ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों' की तैनाती का सुझाव दिया है. ये अधिकारी घूम-घूमकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रह जाए. पार्टी का मानना है कि इस अभियान के मौजूदा तरीके से लाखों लोगों, खासकर गरीब और प्रवासी मज़दूरों का नाम कटने का खतरा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
विश्लेषण
अजाज़ अशरफ़: ‘झटका और प्रताड़ना’ सरकार की स्थापित नीति है
वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमनिस्ट अजाज़ अशरफ़ ने मिड डे में बताया है कि सरकार जब चाहे लोगों को शॉक ट्रीटमेंट तो दे देती है, हालांकि उसके नतीज़ों के बारे बात नहीं करती. उनके लेख के कुछ अंश.
बिहार का अनुभव यह दिखाता है कि लोगों को समय-समय पर झटके देना, भले ही इससे उन्हें कितनी भी प्रताड़ना क्यों न झेलनी पड़े, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन एक स्थापित राजकीय नीति बन गई है. इस नीति का दिखावटी उद्देश्य हिंदुत्व की व्यापक विचारधारा के तहत एक अधिक नैतिक, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण करना है. लेकिन इसके परिणामों ने मेहनतकश जनता के बजाय निश्चित रूप से धनी वर्गों का पक्ष लिया है.
सरकार की इसी 'झटका और प्रताड़ना' नीति के कारण बिहार के लोगों से अचानक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए उनकी नागरिकता का प्रमाण देने के लिए कहा गया है. मताधिकार से वंचित होने के दुःस्वप्न से पीड़ित, वे भारत के चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 नागरिकता दस्तावेजों में से किसी एक को हासिल करने के लिए हताशा में इधर-उधर भाग-दौड़ कर रहे हैं.
सरकार की 'झटका और प्रताड़ना' नीति 8 नवंबर, 2016 से विकसित होनी शुरू हुई, जब चार घंटे के नोटिस पर उच्च-मूल्य वाले करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें नए बैंक नोटों से बदलने के लिए बैंकों में कभी न खत्म होने वाली कतारें लग गईं. नकदी की कमी ने असंगठित क्षेत्र से उसकी जीवनदायिनी छीन ली—नौकरियां गायब हो गईं और कृषि पिछड़ गई.
इस नीति ने 24 मार्च, 2020 को एक बड़ी छलांग लगाई, जब देश को COVID-19 महामारी से निपटने के लिए पूर्ण तालाबंदी के तहत रखा गया. जैसे ही कार्यस्थल और यातायात के साधन बंद हुए, और बिना किसी आय या बचत के जीवित रहने के लिए, शहरों में करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गांवों को लौटने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने लगे, और उन्होंने अकथनीय दुख का अनुभव किया.
इन तीनों ही मामलों में, सरकार ने सामूहिक शॉक थेरेपी देने के लिए एक नेक या नैतिक कारण का हवाला दिया. बिहार में, राज्य का दावा है कि गैर-नागरिकों, यानी अवैध अप्रवासियों को मतदाता सूची से हटाना महत्वपूर्ण है, कहीं ऐसा न हो कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दूषित कर दें. नोटबंदी का औचित्य भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना और काले धन के उपयोग को हतोत्साहित करना था. लॉकडाउन का उद्देश्य लोगों को मृत्यु से बचाना था, क्योंकि उन पर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का भरोसा नहीं किया जा सकता था.
ये सामूहिक शॉक थेरेपी उस गहरे अविश्वास को दर्शाती हैं जो सरकार को लोगों पर है. वह उन्हें इतना पतित या अज्ञानी मानता है कि वे नैतिक रूप से सही या तर्कसंगत रास्ता नहीं अपना सकते. इसलिए, सरकार उन्हें अचानक चौंका देती है, यह मानते हुए कि उन्हें उसे धोखा देने के लिए समय और अवसर से वंचित किया जाना चाहिए.
इस प्रकार, बिहार के लोगों को मतदाता के रूप में नामांकन के लिए आधार कार्ड दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि यह व्यापक रूप से लोगों के पास है. राज्य की निहित धारणा यह है कि आधार धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो सकता है. नोटबंदी को गोपनीयता के पर्दे में इसलिए रखा गया ताकि जमाखोरों को उनके अवैध धन के भंडार को ठिकाने लगाने का मौका न मिले. लॉकडाउन को सख्ती से लागू करना पड़ा क्योंकि एक पितृसत्तात्मक राज्य ने लोगों को जिद्दी बच्चों के रूप में देखा.
सरकार ने अपनी शॉक थेरेपी के माध्यम से लोगों को जो प्रताड़ना दी है, वह समान रूप से वितरित नहीं हुई है. बिहार में, यह निम्नवर्गीय लोग हैं जो मताधिकार से वंचित होने से डरते हैं, न कि अभिजात्य वर्ग, क्योंकि उनके पास चुनाव आयोग के 11 नागरिकता दस्तावेजों में से कम से कम एक तो निश्चित रूप से होगा.
न ही सरकार एक बेहतर भारत बनाने में सफल हुई है. लगभग सभी विमुद्रीकृत करेंसी नोटों के बैंकों में वापस आने के साथ, अर्थव्यवस्था से काला धन समाप्त नहीं हुआ. इसका तात्पर्य यह है कि धनी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र का हिस्सा रहे लोगों पर इसका पंगु बना देने वाला प्रभाव पड़ा. लॉकडाउन से उनकी परेशानियाँ और बढ़ गईं. महत्वपूर्ण बात यह है कि, जैसा कि अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने बताया है, जिस मांग को असंगठित क्षेत्र अब पूरा नहीं कर सकता था, वह संगठित क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गई.
कृषि क्षेत्र में बड़े निजी निगमों के प्रवेश को सुगम बनाना ही सरकार द्वारा किसान समुदाय को एक झटका देने के पीछे की प्रेरणा थी, जो 2020 में बनाए गए तीन कृषि कानूनों के माध्यम से दिया गया. यह उनके लिए एक झटका था क्योंकि उनके जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाले कानूनों को पारित करने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया था.
जो लोग सरकार की सत्ता के सूत्रधार हैं, वे यह सुझाव देते प्रतीत हुए कि किसानों से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे अनाड़ी मूर्ख थे जो यह नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है. इससे भी बदतर, राज्य ने सोचा कि महामारी-जनित प्रतिबंध सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाकर किसानों को विरोध करने से रोक देंगे. लेकिन उन्होंने विरोध किया, दिल्ली के बाहर एक साल तक बैठे रहे—जिसमें 700 से अधिक की मृत्यु हो गई—इससे पहले कि राज्य पीछे हट गया.
कश्मीरियों को झटका देने का तरीका अन्य मामलों में अपनाए गए तरीके से उल्लेखनीय रूप से भिन्न था. सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले कश्मीर में सेना की भारी तैनाती की, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में एक महीने से अधिक समय तक कर्फ्यू लगाया गया और 4000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया. इंटरनेट 175 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था.
यह लगभग ऐसा था जैसे पूरे कश्मीर को कोमा में डालना पड़ा हो ताकि उसे दिए गए उच्च-वोल्टेज के झटके के कारण वह दर्द से छटपटाए नहीं. इस झटके का औचित्य? कश्मीर में उग्रवाद को जड़ से खत्म करना और इसे भारत के साथ एकीकृत करना. अप्रैल में हुए पहलगाम नरसंहार ने प्रदर्शित किया कि ये लक्ष्य अभी भी पहुंच से दूर हैं.
नैतिकता और वैचारिक हठधर्मिता की धारणाओं ने सरकार को लोगों को प्रताड़ित करने के लिए प्रेरित किया है, जिनमें विडंबना यह है कि संप्रभुता निहित है. शायद राज्य के कर्णधार उन कार्यों के परिणामों को समझने के लिए बहुत अज्ञानी हैं जो वे इसके नाम पर करते हैं. या शायद वे मानते हैं कि अंडे तोड़े बिना आमलेट नहीं बनाया जा सकता. अंतिम दुर्भाग्य यह है कि सरकार द्वारा पकाए गए आमलेट का स्वाद चखने का मौका केवल कुछ ही लोगों को मिलता है.
एयर इंडिया हादसा
बोइंग विमानों की सुरक्षा 'भगवान भरोसे,' रिकॉर्ड में 65 इंजन फेल और 11 ‘मेडे कॉल’
जहां एक ओर डीजीसीए और एयरलाइंस बोइंग विमानों के तकनीकी पहलुओं की जांच में जुटी हैं, वहीं विशेषज्ञों और पायलट यूनियनों ने जांच की प्रक्रिया और निष्कर्षों में पारदर्शिता की मांग की है. 'द हिन्दू' की रिपोर्ट है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना के बाद भारत के नागर विमानन नियामक डीजीसीए (डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने देश की सभी एयरलाइनों को बोइंग विमानों में फ्यूल कट-ऑफ स्विच की जांच करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश उस प्रारंभिक रिपोर्ट के दो दिन बाद जारी किया गया जिसमें पाया गया था कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के फ्यूल स्विच उड़ान के दौरान बंद हो गए थे.
हालांकि डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया, लेकिन उसने यह आदेश इसलिए जारी किया क्योंकि भारत सहित कई अन्य देशों की विमानन कंपनियों ने 2018 की अमेरिकी सुरक्षा एडवाइजरी के आधार पर फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग प्रणाली की जांच शुरू कर दी है. इसी क्रम में दक्षिण कोरिया भी अपने सभी बोइंग विमानों की जांच कराने की तैयारी कर रहा है.
रिपोर्ट पर उठे सवाल, ‘पायलट दोष’ पर निंदा : वहीं, प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर विमानन विशेषज्ञों और पायलट संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. अंतरराष्ट्रीय पायलट संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयर लाइन पॉयलट एसोसिएशन (आईएफएएलपीए) ने बयान जारी कर कहा है कि यह रिपोर्ट अधूरी, अनुत्तरित सवालों से भरी है और इसका झुकाव पायलट त्रुटि की ओर है. "ऐसी किसी भी प्रारंभिक रिपोर्ट से निष्कर्ष निकालना अनुमान की श्रेणी में आता है," संगठन ने कहा. आईएफएएलपीए, जो 100 देशों के 1 लाख पायलटों का प्रतिनिधित्व करता है, ने रिपोर्ट के "स्वर और दिशा" पर सवाल उठाते हुए तथ्य-आधारित और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
पायलट बातचीत गायब, विशेषज्ञों ने जताई आपत्ति : लीहम न्यूज एंड एनालिसिस के एविएशन विशेषज्ञ ब्योर्न फेहरम ने फायनेंशियल टाइम्स से बातचीत में रिपोर्ट को "बहुत धुंधली और अनिश्चित" बताया और कहा कि इसमें पायलटों की बातचीत के प्रत्यक्ष अंश नहीं दिए गए हैं, जो अन्य देशों की रिपोर्टिंग में आमतौर पर होते हैं. एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने भी एक आंतरिक ज्ञापन में माना कि रिपोर्ट से “कुछ स्पष्टता तो आई है, लेकिन इससे कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं,” जिससे "मीडिया में नई अटकलों का दौर शुरू हो गया है."
आरटीआई जवाब में खुलासा: 17 महीनों में 11 ‘मेडे कॉल’ और 65 इंजन फेल : 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरटीआई के ज़रिए प्राप्त जानकारी से यह सामने आया है कि बीते 17 महीनों में 11 विमानों ने ‘मेडे कॉल’ दी, जिनमें AI-171 की दुर्घटना और एक इंडिगो फ्लाइट की आपात लैंडिंग शामिल नहीं है. इसके अलावा, 2020 से अब तक 65 बार इन-फ्लाइट इंजन फेल होने की घटनाएं दर्ज हुई हैं. डीजीसीए ने यह भी स्वीकार किया कि ज्यादातर तकनीकी खराबियां टेकऑफ़ या उड़ान के बीच में हुईं, जो भारतीय विमानों में तकनीकी गड़बड़ियों की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है.
दिल्ली दंगे
जमानत पर झूठी कड़ी: सॉलिसिटर जनरल ने अनुमान के आधार पर जोड़ा इमाम को ट्रम्प से
(उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और शरजील इमाम 2020 से दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में बिना मुकदमे के जेल में हैं. 9 जुलाई 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया. | साभार : आर्टीकल 14)
"यह हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि यह राज्य का अंतिम तर्क था, और हम इसका खंडन नहीं कर सके क्योंकि फैसला सुरक्षित कर लिया गया था,". शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम की यह टिप्पणी सिर्फ़ एक जुमला नहीं, बल्कि एक पूरी न्याय प्रक्रिया पर सवाल है, जो तर्क की जगह अनुमान और आरोप की जगह व्याख्या से भरी हुई लगती है. 'आर्टीकल 14' के लिए बेतवा शर्मा की रिपोर्ट है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेल में बंद मुस्लिम कार्यकर्ताओं उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और शरजील इमाम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो अंतिम तर्क दिया, वह अनुमान, निष्कर्ष और अतिशयोक्ति पर आधारित था, और इसमें ठोस सबूतों का अभाव था.
9 जुलाई 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने दावा किया कि शरजील इमाम ने 23 जनवरी 2020 को अपने भाषण में ‘चार सप्ताह’ का जो उल्लेख किया था, वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के लिए तय समयसीमा को दर्शाता है और यह कथित साजिश की एक समयरेखा की ओर इशारा करता है.
हालांकि 'आर्टीकल 14' द्वारा इमाम के भाषणों की जांच के अनुसार, यह ‘चार सप्ताह’ का संदर्भ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ दायर 100 से अधिक याचिकाओं पर जवाब देने के लिए दिए गए समय से था. शरजील इमाम ने 22 जनवरी को आसनसोल और 23 जनवरी को बिहार के गया में दिए अपने भाषणों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का स्पष्ट उल्लेख किया था.
'आर्टीकल 14' ने यह भी बताया कि ट्रम्प की भारत यात्रा की तारीखें 11 फरवरी 2020 तक सार्वजनिक नहीं हुई थीं, जबकि इमाम को 28 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था. फिर भी, मेहता ने यह दावा किया कि इमाम "संभावित तारीख" का उल्लेख कर रहे थे, क्योंकि यह समाचारों में था कि ट्रम्प चार सप्ताह में आ सकते हैं.
इस अंतिम तर्क के जवाब में इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने Article 14 को बताया, "यह हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला था क्योंकि यह राज्य का अंतिम तर्क था, और हम इसका खंडन नहीं कर सके क्योंकि फैसला सुरक्षित कर लिया गया था."
उन्होंने कहा कि भाषण में ‘चार सप्ताह’ का उल्लेख स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के संदर्भ में था, न कि किसी अवैध कार्रवाई के आह्वान में. उनके अनुसार, सॉलिसिटर जनरल जैसे वरिष्ठ अधिकारी का ऐसा बयान न्यायपालिका को पक्षपातपूर्ण बना सकता है. "अगर फैसला किसी गलत, गलत तरीके से पेश किए गए बयान पर आधारित होता है, तो यह न्याय का मजाक है."
अभियोजन पक्ष द्वारा इमाम और अन्य कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और सबूत-विहीन दावों से बने हुए हैं. अभियोजन की ओर से दिए गए अन्य तथ्यों में संरक्षित गवाहों के बयान, व्हाट्सएप संदेश और भाषणों के अंश शामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कथित साजिश को ट्रम्प की यात्रा से नहीं जोड़ता.
इमाम के 23 जनवरी वाले भाषण में ‘चार सप्ताह’ का ज़िक्र CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतिक्रिया में था, जिसे अभियोजन ने तोड़-मरोड़कर दंगे की तैयारी से जोड़ने की कोशिश की. जस्टिस नवीन चावला ने जब मेहता से पूछा कि उस व्हाट्सएप संदेश का लेखक, जिसमें ट्रम्प की यात्रा का ज़िक्र था, आरोपी क्यों नहीं है, तो यह अभियोजन की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है.
इस मामले में 18 में से 16 आरोपी मुस्लिम हैं, जबकि दंगों में मारे गए 53 लोगों में से तीन-चौथाई मुस्लिम थे. पुलिस ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक ऐसी कथित साजिश, जो मुस्लिमों द्वारा रची गई थी, उसमें मुस्लिमों की ही जान ज़्यादा क्यों गई.
इन कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाएं कई वर्षों से लंबित हैं. कुछ की याचिकाएं तीन साल से दिल्ली उच्च न्यायालय में अटकी हैं. इमाम और उमर खालिद इस मामले में लगभग पांच साल से बिना मुकदमे के जेल में हैं और इस दौरान मुकदमे की कार्यवाही भी पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ी है.
साजिश की एफआईआर 6 मार्च 2020 को दर्ज हुई थी, लेकिन पांच चार्जशीटें इसके तीन साल बाद तक दायर होती रहीं. आरोप तय करने की प्रक्रिया भी लंबी खिंचती रही है. अभियोजन पक्ष ने एक साल बाद स्वीकार किया कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी और लोगों को जोड़ने की संभावना है.
यह रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि पुलिस ने बार-बार कुछ ही भाषणों और गवाहों के बदले हुए बयानों के आधार पर एक बड़ा और संगठित दंगे की साजिश का मामला गढ़ा है, लेकिन किसी विश्वसनीय या ठोस सबूत से यह नहीं बताया कि इन आरोपियों ने हिंसा को कैसे अंजाम दिया. ये पूरा मामला भारतीय न्याय प्रणाली में लंबे समय तक विचाराधीन कैद, राजनीतिक असहमति के दमन और सबूत के बिना गंभीर आरोपों की रणनीति को सामने लाकर रख देता है. यह एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि क्या हम ‘जमानत, जेल नहीं’ के संवैधानिक सिद्धांत से दूर हटते जा रहे हैं?
चीन ने घटाई सप्लाई, भारत में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक खरीफ सीजन के उफान पर, देश के कई राज्यों के किसान डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खाद की कमी से जूझ रहे हैं. यूरिया के बाद डीएपी भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद है. इस किल्लत की मुख्य वजह चीन द्वारा डीएपी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हैं. चीन ने अपने किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है. चीन दुनिया में डीएपी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, इसलिए उसके इस फैसले का असर भारत पर सीधा पड़ा है. भारत अब सऊदी अरब, मोरक्को, रूस और जॉर्डन जैसे देशों से डीएपी खरीद रहा है, लेकिन ये देश चीन की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
इस कमी का असर ज़मीनी स्तर पर दिखने लगा है. ‘द हिंदुस्तान’ टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरा है. कांग्रेस ने विधानसभा में आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ 2025 के लिए डीएपी वितरण का लक्ष्य 30,000 टन घटा दिया. इसके बावजूद, अब तक केवल 1.01 लाख टन खाद की ही आपूर्ति हो पाई है. किसानों का कहना है कि समय पर खाद न मिलने से उनकी फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे उनकी आमदनी घटेगी. यह संकट दिखाता है कि भारत अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे देशों, खासकर चीन पर कितना निर्भर है.
चीन से संबंधों पर जयशंकर के बयान पर कांग्रेस ने की संसद में बहस की मांग
विदेश मंत्री एस. जयशंकर के चीन के साथ संबंधों में सुधार वाले बयान पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री आखिरकार मानसून सत्र में चीन के मुद्दे पर संसद में बहस के लिए राजी होंगे. पार्टी ने सवाल किया कि जब 1962 के युद्ध के बीच में इस पर चर्चा हो सकती है, तो अब क्यों नहीं. कांग्रेस ने कहा कि चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण शक्ति और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगले एक दशक में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है. ऐसे में चीन से पैदा होने वाली सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाना बहुत ज़रूरी है.
यह बयान तब आया जब बीजिंग दौरे पर गए एस. जयशंकर ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कज़ान में हुई मुलाकात के बाद से भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है. इस पर कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि शायद विदेश मंत्री को हाल की कुछ घटनाओं को याद दिलाने का समय आ गया है. उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया. उसने पाकिस्तान को J-10C लड़ाकू विमान, PL-15E हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और कई तरह के ड्रोन जैसे हथियार सिस्टम के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया."
ओडिशा: यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर छात्रा ने दी जान
ओडिशा में यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने से दुखी होकर कैंपस में खुद को आग लगाने वाली 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा की भुवनेश्वर के एम्स में मौत हो गई है. बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और प्रिंसिपल से इसकी शिकायत भी की थी. लेकिन जब उसकी शिकायत को कथित तौर पर हल्के में लिया गया, तो उसने शनिवार को कॉलेज की मुख्य इमारत के पास खुद को आग लगा ली. इस घटना के बाद बीजू जनता दल (बीजेडी) और कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने गुरुवार को बंद का भी ऐलान किया है. इस घटना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओडिशा की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे "सिस्टम द्वारा की गई एक संगठित हत्या" बताया. राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "जिन लोगों को उसकी रक्षा करनी थी, वे उसे तोड़ते रहे. हमेशा की तरह, भाजपा के सिस्टम ने आरोपी को बचाना जारी रखा और एक निर्दोष बेटी को खुद को आग लगाने के लिए मजबूर कर दिया." उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, "मोदी जी, चाहे ओडिशा हो या मणिपुर - देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं और मर रही हैं. और आप? आप चुप रहते हैं."
मुंबई के खराब टॉयलेट्स पर रिपोर्ट देने वाले एनजीओ की होगी जांच, मंत्री ने पूछे मंशा पर सवाल
महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने प्रजा फाउंडेशन नाम के एनजीओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. वजह यह है कि इस एनजीओ ने मुंबई में सार्वजनिक शौचालयों की खराब हालत पर एक रिपोर्ट जारी की थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि 2023 तक शहर के 6,800 सार्वजनिक शौचालयों में पानी और बिजली की सप्लाई नहीं थी. साथ ही, एक शौचालय का इस्तेमाल औसतन 752 पुरुष और 1,820 महिलाएं करती हैं, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है. इस रिपोर्ट को शिवसेना (UBT) के MLC सुनील शिंदे ने विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उठाया था.
इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय, उद्योग मंत्री उदय सामंत ने रिपोर्ट जारी करने वाले एनजीओ की मंशा पर ही सवाल उठा दिए. द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, सामंत ने कहा, "इस एनजीओ का उद्देश्य क्या है? हमें इसकी जांच करने की जरूरत है." वहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने मंत्री के हवाले से लिखा, "हमें ऐसी रिपोर्ट बनाने के पीछे प्रजा फाउंडेशन के इरादों की जांच करनी होगी." सरकार के इस रवैये की आलोचना हो रही है कि वह समस्या को सुलझाने के बजाय, समस्या उजागर करने वालों की ही जांच करा रही है.
ट्रम्प का 22वीं बार दावा, मैंने भारत-पाकिस्तान का परमाणु युद्ध रुकवाया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कराने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी मध्यस्थता ने दोनों देशों के बीच एक संभावित युद्ध को टाल दिया. कांग्रेस पार्टी के अनुसार, पिछले 65 दिनों में यह 22वीं बार है जब ट्रम्प ने ऐसा दावा किया है. नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ एक बैठक के दौरान ट्रम्प ने कहा, "हम युद्धों को निपटाने में बहुत सफल रहे हैं. आपके सामने भारत और पाकिस्तान हैं. रवांडा और कांगो का मामला है, जो 30 साल से चल रहा था. वैसे, जिस तरह से हालात बिगड़ रहे थे, भारत और पाकिस्तान के बीच एक हफ्ते के अंदर परमाणु युद्ध हो जाता. हालात बहुत खराब हो रहे थे." ट्रम्प पहले भी कई बार कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं, जिसे भारत ने हमेशा खारिज किया है. भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है. हालांकि, ट्रम्प अपने बयानों के जरिए यह दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि उनकी वजह से दक्षिण एशिया में शांति बनी हुई है. उनके इस हालिया बयान को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है.
मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए बनाए थे सरकारी अस्पताल, पर अब बेचे जा रहे
देश में, लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है, वह जन विश्वास के साथ किसी विश्वासघात से कम नहीं है. सरकारी अस्पतालों के निर्माण में करदाताओं की हजारों करोड़ रुपये की रकम, सार्वजनिक भूमि और सामूहिक प्रयास के साथ दशकों का निवेश इस उद्देश्य से किया गया था कि ये सबको मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे. लेकिन, अब “पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप” (पीपीपी) के नाम पर इस बुनियादी ढांचे को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे पीपीपी वास्तव में “पीपीटी” (पीपुल पे ट्वाइस) बन गया है, यानी लोग दो बार भुगतान करते हैं. “टाइम्स ऑफ़ इंडिया” में रमा नागराजन लिखती हैं कि नागरिक पहले तो इन अस्पतालों के निर्माण के लिए भुगतान करते हैं, और फिर दोबारा तब, जब उसी अस्पताल में महंगी निजी चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्हें मजबूरी में पैसे खर्च करने पड़ते हैं. इस खुलेआम लूट को उजागर करना कोई आसान काम नहीं है. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के पंद्रह अलग-अलग संस्करणों के रिपोर्टरों ने मिलकर 100 से अधिक अस्पतालों, 30,000 बिस्तरों और 1,400 एकड़ की प्रमुख सार्वजनिक भूमि का डेटा इकट्ठा किया और यह पाया कि स्वास्थ्य सेवाओं या अस्पतालों का व्यापक पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है. गहराई से किया गया यह विश्लेषण किसी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता. यह रिपोर्ट बताती है कि विकास के नाम पर अस्पतालों को बेचा जा रहा है और यह सार्वजनिक संपत्ति की ऐसी व्यवस्थित लूट को उजागर करती है, जिसमें बीमार और गरीब लोग अकेले छोड़ दिए गए हैं और पूरा तंत्र अब उनके खिलाफ काम कर रहा है.
सैर पर निकले फौजा सिंह की कार टक्कर में मौत
पंजाब के निवासी फौजा सिंह, जिन्होंने कथित तौर पर 100 वर्ष की उम्र में मैराथन दौड़कर दुनिया को चकित कर दिया था, का कल जालंधर जिले में अपनी रोज़ाना की सैर के दौरान एक कार की टक्कर लगने से निधन हो गया. जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण अधिकारियों ने उनकी सटीक उम्र की पुष्टि नहीं की, लेकिन उनकी कहानी और उपलब्धियों ने उन्हें कई प्रशंसक और समर्थक दिलाए हैं. “द न्यूयॉर्क टाइम्स” में जरे लॉन्गमैन ने अपने शोक संदेश में इस "टर्बन वाला टॉरनेडो" की जीवन गाथा बताई है, जिसमें फौजा सिंह के 2011 के आश्चर्यजनक और विवादास्पद कारनामों का जिक्र है.
विश्लेषण
महाराष्ट्र भाषा विवादः हिंदुत्ववादी राजनीति का हथियार है हिंदी
दिल्ली विश्वचवद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने ‘सत्य हिंदी’ में महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर एक लेख के जरिए कहा है कि मुंबई के भाषा विवाद के बहाने लोगों का ध्यान एक बार फिर हिंदी पर चला गया है. भारतीय जनता पार्टी नीत महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य करने का आदेश जारी किया. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टियों ने इसका विरोध किया. सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा.
महाराष्ट्र सरकार के इस फ़ैसले के बाद तथाकथित हिंदी भाषी इलाक़ों में रोष देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर ‘हिंदीवाले’ अनेक लोग अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं. प्रतिक्रिया का कारण यह तो है ही कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने से इनकार कर दिया गया बल्कि इसलिए भी है कि ‘मराठीवादियों’ ने कई लोगों पर यह कहकर हमला किया कि वे मुंबई में रहकर हिंदी क्यों बोल रहे हैं, मराठी क्यों नहीं. इसकी प्रतिक्रिया में यह कहा जा रहा है कि किसी को कोई भाषा बोलने से रोका नहीं जा सकता और किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह एक ख़ास भाषा बोले.
इसमें कोई शक नहीं कि जो मराठी न बोल पाने के लिए लोगों को पीट रहे हैं उन्हें कोई मराठी की चिंता नहीं. वे एक प्रकार की बहुसंख्यकवादी राजनीति में विश्वास करते हैं. मराठी इस बहुसंख्यकवादी राजनीति का आधार है. यही बात उनके बारे में कही जा सकती है जो हिंदी का नारा लगा रहे हैं. उन्हें भी हिंदी से लेना देना नहीं. वे भी एक ख़ास तरह की बहुसंख्यकवादी राजनीति के अभ्यासी या पैरोकार हैं जिसका आधार हिंदी है.
जब कोई भाषा के नाम पर हिंसा करने लगे तब मसला भाषा का नहीं होता. वह वास्तव में उस हिंसा के सहारे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है. अपने समुदाय का. वह दूसरे को बतलाना चाहता है कि उसके इलाक़े में उसका दबदबा है. ख़ासकर जब भाषा के नाम पर सामूहिक हिंसा की जा रही हो.
हिंदीवालों का कहना है कि हमने तो कभी किसी पर हिंदी बोलने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की, उनपर हिंसा नहीं की. लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि दिल्ली हो या पटना या बनारस, वहाँ रहनेवाले तमिल या मलयाली या मणिपुरी लोगों ने ख़ुद ब ख़ुद कामचलाऊ या उससे आगे की हिंदी सीखी है. उन्हें किसी को यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. वे यह बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के ही करते हैं. प्रायः उनके बच्चे अपने स्कूलों में भी हिंदी सीखते हैं.
लेकिन तमिलनाडु या कर्नाटक में रहनेवाले स्थानीय निवासी लाज़िमी तौर पर हिंदी सीखें, इसका कोई तर्क नहीं है. यह तर्क कि हिंदी सीखने से भारतीय होने में उन्हें मदद मिलेगी, लचर है. क्या प्रामाणिक भारतीय होने के लिए हिंदी जानना ज़रूरी है? हिंदीवाले अपने आप ही भारतीय हो जाते हैं? बिना कोई और भाषा सीखे?
हिंदी भारत में एकमात्र संपर्क भाषा है, यह मिथ टूट चुका है. अंग्रेज़ी यह काम अलग-अलग स्तर पर करने लगी है. कॉरपोरेट संसार में या सरकारी दफ़्तरों या विश्वविद्यालयों में एक दूसरे से बातचीत के लिए हिंदी की ज़रूरत नहीं है. टूटी फूटी या अपने अपने तरीक़े की अंग्रेज़ी से लोग काम चला लेते हैं. ऐसा नहीं कि हिंदी न जानने की हालत में भारत में किसी की ज़िंदगी कहीं मुश्किल होनेवाली है.
हिंदी के पक्षधर लोगों को हमेशा इस बात से हैरानी होती है कि महाराष्ट्र या तमिलनाडु या कर्नाटक में हिंदी का विरोध क्यों किया जा रहा है. या उन्हें उन क्षेत्रों की भाषा बोलने को बाध्य क्यों किया जा रहा है? यहाँ तक कि हिंदीवाले यह भी चाहते हैं कि उनसे राह रस्म के लिए दूसरे राज्यों के लोग अपने राज्यों में हिंदी सीखें. कुछ वक्त पहले एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें बंगलोर में एक बैंककर्मी ग्राहक से ज़िद कर रही है कि वह उससे सिर्फ़ हिंदी में ही बात कर सकती है. आम तौर पर जनता के साथ कारोबार करनेवाले स्थानीय भाषा सीख लेते हैं, वे प्रशासनिक अधिकारी हों या डॉक्टर या खोमचेवाला. लेकिन अब यह बात उद्धतता के साथ कही जाती है कि हम कन्नड़ या मराठी या बांग्ला नहीं बोलेंगे, जो करना हो कर लो. इस अहंकार का स्रोत क्या है?
क्या हिंदीवाले यह समझते हैं कि हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत है क्योंकि उनकी संख्या सबसे अधिक है? क्या वे दूसरी भाषावालों को कमजोर मानते हैं क्योंकि उनकी तादाद कम है?क् या वे यह सोचते हैं कि दिल्ली की हुकूमत उनकी है और बाक़ी सब उनके सूबे हैं? क्या इसीलिए वे मानते हैं कि मुंबई में मराठी बोलना उनके लिए ज़रूरी नहीं जबकि मुंबईवालों को हिंदी बोलना चाहिए?
हिंदीवाले समझ नहीं पाते कि हिंदी फ़िल्में जहाँ बनती हैं, उस शहर के लोग हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों हर जगह हिंदी का विरोध होता है? वे कभी यह नहीं सोचते कि हर जगह हिंदी सरकार के कंधे पर चढ़कर जाती है. सरकारी आदेशों के माध्यम से, सरकारी पैसे से हिंदी का साम्राज्य फैलाया जाता है. और यह सब इसलिए होता है कि संसद में हिंदीवालों की संख्या सबसे अधिक है.
हिंदी पर भारत की सारी भाषाओं के मुक़ाबले सबसे अधिक पैसा खर्च किया जाता है. उसके लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों में विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं. अलग अलग जगह हिंदी अनुवादकों की सबसे अधिक बहाली होती है. सरकारी हिंदी में वहाँ भी ख़तोकिताबत की जाती है जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं. यह सब कुछ कन्नड़ या तमिल या बांग्ला बोलनेवाले देखते हैं और उसके पीछे की राजनीति समझते हैं.भारत के संसाधनों पर उनकी भाषाओं का भी अधिकार है. लेकिन पक्षपात हिंदी के साथ किया जाता है.
हिंदी दूसरे क्यों सीखें? हिंदीवालों को उसके बारे में कुछ भ्रम हैं. जैसे यह कि वह संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है. अंग्रेज़ी के मुक़ाबले भी. वे भूल जाते हैं कि प्रत्येक भाषा के पास अपना व्याकरण है क्योंकि हरेक भाषा की अपनी व्यवस्था है. भोजपुरी की भी और बज्जिका की भी. आदिवासी भाषाएँ भी वैज्ञानिक हैं जैसे अंग्रेज़ी या अरबी. इसलिए हिंदी की ‘वैज्ञानिकता’ उसकी श्रेष्ठता और अनिवार्यता की दलील नहीं. हर भाषा वैज्ञानिक होती है.
फिर दूसरों के लिए उसकी क्या उपयोगिता है? क्या वह संसार के ज्ञान का आगार है? क्या उसके ज़रिए हम भारत और दुनिया के साहित्य से आसानी से परिचित हो पाते हैं? क्या इसके लिए कोई तमिलभाषी हिंदी सीखना चाहेगा? इस मामले में भी वह भारत की दूसरी भाषाओं की मदद नहीं कर पाती. यह ठीक है कि पिछले 70 साल से नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी और दूसरे संस्थानों ने हिंदी में अनुवाद करवाया है. अव्वल तो वह बहुत कम है, और वह भी प्रायः रचनात्मक साहित्य है. यह सब कुछ हिंदी के पहले अंग्रेज़ी में उपलब्ध हो जाता है. फिर हिंदी की कोई अनिवार्यता नहीं बचती.
हिंदी का सबसे बड़ा उपयोग राजनीतिक है. हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए हिंदी अनिवार्य है. इस पर हमने विचार नहीं किया कि हिंदुत्व के सिद्धांतकारों ने हिंदी को हिंदुत्व का सबसे कारगर वाहक क्यों माना. इसका कारण यह था कि सबसे अधिक ‘हिंदू संख्या’ उन्हीं इलाक़ों से तैयार की जा सकती थी जो ‘हिंदीभाषी’ इलाके हैं. उसी से हिंदू बहुसंख्या का निर्माण किया जा सकता था. हिंदी एक तरह से हिंदुत्ववादी राजनीति का बाहुबल है.
जबलपुर के मेरे एक बंगाली मित्र ने बतलाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी ने, जो ख़ुद बांग्लाभाषी हैं, बंगालियों की एक सभा को बांग्ला की जगह हिंदी में संबोधित किया. यह ख़ासी हिमाक़त है कि बंगालियों से एक बंगाली हिंदी में बात करे. यह जोखिम आर एस एस के उस अधिकारी ने क्यों उठाया? उस स्वयंसेवक ने बंगालियों को समझाया कि सारे बंगाली कन्नौज से बंगाल गए थे इसलिए हिंदी ही उनकी असली भाषा है. आर एस एस ने बंगाल जाकर यह नारा क्यों लगाया: नो दुर्गा, नो काली, ओनली राम ऐंड बजरंगबली?
दुर्गा की जगह राम वास्तव में बांग्ला को हिंदी से विस्थापित करने की कोशिश है. वैसे ही जैसे केरल में बाली की जगह वामन को स्थापित करने का प्रयास मलयालम की जगह हिंदी लाने की कोशिश है. फिर स्पष्ट करना ज़रूरी है कि यह हिंदी हिंदुत्ववादी राजनीति का उपकरण या हथियार है, यह गाँधी, प्रेमचंद ,महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय या ओमप्रकाश वाल्मीकि की हिंदी नहीं है.यह वह हिंदी है जिससे सारे उर्दू शब्दों को छाँट छाँटकर बाहर किया जाता है और शुद्ध हिंदू बनाया जाता है या संस्कृत की पुत्री के रूप में उसका संस्कार किया जाता है.
यह शिकायती, क्रोधी और हिंसक हिंदी है और हिंदुत्व की सवारी है. इसीलिए सुहास पलशीकर ने ठीक लिखा है कि हिंदी का विरोध करनेवाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मालूम होना चाहिए कि अगर वे हिंदुत्व की राजनीति करते रहेंगे तो हिंदी से बचना कठिन होगा.उन्हें हिंदुत्व की हिंदी को देखना चाहिए. वे जो करें, हिंदीवालों को अपने स्वास्थ्य के लिए इस हिंदीवाद से छुटकारा पाना और जल्दी से जल्दी यह करना बहुत ज़रूरी है.
भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली
'द हिंन्दू' की रिपोर्ट है कि यमन में हूथी प्रशासन द्वारा फांसी की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फिलहाल अस्थायी राहत मिली है. उन्हें कल फांसी दी जानी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद फांसी को टाल दिया गया है. भारत सरकार स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में लगातार बनी हुई थी, बावजूद इसके कि यह मामला बेहद संवेदनशील है. निमिषा प्रिया पर 2018 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार की हत्या का आरोप सिद्ध हुआ था, जिसके बाद उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई. यमन में लागू शरिया कानून के तहत, यदि वह मृतक के परिवार को "दीया" यानी रक्तपात मुआवज़ा देती हैं, तो फांसी से राहत मिल सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के परिवार से बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत के विवरण अभी स्पष्ट नहीं हैं. भारत सरकार आधिकारिक रूप से हूथी शासन को मान्यता नहीं देती, जिसने प्रिया को सजा सुनाई है. फिलहाल निमिषा प्रिया की जान बच गई है, लेकिन उनका भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है.
अरुणाचल में मेगा डैम का विरोध जारी, ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को लिखा पत्र
'द वायर' की रिपोर्ट है कि अरुणाचल प्रदेश के तीन ज़िलों के ग्रामीणों ने सोमवार को अपर सियांग ज़िले के गेगू गांव में एक रैली निकालकर प्रस्तावित सियांग अपर बहुद्देश्यीय परियोजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. सियांग इंडिजेनस फार्मर्स फोरम ने प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा को एक पत्र लिखकर इस परियोजना और इसके ज़मीनी स्तर पर जारी "पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट" चरण का कड़ा विरोध जताया है. फोरम की युवा इकाई ने यह भी आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट साइट की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबकि स्थानीय लोगों से कोई सहमति नहीं ली गई है.
फोरम ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के उस दावे का भी खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रामीणों ने परियोजना के लिए अपनी सहमति दी है. ग्रामीणों ने कहा कि ऐसा कोई सामूहिक निर्णय या सहमति नहीं दी गई है. ग्रामीणों में इस परियोजना को लेकर गहरी चिंता है, खासकर संभावित विस्थापन, खेती की ज़मीन के नुकसान और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर. इस विरोध प्रदर्शन और पत्र के ज़रिए ग्रामीणों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि बिना स्थानीय समुदाय की स्पष्ट और स्वैच्छिक सहमति के किसी भी तरह की कार्यवाही को रोक दिया जाए.
यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित है और राज्य सरकार व केंद्र के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ऊर्जा उत्पादन व सिंचाई जैसे उद्देश्यों के लिए तैयार की जा रही है, लेकिन स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे अपनी ज़मीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा मान रहा है. फिलहाल सरकार की ओर से इस ताज़ा विरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
पुलिस को मॉब लिंचिंग का केस दर्ज करना था, लेकिन सामान्य हत्या की धारा लगाई, जांच रोकी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग के एक मामले की पुलिस जांच पर रोक लगा दी है, क्योंकि पुलिस ने इसे “सामान्य हत्या की धारा” के अंतर्गत दर्ज किया, जबकि इसे नफरत से प्रेरित मॉब लिंचिंग को लेकर बनी बीएनएस की धारा 103 (2) के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था, जो अधिक सख्त है और पहचान आधारित नफरत से प्रेरित पांच या अधिक लोगों की भीड़ द्वारा की गई हिंसा को अपराध मानती है.
“टाइम्स ऑफ़ इंडिया” के अनुसार, हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के तहसीन एस पूनावाला दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिक विस्तार से अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. इन दिशानिर्देशों में मॉब लिंचिंग के मामलों से निपटने के लिए रोकथाम, जवाबदेही और पीड़ित सहायता पर ज़ोर दिया गया है. इसमें हर ज़िले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, एफआईआर में देरी न होना, पीड़ित या उनके परिजनों को अंतरिम मुआवज़ा, समयबद्ध चार्जशीट और ट्रायल, और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जैसी बातों का प्रावधान है.
यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अविनाश सक्सेना की बेंच ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर दिया, जिसे मृतक शहीदीन कुरैशी (37) के बड़े भाई मोहम्मद आलम ने दाखिल किया था. शहीदीन को 30 दिसंबर को खुद को गौरक्षक कहने वाले कुछ लोगों ने मार डाला था. अदालत ने पाया कि शहीदीन पर हमला करने वाली भीड़ की परिस्थितियां बीएनएस की धारा 103(2) के तहत कार्रवाई के लिए पर्याप्त थीं. अगली सुनवाई 5 अगस्त के लिए निर्धारित है. याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने हमलावरों को बचाया और अपराध रोकने के कर्तव्य में चूक की.
कांवड़ यात्रा मार्ग पर क्यूआर कोड, सुप्रीम कोर्ट का यूपी और उत्तराखंड सरकारों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजन विक्रेताओं को बैनरों पर क्यूआर कोड वाले स्टिकर लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर जवाब देने के लिए उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को एक सप्ताह का समय दिया है. मंगलवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए इस मामले को अगले मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया. हालांकि, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन आवेदकों की ओर से सीनियर एडवोकेट शदान फरासत ने कहा कि यह मामला “समय-संवेदनशील” है क्योंकि कांवड़ यात्रा अगले दस-बारह दिनों में समाप्त हो जाएगी.
‘लाइव लॉ’ के अनुसार, आवेदकों—प्रोफेसर अपूर्वानंद और सामाजिक कार्यकर्ता आकार पटेल—का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बचने के लिए अधिकारियों ने इस वर्ष नए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कांवड़ मार्ग पर सभी भोजनालयों को क्यूआर कोड लगाने के लिए बाध्य किया गया है, जिससे स्वामियों के नाम और पहचान का पता चलता है. उनका दावा है कि इस निर्देश का उद्देश्य तीर्थ मार्ग पर विक्रेताओं की धार्मिक प्रोफाइलिंग करना है. आवेदकों के अनुसार, सरकार के इन निर्देशों को कानून का कोई समर्थन नहीं है, और इनका मकसद धार्मिक ध्रुवीकरण तथा भेदभाव को बढ़ावा देना है. ये निर्देश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि विक्रेताओं को उनकी पहचान का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
चलते-चलते
लद्दाख में बढ़ते हुए हिम तेंदुए
हिमालय की ऊंची और दुर्गम चोटियों पर एक मायावी शिकारी घूमता है, जिसे 'पहाड़ों का भूत' भी कहा जाता है—हिम तेंदुआ. इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हाल ही में हुए भारत के सबसे बड़े सर्वेक्षण ने इस रहस्यमयी जीव की दुनिया पर नई रोशनी डाली है. लद्दाख के 59,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस दो-वर्षीय अध्ययन से पता चला है कि यह क्षेत्र लगभग 477 हिम तेंदुओं का घर है, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 68% है. यह सर्वेक्षण न केवल अपनी विशालता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी अनूठी तकनीक के लिए भी जाना जाता है.
शोधकर्ताओं ने हिम तेंदुओं की पहचान के लिए उनके शरीर के पैटर्न के बजाय माथे पर बने अनोखे पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया, जो किसी इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है. यह तरीका ज़्यादा सटीक साबित हुआ और इससे भारत की पहली राष्ट्रीय हिम तेंदुआ फोटो लाइब्रेरी बनाने में भी मदद मिली. अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले थे. 61% से अधिक हिम तेंदुए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर, यानी इंसानों और मवेशियों के साथ साझा इलाकों में रहते पाए गए. यह लद्दाख की स्थानीय बौद्ध संस्कृति और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व की उनकी परंपरा को दर्शाता है, जिसके कारण यहां उनका अवैध शिकार नहीं होता.
लेकिन इस सकारात्मक तस्वीर के साथ भविष्य की कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं. बढ़ता पर्यटन, सड़क और बांधों का निर्माण, और जलवायु परिवर्तन इनके आवास के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं. इनमें सबसे बड़ी और तत्काल चिंता आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या है, जो सैन्य शिविरों और कस्बों के पास जमा होने वाले कचरे के कारण पनप रहे हैं और हिम तेंदुओं पर हमला कर रहे हैं. यह अध्ययन इस बात पर ज़ोर देता है कि संरक्षण सिर्फ पार्कों तक सीमित नहीं रह सकता. किसी भी विकास कार्य को पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन करने के बाद ही मंजूरी मिलनी चाहिए और जानवरों के लिए "ग्रीन कॉरिडोर" बनाने को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि यह मायावी शिकारी हिमालय की ऊंचाइयों पर हमेशा सुरक्षित रह सके.
पाठकों से अपील :
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.