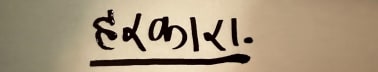17/11/2025: बीजेपी तभी हारेगी, जब वह खुद चाहे | हसीना को सज़ा ए मौत, ढाका अलर्ट | हर इंडेक्स पर लुढ़कता भारत | लाश का धर्मांतरण | आज़म खान, बेटे को फिर सज़ा | बिहार पर ज़ोया हसन, श्रवण गर्ग
‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.
निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फ़लक अफ़शां
आज की सुर्खियां
आनंद तेलतुंबडे अब बीजेपी को हराना नामुमकिन?
शेख़ हसीना को सज़ा-ए-मौत ढाका में हाई अलर्ट
सऊदी में दर्दनाक हादसा बस में ज़िंदा जले 45 भारतीय
रूस पर ट्रंप का नया दांव दोस्तों पर भी लगेगी पाबंदी भारत-चीन पर नज़र
आज़म खान फिर सलाखों के पीछे दो महीने की आज़ादी खत्म बेटे संग सात साल की सज़ा
असम में चुनावी आहट मतदाता सूची में फेरबदल की तैयारी एसआर का आदेश, एसआईआर का इंतज़ार
मनरेगा से 27 लाख नाम गायब ई-केवाईसी की मार
आकार पटेल हर पायदान पर फिसलता भारत
ज़ोया हसन बिहार में पैसा और महिला का खेल
आदिवासी ईसाइयों पर क़हर पहले शव का धर्म बदला फिर करने दिया अंतिम संस्कार
लाल किला विस्फोट मामला एक और कश्मीरी गिरफ़्तार पूछताछ से टूटे पिता ने दी जान
देश का खज़ाना फिर खाली विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट डॉलर के मुक़ाबले रुपया कमज़ोर
विश्लेषण बिहार चुनाव
आनंद तेलतुंबडे : बीजेपी तब तक नहीं हारेगी, जब तक खुद न चाहे
लेखक पीआईएल के पूर्व सीईओ, आईआईटी खड़गपुर और जीआईएम, गोवा में प्रोफ़ेसर हैं. वह एक लेखक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता भी हैं. यह लेख द वायर में प्रकाशित हुआ. उसके प्रमुख अंश.
बिहार चुनाव के नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सत्ता की हर संभव ताकत का इस्तेमाल करने के बाद चुनावों में भारी जीत हासिल की – चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से लेकर, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद नीतीश कुमार द्वारा महिला मतदाताओं को खुलेआम अवैध तरीके से 10,000 रुपये हस्तांतरित करने तक. इस बीच, विपक्ष “वोट चोरी” और प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी जैसे अस्पष्ट वादों के नारों पर चुनाव लड़ रहा था. पिछले एक दशक के लगभग हर चुनाव की तरह, यह मुक़ाबला किसी भी लिहाज़ से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था.
फिर भी, ज़्यादा गंभीर सवाल यह है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, ने यह कैसे समझा कि वह किसके खिलाफ़ है. उसने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वह अपने विरोधी की प्रकृति या हो रहे राजनीतिक बदलाव के पैमाने को पहचानती है. अपनी “हमेशा की तरह काम करने” वाली जड़ता में फँसी कांग्रेस ने उसी पटकथा को दोहराया जिसने उसे लगातार हार दिलाई है.
निराशाजनक बात सिर्फ़ विपक्ष का पंगु होना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, नीति विश्लेषकों और राजनीतिक टिप्पणीकारों की विफलता भी है. ऐसे समय में जब मुख्यधारा का मीडिया बड़े पैमाने पर सत्ताधारी पार्टी के भोंपू के रूप में काम करता है, स्वतंत्र विचारकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. इसके बजाय, संपादकीय पन्नों, यूट्यूब चैनलों, अकादमिक मंचों और नागरिक समाज के दायरों में की गई टिप्पणियों ने एक गहरी बीमारी को उजागर किया: सच्चाई का सामना करने से इनकार.
वही घिसे-पिटे जुमले फिर से सामने आए – एंटी-इनकंबेंसी, जातिगत समीकरण और आखिरी मिनट की “लहरों” के कर्मकांडी संदर्भ – मानो भारत अभी भी एक सामान्य लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर काम कर रहा हो. उनके विश्लेषण सतही, रणनीतिक रूप से खोखले और उन ढाँचागत बदलावों से अनभिज्ञ बने हुए हैं, जिन्होंने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया है. संस्थाओं का सुनियोजित क्षरण, संवैधानिक उल्लंघनों का पैमाना और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों का ढहना उनके विश्लेषण के ढाँचे में शायद ही कहीं नज़र आता है.
क्या बिहार अप्रत्याशित था?
2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता खोने के कगार पर पहुँचने के बाद, बीजेपी ने अपनी पसंदीदा रणनीति, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर किसी भी तरह की निर्भरता को छोड़ दिया और इसके बजाय चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए कठोर, व्यवस्थागत हेरफेर की ओर रुख किया. यह 2024 के बाद के हर विधानसभा चुनाव - हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पष्ट था. उसने झारखंड को छोड़कर सभी चुनाव जीते, जो एक अकेला अपवाद है और जो आसानी से उसके कार्यकर्ताओं के “व्हाट-अबाउटरी” (दूसरों पर उंगली उठाने की आदत) को बनाए रखता है और जनता के सामने संस्थागत वैधता का भ्रम बनाए रखने में मदद करता है.
इनमें से तीन राज्यों में, विपक्ष की हार चुनावी सूचियों में हेरफेर के दस्तावेजी सबूतों के साथ मेल खाती है – यह एक ऐसा काम है जो चुनाव आयोग की सक्रिय मिलीभगत के बिना असंभव है. चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया उस तरह से पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ, जिस तरह से उसने विपक्षी नेताओं के ज्ञापनों को खारिज कर दिया.
यह पैटर्न बिहार में और भी सख़्त हो गया. चुनाव आयोग द्वारा विवादास्पद ‘एसआईआर’ पर ज़ोर देना, जिसे एक अपारदर्शी कार्यप्रणाली और स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण इरादे से अंजाम दिया गया, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि बीजेपी ने एक भी वोट डाले जाने से बहुत पहले ही परिणाम लिखने का इरादा कर लिया था. एक स्कूली बच्चा भी समझता है कि अगर रेफ़री ही दुश्मन बन जाए, तो मैच नहीं जीता जा सकता. इसे विपक्ष को यह समझने के लिए झकझोर देना चाहिए था कि एक समान राजनीतिक प्रतिक्रिया की ज़रूरत है – जिसमें उस चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प भी शामिल है जिसकी ईमानदारी पहले ही खत्म कर दी गई थी.
इसलिए, बिहार का फ़ैसला कोई रहस्यमयी राजनीतिक आश्चर्य नहीं था. यह उस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम था जो सबके सामने घटित हो रही थी. फिर भी विपक्ष और टिप्पणीकारों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी मौलिक नहीं बदला हो. उनके आचरण ने मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया कि मुक़ाबला अभी भी खुला है, संस्थाएँ तटस्थ हैं, और चुनावी लोकतंत्र की परिचित लय अभी भी लागू होती है. यह भोलापन नहीं था; यह ज़िम्मेदारी से मुँह मोड़ना था. एक ढाँचागत रूप से धांधली वाले मुक़ाबले को “हमेशा की तरह” मानने पर ज़ोर देकर, उन्होंने इसे पवित्र बनाने में मदद की.
संपादकीय, पैनल चर्चाओं और संपादकीय उपदेशों में, वही थके हुए आश्वासन दोहराए गए: कि भारतीय चुनाव प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं, कि व्यवस्था में अभी भी आंतरिक सुधार की गुंजाइश है, और यह कि सत्ताधारी दल को सामान्य राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से रोका जा सकता है. यदि कोई केवल इस व्याख्याकार वर्ग पर भरोसा करे, तो कोई भारत को एक क्रियाशील लोकतंत्र समझ सकता है, न कि एक ऐसा राज्य जिसमें नाटकीय ढाँचागत परिवर्तन हुए हैं.
चुनावी मैदान अब समान नहीं रहा; निगरानी करने वाली संस्थाओं को अनुपालन के लिए झुका दिया गया है; और कार्यपालिका की शक्ति बिना किसी वास्तविक बाधा के काम करती है. इसमें से कुछ भी छिपा नहीं है. जो छिपा है – जानबूझकर – वह है इस वास्तविकता की स्वीकृति उन लोगों द्वारा जो सत्ता से सच बोलने का दावा करते हैं.
विपक्ष का अंधापन हानिकारक है, लेकिन बुद्धिजीवियों और टिप्पणीकारों का बचना इससे भी बदतर है. उनकी भूमिका केवल विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण को उजागर करना है. इसके बजाय, उन्होंने इस कल्पना की रक्षा करना चुना है कि मतदाताओं के बेहतर व्यवहार या अधिक अनुशासित विपक्ष के माध्यम से व्यवस्था को सुधारा जा सकता है. यह नैरेटिव न केवल भ्रामक है; यह मिलीभगत वाला है. यह लोगों को आश्वस्त करता है कि वे अभी भी एक परिचित राजनीतिक दुनिया में रहते हैं, जबकि वास्तव में, उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है.
गणतंत्र के ढाँचागत क्षय का सामना करने से इनकार करके, विपक्ष और टिप्पणीकारों ने उन प्रक्रियाओं को ही वैधता प्रदान की जो इसे खोखला कर रही थीं. बिहार अप्रत्याशित नहीं था. जो अनुमानित – और दुखद – था, वह था प्रतिष्ठान का यह दृढ़ संकल्प कि वह ऐसा अभिनय करे जैसे कुछ भी नहीं बदला हो, भले ही लोकतांत्रिक मुखौटा सबके सामने ढह रहा हो.
बीजेपी के किलेबंदी की प्रक्रिया
अगर विपक्ष ने अपनी संवैधानिक भूमिका निभाई होती, और अगर बौद्धिक और मीडिया टिप्पणीकारों ने अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी का एक अंश भी निभाया होता, तो चल रहे संस्थागत क्षय को रोका जा सकता था. इसके बजाय, वे पूरी तरह से विफल रहे – जिससे बीजेपी को बिना किसी सार्थक प्रतिरोध के कदम-दर-कदम अपनी शक्ति को मज़बूत करने का मौका मिला.
वित्तीय इंजीनियरिंग और चुनावी बॉन्ड : सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 2017-18 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के साथ आया. पारदर्शिता सुधार के रूप में प्रचारित इस योजना ने अपारदर्शिता को संस्थागत बना दिया और राजनीतिक वित्तपोषण को निर्णायक रूप से सत्ताधारी दल की ओर झुका दिया. कॉरपोरेट दानदाता – जो लाइसेंस, मंज़ूरी और सरकारी अनुबंधों पर निर्भर हैं – गुमनाम रूप से दान कर सकते थे, जिससे लेन-देन की व्यवस्था को सार्वजनिक जाँच से प्रभावी ढंग से बचाया जा सके.
एडीआर और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के अध्ययनों से पता चला कि बीजेपी ने बॉन्ड से जुड़े दान का भारी बहुमत हासिल किया. इस भारी-भरकम फंड का इस्तेमाल बेजोड़ विज्ञापन, अभियान रसद, डिजिटल पहुँच और संगठनात्मक पैठ में किया गया. पैसा एक हथियार बन गया – अकेले इसके पैमाने ने यह सुनिश्चित किया कि बीजेपी राजनीतिक बाज़ार पर हावी हो सके और विपक्षी अभियानों को डुबो सके.
नौकरशाही और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्रीकरण : सत्ता में आने पर, बीजेपी ने प्रशासनिक तंत्र को नया आकार देने के लिए तेज़ी से कदम उठाए. मोदी के गुजरात शासन के नौकरशाहों को दिल्ली भर में प्रमुख पदों पर रखा गया, जिससे दीर्घकालिक वफ़ादारी सुनिश्चित हुई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालयों, नियामक निकायों, सांस्कृतिक संस्थानों और अनुसंधान परिषदों में स्थापित किया गया.
“लैटरल एंट्री” की शुरुआत ने इस प्रभाव को और बढ़ाया, जिसमें चुने हुए टेक्नोक्रेट्स – कई वैचारिक रूप से गठबंधन में – को महत्वपूर्ण नीति और नियामक भूमिकाओं में रखा गया. समानांतर रूप से, सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, जो न्यायपालिका को अधीन करने की इच्छा का संकेत था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन कार्यपालिका ने अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया – नियुक्तियों में देरी, चयनात्मक पदोन्नति और तबादले – दबाव बनाने के लिए. इसका कुल प्रभाव यह हुआ है कि नौकरशाही और न्यायिक प्रणाली कार्यपालिका को चुनौती देने में हिचकिचाती है.
जांच एजेंसियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, आयकर विभाग और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को राजनीतिक अनुशासन के उपकरणों के रूप में तैनात किया गया है. विपक्षी नेताओं के खिलाफ़ ईडी के मामलों में विस्फोट – जिनमें से 90% से ज़्यादा प्रतिद्वंद्वी दलों के हैं – अपने आप में बहुत कुछ कहता है. जांच बिना किसी दोषसिद्धि के वर्षों तक चलती है; प्रक्रिया ही सज़ा है. छापे चुनाव, गठबंधन बनाने के प्रयासों और आंतरिक पार्टी संकटों के साथ मेल खाते हैं. यह सर्वव्यापी खतरा विपक्षी दलों को पंगु बना देता है, नेताओं को चुप्पी, समझौते या दलबदल के लिए मजबूर करता है.
डिजिटल प्रचार और मीडिया पर कब्ज़ा : भारत में किसी भी पार्टी ने डिजिटल क्षेत्र का इतना आक्रामक इस्तेमाल नहीं किया है जितना बीजेपी ने किया है. इसका आईटी सेल एक पेशेवर, डेटा-संचालित प्रभाव तंत्र के रूप में काम करता है जो सहमति गढ़ने, आक्रोश को निर्देशित करने और बड़े पैमाने पर विरोधियों को बदनाम करने में सक्षम है. मुख्यधारा का मीडिया, जो तेजी से कॉर्पोरेट स्वामित्व वाला और सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर है, भी इसका अनुसरण करता है. असहमति की आवाज़ों को हाशिए पर डाल दिया जाता है, खोजी पत्रकारिता का गला घोंट दिया जाता है, और सार्वजनिक बहस सत्ताधारी दल के नैरेटिव से भर जाती है. धारणा पर नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना संस्थाओं पर नियंत्रण.
नीति आयोग के माध्यम से आर्थिक केंद्रीकरण : योजना आयोग को भंग करने और नीति आयोग के निर्माण ने आर्थिक शासन को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधीन कर दिया. इस नए निकाय में संघीय जाँच का अभाव है, जिससे केंद्र रणनीतिक रूप से धन पहुंचाकर राजनीतिक रूप से वफ़ादार राज्यों को पुरस्कृत कर सकता है, जबकि विपक्ष-शासित राज्यों को कमज़ोर कर सकता है. आर्थिक शक्ति का यह केंद्रीकरण राजनीतिक मज़बूती को और बढ़ाता है और संघवाद को कमज़ोर करता है.
हिंदुत्व की वैचारिक पकड़ को मज़बूत करना : बीजेपी ने सफलतापूर्वक अपने सामाजिक आधार को उच्च-जाति के समर्थन से आगे बढ़ाया है, और ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के बीच गहरी पैठ बनाई है. यह पुनर्संरेखण धार्मिक राष्ट्रवाद, लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और मोदी को एक वंचित वर्ग के नेता के रूप में पेश करने के मिश्रण के माध्यम से हासिल किया गया. साथ ही, सांस्कृतिक संस्थानों, स्कूल पाठ्यक्रम, विरासत की राजनीति और धार्मिक प्रतीकों में निवेश यह सुनिश्चित करता है कि हिंदुत्व सामाजिक ताने-बाने में समा जाए. चुनावी चक्र आते-जाते रहते हैं, लेकिन वैचारिक सामान्यीकरण बना रहता है.
पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी : आरटीआई अधिनियम को कमज़ोर करने और सूचना आयोग को अधीन करने से नागरिकों की राज्य के कार्यों की जाँच करने की क्षमता कम हो गई है. यह अपारदर्शिता राजनीतिक संरक्षण नेटवर्क की सहायता करती है, वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों को बचाती है, और सत्ताधारी दल को लोकतांत्रिक निगरानी से बचाती है. गोपनीयता की संस्कृति शासन की एक ढाँचागत विशेषता बन जाती है.
राज्य-स्तरीय राजनीतिक इंजीनियरिंग : बीजेपी की आक्रामक दलबदल की राजनीति – जिसे “ऑपरेशन कमल” के नाम से जाना जाता है – ने कई विपक्षी सरकारों को गिराया या अस्थिर किया है. ये ऑपरेशन प्रलोभन, एजेंसियों के दबाव और रणनीतिक समय के माध्यम से संभव होते हैं. संदेश स्पष्ट है: राज्य स्तर पर चुनावी परिणाम सशर्त, प्रतिवर्ती और केंद्रीय इंजीनियरिंग के अधीन हैं.
चुनाव आयोग पर कब्ज़ा : चुनाव आयोग, जो कभी एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुरक्षा कवच था, को उत्तरोत्तर कमज़ोर किया गया है. सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा आचार संहिता के घोर उल्लंघनों के खिलाफ़ कार्रवाई करने में इसकी अनिच्छा और विपक्षी हस्तियों के खिलाफ़ शिकायतों पर कार्रवाई करने में इसकी तत्परता इस परिवर्तन को दर्शाती है. नियुक्ति पैनल पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को लाने वाले संशोधन ने प्रभावी रूप से नियुक्तियों पर कुल नियंत्रण प्रधानमंत्री को सौंप दिया. संस्थागत कब्जे से पहले से ही तनावग्रस्त व्यवस्था में, एक समझौतावादी चुनाव आयोग चुनावी ईमानदारी के दिल पर हमला करता है. बल्कि, यह लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी बजाने जैसा है.
विपक्ष की अपर्याप्त और भ्रामक प्रतिक्रियाएँ
जबकि बीजेपी एक दुर्जेय राजनीतिक मशीन का निर्माण कर रही थी, विपक्ष आत्मसंतुष्ट, खंडित और रणनीतिक रूप से दिशाहीन बना रहा. उनकी विफलता सामयिक नहीं बल्कि ढाँचागत है.
खंडित और प्रतिक्रियावादी राजनीति : विपक्षी दल घटनाओं को आकार देने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करते हैं. वे तब प्रतिक्रिया करते हैं जब बीजेपी पहले ही राजनीतिक परिदृश्य को बदल चुकी होती है – चाहे वह चुनावी बॉन्ड, संस्थागत कब्ज़ा, या संघीय अतिक्रमण पर हो. जब तक वे विरोध करते हैं, तब तक बीजेपी को फायदा मिल चुका होता है.
अदालतों पर अत्यधिक निर्भरता : निरंतर लामबंदी के बजाय, विपक्ष ने हर बड़े राजनीतिक मुद्दे – ईडी के उत्पीड़न से लेकर चुनावी बॉन्ड तक – को अदालतों में ले जाया है. लेकिन जिस संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र पर वे भरोसा करते हैं, वह पहले ही समझौता कर चुका है. न्यायिक हस्तक्षेप, जब वे आते हैं, तो वे देरी से, आंशिक या अप्रभावी होते हैं. याचिकाओं के माध्यम से की जाने वाली राजनीति, जन लामबंदी के बजाय, लोकतंत्र को कमज़ोर करती है.
नाममात्र की एकता और लगातार अविश्वास : यूपीए या इंडिया जैसे गुट ज़मीन से ज़्यादा कागज़ों पर मौजूद हैं. सीटों के बँटवारे के झगड़े, आपसी संदेह और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता समन्वित अभियानों को रोकते हैं. बीजेपी लक्षित दलबदल रणनीतियों और क्षेत्र-विशिष्ट कल्याणकारी लोकलुभावनवाद के माध्यम से इसका फायदा उठाती है.
हिंदुत्व का सामना करने में विफलता : विपक्ष की सबसे गंभीर विफलता वैचारिक है. एक स्पष्ट संवैधानिक प्रति-दृष्टि की पेशकश करने के बजाय, विपक्षी दलों ने नरम-हिंदुत्व का रुख अपनाया है. इसने केवल बीजेपी के मैदान को वैध बनाया. बहुसंख्यकवाद का सीधे सामना करने से इनकार करते हुए, उन्होंने वैचारिक युद्धक्षेत्र खाली कर दिया है.
संगठनात्मक खोखलापन : बीजेपी-आरएसएस का गठजोड़ एक अनुशासित, कैडर-आधारित मशीन है. इसके विपरीत, कांग्रेस संगठनात्मक रूप से खोखली है, जो कुछ नेताओं और चुनाव के समय के अभियानों पर निर्भर है. क्षेत्रीय दल परिवार-केंद्रित बने हुए हैं और उनमें वैचारिक आधार की कमी है. ज़मीनी स्तर पर कोई उपस्थिति न होने के कारण, विपक्ष बूथ-स्तर की लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाता है.
जांच एजेंसी के दुरुपयोग पर कमज़ोर प्रतिक्रिया : विपक्षी नेता छापों की निंदा करते हैं, लेकिन लक्षित होने के बाद अक्सर चुप हो जाते हैं. कुछ चुपचाप सौदे कर लेते हैं; अन्य राजनीतिक गतिविधि से पीछे हट जाते हैं. नेताओं की रक्षा करने या एजेंसी की ज्यादती के खिलाफ़ समर्थकों को जुटाने के लिए कोई सामूहिक रक्षा रणनीति, कानूनी टीम या संगठनात्मक तंत्र मौजूद नहीं है.
नैरेटिव पर प्रभुत्व का मुकाबला करने में असमर्थता : विपक्ष का संचार अव्यवसायिक है. कोई समन्वित डिजिटल उपस्थिति नहीं है, कोई डेटा-संचालित रणनीति नहीं है, कोई एकीकृत संदेश नहीं है. मीडिया के पूर्वाग्रह के बारे में शिकायतें खोखली लगती हैं जब वे वैकल्पिक मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र या स्थायी संचार बुनियादी ढाँचे में निवेश करने में विफल रहे हैं.
दलबदल की राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं : विपक्ष की आंतरिक अस्थिरता दलबदल को आसान बनाती है. वैचारिक सामंजस्य या आंतरिक लोकतंत्र के बिना, पार्टियाँ अवसरवादी नेताओं को नहीं रोक सकतीं. बीजेपी का “ऑपरेशन कमल” इसी कमज़ोरी पर फलता-फूलता है.
सामाजिक गठबंधनों को फिर से बनाने में विफलता: जबकि बीजेपी ने सफलतापूर्वक ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को लुभाया, विपक्ष पुराने जातिगत फ़ार्मूलों और प्रतीकात्मक इशारों से चिपका रहा. वे सामाजिक न्याय का एक नया ढाँचा तैयार करने में विफल रहे जो समकालीन आकांक्षाओं और असुरक्षाओं का जवाब देता.
कमज़ोर संघीय प्रतिरोध : संघीय मानदंडों पर बार-बार के हमलों के बावजूद – धन रोकने, राज्यपाल के हस्तक्षेप और दंडात्मक एजेंसियों के माध्यम से – विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों ने एक संयुक्त संघीय गुट नहीं बनाया है. बीजेपी का केंद्रीकरण का एजेंडा निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है.
राहुल गांधी की विफलता
राहुल गांधी ने निश्चित रूप से एक लंबा सफ़र तय किया है – अपना जनेऊ और भगवा वस्त्र दिखाकर खुद को एक हिंदू भक्त के रूप में प्रस्तुत करने के दिनों से लेकर, अब खुद को जनता के आदमी के रूप में पेश करने तक. लेकिन उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति अभी भी मोदी के साथ व्यक्तिगत मुकाबले पर एक गलत निर्भरता को दर्शाती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीतिक कला आरएसएस स्कूल में गढ़ी गई है. यदि राहुल गांधी ने कमजोरियों का एक ईमानदार विश्लेषण किया होता, तो उन्होंने इस दृष्टिकोण की निरर्थकता को देख लिया होता. उनका असली काम कांग्रेस संगठन को उसकी कमज़ोर स्थिति से फिर से बनाना और विपक्षी दलों के बीच स्थायी एकता बनाना था. दोनों मोर्चों पर उनकी विफलता ने देश को भारी कीमत चुकाई है.
एक व्यवस्थागत संकट और नींद में चलता विपक्ष : बीजेपी का राजनीतिक प्रभुत्व रहस्यमय नहीं है; यह एक दशक लंबी संस्थागत, वैचारिक, वित्तीय और संगठनात्मक मज़बूती की परियोजना का उत्पाद है. जो आश्चर्यजनक है, वह है विपक्ष का राजनीति को चुनाव, नारे और गठबंधनों से परे फिर से सोचने से इनकार करना. वे यह पहचानने में विफल रहे हैं कि वे एक केंद्रीकृत, दमनकारी, डेटा-संचालित, वित्तीय रूप से बेजोड़ राजनीतिक मशीन का सामना कर रहे हैं, जिसे एक विशाल वैचारिक नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है.
भारत स्थायी तानाशाही शासन की ओर बढ़ रहा है, फिर भी विपक्ष आधे-अधूरे गठबंधनों, अदालती याचिकाओं और मीडिया साउंडबाइट्स के साथ प्रतिक्रिया करता है. इस बीच, राजनीतिक टिप्पणीकार उन घिसे-पिटे जुमलों को दोहराते हैं जो संकट को उजागर करने के बजाय अस्पष्ट करते हैं.
बीजेपी का प्रभुत्व न केवल अपनी रणनीति के कारण बना हुआ है, बल्कि इसलिए भी कि विपक्ष ने राजनीति को एक जन, वैचारिक और संगठनात्मक परियोजना के रूप में त्याग दिया है. जब तक वे इस वास्तविकता का सामना नहीं करते, बिहार जैसी हार जारी रहेगी – पहले से बताई गई, टाली जा सकने वाली, और फिर भी अपरिहार्य.
बिहार चुनाव इस बात की पुष्टि करता है कि भविष्य में बीजेपी तब तक कोई चुनाव नहीं हारेगी, जब तक वह खुद हारना न चाहे.
हरकारा डीपडाइव
श्रवण गर्ग : बिहार चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ़ एक ‘पोखरण’ था, और हम सब सोते रह गए
बिहार चुनाव के नतीजों की धूल अब छंट चुकी है, लेकिन इस धूल के नीचे जो तस्वीर दबी है, वह सिर्फ़ राजनीतिक हार-जीत की नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सुनियोजित क्षरण की है. वरिष्ठ पत्रकार और विचारक श्रवण गर्ग इसे भारत के लोकतंत्र के खिलाफ़ एक ‘पोखरण’ की संज्ञा देते हैं - एक ऐसा गुप्त और प्रभावशाली ऑपरेशन, जिसने व्यवस्था की नींव हिला दी है, और हमें ख़बर तक नहीं हुई.
हरकारा डीप डाइव में निधीश त्यागी के साथ बातचीत में, श्रवण गर्ग ने उस ख़तरे की घंटी बजाई, जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया का शोर दबा रहा है. उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे देश में चुनाव हो रहे हैं, हम पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टीट्यूशनली कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, हम ख़त्म हो रहे हैं.”
पोखरण से तुलना क्यों? गर्ग बताते हैं कि जैसे 1974 में इंदिरा गांधी ने दुनिया को बिना भनक लगे पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया था, ठीक उसी तरह बिहार में चुनाव आयोग के ‘वॉर रूम’ से लोकतंत्र के खिलाफ़ एक परीक्षण किया गया है. यह परीक्षण सफल रहा है और अब इसके हथियार बनाकर दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया जाएगा. इस परीक्षण ने भारत को रूस, चीन और हंगरी जैसे निरंकुश देशों की कतार में एक कदम और क़रीब ला दिया है.
‘हिंदू राष्ट्र’ एक ध्यान भटकाने वाला मुद्दा इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने की बहस एक छलावा है. असली मक़सद भारत को एक निरंकुश (Autocratic) राष्ट्र बनाना है. एक बार जब देश पूरी तरह निरंकुश हो जाएगा, तो उसे ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित करना महज़ एक मिनट की औपचारिकता होगी. इसलिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, वे उस बड़े ख़तरे को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, जो दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है.
विपक्ष की सबसे बड़ी ग़लती श्रवण गर्ग विपक्ष की रणनीति पर भी तीखा प्रहार करते हैं. उनका मानना है कि विपक्ष एक पहाड़ चढ़ने वाले उस व्यक्ति की तरह है, जो ऊपर देखने के बजाय बार-बार पीछे खाई में देख रहा है. वह कहते हैं, “हम पीछे की चोरी को पकड़ रहे हैं और आगे की चोरी रोक नहीं रहे हैं.” राहुल गांधी का ‘हाइड्रोजन बम’ हरियाणा के पुराने चुनावों के डेटा पर आधारित था, लेकिन उनकी आंखों के सामने बिहार लुट गया और वे कुछ नहीं कर पाए. अब वे बिहार की रिपोर्ट तैयार करेंगे और तब तक बंगाल, केरल और असम भी निपट जाएंगे.
शेख़ हसीना को सज़ा ए मौत , भारत से बांग्लादेश ने सौंपने की मांग, ढाका में हाई अलर्ट
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल) ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई. उन्हें पिछले वर्ष के छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध किए गए कथित अपराधों का दोषी पाया गया, जिसके कारण उनकी अवामी लीग सरकार का पतन हुआ था. तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने हसीना के दो सहयोगियों — पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून — के खिलाफ भी इन्हीं आरोपों पर फैसला सुनाया. “अल जज़ीरा” के मुताबिक, न्यायाधिकरण ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के इस्तेमाल में शामिल होने के लिए पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी मौत की सज़ा सुनाई. इसी के साथ बांग्लादेश ने मांग की है कि भारत को हसीना और खान को “तत्काल उसे सौंप देना” चाहिए. हसीना को न्याय को बाधित करने, प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश देने और दंडात्मक हत्याओं को रोकने के लिए उपाय करने में विफल रहने के “तीन मामलों में दोषी पाया गया.”
“द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” की ऑनलाइन डेस्क के मुताबिक, न्यायाधीश गुलाम मुर्तज़ा मजूमदार ने ढाका में खचाखच भरे न्यायालय में पढ़कर सुनाया, “हमने उन्हें केवल एक ही सज़ा देने का फैसला किया है — वह है, मौत की सज़ा.” हालांकि, न्यायाधिकरण ने अल-मामून को मौत की सज़ा से बख्श दिया, क्योंकि वह सरकारी गवाह बन गए थे.
न्यायाधिकरण के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और घातक हथियारों के उपयोग का आदेश दिया था, जिसका खुलासा दक्षिण ढाका नगर निगम के महापौर के साथ उनकी बातचीत में हुआ था. फोरेंसिक जांच में सीडी और रिकॉर्डिंग को प्रामाणिक माना गया. न्यायाधिकरण ने यह भी टिप्पणी की कि हसीना ने विरोध कर रहे छात्रों की हत्या का आदेश दिया था, और इस बात पर ध्यान दिया कि ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ उनकी बातचीत के रिकॉर्ड उपलब्ध थे. न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि हसीना ने नफरत भरे भाषण दिए और शकील नामक एक सहयोगी के साथ फोन पर बातचीत में उससे उन 226 लोगों को मारने के लिए कहा जिनके नाम उनके खिलाफ दायर मामलों से जुड़े थे. कुल मिलाकर, पाँच में से दो मामलों (हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने) में उन्हें मौत की सज़ा, वहीं बाकी में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. अदालत ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फाँसी की सज़ा सुनाई.
याद रहे, शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद देश छोड़ दिया था. विगत 15 महीनों से दोनों नेता भारत में पनाह लेकर रह रहे हैं. इस बीच “द हिंदू” के अनुसार, फैसले के मद्देनज़र पूरे ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के आसपास सेना, पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है. हसीना की पार्टी, बांग्लादेश अवामी लीग द्वारा बुलाए गए दो दिवसीय लॉकडाउन के दौरान देश के कई हिस्सों में अशांति फैल गई. कुछ जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाले और कच्चे बम भी फेंके गए.
सऊदी में उमराह करने गए यात्रियों के साथ बड़ा हादसा, बस में लगी आग, 45 भारतीयों की मौत
सऊदी अरब में उमराह के लिए जा रहे यात्रियों को ले जा रही एक बस टैंकर लॉरी से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई, जिसमें 20 महिलाओं और 11 बच्चों सहित 45 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई. आव्रजन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ज्यादातर मृतक हैदराबाद शहर के थे. बताया गया है कि 46 यात्रियों को ले जा रही इस बस में केवल एक व्यक्ति जीवित बचा है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है.
यह दुर्घटना कथित तौर पर बद्र और मदीना के बीच मुफ़रहाथ क्षेत्र में एक चौड़ी और तेज़ रफ़्तार वाली सड़क पर भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30 बजे हुई. जिस समय हादसा हुआ, उस वक्त बस में सवार अधिकतर यात्री सो रहे थे.
“द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने बताया कि 9 नवंबर को कुल 54 लोग हैदराबाद से जेद्दा के लिए रवाना हुए थे. उन्हें 23 नवंबर को वापस लौटना था. 54 लोगों में से चार लोग रविवार को अलग से कार से मदीना गए थे, जबकि अन्य चार मक्का में ही रुक गए थे
रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर ‘कठोर प्रतिबंध’ लगेगा, एक्ट की तैयारी: ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि जो भी देश रूस के साथ व्यापार करेगा, उस पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे. उनका कहना है कि उनकी सरकार और रिपब्लिकन नेता रूस के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं.
“पीटीआई” के मुताबिक रविवार को पत्रकारों ने ट्रम्प से पूछा कि क्या अब कांग्रेस को रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए नया कानून पास कर देना चाहिए. इस पर ट्रम्प ने कहा, “मैं सुन रहा हूं कि वे ऐसा कर रहे हैं, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है.”
ट्रम्प ने आगे कहा, “रिपब्लिकन नए कानून ला रहे हैं… रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे. वे इस सूची में ईरान को भी जोड़ सकते हैं… यह सुझाव मैंने ही दिया था.”
उन्होंने दोहराया, “रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बहुत कठोर कार्रवाई होगी. हम ईरान को भी इसमें शामिल कर सकते हैं.” ट्रम्प प्रशासन ने रूस की ऊर्जा खरीद पर 25% शुल्क लगाया है और भारत पर कुल 50% शुल्क लगाया गया है—जो दुनिया के सबसे ऊँचे शुल्कों में से एक है.
इसी बीच, सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक विधेयक पेश किया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद और पुनर्विक्रय पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है. इस प्रस्ताव को सीनेट की विदेश संबंध समिति से लगभग सर्वसम्मत समर्थन मिला है.
ग्राहम और सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर ‘रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025’ पेश किया है. इस कानून का मकसद उन देशों पर भारी टैरिफ और प्रतिबंध लगाना है, जो रूस को तेल और गैस खरीदकर पैसा दे रहे हैं और यूक्रेन में चल रहे पुतिन के युद्ध को ताकत पहुँचा रहे हैं. इस प्रस्ताव को सीनेट में 85 सांसदों का समर्थन मिला है.
जुलाई में जारी एक संयुक्त बयान में ग्राहम और ब्लूमेंथल ने कहा था, “राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी टीम रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया और कड़ा कदम उठा रहे हैं… लेकिन इस युद्ध को रोकने का असली दबाव तो चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर ही बनेगा, क्योंकि ये देश सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को मदद पहुंचा रहे हैं.
आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला को फिर सज़ा, 7 साल की जेल, 2 माह पहले ही छूटे थे
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के जेल से बाहर आने के लगभग दो महीने बाद, रामपुर की एक अदालत ने आज सोमवार को उन्हें और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान को दो पैनकार्ड से जुड़े जालसाजी के एक मामले में सात साल कैद की सज़ा सुनाई. अदालत ने दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया. अब्दुल्ला इस मामले में ज़मानत पर बाहर थे.
“द इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, सोमवार सुबह, अदालत ने आज़म और उनके बेटे को दोषी ठहराया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. अभियोजन (रामपुर) के संयुक्त निदेशक, रोहताश कुमार पांडे ने कहा, “उन पर जुर्माना भी लगाया है. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. अदालत ने इस मामले में अभियोजन के नौ और बचाव पक्ष के 18 गवाहों की जांच की. आज़म के वकील नासिर सुल्तान ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे.
बता दें, इस साल 23 सितंबर को, आज़म को लगभग दो साल हिरासत में बिताने के बाद ज़मानत पर सीतापुर जेल से रिहा किया गया था. रामपुर सदर से 10 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान को सपा के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक माना जाता है और वह लंबे समय से पार्टी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं. उनकी कानूनी मुश्किलें 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले उनके खिलाफ दर्ज एक हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले से शुरू हुईं — जो उनके खिलाफ शुरू किए गए पहले मामलों में से एक था. यूपी पुलिस रिकॉर्ड आगे दिखाते हैं कि 2017 में यूपी में भाजपा के सत्ता में आने के बाद आज़म के खिलाफ इनमें से 81 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे. वर्तमान मामले सहित, आज़म को सात मामलों में दोषी ठहराया गया है — रामपुर में छह और मुरादाबाद में एक. उन्होंने इन सभी दोषसिद्धियों के खिलाफ अपील दायर की है और उनमें से छह में ज़मानत हासिल कर ली है. इसके अलावा, खान को छह अन्य मामलों में बरी कर दिया गया है. हालांकि, राज्य सरकार ने इनमें से कुछ के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील की है, और अपीलें लंबित हैं.
असम में मतदाता सूचियों के “एसआर” का आदेश, ‘एसआईआर’ का नहीं
चुनाव आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूचियों के ‘विशेष पुनरीक्षण’ (एसआर) का आदेश दिया, जिससे अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मंच तैयार हो गया है.
“द टेलीग्राफ” के मुताबिक, चुनाव आयोग द्वारा असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 राज्य के लिए विशेष पुनरीक्षण करने की योग्यता तिथि होगी. अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूचियों के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच में आता है. ज्ञात रहे कि पिछले महीने, चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का आदेश दिया था. इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे. असम के “एसआईआर” की घोषणा अलग से की जाएगी.
मनरेगा: 27 लाख मजदूरों के नाम हटाए
केंद्र सरकार की ग्रामीण रोज़गार योजना, मनरेगा के डेटाबेस से इस साल 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच लगभग 27 लाख मज़दूरों के नाम हटा दिए गए. “द हिंदू” की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह संख्या इसी अवधि में जोड़े गए 10.5 लाख नए नामों से कहीं ज़्यादा है. नामों को हटाने में यह तेज़ी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार अयोग्य लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए सभी श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पर ज़ोर दे रही है.
कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों के एक संघ “लिब टेक” ने मनरेगा डेटाबेस से नाम हटाने की इस “असामान्य” दर पर चिंता जताई है. विश्लेषण के अनुसार, पिछले छह महीनों में लगभग 15 लाख नाम हटाए गए थे. लेकिन सिर्फ एक महीने में यह आंकड़ा बढ़कर 27 लाख हो गया, जो पिछले छह महीने के कुल आंकड़े का लगभग दोगुना है.
“लिब टेक” के विश्लेषण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले छह महीनों में, योजना में कुल 83.6 लाख मज़दूर शुद्ध रूप से जोड़े गए थे. लेकिन नवंबर के मध्य तक, यह संख्या घटकर 66.5 लाख रह गई, जिससे एक महीने में प्रभावी रूप से 17 लाख मज़दूर कम हो गए. विश्लेषण में यह भी पाया गया कि हटाए गए लाभार्थियों में से 6 लाख सक्रिय मज़दूर थे, यानी वे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक दिन काम किया था.
जिन राज्यों में ई-केवाईसी पूरा करने की दर ज़्यादा है, वे नाम हटाने में सबसे आगे हैं. आंध्रप्रदेश, जहां 78.4% श्रमिकों ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, में 15.92 लाख नाम हटाए गए. तमिलनाडु (67.6%) में 30,529 और छत्तीसगढ़ (66.6%) में 1.04 लाख नाम हटाए गए.
हालांकि, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने ई-केवाईसी अभियान और हटाए गए नामों के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मनरेगा जॉब कार्ड का सत्यापन एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों की है.
सरकार ने ई-केवाईसी को सत्यापन की एक अतिरिक्त परत के रूप में इसलिए पेश किया क्योंकि यह पाया गया था कि एनएमएमएस (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम) प्लेटफॉर्म का “दुरुपयोग” हो रहा था. मंत्रालय ने पाया था कि श्रमिकों की जियो-टैग की गई तस्वीरों के बजाय “अप्रासंगिक या असंबंधित तस्वीरें” अपलोड की जा रही थीं.
“लिब टेक” के एक वरिष्ठ शोधकर्ता चक्रधर बुद्ध ने कहा, “नाम हटाने का मौजूदा पैटर्न आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को लागू करने जैसा ही है, जिसमें 2021-22 और 2022-23 के बीच हटाए गए नामों में 247% की वृद्धि देखी गई थी.” उन्होंने कहा, “जब भी आधार से जुड़ी कोई नई तकनीक पेश की जाती है—चाहे वह एबीपीएस हो या अब ई-केवाईसी—इसे सत्यापन को मज़बूत करने के लिए लाया जाता है, लेकिन यह वास्तविक मज़दूरों के लिए नई बाधाएं पैदा कर देता है और बड़े पैमाने पर उन्हें योजना से बाहर कर देता है.”
विश्लेषण
आकार पटेल: तमाम सूचकांकों पर नीचे की ओर खिसकता ‘न्यू इंडिया’
लेखक पत्रकार, स्तंभकार और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के प्रमुख हैं.
कुछ साल पहले, नीति आयोग ने कहा था कि वह उन सभी 29 (बाद में 32) वैश्विक सूचकांकों के लिए एक ‘सिंगल, जानकारी भरा डैशबोर्ड’ तैयार करेगा, जिन पर भारत की रैंकिंग होती है. निगरानी का यह काम ‘सिर्फ़ रैंकिंग सुधारने के लिए नहीं था, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने, सुधारों को आगे बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और विश्व स्तर पर भारत की धारणा को एक आकार देने’ के लिए था.
वजह चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यह हमें खुद ऐसा करने से नहीं रोकना चाहिए. अपनी एक किताब के लिए, मैंने चार दर्जन से ज़्यादा वैश्विक सूचकांकों को देखा, ताकि यह तुलना कर सकूँ कि 2014 के मुकाबले भारत आज कहाँ खड़ा है. मैं समय-समय पर इन आँकड़ों को फिर से देखता हूँ और यह जानना उपयोगी है कि स्थिति क्या है. आइए एक नज़र डालते हैं.
मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स-एचडीआई) पर, 2014 में भारत की रैंक 130 थी और आज भी उसकी रैंक वही है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि “असमानता भारत के एचडीआई को 30.7% तक कम कर देती है, जो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान में से एक है. स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता में सुधार हुआ है, लेकिन आय और लैंगिक असमानताएँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं. महिला श्रम बल की भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी है”.
सिविकस मॉनिटर ने भारत के नागरिक समाज के दायरे को ‘बाधित’ से घटाकर ‘दमित’ कर दिया. इसमें कहा गया है कि “दुनिया में इस रेटिंग (दमित) के साथ कुल 49 देश हैं. यह रेटिंग आम तौर पर उन देशों को दी जाती है जहाँ सत्ताधारी नागरिक अधिकारों का भारी विरोध करते हैं, और मौलिक अधिकारों के पूर्ण उपयोग पर कानूनी और व्यावहारिक दोनों तरह की बाधाएँ लगाते हैं.”
लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स हार्ड पावर को मापता है. भारत का स्कोर 41.5 से गिरकर 39.1 हो गया, जिससे उसने ‘बड़ी शक्ति’ का दर्जा खो दिया. इंस्टीट्यूट का कहना है कि “भारत अपने उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए क्षेत्र में उम्मीद से कम प्रभाव डालता है, जैसा कि देश के निगेटिव पावर गैप स्कोर से पता चलता है. 2024 में इसका निगेटिव पावर गैप एशिया पावर इंडेक्स की शुरुआत के बाद से सबसे ज़्यादा था.”
फ्रीडम हाउस का ‘फ्रीडम इन द वर्ल्ड’ सूचकांक कानून के शासन, राजनीतिक बहुलवाद और चुनाव, सरकार के कामकाज, नागरिक स्वतंत्रता आदि को देखता है. 2014 में भारत को 77 की रेटिंग दी गई थी और ‘स्वतंत्र’ का दर्जा दिया गया था. 2025 में यह घटकर 63 हो गया और दर्जा घटाकर ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ कर दिया गया. (जब ऐसा पहली बार हुआ तो सरकार नाराज़ हुई थी, लेकिन बाद में उसने ऐसी रिपोर्टों पर टिप्पणी करना बंद कर दिया). फ्रीडम हाउस ने कहा कि “हालांकि भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, लेकिन सरकार ने भेदभावपूर्ण नीतियों की अध्यक्षता की है और मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाले उत्पीड़न में वृद्धि हुई है”.
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक ‘रूल ऑफ लॉ इंडेक्स’ प्रकाशित करता है, जो देशों की आपराधिक और नागरिक न्याय प्रणाली, मौलिक अधिकार, सरकारी शक्तियों पर अंकुश, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, पारदर्शी सरकार, व्यवस्था और सुरक्षा तथा नियामक प्रवर्तन की निगरानी करता है. भारत 2014 की अपनी 66वीं रैंकिंग से गिरकर विश्व स्तर पर 86वें स्थान पर आ गया है. संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा और डिस्टोपिया को देखती है. भारत 2014 में 111वें स्थान से खिसककर 118वें पर आ गया है.
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर भारत 2014 में 140वें स्थान से गिरकर आज 151वें स्थान पर आ गया है. आरएसएफ का कहना है कि “पत्रकारों के खिलाफ़ हिंसा, मीडिया के मालिकाने का अत्यधिक केंद्रीकरण, और राजनीतिक पक्षपात के साथ, ‘दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र’ में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है.” काटो इंस्टीट्यूट के ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पर भारत 2014 में 87वें स्थान से खिसककर 110वें स्थान पर पहुँच गया. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर भारत 2014 में 114वें स्थान से आज 131वें स्थान पर पहुँच गया है.
इसके कारण बताए गए कि ‘संसद में महिला प्रतिनिधित्व 2025 में 14.7% से घटकर 13.8% हो गया, जिससे इस संकेतक का स्कोर लगातार दूसरे साल 2023 के स्तर से नीचे आ गया. इसी तरह, मंत्री पदों में महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर 5.6% हो गई.’
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर भारत के मीडिया में नियमित रूप से रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन अब ज़्यादा नहीं होती. भारत 2014 में 85वें स्थान से आज दुनिया में 96वें स्थान पर पहुँच गया है.
हेरिटेज फाउंडेशन का ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इन चीज़ों की निगरानी करता है: कानून का शासन, सरकार का आकार, नियामक दक्षता और खुले बाज़ार. भारत 2014 में 120वें स्थान पर था और आज 128वें स्थान पर है. दिए गए कारण: “बाज़ार-उन्मुख सुधारों के साथ प्रगति असमान रही है. एक कुशल कानूनी ढाँचे के अभाव में दीर्घकालिक आर्थिक विकास की नींव कमज़ोर बनी हुई है. उद्यमियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. भारत का नियामक ढाँचा बोझिल है” वगैरह.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख, बच्चों में बौनापन, और कुपोषण की निगरानी करता है. 2014 में, भारत 76 देशों में 55वें स्थान पर था. आज भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है. रिपोर्ट कहती है कि “भारत में भूख का स्तर गंभीर है.”
जब भारत हंगर इंडेक्स पर तेज़ी से नीचे गिरने लगा, तो सरकार ने 2021 में संसद में कहा कि यह संभव नहीं है कि भारतीय भूखे हों और “हमें ऐसी रिपोर्टों के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए.”
समय के साथ इन सूचकांकों पर हमारी स्थिति बदल गई है. पहले, हमने मान लिया कि सुशासन से फ़र्क पड़ेगा. फिर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन सूचकांकों में आँकड़े खराब थे और वैसे भी ये संस्थान हमारे प्रति पूर्वाग्रह रखते थे. और बाद में, यह तय किया गया कि इन खबरों को बस नज़रअंदाज़ कर दिया जाए, हालांकि आँकड़े आते रहे और अब भी आ रहे हैं.
मीडिया की सामान्य रुचि के अभाव में, यह पता लगाना व्यक्ति पर छोड़ दिया गया है कि क्या बदलाव हुए हैं, और न्यू इंडिया किस दिशा में यात्रा कर रहा है.
ज़ोया हसन: महिलाओं की मतदान शक्ति में इस वृद्धि का वास्तव में मतलब इतना सीधा नहीं
लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में प्रोफ़ेसर एमेरिटा हैं. यह लेख द वायर में प्रकाशित हुआ है. उसके प्रमुख अंश.
जैसे ही अंतिम वोटों की गिनती हुई, बिहार एक ऐसी राजनीतिक पटकथा के साथ जागा, जिसकी बहुत कम लोगों ने पूरी तरह से उम्मीद की थी. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 200 से ज़्यादा सीटों के साथ सत्ता में ज़बरदस्त वापसी की, जो अर्थव्यवस्था, नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य या कानून और व्यवस्था पर कोई ठोस प्रगति न होने के बावजूद लगभग 90% की आश्चर्यजनक स्ट्राइक रेट थी.
यह शानदार जीत दर्शाती है कि शासन के प्रदर्शन से परे की ताकतों ने जनादेश को कैसे आकार दिया: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) का संदिग्ध आचरण, महिलाओं को लक्षित नकद हस्तांतरण, लचीले जाति-सामाजिक गठबंधन, एनडीए का ‘जंगल राज’ का नैरेटिव, नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति की एक देर से उठी लहर और गृह मंत्री अमित शाह के वोट प्रबंधन कौशल से संचालित बीजेपी की दुर्जेय चुनावी मशीनरी. इन सबने मिलकर एक ऐसा परिणाम दिया जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा था.
एक दशक से ज़्यादा समय से, महिला मतदाताओं ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को लगातार नया आकार दिया है. उनकी बढ़ती मतदान दर, अलग-अलग प्राथमिकताएँ और चुनावी मुक़ाबलों में निर्णायक वज़न ने हर पार्टी को उन्हें लुभाने के लिए मजबूर किया है. जैसा कि कई मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है, एनडीए की 2025 की रणनीति ‘पैसा और महिला’ के इर्द-गिर्द घूमती थी: महिला मतदाताओं के लिए एक जानबूझकर की गई पेशकश जिसने नकद हस्तांतरण और रोज़गार से जुड़े समर्थन को अपने अभियान के केंद्र में रखा.
इन उपायों को अब महिला मतदान में वृद्धि के प्रमुख चालकों के रूप में व्यापक रूप से उद्धृत किया जाता है, जिसे कई लोग एनडीए की भारी जीत में एक निर्णायक कारक मानते हैं.
बिहार में कुल मतदान 66.91% रहा, जो 1951 के बाद सबसे ज़्यादा है. महिला मतदान 71.6% तक पहुँच गया, जो पुरुषों के 62.8% से कहीं आगे था. यह 2015 (60.48%) और 2020 (59.69%) में महिलाओं के मतदान से एक तेज़ वृद्धि है, जिससे 2025 का चुनाव महिला राजनीतिक भागीदारी के मामले में एक स्पष्ट मील का पत्थर बन गया है. चुनाव आयोग के प्रारंभिक आँकड़ों के अनुसार, महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में कम से कम 4.34 लाख ज़्यादा वोट डाले, जो कि उल्लेखनीय है, यह देखते हुए कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में लगभग 42 लाख कम महिलाएँ थीं.
यह विरोधाभास, कम पंजीकरण लेकिन ज़्यादा भागीदारी, महिला वोट की बढ़ती राजनीतिक ताकत को रेखांकित करता है. मतदान के पैटर्न का विश्लेषण यह भी इंगित करता है कि महिला मतदाताओं के ज़्यादा अनुपात वाले जिलों में जनता दल (यूनाइटेड) के लिए मज़बूत समर्थन की प्रवृत्ति थी, जो इस वृद्धि के राजनीतिक महत्व को पुष्ट करता है.
यह विरोधाभास तब और भी तीखा हो जाता है जब इसे चुनाव से ठीक पहले किए गए ‘एसआईआर’ की पृष्ठभूमि में देखा जाता है. इस प्रक्रिया में शुद्ध रूप से ऐसे नाम हटाए गए, जिनका असर महिलाओं पर असमान रूप से पड़ा, जबकि पुरुष तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित हुए. परिणामस्वरूप, बिहार के मतदाता वर्ग में लिंगानुपात अंतिम एसआईआर सूचियों में फिसलकर 892 पर आ गया, जो एक साल पहले 907 था. ‘द हिंदू’ द्वारा किए गए एक सांख्यिकीय विश्लेषण में पाया गया कि युवा महिलाएँ (18-29 वर्ष) सबसे ज़्यादा प्रभावित हुईं, विशेष रूप से ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ श्रेणी के तहत हटाए गए नामों में.
यह पैटर्न बताता है कि शादी के बाद स्थानांतरित होने वाली महिलाओं को नाम हटाने का खामियाज़ा भुगतना पड़ा, इस पर बहुत कम स्पष्टता है कि क्या उन्हें बाद में उनके नए निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकित किया गया था.
बिहार से पुरुषों का असाधारण रूप से ज़्यादा पलायन यह समझाने में मदद करता है कि मतदाता सूची में कम उपस्थिति के बावजूद महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज़्यादा क्यों रहा. कामकाजी उम्र के पुरुषों का एक बड़ा हिस्सा राज्य से अनुपस्थित होने के कारण, महिलाएँ सक्रिय मतदाता वर्ग का एक बड़ा हिस्सा बनती हैं. इन जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं में अंतिम समय में नकद हस्तांतरण ने भागीदारी को इस तरह से बढ़ाया जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के किसी भी गहरे होने के बजाय प्रशासनिक और आर्थिक हस्तक्षेपों को ज़्यादा दर्शाता है.
जब तक चुनाव आयोग मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की अखंडता और नाम हटाने के पैटर्न पर स्पष्टता प्रदान नहीं करता, तब तक महिलाओं के मतदान में वृद्धि को सावधानी से देखा जाना चाहिए.
फिर भी, उपलब्ध साक्ष्य इंगित करते हैं कि 2025 के चुनावों के दौरान मतदान में यह वृद्धि एनडीए के लिए निर्णायक रूप से फ़ायदेमंद रही. यह संकेत देता है कि महिला मतदाता बिहार में एक मुख्य चुनावी क्षेत्र बन गई हैं, विशेष रूप से सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए. उनका कुल मतदान में पुरुषों से आगे निकलना एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक बदलाव है, जो मान्यता का पात्र है.
फिर भी एक ज़्यादा मतदान स्पष्ट रूप से लिंग-समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है. जब तक महिलाएँ विधायक के रूप में भी नहीं चुनी जातीं, तब तक उनका चुनावी वज़न पूरी तरह से विधायी प्रभाव में नहीं बदल सकता. यह लोकतांत्रिक विरोधाभास स्पष्ट है: महिलाएँ एक दुर्जेय वोटिंग ब्लॉक के रूप में उभर रही हैं, जबकि विधायिका के भीतर उनकी उपस्थिति असमान रूप से कम बनी हुई है.
इस अलगाव को दर्शाते हुए, बिहार में महिला वोट की केंद्रीयता के बावजूद, पार्टियों ने महिलाओं को केवल नाममात्र की टिकटें आवंटित कीं, इस लिहाज से यह एक हैरान करने वाली विडंबना है कि चुनाव उनके समर्थन पर टिका था. टिकटों के सटीक वितरण या अंततः जीतने वाली महिलाओं की संख्या पर विश्वसनीय डेटा अभी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि केवल 258 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा.
महिलाएँ बिहार में, साथ ही कई अन्य राज्यों में, चुनाव अभियानों के दौरान सबसे ज़्यादा लुभाया जाने वाला वोट बैंक हो सकती हैं, फिर भी वे चुनावों के बाद सत्ता के गलियारों से काफी हद तक अनुपस्थित रहती हैं. यह अंतर चुनावी रूप से संचालित भागीदारी की सीमाओं को उजागर करता है. कल्याणकारी योजनाएँ उन्हें लक्षित करना जारी रख सकती हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकार-बोध और प्रतिनिधित्व के लिए उनकी गहरी आकांक्षाएँ अधूरी रहती हैं. कई ग्रामीण क्षेत्रों में, बढ़ता कर्ज और लगातार नौकरियों की कमी अब राज्य के बार-बार दोहराए जाने वाले ‘सशक्तिकरण’ आख्यान पर भारी पड़ रही है.
इसी संदर्भ में नीतीश कुमार के लगभग दो दशक के कार्यकाल ने लक्षित आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं के कल्याण पर एक लंबे समय से ध्यान केंद्रित किया है. सितंबर में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना’, महिलाओं पर केंद्रित पहलों की एक लंबी परंपरा का अनुसरण करती है: 2006 में स्कूली छात्राओं को साइकिल प्रदान करने से लेकर, बिहार के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को स्थापित करने तक, सरकारी नौकरियों में आरक्षित पदों तक, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के जीविका नेटवर्क का विस्तार करने और बाद में, 2016 की शराबबंदी नीति तक. इन सभी उपायों ने महिलाओं को राज्य के कल्याणकारी ढाँचे के केंद्र में रखा है.
इस योजना ने महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपये तक का वादा किया था. इसकी 10,000 रुपये की पहली किस्त चरणों में जारी की गई, जिसकी शुरुआत 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को इसे प्राप्त करने से हुई, जो योजना के अनावरण के ठीक एक दिन बाद और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से दस दिन पहले था.
अतिरिक्त भुगतान अक्टूबर में भी जारी रहे, यहाँ तक कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी, अंततः बिहार भर में लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 1.21 करोड़ हो गई. 10,000 रुपये के इस सीधे हस्तांतरण ने एनडीए, विशेष रूप से जद(यू) के लिए भारी चुनावी लाभांश दिया.
विपक्षी दलों ने इसे औपचारिक रूप से एक उल्लंघन के रूप में चुनौती दी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे “चल रही योजना” के रूप में वर्गीकृत करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. इसलिए, नकद वितरण आयोग की निष्क्रियता के कारण निर्बाध रूप से जारी रहा. उनका जारी रहना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था और समय ने गंभीर नैतिक चिंताएँ पैदा कीं. यह नकद हस्तांतरण योजना, जिसे कई आलोचकों ने एक तरह की “रिश्वत” के रूप में वर्णित किया, एक प्रमुख आकर्षण बन गई और एनडीए की भारी जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह सब चुनाव आयोग की जाँच के बिना हुआ.
यह चूक महिला वोट पर बहस के केंद्र में है: यदि महिलाओं के मतदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उस अवधि के दौरान जारी किए गए हस्तांतरणों से आकार लिया गया था, जिसका उद्देश्य एक समान अवसर सुनिश्चित करना था, तो उस वोट की अखंडता का मूल्यांकन चुनाव आयोग के गैर-निर्णय की जाँच किए बिना नहीं किया जा सकता.
इन परिस्थितियों में, एनडीए के विकास, कानून और व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के नैरेटिव ने महिला मतदाताओं के बीच महागठबंधन की अपील की तुलना में ज़्यादा आकर्षण प्राप्त किया, जिससे अभूतपूर्व महिला मतदान के बीच ज्वार को अपने पक्ष में मोड़ने में मदद मिली. फिर भी यह उछाल गहरी ढाँचागत चिंताओं के साथ असहज रूप से बैठता है: तिरछी मतदाता सूची, बड़े पैमाने पर नाम हटाना और आचार संहिता के अनसुलझे उल्लंघन.
कुल मिलाकर, ये मुद्दे इस बात को जटिल बनाते हैं कि महिलाओं की मतदान शक्ति में इस वृद्धि का वास्तव में क्या मतलब है. वे एक ऐसे उछाल की ओर इशारा करते हैं जो बढ़ती राजनीतिक चेतना से कम, बल्कि ‘महिला और मनी’ के गठजोड़ और कल्याणकारी योजनाओं, राजनीतिक वफ़ादारी और चुनावी ईमानदारी में कमियों के मिश्रण से ज़्यादा प्रभावित हुआ है.
पहले “शव का धर्मांतरण” कराया, इसके बाद करने दिया ईसाई आदिवासी का अंतिम संस्कार
ओडिशा के नबरंगपुर ज़िले के मेंजर गांव की रहने वाली बुडई हरिजन की आवाज़ भर्रा गई, जब उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें अपने पति मदनु हरिजन के अंतिम संस्कार में ईसाई रीति छोड़ने को मजबूर किया गया. उनके पति मदनु हरिजन की मौत के बाद जब शव गांव लाया गया, तो 30-40 लोगों की भीड़ ने ईसाई रीति से दफनाने का विरोध किया और शव का “शुद्धिकरण” कर हिंदू रीति से दफनाने के लिए मजबूर किया.
गांव में लगभग आठ दलित–आदिवासी ईसाई परिवार हैं, जबकि लगभग 2,000 की आबादी गैर-ईसाई है. भीड़ ने कहा कि जब तक शव को “हिंदू धर्म में परिवर्तित” नहीं किया जाएगा,दफ़नाने नहीं दिया जाएगा.रिपोर्ट के अनुसार, यह गतिरोध दो दिन चला. शव सड़ने लगा तो परिवार हार मान गया और हिंदू रीति से दफनाने को विवश हुआ.
“आर्टिकल-14” के सैयद अ़फ़्फ़ान की रिपोर्ट दिखाती है कि ओडिशा और अन्य आदिवासी इलाकों में ईसाइयों पर हमले और धमकाने की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं. 2 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन गांवों के बैनरों को वैध ठहराया, जिनमें पादरियों और ईसाई धर्मांतरितों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था.
ओडिशा, जहां देश की तीसरी सबसे बड़ी आदिवासी आबादी रहती है, वहां 70% ईसाई जनसंख्या आदिवासी समुदायों से आती है. यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) के अनुसार 2023 में राज्य में ईसाइयों पर 7 हमले हुए, जो 2024 में बढ़कर 14 हो गए. 2025 के पहले छह महीनों में घटनाएं बढ़कर 8 हो चुकी थीं. पूरे देश में 2014 से 2024 के बीच 4,316 घटनाएँ दर्ज की गईं, 2024 में ये संख्या 834 तक पहुंच गई, लगभग 500% की वृद्धि हुई है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनीतिक माहौल भी इन घटनाओं को प्रभावित करता है. 2024 में ओडिशा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद घटनाएं और बढ़ी हैं, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि ये घटनाएँ धर्मांतरण कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ “स्थानीय प्रतिक्रिया” हैं. इस बीच, कई गांवों में ईसाइयों को मृतकों का अंतिम संस्कार करने से रोका जा रहा है. कुछ परिवारों को मजबूर किया गया कि वे मृतक को “हिंदू घोषित” करें, तभी दफनाने की अनुमति मिलेगी. एक गांव में पुलिस के जाने के बाद शव को कब्र से निकालकर जंगल में जला दिया गया. कई परिवारों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया, उनकी पानी, बिजली जैसी सुविधाएँ भी काट दी गईं.
रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच ओडिशा में आठ बड़े मामले सामने आए, पांच में दफ़नाने से रोकने और तीन में हिंसक हमलों के हैं . एक घटना में पादरियों और भक्तों पर 300 लोगों की भीड़ ने हमला किया. एफआईआर में दर्ज है कि भीड़ हथियारों के साथ “इरादा बनाकर” आई थी. कई पीड़ित गांव छोड़ने को मजबूर हुए क्योंकि उन्हें फिर से हमला होने का डर था. एक और घटना में, गजपति ज़िले के एक चर्च में पुलिस कर्मियों ने मूर्तियाँ तोड़ीं, खाद्यान्न जलाया और प्रार्थना स्थल को नुकसान पहुंचाया. दो ननों और एक पादरी की पिटाई भी की गई.
लाल किला विस्फोट:
एनआईए ने उमर के एक और सहयोगी को किया गिरफ्तार, लेकिन परेशान पिता ने जान दी
दिल्ली में लालकिला विस्फोट मामले में पहली गिरफ्तारी के एक दिन बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कश्मीर का रहने वाला है. उस पर कार बम धमाके से पहले ड्रोन को संशोधित करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करने का आरोप है.
“द इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान कासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में हुई है, जो जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काज़ीगुंड का निवासी है. वह उमर नबी का करीबी सहयोगी था, जो कथित तौर पर वह कार चला रहा था जो 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर फट गई थी. एनआईए के प्रवक्ता ने कहा, “वह हमले के पीछे एक सक्रिय सह-साजिशकर्ता था और उसने आतंकवादी, उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकवादी नरसंहार की योजना बनाने का काम किया था.” रविवार को, एनआईए ने उमर नबी के कश्मीर स्थित एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान आमिर राशिद अली के रूप में हुई है, जिसके नाम पर हमले में शामिल हुंडई i20 पंजीकृत थी. उसे एनआईए द्वारा दिल्ली से (जहां उसे पूछताछ के लिए लाया गया था) गिरफ्तार किया गया, जिसने दिल्ली पुलिस से यह मामला लेने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया था. जांच में पता चला है कि साम्बोरा, पंपोर का निवासी अली भी कथित आत्मघाती हमलावर, उमर के साथ साज़िश में शामिल था. इधर, “द प्रिंट” के मुताबिक दो और घायलों के दम तोड़ने के बाद दिल्ली कार विस्फोट मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, पीड़ितों में से एक ने कल दम तोड़ दिया, जबकि विनय पाठक नामक एक अन्य पीड़ित की आज मृत्यु हो गई.
बेटे और भाई के अलावा बिलाल को भी बुलाया था थाने, परेशान होकर खुद को लगाई थी आग
इस बीच, “द वायर” में जहांगीर अली के अनुसार,’टेरर मॉड्यूल’ मामले में कई कश्मीरियों से पूछताछ की जा रही है. कासिर बिलाल वानी के पिता बिलाल अहमद वानी को भी 15 नवंबर को पूछताछ के लिए काज़ीगुंड पुलिस स्टेशन बुलाया गया था. पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद वे मानसिक रूप से बहुत टूट चुके थे. अगले दिन 16 नवंबर को उन्होंने खुद को आग लगा ली थी. उन्हें, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उन्होंने दम तोड़ दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, काज़ीगुंड पुलिस स्टेशन में उनके बेटे कासिर बिलाल और भाई नबील अहमद से फरीदाबाद ‘टेरर मॉड्यूल’ केस में पूछताछ की जा रही थी. टेरर मॉड्यूल केस में यह तीसरी मौत है. बिलाल अहमद वानी, डॉक्टर आदिल अहमद राथर के पड़ोसी थे, जो यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए ‘टेरर मॉड्यूल’ केस के एक आरोपी हैं. वानी के रिश्तेदारों ने बताया कि राथर से जुड़े होने के शक में कई लोगों को इलाके से उठाया गया है. “मकतूब मीडिया” की खबर है कि बिलाल ने पुलिस से आग्रह किया था कि उसे अपने बेटे से एक बार मुलाकात करने दी जाए, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद उसने खुद को आग लगा ली. इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वानी ने अधिकारियों से “बस उसे देखने” की गुहार लगाई थी, “लेकिन इससे इनकार कर दिया गया.” उन्होंने कहा कि “इस स्तर की मनमानी केवल घावों को गहरा करती है और निराशा पैदा करती है,” और चेतावनी दी कि जब युवा पुरुषों को “आकस्मिक रूप से” उठाया जाता है, तो यह पूरी पीढ़ी को “अंधेरे रास्तों की ओर धकेलने” का जोखिम पैदा करता है. इससे पहले श्रीनगर के नौगाम थाने में शुक्रवार (14 नवंबर) रात को हुए धमाके में एक दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे की मौत हुई थी. वह तीन बच्चों के पिता और परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे. परिवार के अनुसार, उन्हें जांच टीम ने फरीदाबाद से बरामद 2,900 किलो विस्फोटक सामग्री को सिलकर सील करने के लिए बुलाया था, तभी धमाका हो गया. इसके अलावा, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े एक अन्य नागरिक, गंदेरबल के बिलाल अहमद मसूद, की पहचान लाल क़िले धमाके में मारे गए लोगों में की गई थी.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर घटा
रिज़र्व बैंक ने बताया कि 7 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.699 अरब डॉलर कम होकर 687.034 अरब डॉलर रह गया. इससे पहले वाले हफ्ते में भी भंडार 5.623 अरब डॉलर घटा था. “पीटीआई” ने आरबीआई के हवाले से रिपोर्ट किया है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ 2.454 अरब डॉलर घटकर 562.137 अरब डॉलर रह गईं. सोने का भंडार भी 195 मिलियन डॉलर कम हुआ और अब 101.531 अरब डॉलर है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) 51 मिलियन डॉलर घटकर 18.594 अरब डॉलर हो गए. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत की स्थिति इस हफ्ते भी 4.772 अरब डॉलर पर कायम रही.
अपील :
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.