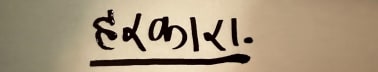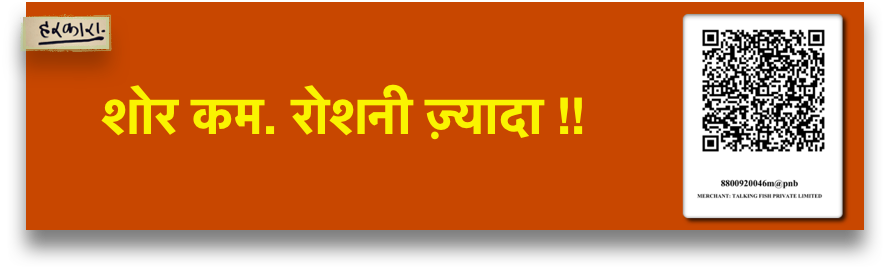21/08/2025: चीन पर यू-टर्न ? | केंचुआ से न लवासा खुश हैं न कुरैशी | राजनीति में अपराध पर विधेयक | 27 माह बाद भी सुलगता मणिपुर | सरन के भारत को 4 सबक | शुक्ला जी का अंतरिक्ष टिकट 548 करो
‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा!
निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल
आज की सुर्खियां:
सीमा विवाद पर भारत का यू-टर्न?
"वोट चोरी" पर घमासान:
पूर्व चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और एस. वाई. क़ुरैशी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं.
मंत्रियों पर शिकंजा कसने वाला विधेयक पेश
दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला:
27 महीने बाद भी मणिपुर अशांत: पीयूसीएल की स्वतंत्र ट्रिब्यूनल रिपोर्ट में खुलासा
मणिपुर टेप्स पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार:
अलास्का बैठक के बाद के सबक
रूस और यूक्रेन के बीच समझौता बहुत मुश्किल है.
कर्नाटक में दलितों के लिए आंतरिक आरक्षण
'अग्नि-5' मिसाइल का सफल परीक्षण
विवादों में मराठी फिल्म 'खालिद का शिवाजी'
चीन के साथ विवाद पर भारत का यू-टर्न?

द वायर के मुताबिक एक तरफ़ जहां मोदी सरकार उत्तरी सीमा पर बनी यथास्थिति को 'चीन के साथ सामान्य स्थिति वापस आ गई है' के रूप में पेश कर रही है, वहीं उसने एक चौंकाने वाला कूटनीतिक यू-टर्न लिया है. चीनी विदेश मंत्री वांग यी के दिल्ली दौरे के दूसरे दिन भारत ने घोषणा की कि वह चीन के साथ सीमा के परिसीमन में 'अर्ली हार्वेस्ट' की संभावना तलाशेगा. 'अर्ली हार्वेस्ट' का विचार बीजिंग ने पहली बार 2017 में उठाया था, जिसमें सिक्किम के साथ सीमा को आंशिक रूप से निपटाना शामिल था. यह शायद मोदी सरकार का चीन पर सबसे महत्वपूर्ण यू-टर्न हो सकता है, क्योंकि यह 2005 के उस समझौते को पलट देता है, जिसमें यह तय हुआ था कि सीमा विवाद को एक पैकेज डील के रूप में ही सुलझाया जाएगा. भारत की यह रियायत वाशिंगटन के लगातार टैरिफ़ हमलों और उर्वरकों, दुर्लभ खनिजों (rare earths) और टनल-बोरिंग मशीनों पर भारत की चिंताओं को दूर करने के चीन के कथित वादों से प्रेरित हो सकती है. जैसा कि आकार पटेल ने कहा, "ट्रम्प से दांत पर लात खाने के बाद शी की चापलूसी करना, और उससे पहले शी से दांत पर लात खाने के बाद ट्रम्प की चापलूसी करना, मेरे विचार में बहुत अच्छा क़दम था".
हालांकि भारतीय मीडिया में चीन द्वारा भारत को दुर्लभ खनिजों के निर्यात नियंत्रण में ढील देने की ख़बरें चल रही हैं, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने रॉयटर्स के सवाल पर अस्पष्ट जवाब दिया. उन्होंने कहा, "मैं इन मीडिया रिपोर्टों से परिचित नहीं हूं. सिद्धांत रूप से, चीन वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता बनाए रखने के लिए संबंधित देशों के साथ संवाद और सहयोग मज़बूत करने को तैयार है." वांग ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाक़ात की, जिन्होंने पुष्टि की कि वह इस महीने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन का दौरा करेंगे. वांग की यात्रा के कुछ ठोस परिणामों में सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, पर्यटकों, पत्रकारों और व्यवसायियों के लिए वीज़ा आसान बनाने और मानवीय आधार पर चीन द्वारा भारत के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने पर सहमति बनी. दिल्ली के बाद वांग काबुल और इस्लामाबाद जाएंगे. जब पीटीआई ने पूछा कि क्या वांग पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को उठाएंगे, तो चीनी प्रवक्ता का जवाब नपा-तुला था. उन्होंने कहा कि चीन-पाकिस्तान के रिश्ते किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करते और वे भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग चाहते हैं. भारत-चीन वार्ता में क्या हासिल हुआ, इसका विस्तृत मूल्यांकन मनोज केवलरमानी ने किया है.
श्याम सरन ने गिनवाये अलास्का से मिले चार सबक
भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा है कि यूक्रेन में रूस की "शांति के लिए ज़मीन" की मांग को ट्रम्प का समर्थन और वाशिंगटन के प्रति यूरोप की अधीनता, सत्ता के बदलते समीकरणों का संकेत है. भारत के लिए इसका मतलब अमेरिकी शत्रुता के लिए तैयार रहना और अपने लिए घटते रणनीतिक स्थान में काम करना है. वह पूछते हैं कि भारत अलास्का और वाशिंगटन से क्या सबक़ ले सकता है:
एक, अहंकारी नेता की चापलूसी करना आत्म-पराजय है. यह बार-बार अपमान का रास्ता खोलता है.
दो, इस धारणा को छोड़ देना चाहिए कि रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंधों में कोई भी रोक भारत को रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले 25% अतिरिक्त टैरिफ़ से राहत देगी. इन दंडात्मक टैरिफ़ों का संबंध रूस से ज़्यादा भारत से है.
तीन, भारत को अमेरिका की लंबे समय तक की शत्रुता के लिए तैयार रहना चाहिए. उम्मीद है कि यूरोप की तरह घोर अधीनता दिखाने के प्रलोभन से बचा जाएगा. स्वाभिमान और आत्म-सम्मान खोकर कोई भी आर्थिक राहत पाने लायक नहीं है. हमारी प्रतिक्रियाएं नपी-तुली होनी चाहिए.
चार, भारत को इस वास्तविक संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि ट्रम्प एक और शक्तिशाली नेता, चीन के शी जिनपिंग के साथ एक 'बड़ी सौदेबाज़ी' कर सकते हैं.
एक अच्छी भू-राजनीतिक स्थिति से, भारत को अब हाशिये पर धकेला जा रहा है, जिससे उसकी अपनी भूमिका कम हो गई है. इसके लिए विवेक, धैर्य और बड़ी पहलों के बजाय छोटी-छोटी सफलताओं को हासिल करने की नीति की आवश्यकता है. यह तूफ़ान भी गुज़र जाएगा.
केंचुआ / वोट चोरी
संजय कुमार ने अनजाने में साबित कर दिया, राहुल गांधी का दावा सही है
इस बीच संजय कुमार के दावे के संदर्भ में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप को सही ठहराया जा रहा है. प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने “एक्स” पर लिखा, (1) “महाराष्ट्र 2024 विधानसभा चुनाव के बारे में राहुल गांधी और कांग्रेस का लगातार क्या आरोप रहा है? यही न कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मात्र पांच महीनों में निर्वाचकों और मतदाताओं की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी हुई. इन नए मतदाताओं में से अधिकांश ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को वोट दिया और लोकसभा का नतीजा पलट गया.
(2) संजय कुमार ने दो विधानसभा क्षेत्रों (रामटेक और देवलाली) का डेटा दिखाकर इसके ठीक उलट दावा किया और राहुल गांधी का आरोप गलत साबित करने की कोशिश की. संजय ने कहा कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल वोट घटे हैं, फिर भी बीजेपी गठबंधन लोकसभा में हारने के बाद यहां विधानसभा चुनाव जीत गया.
(3) संजय का डेटा गलत निकला. वास्तव में, इन दोनों विधानसभाओं ने वही साबित किया जो राहुल गांधी ने कहा था – यानी, कुल मतदाता और मतों की संख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ी और बीजेपी गठबंधन ने इसी बढ़त की बदौलत जीत हासिल की.
(4) इसलिए, जब संजय कुमार ने अपनी पोस्ट डिलीट कर गलती मान ली, तब उन्होंने अनजाने में यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र के मामले में राहुल गांधी का दावा सही है.
(5) बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और मीडिया ने अंधाधुंध भाजपा के निर्देशों और पोस्ट टेम्पलेट्स का अनुसरण करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी का महाराष्ट्र वाला आरोप इस घटना से गलत साबित हुआ.
सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है – यह घटना साबित करती है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संदिग्ध है. चुनाव आयोग के अधिकारियों की बीजेपी के साथ यह नंगी और बेवक़ूफ़ाना मिलीभगत, यह और भी साफ़ दिखाती है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से समझौता कर चुका है.
“वोट चोरी” पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल
बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में कथित हेरफेर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. इसकी जांच के लिए कोर्ट में एक पीआईएल लगाकर मांग की गई है कि पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाए. याचिकाकरता वकील और कांग्रेस सदस्य रोहित पांडे ने कहा कि उनकी एक सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए आ सकती है. सुचित्रा कल्याण मोहंती के अनुसार, पांडे ने यह याचिका लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों का हवाला देते हुए दायर की है.
महाराष्ट्र में सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर
महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. उन पर गलत जानकारी देने और चुनाव संबंधी उल्लंघनों से जुड़े आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 175, 353(1)(बी), 212 और 340(1)(2) के तहत केस दर्ज हुआ है. संजय कुमार ने 17 अगस्त को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की तुलना में पांच माह बाद महाराष्ट्र विधानसभा की दो सीटों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से कम हो गए थे. हालांकि, 19 अगस्त को उन्होंने पोस्ट डिलीट करके गलत आंकड़ों के लिए माफी मांगी थी.
पूर्व चुनाव आयुक्तों की राय में अति हो रही है
अशोक लवासा: जिसकी लाठी उसकी भैंस सही तरीका नहीं | एस. वाई. क़ुरैशी: आयोग के लिए पारदर्शिता की ओर लौटना ज़रूरी
भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हालिया विवाद पर दो पूर्व चुनाव आयुक्तों, अशोक लवासा और एस. वाई. क़ुरैशी, ने इंडियन एक्सप्रेस में गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं. दोनों ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हैं, लेकिन उनके तर्क अलग-अलग दृष्टिकोणों पर आधारित हैं. लवासा "ताकत बनाम न्याय" के दार्शनिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि क़ुरैशी "पारदर्शिता और विश्वास" के व्यावहारिक मुद्दे पर ज़ोर देते हैं.
अशोक लवासा अपने लेख में चुनाव आयोग की कार्रवाई को "माइट इस राइट यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत के आधुनिक संस्करण के रूप में देखते हैं, जहाँ सत्ता में बैठे लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों के अधिकारों को कुचलने के लिए करते हैं.
मनमानी और अभूतपूर्व प्रक्रिया: लवासा तर्क देते हैं कि चुनाव आयोग ने एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई है जिसका कोई पिछला उदाहरण नहीं है और जिसमें कोई तर्क नहीं है. करोड़ों मतदाताओं को अपनी पहचान फिर से साबित करने के लिए मजबूर करना, जबकि वे पहले से ही सूची में थे, सत्ता का एकतरफा प्रयोग है. चुनाव आयोग यह समझाने में विफल रहा है कि उसने अपनी ही समय-परीक्षित प्रक्रिया को क्यों त्याग दिया.
संवैधानिक अधिकार को लिपिकीय प्रक्रिया बनाना: उनका सबसे शक्तिशाली तर्क यह है कि इस प्रक्रिया ने मतदान के संवैधानिक अधिकार को एक "ड्राइविंग लाइसेंस" की तरह बना दिया है जिसे समय-समय पर नवीनीकृत करने की आवश्यकता है. एक 95 वर्षीय मतदाता, जो 1951 से सूची में है, केवल एक फॉर्म जमा न करने के कारण हटाया जा सकता है. यह एक मौलिक अधिकार को एक मामूली लिपिकीय कार्य के अधीन करना है.
न्याय के बजाय सज़ा: लवासा इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सूची से नाम हटाना केवल "हटाना" नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से "मिटा देना" है. नागरिक को अपील का कोई सीधा रास्ता नहीं दिया गया है, सिवाय इसके कि वह नए सिरे से आवेदन करे. यह प्रक्रिया सुधार के बजाय दंडात्मक है.
सबसे कमजोरों पर प्रभाव: वह उन नागरिकों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र, स्कूली शिक्षा या भूमि जैसे दस्तावेज़ नहीं हैं. यह प्रक्रिया सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पड़े लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने का एक आसान ज़रिया बन सकती है.
लवासा के अनुसार, चुनाव आयोग की यह कार्रवाई सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक संस्था द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग है, जो न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर प्रक्रियात्मक कठोरता को प्राथमिकता दे रही है. यह कानूनी होने और न्यायपूर्ण होने के बीच के अंतर को उजागर करता है.
एस. वाई. क़ुरैशी का लेख चुनाव आयोग की घटती पारदर्शिता और जनता के विश्वास में आई कमी पर केंद्रित है. वह ऐतिहासिक उदाहरणों का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि चुनाव आयोग अपने ही स्थापित सिद्धांतों से कैसे भटक गया है.
ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं से विचलन: क़ुरैशी 2007 के उत्तर प्रदेश चुनावों के "SAD" (शिफ्टेड, एब्सेंट, डेड) मतदाता मॉडल का उदाहरण देते हैं. उस समय, चुनाव आयोग ने संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाने के बजाय, उनकी एक अलग सूची बनाई और मतदान के दिन उनकी पहचान की पुष्टि की. यह तरीका फर्जी मतदान को रोकने में सफल रहा और किसी को मताधिकार से वंचित भी नहीं किया गया. आज की प्रक्रिया उस बेहतर मॉडल के ठीक विपरीत है.
अधूरी और भ्रामक पारदर्शिता: क़ुरैशी की मुख्य आलोचना यह है कि चुनाव आयोग ने यह तो बताया कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि कितने नए नाम जोड़े गए हैं. यह एक अधूरी तस्वीर पेश करता है, क्योंकि फर्जी नामों को जोड़ना भी एक बड़ी समस्या है. पूरी पारदर्शिता के बिना, यह प्रक्रिया संदेह पैदा करती है.
पुरानी बुद्धिमत्ता को नकारना: वह सवाल करते हैं कि चुनाव आयोग ने नए सिरे से सूची बनाने का फैसला क्यों किया, जबकि पिछले दो दशकों से आयोगों ने इस प्रथा को बंद कर दिया था. उनका सवाल है, "क्या पिछले आयोग कम बुद्धिमान थे?" यह मौजूदा चुनाव आयोग के फैसले के तर्क पर सीधा हमला है.
विश्वास बहाली के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है: क़ुरैशी का मानना है कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा उसके निष्पक्ष होने की धारणा पर बनी है. सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को हटाए गए नामों और कारणों को सार्वजनिक करने का निर्देश एक स्वागत योग्य कदम है. चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी होना होगा.
क़ुरैशी के लिए, यह संकट विश्वास और पारदर्शिता का है. चुनाव आयोग को अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए न केवल यह दिखाना होगा कि उसने कितने अयोग्य मतदाताओं को हटाया है, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उसने कितने योग्य मतदाताओं को जोड़ा है और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है.
इसी पर हरकारा डीपडाइव लेखक और खोजी पत्रकार पूनम अग्रवाल के साथ
पीयूसीएल के स्वतंत्र ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट
27 महीने बाद मणिपुर, अभी भी अशांत
पीयूसीएल द्वारा पिछले साल गठित एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल ने मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के कारणों और राज्य के मौजूदा हालात पर बुधवार 20 अगस्त को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें न्याय, शांति और जवाबदेही के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली जूरी ने हिंसा में जीवित बचे लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर कहा कि राज्य की संस्थाओं और प्राधिकृत अधिकारियों ने संरक्षण देने के बजाय स्थानीय लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया. केंद्र सरकार मणिपुर में कानून के शासन और संविधान की व्यवस्था बनाए रखने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रही. ट्रिब्यूनल के सामने बड़े पैमाने पर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.
जूरी ने साक्ष्यों के आधार पर संघर्ष के कई मूल कारणों को पहचाना. इनमें ऐतिहासिक जातीय विभाजन, सामाजिक-राजनीतिक हाशिये पर डालना और ज़मीन विवाद जैसे पहले से मौजूद कारक शामिल थे. अविश्वास और शत्रुता को बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया पर चलाया गया घृणा अभियान और राजनीतिक नेतृत्व के बयानों ने भी बड़ी भूमिका निभाई.
27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट का वह निर्देश, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी, कुकी-ज़ो और नागा समूहों द्वारा उनके संवैधानिक संरक्षणों के लिए खतरे के रूप में देखा गया. इसी चिंगारी ने पहाड़ी ज़िलों में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया. नतीजतन 3 मई 2023 को बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज किया गया. प्रारंभ में ये आंदोलन अधिकतर शांतिपूर्ण थे, लेकिन कुछ स्थानों पर हिंसा भड़क उठी, जिसने बाद में पूरे राज्य को घेर लिया.
पलायन के ठोस प्रमाण नहीं : मैतेई पक्ष की गवाहियों में अक्सर यह दावा किया गया कि म्यांमार से कुकी-ज़ो समुदाय का लगातार पलायन हो रहा है. परंतु जूरी ने आंकड़ों के अध्ययन से पाया कि इस दावे के ठोस प्रमाण नहीं हैं.
अफीम (पॉपी) की खेती की कथा : इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की “ड्रग्स विरोधी युद्ध” नीति से जोड़कर कुकी समुदाय को अपराधी ठहराने का प्रयास किया गया. कुकी गवाहों ने इसे षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि असली खिलाड़ी विभिन्न समुदायों से थे और सरकारी तंत्र में भी बैठे थे. गवाहों ने यह भी संदेह जताया कि इस संघर्ष के पीछे बड़े भू-राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं. मीडिया की भूमिका को भी जूरी ने गंभीर रूप से चिन्हित किया. प्रिंट मीडिया पक्षपाती रहा जबकि डिजिटल और सोशल मीडिया ने अप्रमाणित व भड़काऊ सामग्री फैलाई.
हिंसा की प्रकृति और राज्य की भूमिका : रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यह हिंसा स्वतःस्फूर्त नहीं थी, बल्कि नियोजित, जातीय रूप से लक्षित और राज्य संस्थाओं की विफलता की देन थी. पीड़ितों में गहरी धारणा बनी रही कि राज्य ने या तो हिंसा को होने दिया या उसमें सक्रिय भाग लिया. पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के कुछ निर्णयों एवं प्रशासनिक कार्यवाही को हिंसा की चिंगारी मानकर बार-बार उल्लेख किया गया. उग्रवादी संगठनों अरामबाई तेंगगोल और मैतेई लीपुन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. लंबे समय तक सार्वजनिक विरोध के बावजूद बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 तक पद नहीं छोड़ा.
यौन हिंसा और मानवीय संकट : जूरी गहराई से व्यथित रही कि हिंसा के दौरान लोगों की हत्या, अंग-भंग, निर्वस्त्र करना और सामूहिक यौन हिंसा तक हुई. सोशल मीडिया पर इन अत्याचारों को प्रसारित भी किया गया. गवाहियों में यह दर्ज है कि यौन हिंसा की कई घटनाएं भय और संस्थागत सहयोग की कमी के कारण दर्ज ही नहीं हुईं. महिलाओं ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने न केवल उनकी मदद करने से इनकार किया बल्कि कई बार भीड़ के हवाले तक कर दिया.
राहत और पुनर्वास : राहत व पुनर्वास के प्रयास बेहद अपर्याप्त, विलंबित और असमान थे. राहत शिविरों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और आजीविका-शिक्षा की पुनर्स्थापना लगभग न के बराबर रही. संयुक्त त्वरित आवश्यकता मूल्यांकन (जेआरएनए) और गीता मित्तल समिति की सिफारिशें भी ज्यादातर लागू नहीं हुईं.
स्वास्थ्य व्यवस्था का पतन : स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया. अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर हमले हुए, उपकरण लूट लिए गए और सुरक्षा संकट के कारण डॉक्टर व स्टाफ भाग खड़े हुए. आंतरिक रूप से विस्थापित लोग जो राहत शिविरों में पहुंचे, वे और भी खराब हालात में रहे. महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की स्थिति सबसे अधिक प्रभावित हुई. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी दर्ज की गईं.
न्यायपालिका और विधि-व्यवस्था : रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यायिक और संवैधानिक तंत्र हिंसा के दौरान पूरी तरह विफल रहा. इसमें अदालतों द्वारा त्वरित निर्देशों का अभाव, चयनित एफआईआर दर्ज करना, गंभीर अपराधों की जांच का अभाव और पुलिस की संलिप्तता स्पष्ट की गई है. केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून के शासन को लागू करने में विफल रहीं.
जूरी की सिफारिशें : मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना, एक स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन, जो हजारों मामलों की जांच करे और सुरक्षा बलों की भूमिका पर भी पूछताछ करे. घृणा-प्रचार और भड़काऊ भाषण देने वालों व उन्हें रोकने में विफल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई. स्थायी शांति के लिए ढांचागत बदलाव, समुदायों के बीच संवाद, कानूनी जवाबदेही और नैतिक नेतृत्व अनिवार्य हैं.
निष्कर्ष : जातीय हिंसा के 27 महीने बाद भी मणिपुर अब तक अशांत ही है. यह सामूहिक विफलता है, जिसे अब नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.
मणिपुर टेप्स: सुप्रीम कोर्ट ने सीएफएसएल को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि केंद्र सरकार की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (सीएफएसएल) का मणिपुर टेप्स मामले को संभालने का तरीका "गलत दिशा में लगता है" और सरकार "केवल असमंजसपूर्ण जवाब दे रही है." कोर्ट ने यह भी कहा कि सीएफएसएल को टेप्स की जांच के लिए कहा गया था — जिनमें कथित रूप से मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बिरेंद्र सिंह को राज्य में जारी जातीय हिंसा के लिए खुद को शामिल बताया जा रहा है— लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरी रिकॉर्डिंग के प्रमाणीकरण की कोशिश कर रहे हैं.
गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पीएम, सीएम और मंत्रियों पर रोक के लिए विवादास्पद विधेयक पेश, विपक्ष का भारी विरोध
20 अगस्त, 2025 को संसद के एक नाटकीय सत्र में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो संविधान संशोधन विधेयक पेश किए. इन विधेयकों का उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद पर बने रहने से अयोग्य ठहराना है, यदि वे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करते हैं और उन्हें लगातार 30 दिनों तक जेल में रहना पड़ता है. सरकार ने इस कदम को राजनीति को स्वच्छ बनाने और नेतृत्व में ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बताया है. हालांकि, इस पर व्यापक विवाद खड़ा हो गया है. विपक्षी दलों ने इसे संघवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर हमला करार दिया है. विधेयकों में प्रस्ताव है कि इस तरह की क़ैद होने पर पद से स्वतः ही हटा दिया जाएगा, जिससे आरोपी नेता मुक़दमे के दौरान सत्ता में बने नहीं रह सकेंगे. यह विधेयक लोकसभा में हंगामेदार दृश्यों के बीच पेश किया गया, जहाँ विपक्षी सदस्यों ने ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाज़ी की और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए इन विधेयकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.
अमित शाह ने तर्क दिया कि ये उपाय शासन में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक हैं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि "क़ानून से ऊपर कोई नहीं है". उन्होंने घोषणा की कि विधेयकों को आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा जाएगा, जिसमें दोनों सदनों और विभिन्न दलों के सदस्य शामिल होंगे, ताकि व्यापक विचार-विमर्श हो सके. यह रियायत कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों सहित विपक्षी नेताओं के भारी दबाव के बाद दी गई, जिन्होंने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए गहन समीक्षा की मांग की थी. हालांकि, आलोचक इन विधेयकों को राजनीति से प्रेरित मानते हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इन्हें "असंवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए ख़तरा" बताया. उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल केंद्र का विरोध करने वाली राज्य सरकारों के ख़िलाफ़ एक हथियार के रूप में किया जा सकता है. क़ानूनी विशेषज्ञों ने भी इन चिंताओं को दोहराया है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मौजूदा क़ानूनों के साथ संभावित टकरावों का उल्लेख किया है, जो पहले से ही दोषी सांसदों को अयोग्य ठहराता है, लेकिन केवल आरोप लगने वालों को नहीं. विधेयकों का दायरा भ्रष्टाचार, आतंकवाद और आर्थिक अपराधों सहित "गंभीर आरोपों" तक फैला हुआ है, लेकिन इसमें स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव है, जिससे मनमाने ढंग से लागू किए जाने की आशंका बढ़ गई है. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इस पहल का बचाव करते हुए,
शाह ने एक लंबे पोस्ट में विस्तार से बताया: "लंबे समय से, गंभीर आरोपों का सामना करने वाले नेता सत्ता से चिपके रहे हैं, जिससे जनता का विश्वास कम हुआ है. ये विधेयक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं. अब, भारत के लोगों को यह तय करना होगा कि वे स्वच्छ राजनीति चाहते हैं या यथास्थिति". उन्होंने सुधार की आवश्यकता को सही ठहराने के लिए पिछले घोटालों, जैसे कोयला आवंटन घोटाले और राजनेताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के उदाहरण दिए. बीजेपी के भीतर समर्थक इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक "विकसित भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप एक साहसिक भ्रष्टाचार-विरोधी उपाय बता रहे हैं. विपक्ष का हंगामा सदन से बाहर भी जारी रहा, जहाँ कई गैर-बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इन विधेयकों को पारित होने पर क़ानूनी रूप से चुनौती देने की कसम खाई. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे "केंद्र का अतिक्रमण" कहा, जबकि तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने राज्य की स्वायत्तता पर इसके प्रभावों के बारे में चेतावनी दी. विश्लेषकों का सुझाव है कि ये विधेयक भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकते हैं, जिससे संभावित रूप से गठबंधन सरकारों में अस्थिरता आ सकती है, जहाँ नेताओं को अक्सर लंबी क़ानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है. आर्थिक दृष्टिकोण से, इसका समय वैश्विक अनिश्चितताओं के साथ मेल खाता है, जिसमें संभावित ट्रम्प प्रशासन के तहत अमेरिकी टैरिफ़ में वृद्धि भी शामिल है, जो भारत के निर्यात-संचालित विकास को प्रभावित कर सकती है. कुछ लोग इन विधेयकों को महंगाई और बेरोज़गारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में अभी भी ज़्यादा हैं, जहाँ मतदाता शासन की कमियों से निराश हैं. जेपीसी को मामला भेजे जाने से अस्थायी राहत मिली है, लेकिन आने वाले हफ़्तों में बहस तेज होने की उम्मीद है. यदि ये क़ानून बन जाते हैं, तो वे चुनावी सुधारों के लिए मिसाल क़ायम कर सकते हैं, लेकिन इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण के गहरे होने का ख़तरा भी है. जैसे-जैसे हिंदी पट्टी के पाठक इस पर विचार कर रहे हैं, सवाल यह उठता है: क्या यह लोकतंत्र को मज़बूत करता है या उसे कमज़ोर करता है. इन विधेयकों का भाग्य भारत की जीवंत लेकिन खंडित राजनीति में जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिशोध के बीच संतुलन की परीक्षा लेगा.
द वायर में श्रावस्ती दासगुप्ता लिखती हैं कि संसद में पेश किए गए विधेयकों पर बहस के दौरान, जिसमें कहा गया है कि हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद पर बने रहने की अनुमति देना 'संवैधानिक नैतिकता में बाधा' डालना है, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि 2010 में जब गुजरात के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में गिरफ़्तार किया गया था, तब नैतिकता का क्या हुआ था. इसके जवाब में शाह ने कहा कि उन्होंने गिरफ़्तार होने से पहले ही 'नैतिक आधार पर इस्तीफ़ा' दे दिया था. इस पर पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने पूछा है कि क्या यह 'व्यपगत के सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) की वापसी है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति थी. उनका यह सवाल इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों का इस्तेमाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी या झारखंड जैसी विपक्षी शासित सरकारों पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया है. राजद सांसद मनोज झा का कहना है कि विपक्ष के नेताओं के ख़िलाफ़ हालिया कार्रवाइयां लोकतंत्र की नींव को ही ख़तरे में डालती हैं. उन्होंने कहा, "जब जांच एजेंसियां राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बन जाती हैं, तो लोकतंत्र खुद कटघरे में खड़ा हो जाता है. प्रस्तावित विधेयक कार्यपालिका की पकड़ को और मज़बूत करेगा और यह हमारे लोकतंत्र के ताबूत में आख़िरी कील ठोकने जैसा होगा." इस पूरे मामले का निचोड़ यह है कि मोदी सरकार की एक लंबी रणनीति राज्य सरकारों पर विपक्ष की पकड़ को कमज़ोर करना है, लेकिन इस विवादास्पद कदम को लाने की जल्दबाज़ी का एक तात्कालिक कारण 'वोट चोरी' के आरोपों से सुर्खियों को हटाना भी हो सकता है.
मान्यवर, गृह मंत्री जी, अपने 94 सांसदों को तत्काल इस्तीफा देने के लिए कहें
लेखक संजय झा ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए दो संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर एक रोचक पोस्ट लिखी है. शाह को संबोधित पत्रनुमा इस पोस्ट में झा ने कहा,
प्रिय गृह मंत्री जी,
मान्यवर, दान-धर्म की शुरुआत घर से होनी चाहिए. भाजपा के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 (अर्थात 39%) ने आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है. इनमें से भाजपा के 63 सांसदों (26%) ने “गंभीर आपराधिक मामले” घोषित किए हैं, जिनमें शामिल हैं:- बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध (स्रोत: एडीआर).
मान्यवर, कृपया उन्हें तत्काल इस्तीफा देने के लिए कहें (कृपया यह न कहें कि “नया विधेयक केवल भविष्य में आने वाले मामलों पर लागू होगा”). आपको अपने शब्दों को कर्म से साबित करना होगा, सर. जनता आपको देख रही है.
मान्यवर, एक और प्रश्न. यदि भाजपा को पता था कि इन लोगों ने शपथपत्र में इन अपराधों की घोषणा की है, तो आपने उन्हें टिकट कैसे दे दिए? जबकि आपको अच्छी तरह पता था कि उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं??? मान्यवर, आपके उत्तर की मैं अत्यधिक सराहना करूंगा. बहुत-बहुत धन्यवाद.
लोकसभा ने रिकॉर्ड समय में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल पारित किया
लोकसभा ने 20 अगस्त, 2025 को केवल सात मिनट में ध्वनि मत से 'ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025' पारित कर दिया. आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य तेजी से बढ़ते इस उद्योग को विनियमित करना है, जिसमें लत, मनी लॉन्ड्रिंग और कम उम्र के बच्चों की पहुंच जैसी समस्याओं का समाधान करना है. आलोचकों ने इसे जल्दबाज़ी में पारित किए जाने की निंदा करते हुए तर्क दिया है कि इसमें गोपनीयता और गेमिंग करों से राज्यों के राजस्व जैसे मुद्दों पर सार्थक बहस को दरकिनार कर दिया गया. 3 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाले इस क्षेत्र में पबजी और फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे लोकप्रिय गेम शामिल हैं. हिंदी पट्टी के युवाओं के लिए, जहाँ मोबाइल गेमिंग बड़े पैमाने पर है, ये नियम शोषण पर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन मनोरंजन के विकल्पों को भी सीमित कर सकते हैं. वैष्णव ने उम्र सत्यापन और खर्च की सीमा सहित उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला. विधेयक अब राज्यसभा में जाएगा, जहाँ संशोधनों की उम्मीद है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त, 2025 को नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से आयोजित "जन सुनवाई" कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया. 30 साल के एक अज्ञात व्यक्ति ने दस्तावेज़ जमा करने के बहाने उनके पास पहुँचकर उन पर शारीरिक हमला कर दिया. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए हमलावर को मौक़े पर ही हिरासत में ले लिया. गुप्ता को मामूली चोटें आईं और उन्हें एहतियाती जांच के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई गई है. इस घटना ने राजनीतिक दलों में आक्रोश पैदा कर दिया है. आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे "कायरतापूर्ण कृत्य" बताया है और इसका संबंध विपक्षी ताक़तों से होने की आशंका जताई है. पुलिस जांच कर रही है और शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि हमलावर की शहरी विकास नीतियों से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतें हो सकती हैं. यह घटना भारत की राजधानी में सार्वजनिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है, जहाँ राजनीतिक तनाव अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर फैल जाता है. हिंदी पट्टी में, जहाँ इसी तरह के शिकायत निवारण कार्यक्रम आम हैं, यह जनता से सीधे जुड़ने वाले नेताओं के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े करता है. विपक्षी दलों ने एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, उन्हें डर है कि यह आगामी विधानसभा चुनावों के बीच एक बड़ी साज़िश का हिस्सा हो सकता है. गुप्ता, जो महिला सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर अपने ध्यान के लिए जानी जाती हैं, ने ऐसे कार्यक्रमों को जारी रखने की कसम खाई और कहा, "हमले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को नहीं रोक सकते".
राहुल गांधी का सवाल: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां 'छिपे' हैं और चुप क्यों हैं?
द हिंदू के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से सार्वजनिक जीवन से दूर रहने पर सवाल उठाया है. बुधवार को विपक्ष के संयुक्त उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के सम्मान समारोह में बोलते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि धनखड़ के पद छोड़ने के पीछे एक "कहानी" है और वह आश्चर्यचकित हैं कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां "वह एक शब्द भी नहीं कह सकते" और उन्हें "छिपना पड़ रहा है". लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "पुराने उपराष्ट्रपति कहां गए. वह छिपे क्यों हैं?". उन्होंने कहा कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, के.सी. वेणुगोपाल ने उन्हें बताया कि उपराष्ट्रपति "चले गए". राहुल गांधी ने कहा कि धनखड़, जो राज्यसभा में 'गरजते' थे, अब 'पूरी तरह से चुप' हो गए हैं. बाद में उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में भी यही सवाल दोहराया. गौरतलब है कि धनखड़ ने 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था, जबकि ऐसे संकेत थे कि सत्तारूढ़ दल के साथ उनके बिगड़ते संबंधों ने उन्हें पद छोड़ने के लिए प्रेरित किया होगा.
वैकल्पिक मीडिया
कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण, कैबिनेट ने 6:6:5 फॉर्मूला मंजूर किया
द मूकनायक के मुताबिक कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार रात एक लंबी कैबिनेट बैठक के बाद अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के लिए आंतरिक आरक्षण का एक नया फॉर्मूला तय किया है. इसके तहत राज्य में एससी वर्ग के लिए मौजूद 17% आरक्षण को तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुए इस फैसले के अनुसार, सबसे पिछड़े दलित समुदायों (दलित लेफ्ट, जैसे माडिगा) को 6% आरक्षण मिलेगा, जबकि सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत आगे माने जाने वाले दलित राइट (जैसे होलेया) को भी 6% आरक्षण दिया जाएगा. बाकी बचे 'स्पर्श योग्य' और अन्य एससी समूहों को 5% आरक्षण मिलेगा. यह निर्णय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एच.एन. नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका गठन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 के फैसले के बाद किया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर आंतरिक आरक्षण लागू करने की अनुमति दी थी. दलित लेफ्ट समुदाय, जो लंबे समय से आरक्षण के लाभ से वंचित महसूस कर रहे थे, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में आंतरिक आरक्षण लागू करने का वादा किया था और यह कदम उसी वादे को पूरा करने की एक कोशिश है. इससे पहले, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी आंतरिक आरक्षण का प्रयास किया था, लेकिन वह लागू नहीं हो सका था. इस नए 6:6:5 फॉर्मूले का उद्देश्य दलित लेफ्ट और दलित राइट समूहों के बीच राजनीतिक संतुलन साधना है.
पीएम मोदी की डिग्री: दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला टाला दिल्ली हाई कोर्ट आज उस याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला था, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के दिल्ली विश्वविद्यालय को 1978 में बीए परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी. इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी.हालांकि, आज अदालत ने फैसला नहीं सुनाया. जस्टिस सचिन दत्ता आज बेंच की अध्यक्षता नहीं कर रहे थे और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत अब 25 तारीख को फैसला सुना सकती है.दिल्ली विश्वविद्यालय ने तर्क दिया है कि सार्वजनिक हित के अभाव में "केवल जिज्ञासा" छात्रों की जानकारी का खुलासा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है.
नारियल तेल की कीमत दो साल में लगभग तीन गुना महंगा नारियल तेल की मजबूत मांग बनी हुई है, लेकिन प्रतिकूल मौसम, पेड़ों के अपर्याप्त पुनर्रोपण और बेहतर बीज प्रकारों की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इन कारणों से भारत में दो साल से भी कम समय में इस वस्तु की कीमतें लगभग तीन गुना बढ़ गई हैं. यह "कीमत के प्रति सचेत उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, और जो इसके विशिष्ट स्वाद के आदी हैं... उन्हें विकल्प खोजने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ रही है." कच्चे फल के पानी, खोपरा, दूध और पाउडर जैसे अन्य नारियल उत्पादों की कीमतें भी प्रभावित हुई हैं.
गुजरात के स्कूल में बुर्का पहनी लड़कियों को ‘आतंकवादी’ के रूप में दिखाने पर विवाद
गुजरात के भावनगर में एक प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रस्तुत एक नाटक में बुर्का पहनी हुई लड़कियों को “आतंकवादी” के रूप में दिखाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. शिक्षा विभाग ने इस बारे में रिपोर्ट मांगी है. स्थानीय मुसलमानों ने 'संविधान बचाओ समिति' के बैनर तले अधिकारियों से अपील की कि विद्यालय के शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस नाटक के माध्यम से उनके समुदाय को “गलत तरीके” से पेश किया गया.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस नाटक के वीडियो में कुछ लड़कियां सफेद कपड़ों में एक गीत पर प्रदर्शन करती दिखाई देती हैं, जिसमें कश्मीर की खूबसूरती का बखान किया गया है. कुछ ही पलों बाद तीन लड़कियां बुर्का पहनकर हाथों में “बंदूकें” लिए मंच पर आती हैं और बाकी पर “गोलीबारी” करती हैं, जबकि पृष्ठभूमि में बजती ऑडियो में यह कहा जाता है कि “आतंकवादियों ने पहलगाम हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी.” स्कूल ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के समारोह में “ऑपरेशन सिंदूर” पर आधारित यह नाटक आयोजित किया था.
सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या देश अब तक संविधान निर्माताओं की अपेक्षा पर खरा उतरा है?
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या देश अब तक संविधान निर्माताओं की उस अपेक्षा पर खरा उतरा है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बना रहेगा और दोनों सत्ता केंद्रों के बीच विभिन्न मुद्दों पर परामर्श होगा?
सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान बेंच ने यह टिप्पणी उस समय की जब केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपाल की नियुक्ति और अधिकारों से संबंधित संविधान सभा की बहसों का उल्लेख किया. बेंच को मेहता ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर की गई आलोचना के विपरीत, राज्यपाल का पद राजनीतिक शरण लेने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इसके तहत संविधान प्रदत्त कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं.
राष्ट्रपति संदर्भ पर अपनी दलीलें जारी रखते हुए, जिसमें यह संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अदालत राज्यपालों और राष्ट्रपति पर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से निपटने के लिए समय सीमा थोप सकती है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका पर व्यापक बहस हुई थी, जिसमें संविधान की संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखा गया था.
बेरोज़गारी दर पर सरकार के दावे क्यों मेल नहीं खाते
ब्लूमबर्ग ने अर्थशास्त्री अमित बसोले के हवाले से बताया है कि सरकार के बेरोज़गारी दर के 5.6% से घटकर 5.2% होने के दावे क्यों मेल नहीं खाते. नई श्रम रिपोर्ट में पिछले सप्ताह में कम से कम एक घंटे काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोज़गार में गिना जाता है, जिसमें अवैतनिक पारिवारिक श्रम भी शामिल है. यद्यपि यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानदंडों का पालन करती है, लेकिन यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, जहां अधिकांश नौकरियाँ अनौपचारिक हैं. बसोले ने कहा कि नौकरी की एक उदार परिभाषा बेरोज़गारी का "रूढ़िवादी अनुमान" देती है. उन्होंने कहा कि 1.4 अरब लोगों के देश में, नौकरी का गलत आकलन नीतिगत हस्तक्षेपों में एक बेमेल पैदा कर सकता है. बसोले ने कहा, "हमें अल्परोजग़ार के विश्वसनीय संकेतकों की आवश्यकता है."
बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण
भारत ने बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण क्षेत्र से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका ऐलान रक्षा मंत्रालय ने किया. परीक्षण ने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया. इसे सामरिक बल कमान के तत्वावधान में अंजाम दिया गया. यह मिसाइल ध्वनि की गति से 24 गुना तेज गति तक पहुंचने में सक्षम है और 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है. इसकी पहुंच में लगभग पूरा एशिया, जिसमें उत्तरी चीन भी शामिल है, तथा यूरोप के कुछ हिस्से आते हैं. अग्नि-1 से 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 3,500 किलोमीटर तक है और इन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है.
टीआरपी घोटाला: नाविका कुमार के खिलाफ़ जांच का आदेश दिया
दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को टाइम्स नाउ ग्रुप की एडिटर-इन-चीफ नाविका कुमार के खिलाफ़ जांच करने का आदेश दिया है. यह आदेश एआरजी आउटलायर मीडिया (जो अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी चलाता है) के उन आरोपों के संबंध में है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 2020 में कथित टीआरपी घोटाले से संबंधित गोस्वामी के बारे में मानहानिकारक बयान दिए थे.
भारतीय थिंक-टैंक की दुनिया में हलचल: अडानी बनाम अंबानी
भारतीय थिंक-टैंक की छोटी और लाड़-प्यार वाली दुनिया में उथल-पुथल है. इस साल की शुरुआत में, अडानी समूह ने चिंतन रिसर्च फाउंडेशन (सीआरएफ) की स्थापना की, जो मुकेश अंबानी द्वारा स्थापित ओआरएफ (ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन) जैसा लगता है. अब दक्षिणपंथी इकोसिस्टम के एक वर्ग ने ओआरएफ पर निशाना साधना शुरू कर दिया है.
विवादों में मराठी फिल्म 'खालिद का शिवाजी', प्रदर्शन पर एक महीने की रोक
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हिंदुत्व समूहों के विरोध के बाद एक मराठी फिल्म 'खालिद का शिवाजी' के प्रदर्शन को एक महीने के लिए 'निलंबित' कर दिया है. अज़ीब अहमद बताते हैं कि शिवाजी समर्थक फिल्म ने उन्हें क्यों नाराज़ किया है: "यह फिल्म खालिद नाम के एक मुस्लिम लड़के की कहानी बताती है जो शिवाजी की प्रशंसा करता है और उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेता के रूप में प्रस्तुत करता है."
असम पुलिस ने 'द वायर' के खिलाफ़ दूसरी 'राजद्रोह' की प्राथमिकी सार्वजनिक की
असम पुलिस द्वारा 'द वायर' के सह-संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और एंकर करण थापर को दूसरे 'राजद्रोह' मामले में तलब करने के सात दिनों से अधिक समय बाद, समाचार साइट आज एफआईआर की एक प्रति डाउनलोड करने में सक्षम हुई. यह समन उसी दिन जारी किया गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी. 9 मई को बिजू वर्मा की शिकायतों पर दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकी, 'द वायर' के पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कवरेज के खिलाफ़ है. यह प्राथमिकी सेना और खुफिया एजेंसियों में सेवा दे चुके लोगों सहित 11 स्तंभकारों को एक तदर्थ जांच की संभावना के लिए खोलती है, क्योंकि उनके लेखों और साक्षात्कारों को भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला बताया गया है. प्रेस निकायों और अखबारों के संपादकीय ने इन एफआईआर को मीडिया की स्वतंत्रता पर एक प्रहार के रूप में निंदा की है.
5 साल में 3700 से अधिक लोग गर्मी-लू से मरे : भारत में 2018 से 2022 के बीच गर्मी या लू से 3,700 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. यह जानकारी बुधवार को संसद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में दी गई. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया कि गर्मी से संबंधित मौतों की संख्या 2018 में 890, 2019 में 1,274, 2020 में 530, 2021 में 374 और 2022 में 730 रही.
548 करोड़ : शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष भेजने पर : भारत ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) भेजने वाले Axiom-4 मिशन पर 548 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. यह जानकारी भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी. शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट थे, जिन्होंने अंतरिक्ष में 18 दिन बिताए. यह सिर्फ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा एक निजी वाणिज्यिक अंतरिक्षयान में खरीदी गई सीट की लागत है, और कुछ नहीं.
ट्रम्प के टैरिफ के बाद भारत की मांग घटी, चीन ने खरीदा रूस का सस्ता तेल
सीएनएन में जॉन लियू की हांगकांग से रिपोर्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद भारत की मांग में गिरावट आई है, जिसका फायदा उठाते हुए चीनी रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल के नए ऑर्डर दिए हैं. यह तेल उन रूसी बंदरगाहों से भेजा जाएगा जो आमतौर पर भारत को आपूर्ति करते हैं. विश्लेषकों के अनुसार, चीनी रिफाइनरियों ने अक्टूबर और नवंबर डिलीवरी के लिए रूसी तेल के कम से कम 15 कार्गो हासिल किए हैं. 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल का बहिष्कार किए जाने पर चीन और भारत इसके सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे थे. हाल ही में, ट्रम्प ने रूसी तेल और गैस के आयात के लिए भारत के निर्यातों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की, जिसके कारण भारत ने अपनी खरीद में भारी कटौती की. केप्लर के विश्लेषकों का कहना है कि चीन का यह कदम "अवसरवादी" है, क्योंकि रूसी तेल की कीमत मध्य पूर्वी विकल्पों की तुलना में कम से कम $3 प्रति बैरल सस्ती बनी हुई है. हालांकि ट्रम्प ने चीन पर भी टैरिफ लगाने का संकेत दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए चीनी रिफाइनरियां इस अवसर का लाभ उठा रही हैं. विश्लेषकों का मानना है कि चीन अकेले भारत द्वारा छोड़े गए खालीपन को नहीं भर सकता, क्योंकि भारत रूस से प्रतिदिन लगभग 1.7 मिलियन बैरल खरीदता था, जबकि चीन लगभग 1.2 मिलियन बैरल खरीदता है.
दक्षिण चीन सागर में तनाव चरम पर, चीनी जहाजों की टक्कर ने बढ़ाई चिंता
एक्सियोस के रिपोर्टर कॉलिन डेमारेस्ट लिखते हैं कि दक्षिण चीन सागर में हाल ही में चीनी जहाजों के आक्रामक व्यवहार और आपस में टकराने की घटनाओं ने क्षेत्र में 'अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण' स्थिति पैदा कर दी है. फिलीपींस द्वारा जारी किए गए वीडियो, जिनमें चीनी पोत फिलीपीनी नावों को परेशान करते दिख रहे हैं, बीजिंग के बढ़ते नौसैनिक दबदबे और आक्रामकता को दर्शाते हैं. अगस्त के मध्य में हुई घटनाओं में एक चीनी कोस्ट गार्ड कटर और एक चीनी नौसेना के विध्वंसक का आपस में टकरा जाना, एक चीनी लड़ाकू जेट द्वारा पत्रकारों के विमान को रोकना और एक अमेरिकी युद्धपोत (यूएसएस हिगिंस) को डराने का चीनी दावा (जिसे अमेरिकी नौसेना ने खारिज कर दिया) शामिल है. फिलीपींस की यात्रा से लौटे अमेरिकी सीनेटर टॉड यंग ने क्षेत्र में ऊर्जा को "अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण" बताया. इन घटनाओं के जवाब में अमेरिका और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंध और मज़बूत हो रहे हैं. अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, जबकि फिलीपींस चीन की हरकतों का दस्तावेजीकरण करके दुनिया के सामने ला रहा है, जिसे सीनेटर यंग ने "प्लेबुक लिखना" कहा है. दूसरी ओर, चीन भूमि सुधार, सैन्य किलेबंदी और जहाज निर्माण के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे इस रणनीतिक जलमार्ग में टकराव का खतरा बढ़ गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इस व्यवहार के पीछे प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना, अमेरिका और उसके सहयोगियों को बाहर धकेलना और अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना जैसे कई कारण हैं.
रूस यूक्रेन के बीच समझौता बहुत मुश्किल है
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में मैं अक्सर ये पॉडकास्ट सुनता हूँ. द रेस्ट इज पॉलिटिक्स टोनी ब्लेयर के संचार प्रमुख रहे एलेस्टेयर कैम्पबेल और पूर्व ब्रिटिश राजनयिक रोरी स्टीवर्ट का संवाद है. वे नेताओं के दिमाग में घुस कर, बहुत कौतुहल के साथ, ब्यौरे बताते हुए एक तस्वीर बनाते हैं, जो न सिर्फ रोचक है, बल्कि जानकारीवर्धक भी. कैम्बेल लेबर पार्टी से जुड़े रहे हैं और स्टीवर्ट कंजरवेटिव. इस बार का उनका शो जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के वाशिंगटन डीसी आकर ट्रम्प से मिलने के बारे में है. उनकी बातचीत हाल में हुई मुलाक़ातों, दाँव-पेंचों और उससे जुड़े ड्रामे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें कई मज़ेदार और हैरान करने वाले पहलू भी शामिल हैं.
शुरुआत ट्रम्प और पुतिन की अलास्का में हुई बैठक के ज़िक्र से होती है. उनके मुताबिक एक ऐसी वार्ता जिसने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी. वे बताते हैं कि इस बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोप के दूसरे नेता नेता इतने घबरा गए कि वो फ़ौरन अपना सब काम छोड़कर प्लेन पकड़कर व्हाइट हाउस पहुँच गए. रोरी का मानना है कि ट्रम्प हमेशा से एक ऐसे 'लुढ़कते हुए पत्थर' (rolling boulder) की तरह हैं जो पुतिन की दिशा में ही जा रहा है. उनका कहना है कि ट्रम्प का 24 घंटे में जंग ख़त्म करने का वादा असल में पुतिन को वो सब कुछ देने का वादा था जो वो चाहते हैं. इस पूरे खेल में सिर्फ़ एक ही सवाल है कि क्या पुतिन पर भरोसा किया जा सकता है, और मज़े की बात ये है कि ट्रम्प ही अकेले ऐसे शख़्स हैं जो उन पर भरोसा करने को तैयार दिखते हैं.
ट्रम्प ने अलास्का बैठक से कुछ ही दिन पहले यूरोपीय नेताओं से वादा किया था कि वे पुतिन के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन पुतिन से मिलते ही पलट गए. कैम्पबेल बताते हैं कि यूरोप के नेताओं को पता है कि तारीफ़ के भूखे ट्रम्प को मनाना आसान है और वो हैं, इसलिए उन्होंने वाशिंगटन जाकर उनकी थोड़ी-बहुत चापलूसी की. बातचीत का एक मज़ेदार हिस्सा ये था कि कैसे इस दौरान ट्रम्प के कट्टर समर्थक और उप राष्ट्रपति जे डी वेंस को 'बच्चों वाली टेबल पर बिठा दिया गया, यानी उन्हें बड़े नेताओं की बातचीत से दूर रखा गया. इन नेताओं ने ट्रम्प को घेरकर अपनी बातें मनवाने की कोशिश की, जैसे फ्रांस के मैक्रोन ने साफ़ कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा पूरे यूरोप की सुरक्षा है और हमें भी बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए.
रोरी एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं. वो कहते हैं कि कहीं हम ट्रम्प को ग़लत तो नहीं समझ रहे? क्या हो अगर पुतिन ने ट्रम्प को हराया ही नहीं, बल्कि ट्रम्प चाहते ही यही थे? शायद उन्हें यूक्रेन, नाटो, या यूरोप की कोई परवाह ही नहीं है और उनका मन कहता है, "भाड़ मे जाए यूक्रेन, ये तो वैसे भी रूस का ही हिस्सा है." हो सकता है कि वो तो बस रूस के साथ अच्छे रिश्ते और कारोबार चाहते हैं. इस नज़रिए से देखें तो ट्रम्प भोले नहीं, बल्कि यूरोप की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से उदासीन (indifferent) हैं. वो पुतिन के साथ इसलिए नहीं जा रहे कि उन्हें धोखा मिला, बल्कि इसलिए कि उन्हें फ़र्क़ ही नहीं पड़ता.
इसी बीच, रूस का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है. पुतिन की सेना यूक्रेन से दोगुनी रफ़्तार से सैनिकों की भर्ती कर रही है और मोर्चों पर भी बढ़त बना रही है. इस आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबूत पुतिन के क़रीबी दिमित्रि मेडवेडेव का एक ट्वीट था, जिसमें उन्होंने जेलेंस्की को ‘कीव का जोकर' कहा और यूरोपीय नेताओं का मज़ाक़ उड़ाया कि वो ट्रम्प की चापलूसी कर रहे थे. ये दिखाता है कि रूस को लगता है कि वो ये जंग जीत रहे हैं और उन्हें किसी की परवाह नहीं है.
जब बात शांति समझौते की आती है, तो रोरी का मानना है कि कोई डील होगी ही नहीं. एक तरफ़ रूस समर्थक सौदा है, जिसमें पुतिन को ज़मीन मिले और यूक्रेन को सेना रखने से मना कर दिया जाए. दूसरी तरफ़ यूक्रेन समर्थक डील है, जिसमें उसे नाटो में शामिल होने की आज़ादी मिले. रोरी को लगता है कि ये सब बातें ही हैं. असल में ये मामला एक बर्फीले संघर्ष में बदल जाएगा, ठीक साइप्रस की तरह, जहाँ दशकों से विवाद चल रहा है. जेलेंस्की के लिए अपनी ज़मीन देना आत्मघाती होगा, इसलिए वो कभी नहीं मानेंगे, चाहे ट्रम्प कितना भी दबाव डालें.
पॉडकास्ट का आख़िरी और सबसे मज़ेदार हिस्सा तब आता है जब कैम्पबेल एक ताबड़तोड़ आइडिया देते हैं. वे जानते हैं कि ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार की कितनी ज़्यादा चाह है. वे कहते हैं कि ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक संस्था यूएसएड को दे देना चाहिए, जिसने दुनिया भर में ग़रीबी और भुखमरी मिटाकर युद्ध रोकने में मदद की है. और मज़े की बात ये कि पुरस्कार लेने के लिए ट्रम्प को न्यौता दिया जाए! विश्व राजनीति इतने गंभीर मुद्दों के बीच भी ड्रामा, थिएटर और एबसर्डिटी से भरी हुई है.
इसके पिछला वाला पॉडकास्ट भी मस्त था, जो अलास्का में पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात का विश्लेषण कर रहा था.
पाठकों से अपील :
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.