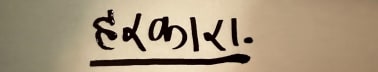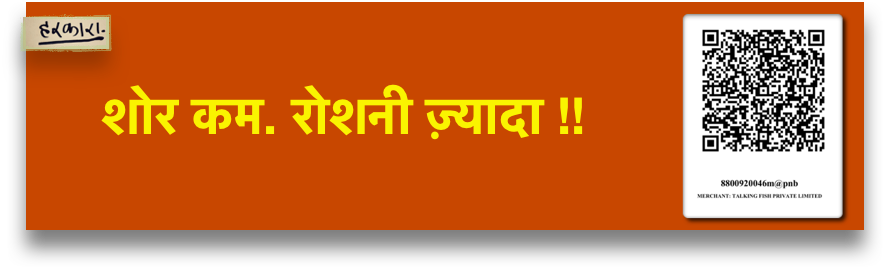25/11/2025 : जुबीन की हत्या की तसदीक | 17 बीएलओ की मौत, देश में एसआईआर | पूजा में शामिल नहीं तो फौजी अफसर बर्खास्त | कश्मीर को लेकर यूएन में फिक्र | पत्रकारिता मुश्किल करती सरकार | हिडमा और बस्तर
‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.
निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फ़लक अफ़शां
आज की सुर्खियां
यूपी में बीएलओ की आत्महत्या से हड़कंप; परिजनों का आरोप, अब तक 17वीं मौत
राहुल गांधी का हमला: एसआईआर ने फैलाई अराजकता, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
ममता का पलटवार: बीजेपी खुद को आयोग न समझे, बंगाल में सीएए का डर फैलाया जा रहा
बंगाल में बीएलओ की मौतों पर ‘अमानवीय दबाव’ का आरोप, ऐप की खामियों से बढ़ी परेशानी
असम सीएम का दावा: ज़ुबीन गर्ग की मौत हादसा नहीं, हत्या; एसआईटी करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एकेश्वरवादी ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी सही, सेना के लिए अयोग्य
नेहरू आर्काइव का खुलासा: ‘वंदे मातरम’ की धुन पर नेहरू की राय और ऐतिहासिक दस्तावेज़
डेटा संरक्षण नियम: सरकार को मिली खुली छूट, खोजी पत्रकारिता पर मंडराया खतरा
सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट: जाति पर न्यायिक फैसलों में विरोधाभास, पदानुक्रम से गरिमा तक का सफर
कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन: यूएन विशेषज्ञों ने जताई चिंता, 2800 गिरफ्तारियों पर सवाल
हरकारा डीप डाइव: हिडमा की मौत और बस्तर में शांति की अधूरी कोशिश का सच
यूक्रेन शांति वार्ता: अमेरिका और रूस के बीच अबु धाबी में गुप्त बैठक, 19 बिंदुओं पर चर्चा
भारत की घटती आबादी: गिरती जन्मदर ने भविष्य पर खड़े किए गंभीर सवाल
भारत के वन: बढ़ते आंकड़ों का भ्रम और प्राकृतिक जंगलों के गायब होने का सच
यूपी में बीएलओ ने जहर खाकर जान दी; परिजनों ने लगाया दबाव का आरोप, देश भर में अब तक 17वीं मौत
उत्तरप्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ड्यूटी में तैनात एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मंगलवार को कथित तौर पर जहर खाने से मौत हो गई. कथित तौर पर अब तक देश भर में बीएलओ की यह सत्रहवीं मौत है. मृतक विपिन यादव जैतपुर माझा के एक सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे. घटना के बाद विपिन की पत्नी सीमा यादव द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. इसमें, विपिन ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर उन पर तरबगंज के एसडीएम, नवाबगंज के बीडीओ, और एक स्थानीय लेखपाल का लगातार दबाव था. हालांकि, जिला प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया.
“फ्री प्रेस” के मुताबिक, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इन दावों को गलत बताते हुए कहा कि शिक्षक “परिवार संबंधी तनाव” में था और उसे ये आरोप लगाने के लिए उकसाया गया होगा. उन्होंने आगे कहा कि विपिन ने अपने आवंटित बूथ पर पर्याप्त काम पूरा कर लिया था और उन्हें किसी भी आधिकारिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा. जिलाधिकारी ने यह भी संकेत दिया कि जांच में विपिन की पत्नी की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.
इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की कड़ी आलोचना की है. उनका आरोप है कि इसके कारण अराजकता फैली है और तीन सप्ताह में 16 बीएलओ की मौत हुई है.
गांधी ने अपने “एक्स” हैंडल पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा, “एसआईआर की आड़ में देश भर में अराजकता फैलाई गई है. हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्याएं– एसआईआर कोई सुधार नहीं, यह एक थोपा गया अत्याचार है.”
उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की प्रणाली नागरिकों को 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन किए गए पन्नों को देखने के लिए मजबूर करती है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को थकाना और वोट चोरी को सुविधाजनक बनाना है. उन्होंने भारत की आईटी शक्ति की तुलना चुनाव आयोग की कागज-आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भरता से की.
भाजपा अपने दफ्तर में तय कर रही सूची, बीजेपी आयोग बना ईसीआई
उधर बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘एसआईआर’ को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक एसआईआर पूरा होने में तीन साल लगते हैं. हमने इसका कभी विरोध नहीं किया, बस इतना ही कहा कि किसी भी वास्तविक वोटर का नाम नहीं काटा जा सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने दफ्तर में बैठकर सूची तय कर रही है. चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते कहा कि उसका काम निष्पक्ष रहना है, बीजेपी कमीशन बनना नहीं. अगर आप (मतदाता) अवैध हैं, तो 2024 में आपने जिस सरकार को वोट दिया था, वह भी अवैध है. उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है और यह पूरी कवायद राजनीतिक मकसद से की जा रही है. उन्होंने कहा, “बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती. अगर उसने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की, तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी.” ममता ने दावा किया कि अगर राज्य के मतुआ बहुल क्षेत्रों में मतदाता नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत खुद को विदेशी घोषित करते हैं, तो उन्हें तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा. सुभेन्दु मैती के मुताबिक, उनका आरोप था कि भाजपा सीमावर्ती क्षेत्रों में एसआईआर के जरिए सीएए लागू करने की कोशिश कर रही है.
बंगाल में काम के बोझ से बीएलओ की मौतें: ‘अमानवीय’ दबाव और ऐप की विफलता
‘द टेलीग्राफ ऑनलाइन’ में देबायन दत्ता और ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) पर काम का अत्यधिक दबाव जानलेवा साबित हो रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि दो महिला बीएलओ ने कथित तौर पर काम के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली है. जलपाईगुड़ी के मालबाजार की 46 वर्षीय शांति मुनी उरांव का शव पेड़ से लटका मिला. उनके पति सुक्कू एक्का ने बताया कि वह एक मतदाता के डेटा को लेकर बहुत परेशान थीं और उन्होंने पहले भी “असहनीय काम के दबाव” की शिकायत की थी. उनके परिवार का कहना है कि वह आईसीडीएस के साथ काम करती थीं और 2016 से बीएलओ थीं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से वह देर रात तक काम करती थीं और थकी हुई रहती थीं. उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया.
रिपोर्ट बताती है कि तकनीकी समस्याएं बीएलओ की मुश्किलें बढ़ा रही हैं. चुनाव आयोग का ऐप अक्सर क्रैश हो जाता है और यह कंप्यूटर के अनुकूल नहीं है, जिससे सारा डेटा फोन से ही भरना पड़ता है. कई बीएलओ तकनीक के जानकार नहीं हैं, जिससे डेटा एंट्री में ज्यादा समय लगता है. नादिया के कृष्णानगर की 51 वर्षीय बीएलओ रिंकू तरफदार की भी मौत हो गई. उनके पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा था, “मैंने 95 प्रतिशत ऑफ़लाइन काम पूरा कर लिया है, लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण मैं ऑनलाइन काम नहीं कर सकती. अगर मैं बीएलओ की ड्यूटी पूरी नहीं कर पाती, तो मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती.”
‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के अनुसार, बीएलओ की मौतें सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गुजरात, राजस्थान और केरल से भी ऐसी खबरें आई हैं. जयपुर में मुकेश जांगिड़ ने कथित तौर पर ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी, जबकि राजस्थान के सवाई माधोपुर में हरि ओम बैरवा की तनाव के कारण मृत्यु हो गई. बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि जो काम दो साल में होता है, उसे एक महीने में पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है. उन्हें खर्चों की प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है और अधिकारियों द्वारा लगातार समय सीमा पूरी करने के लिए धमकाया जा रहा है.
तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की आलोचना की है. पार्टी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि यह दबाव “अमानवीय” है. हालांकि, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही हैं और उन्होंने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा कि पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.
ज़ुबीन गर्ग की मौत ‘सीधी सीधी हत्या’, एक व्यक्ति ने हत्या की, बाकी ने सहयोग किया
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को विधानसभा में टिप्पणी की कि संगीत आइकन ज़ुबीन गर्ग की मौत एक व्यक्ति द्वारा की गई हत्या थी, और अन्य ने सिर्फ सहयोग किया था.
“द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, गर्ग की मौत पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा के दौरान सरमा ने जोर देकर कहा कि यह ‘सीधी सीधी हत्या’ का मामला था. सिंगर ज़ुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी. वह चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रस्तुति के लिए देश गए थे.
सरमा ने कहा, “विपक्षी दलों ने मुझ पर हमला बोला, यह पूछते हुए कि मैं यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकता हूं कि ज़ुबीन की हत्या की गई थी. लेकिन यह कोर्ट के रिकॉर्ड में है कि यह एक हत्या थी. हमने हत्या के आरोप में चार से पांच लोगों को नामजद किया है.”
बिना विवरण साझा किए, उन्होंने कहा कि गर्ग से जुड़ा एक षड्यंत्र कोविड महामारी से भी पहले शुरू हुआ था. उन्होंने संकेत दिया कि यह मौत वित्तीय मामलों से जुड़ी थी. हमारे पास सबूत हैं. इसलिए मैंने एसआईटी से कहा कि वे पहले 8 दिसंबर को हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल करें और फिर जांच का विस्तार करें, ताकि कोई बच न सके. विपक्षी दलों के सदस्यों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए नारे लगाए, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया और उनसे एसआईटी जांच पर भरोसा रखने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई सेना अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, कहा- सेना के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए अयोग्य
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ईसाई भारतीय सेना अधिकारी की सेवाओं की समाप्ति को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसे कथित तौर पर अपनी एकेश्वरवादी मान्यता का हवाला देते हुए रेजिमेंटल सर्व धर्म स्थल (जो प्रतीकात्मक रूप से सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है) में प्रवेश करने से मना करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था.
“द इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि कमालेसन सैकड़ों चीजों में एक उत्कृष्ट अधिकारी हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने अनुशासन और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए जानी जाने वाली भारतीय सेना के लिए अयोग्य है.”
कमालेसन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि कमालेसन को सर्व धर्म स्थल में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं थी. लेकिन, जिस जगह वह पंजाब में तैनात थे, वहां कोई सर्व धर्म स्थल नहीं था, बल्कि केवल एक गुरुद्वारा और एक मंदिर था, और अधिकारी ने केवल तभी मना किया जब उनसे गर्भगृह में प्रवेश करने और अनुष्ठान करने के लिए कहा गया, क्योंकि यह उनकी ईसाई एकेश्वरवादी मान्यताओं के विरुद्ध जाता.
‘वंदे मातरम’ राष्ट्रगान के रूप में व्यावहारिक नहीं, नेहरू आर्काइव में ऐतिहासिक दस्तावेज़
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती पर ‘द नेहरू आर्काइव’ लॉन्च किया गया है, जिसमें 77,000 पेज और 35,000 दस्तावेज़ मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं. इसमें नेहरू द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा गया एक पत्र भी शामिल है जिसमें उन्होंने ‘वंदे मातरम’ बनाम ‘जन गण मन’ पर चर्चा की थी. नेहरू ने लिखा था, “वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से गहराई से जुड़ा है... लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जो गीत आज़ादी की तड़प को दर्शाता है, वह ज़रूरी नहीं कि आज़ादी मिलने के बाद भी उपयुक्त हो. ‘जन गण मन’ में विजय और पूर्ति का भाव है. लेकिन मुख्य विचार संगीत है.” उन्होंने तर्क दिया था कि ‘वंदे मातरम’ की धुन आर्केस्ट्रा या बैंड के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है.
इस आर्काइव में मई 1949 में भारतीय सैनिकों को दिया गया नेहरू का भाषण भी है, जिसमें उन्होंने कश्मीर की रक्षा का संकल्प लिया था. उन्होंने कहा था, “हर राष्ट्र को खून, पसीने और आंसुओं से आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है... भारत कश्मीर की रक्षा के लिए तब तक दृढ़ है जब तक कि राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उसकी सीमाओं से बाहर नहीं हो जाता.” इसके अलावा, 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आयरलैंड के पूर्व राष्ट्रपति को लिखे पत्र में नेहरू ने चीन के आक्रमण को “विश्वासघात” बताया था.
यह आर्काइव जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं. इतिहासकार माधवन पालat और आदित्य मुखर्जी ने बताया कि यह आर्काइव शोधकर्ताओं और पत्रकारों के लिए एक प्रामाणिक स्रोत है, जहां हर शब्द को सर्च किया जा सकता है. इसमें नेहरू के विदेशी दौरों, विभाजन और पहले आम चुनाव से जुड़े दस्तावेज़ शामिल हैं.
नए डेटा संरक्षण नियम: नागरिकों की निजता से ऊपर ‘राज्य’, खोजी पत्रकारिता पर संकट
‘आर्टिकल-14’ की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर 2025 को मंज़ूर किए गए नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम नागरिकों की निजता पर राज्य को तरजीह देते हैं और खोजी पत्रकारिता को लगभग असंभव बनाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ये नियम 2023 के कानून को स्पष्ट करने के लिए लाए गए हैं, लेकिन ये नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं. जहां सरकार को तत्काल शक्तियां मिल गई हैं, वहीं नागरिकों के अधिकार—जैसे डेटा सुधारने या हटाने का अधिकार—2027 के मध्य तक प्रभावी नहीं होंगे. ‘द हिंदू’ के संपादकीय का हवाला देते हुए रिपोर्ट कहती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को तुरंत कमजोर कर दिया गया है.
नियम 23, सरकार को गूगल, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी भी जानकारी की मांग करने की अनुमति देता है और उन्हें उस व्यक्ति को सूचित करने से रोकता है जिसकी जानकारी मांगी गई है. इसके लिए किसी न्यायिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है. यह ‘मेटाडेटा’ तक बिना किसी निशान के पहुंच प्रदान करता है, जिससे पत्रकारों के स्रोतों और व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. विशेषज्ञों और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ने चेतावनी दी है कि पत्रकारों के लिए कोई छूट न होने के कारण, उन्हें अपनी जांच के दायरे में आने वाले लोगों से ही सहमति लेनी पड़ सकती है, जो खोजी रिपोर्टिंग को खत्म कर देगा.
‘डिजीपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन’ ने इसे “परोक्ष सेंसरशिप” करार दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नए नियमों के तहत डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाएगा, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करेगा. यानी जो सरकार सबसे बड़ी डेटा कलेक्टर है, वही निगरानी संस्था को नियंत्रित करेगी. पूर्व न्यायाधीश ए.पी. शाह ने चेतावनी दी है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में संशोधन पारदर्शिता के लिए एक बड़ा झटका है, जो अधिकारियों को “व्यक्तिगत डेटा” का हवाला देकर जनहित की जानकारी देने से मना करने की शक्ति देता है.
सुप्रीम कोर्ट की नई रिपोर्ट; जाति पर न्यायिक विमर्श में विरोधाभास
सुप्रीम कोर्ट के अनुसंधान और योजना केंद्र (सीआरपी) द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सात दशकों में जाति पर न्यायिक विमर्श विरोधाभासी आख्यानों से चिन्हित रहा है. ये आख्यान जातिगत पदानुक्रम की कड़ी निंदा से लेकर उन विवरणों तक फैले हुए हैं जो कलंक को सुदृढ़ करने या संरचनात्मक भेदभाव को कम करने का जोखिम उठाते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है, “यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति और हाशिए पर पड़े समूहों का न्यायिक विवरण महत्वपूर्ण मानक भार वहन करता है. वे इस बात को प्रभावित करते हैं कि कानून गरिमा, समानता, योग्यता और ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने तथा समावेशी विकास को सुविधाजनक बनाने में राज्य की भूमिका की कल्पना कैसे करता है.”
“मकतूब मीडिया” के मुताबिक, 2025 की यह रिपोर्ट 1950 से 2025 तक सकारात्मक कार्रवाई व्यक्तिगत कानूनों और जाति-आधारित अत्याचारों पर संविधान पीठ के फैसलों का विश्लेषण करती है, जिसका दायरा पांच या अधिक न्यायाधीशों की पीठों तक सीमित है. यह रिपोर्ट इस बात पर असंगतियों को उजागर करती है कि न्यायालय ने जाति को कैसे समझा है, उत्पीड़ित समुदायों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की गई भाषा और जाति-आधारित असमानताओं को दूर करने के लिए न्यायपालिका द्वारा समर्थित उपकरण क्या हैं.
अध्ययन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जाति का वर्णन पवित्रता और प्रदूषण में निहित एक कठोर, वंशानुगत पदानुक्रम के रूप में करने और इसे समय के साथ विकृत हुई मूल रूप से “सौम्य” व्यावसायिक प्रणाली के रूप में चित्रित करने के बीच बदलाव किया है. जबकि कई फैसलों में जाति को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन तक पहुंच को आकार देने वाली एक स्थायी संरचना के रूप में स्वीकार किया गया है, अन्य शास्त्रों पर आधारित आख्यानों का सहारा लेते हैं जो उत्पीड़न के वास्तविक अनुभवों को अस्पष्ट करते हैं.
धर्म और जाति पर भिन्न दृष्टिकोण
रिपोर्ट इस बात पर भी न्यायालय के भीतर अलग-अलग विचारों की ओर इशारा करती है कि क्या जाति केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित है या यह एक व्यापक सामाजिक घटना है, जो सभी धर्मों में व्याप्त है. कुछ पीठों ने जाति को हिंदू धर्मशास्त्र से जोड़ा, जबकि अन्य ने ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों के बीच भी जाति-समान पदानुक्रमों को पहचाना, यह देखते हुए कि धर्मांतरण जाति की पहचान या कलंक को समाप्त नहीं करता है.
भाषा और गरिमा का प्रश्न
उत्पीड़ित जाति समुदायों का न्यायालय ने कैसे वर्णन किया है, इसकी जांच करते हुए, रिपोर्ट में शुरुआती फैसलों से बदलाव देखा गया है. पहले के फैसलों में पितृसत्तात्मक रूपकों का इस्तेमाल किया गया था — जैसे कि नुकसान की तुलना “विकलांगता” से करना, “दौड़ के घोड़ों” की कल्पना को जगाना, या सकारात्मक कार्रवाई को “बैसाखी” कहना — जबकि बाद की राय में गरिमा की पुष्टि की गई, ऐतिहासिक भेदभाव को उजागर किया गया, और योग्यता के सामाजिक निर्माण की आलोचना की गई. लेखकों ने चेतावनी दी है कि पहले के सूत्र कलंक को पुन: उत्पन्न करने और आरक्षण को संवैधानिक गारंटी के बजाय दान के रूप में मानने का जोखिम उठाते हैं.
हरकारा डीप डाइव
शुभ्रांशु चौधरी: आदिवासी अधिकार, माओवादी दरार और टूटी हुई शांति की कोशिश
हरकारा डीप डाइव में पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी से लंबी बातचीत में बस्तर के आदिवासी नेता हिडमा की मौत की कहानी कई परतों में खुलती है. यह सिर्फ एक माओवादी कमांडर का अंत नहीं, बल्कि उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जिसमें आदिवासी मुद्दों को बार-बार दबाया गया और राजनीतिक तथा माओवादी दोनों नेतृत्व ने उन्हें लगातार पीछे धकेला.
शुभ्रांशु बताते हैं कि हिडमा की छवि हमेशा “खूंखार मास्टरमाइंड” के रूप में पेश की गई, जबकि असलियत कहीं अधिक जटिल थी. हिडमा स्थानीय आदिवासी समाज से आते थे और पिछले दो सालों में उन्होंने हथियारों से हटकर पेसा, फॉरेस्ट राइट्स और आदिवासी स्वशासन जैसे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता तलाशा. दक्षिण बस्तर की कई डिवीजनल कमेटियों ने भी पहली बार हथियारों को किनारे करने और राजनीतिक बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव लिखा, जिसे हिडमा ने आगे बढ़ाया.
लेकिन जैसा कि शुभ्रांशु बताते हैं, तेलुगु नेतृत्व वाले माओवादी शीर्ष ढांचे ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. दूसरी ओर सरकार ने भी शांति प्रक्रिया को आदिवासी मुद्दों पर आधारित करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई. बातचीत करने की तैयारी दिखाने के बावजूद हिडमा को बार-बार अनसुना किया गया.
इसी बीच संगठन के भीतर भी टूट बढ़ी. कई तेलुगु नेता सरेंडर कर चुके थे और अपने लिए सुरक्षित रास्ते बना रहे थे, जबकि आदिवासी लड़ाके पूरी तरह दो पाटों में पिसने लगे. शुभ्रांशु कहते हैं कि हिडमा अपनी शर्त पर, अपने मुद्दों पर और अपने समाज के लिए सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन यही बात उनके खिलाफ चली गई.
आखिर में हिडमा अकेले पड़ गए. जिस आंदोलन को आदिवासियों की रक्षा करनी थी, वही आंदोलन उनके अधिकारों की आवाज़ को कुचलता गया. सरकार भी उनसे संवाद करने के बजाय सिर्फ सैन्य सफलता पर केंद्रित रही. और इसी अविश्वास तथा सौदेबाजी के माहौल में हिडमा मारे गए. शुभ्रांशु के अनुसार, हिडमा की मौत उस आखिरी पुल को तोड़ देने जैसा है जिसके सहारे बस्तर के आदिवासी अपने मुद्दों को हिंसा से हटाकर संविधान की भाषा में ला सकते थे. अब आंदोलन लगभग खत्म दिखता है, लेकिन आदिवासी हक़ूक़ की लड़ाई वहीं की वहीं खड़ी है, अधूरी, अनसुनी और हाशिए पर.
यूक्रेन शांति योजना: अमेरिका और रूस के बीच अबु धाबी में गुप्त वार्ता
‘एक्सियोस’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल अबु धाबी में रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. यह कदम तब उठाया गया है जब अमेरिकी वार्ताकारों ने एक मसौदा शांति योजना पर यूक्रेन के साथ शुरुआती सहमति बना ली है. एक अमेरिकी अधिकारी और इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने यह पुष्टि की है. एक्सियोस ने बताया कि पिछले मंगलवार को जब उन्होंने इस योजना का खुलासा किया था, तब से कूटनीतिक हलचल मची हुई है. शुरुआत में यूक्रेन अमेरिकी योजना को लेकर चिंतित था, लेकिन जेनेवा में हुई बातचीत और संशोधनों के बाद अब वह आशावादी नज़र आ रहा है. ट्रम्प प्रशासन अब रूस को इस समझौते के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहा है.
ड्रिस्कॉल के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जेफ टॉल्बर्ट ने एक्सियोस को बताया कि ड्रिस्कॉल सोमवार को अबु धाबी पहुंचे और मंगलवार को रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की. टॉल्बर्ट ने कहा, “सेक्रेटरी ड्रिस्कॉल और उनकी टीम यूक्रेन में स्थायी शांति हासिल करने के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा कर रही है. बातचीत अच्छी चल रही है और हम आशावादी हैं.” एक सूत्र के अनुसार, यूक्रेनी सैन्य खुफिया प्रमुख जनरल काइरिलो बुडानोव के नेतृत्व में एक यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल भी अबु धाबी में है और अमेरिका व रूस दोनों की टीमों के साथ बातचीत कर रहा है. पोलिटिको ने सबसे पहले ड्रिस्कॉल की रूसी अधिकारियों के साथ वार्ता की खबर दी थी.
सूत्रों का कहना है कि यूक्रेनी और रूसी सैन्य खुफिया प्रमुख किसी अन्य विषय पर अबु धाबी में मिलने वाले थे, लेकिन ड्रिस्कॉल की यात्रा ने योजना बदल दी. जेनेवा वार्ता के दौरान, अमेरिका और यूक्रेन ने शांति ढांचे को 28 बिंदुओं से घटाकर 19 बिंदुओं तक सीमित कर दिया है. एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन ने सौदे पर सहमति दे दी है, बस कुछ “मामूली विवरण” बाकी हैं. यूक्रेनी अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि सबसे संवेदनशील क्षेत्रीय रियायतों के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच सीधे चर्चा होगी. साथ ही, नाटो के भविष्य और यूरोपीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को इस ढांचे से बाहर रखा गया है.
दूसरी ओर, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संकेत दिया कि यदि नया दस्तावेज़ उन समझौतों से अलग हुआ जो राष्ट्रपति पुतिन के अनुसार उन्होंने अलास्का में ट्रम्प के साथ किए थे, तो रूस इसे स्वीकार नहीं करेगा. इस बीच, रूस ने कीव सहित यूक्रेनी शहरों पर भारी ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखे हैं.
भारत की आबादी अब धीमी पड़ रही, गिरती जन्मदर ने खोले भविष्य के नए सवाल
स्क्रॉल में प्रकाशित डाटा फॉर इंडिया की संस्थापक रुक्मणि एस के लेख के अनुसार भारत की आबादी तेज़ी से बदल रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन इन बदलावों पर भारत में भी उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए. भारत की कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर अब राष्ट्रीय स्तर पर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे जा चुकी है, जिसका मतलब है कि जनसंख्या आने वाले वर्षों में स्थिर या कम हो सकती है.
शहरी भारत में यह गिरावट 2004 में आ गई थी और ग्रामीण भारत भी 2023 में यह और कम होगया है. गरीब परिवारों, कम शिक्षा वाले समुदायों, अनुसूचित जाति-जनजाति और मुस्लिम महिलाओं में जन्म दर अभी भी अन्य समूहों से ज़्यादा है, लेकिन सभी वर्गों में जन्म दर लगातार घट रही है. इतना ही नहीं, केरल और तमिलनाडु जैसे अमीर राज्यों में मुस्लिम महिलाओं की टीएफआर भी बिहार और यूपी की हिंदू महिलाओं से कम है, जो बताता है कि शिक्षा, आय और सामाजिक सुविधाएँ जन्म दर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं.
दक्षिण भारत के कई राज्यों में जन्म दर बहुत पहले ही कम हो गई थी. केरल में यह स्तर 1988 में, तमिलनाडु में 1993 में और आंध्र प्रदेश में 2004 में हासिल हो गया था. साल 2023 तक यूपी और बिहार को छोड़कर लगभग पूरे भारत में जन्म दर ‘रिप्लेसमेंट लेवल’ से नीचे पहुँच चुकी है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में जन्म दर गिरने का तरीका पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है.
यूरोप और अमेरिका में महिलाएँ देर से शादी करती हैं, करियर बनाती हैं और फिर बच्चे कम पैदा करती हैं. भारत में महिलाएँ आज भी 21 साल के आसपास पहला बच्चा पैदा करती हैं, लेकिन अब पहले की तरह तीन-चार बच्चे नहीं बल्कि दो बच्चों के बाद ही परिवार पूरा मान लेती हैं. इसलिए भारत में अंतिम बच्चे के जन्म की उम्र पाँच साल कम हो चुकी है, यानी महिलाएँ अपने सभी बच्चे 20s में ही पैदा कर देती हैं.
लेख में बताया गया है कि दुनिया में जन्म दर गिरने को लेकर जो लोकप्रिय थ्योरी है, कि महिलाओं के करियर और आज़ादी के कारण बच्चे कम होते हैं , वह भारत में बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि भारत की अधिकांश महिलाएँ आज भी लेबर फाॅर्स में शामिल नहीं हैं. फिर भी जन्म दर यूरोपीय देशों जितनी कम हो चुकी है.
अर्थशास्त्री डीन स्पीयर्स और माइकल गेरुसो की नई किताब आफ्टर द स्पाइक के अनुसार दुनिया भर में जन्म दर गिरने का कोई एक यूनिवर्सल कारण नहीं है. बहुत से देश बिना किसी सख़्त नीति के खुद ही कम जन्म दर तक पहुँच जाते हैं. भारत भी उसी वैश्विक परिवर्तन का हिस्सा है, जहाँ छोटे-बड़े बदलाव — बेहतर जीवन, शिक्षा, सुविधा, आराम, निजी समय, और आर्थिक अवसर, परिवारों को कम बच्चे पैदा करने की ओर ले जाते हैं.
लेखक बताते हैं कि दुनिया में जहाँ-जहाँ टीएफआर 1.9 से नीचे गई है, वहाँ फिर कभी आबादी स्थिर करने लायक स्तर तक नहीं लौटी. यानी एक बार जन्म दर नीचे चली जाए, तो उसे ऊपर लाना लगभग असंभव होता है.
संयुक्त राष्ट्र के 2024 के अनुमान बताते हैं कि अगले 75 साल भारत की जन्म दर धीरे-धीरे और घटती जाएगी और 2060 के आसपास भारत की आबादी कम होना शुरू हो सकती है. भारत के पुराने जनसंख्या प्रोजेक्शन बताते थे कि 2035 तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में टीएफआर 1.5 तक गिर जाएगी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि असल गिरावट इससे भी तेज़ है. आने वाले समय में इसका असर रोज़गार, अर्थव्यवस्था और खासकर महिलाओं के जीवन पर पड़ेगा. भारत में बहुत कम महिलाएँ घर के बाहर कमाई वाला काम करती हैं. 20 से 29 साल की उम्र में यह अंतर सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इसी समय वे गर्भावस्था और छोटे बच्चों की देखभाल में लगी होती हैं. अगर महिलाएँ कम उम्र में ही अपने बच्चे पैदा कर लेती हैं, तो उनके पास जल्दी काम पर लौटने का मौका बढ़ जाता है. लेकिन अगर पहला बच्चा देर से होता है, तो उनके काम पर वापस आने का समय भी आगे खिसक जाता है.
लेख का निष्कर्ष यह है कि भारत में गिरती जन्म दर को लेकर घबराहट से पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह बदलाव न किसी साज़िश का नतीजा है और न ही इसे आसानी से उलटा जा सकता है. यह वही वैश्विक प्रक्रिया है जिससे दुनिया गुज़र रही है. असली चुनौती यह है कि भारत बदलते जनसांख्यिक ढाँचे के हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, काम और सामाजिक सुरक्षा की योजना कैसे बनाए. यही वह समय है जब भारत को डेटा-आधारित गंभीर चर्चा की ज़रूरत है ताकि देश आने वाले जनसंख्या परिवर्तन से घबराए नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ सके.
पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, यातना और तोड़फोड़ पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चिंता जताई
संयुक्त राष्ट्र के कम से कम आठ विशेष प्रतिवेदकों ने यह दावा करते हुए शंका जताई कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय अधिकारियों द्वारा कश्मीर में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन किए गए हैं.
विशेषज्ञों ने कहा, “हम एक पर्यटक क्षेत्र पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और पीड़ितों, उनके परिवारों और भारत सरकार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. हालांकि, सभी सरकारों को आतंकवाद का मुकाबला करते समय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का सम्मान करना चाहिए.”
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के हवाले से मकतूब ने लिखा है कि हमले के बाद, भारतीय अधिकारियों ने जम्मू और कश्मीर में व्यापक अभियान शुरू किए, जिसके परिणामस्वरूप पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों सहित लगभग 2,800 व्यक्तियों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया. कुछ को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) या गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हिरासत में लिया गया और उन पर आरोप लगाए गए, जो बिना आरोप या मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देते हैं और इसमें आतंकवाद की अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक परिभाषाएं शामिल हैं. कुछ बंदियों को कथित तौर पर यातना दी गई, उन्हें अज्ञातवास में रखा गया, और उन्हें वकीलों और परिवार के सदस्यों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया.
विशेषज्ञों ने कहा, “हम मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत, हिरासत में संदिग्ध मौतें, यातना और अन्य दुर्व्यवहार, पीट-पीट कर हत्या, और कश्मीरी और मुस्लिम समुदायों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार की रिपोर्टों की निंदा करते हैं.” उन्होंने दंडात्मक घर ढहाने और जबरन बेदखली तथा मनमाने विस्थापन की रिपोर्टों को उजागर किया, जो कथित तौर पर आतंकवादियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के परिवारों को निशाना बनाते हैं, और जिन्हें अदालती आदेश या उचित प्रक्रिया के बिना अंजाम दिया जाता है.
विशेषज्ञों ने कहा, “इस तरह के कार्य सामूहिक दंड का गठन करते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के फैसले का उल्लंघन करते हैं, जिसमें पाया गया था कि इस तरह के विध्वंस असंवैधानिक हैं और जीवन के अधिकार तथा मानव गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जिसमें मनमानी विस्थापन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार शामिल है.”
विशेषज्ञों ने संचार ब्लैकआउट और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की. अधिकारियों ने कथित तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स सहित लगभग 8,000 सोशल मीडिया खातों को अवरुद्ध कर दिया. उन्होंने कहा, “ये उपाय अभिव्यक्ति, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता पर असमानुपातिक प्रतिबंध हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि हमलों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया देश के अन्य हिस्सों में भी महसूस की गई.
विशेषज्ञों के अनुसार, कश्मीरी छात्रों को निगरानी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकार ने विश्वविद्यालयों को उनका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया था. सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हस्तियों द्वारा भड़काई गई मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद भाषण और हिंसा को बढ़ावा मिला. गुजरात और असम में विध्वंस की सूचना मिली, जहां हजारों मुस्लिम घरों, मस्जिदों और व्यवसायों को नष्ट कर दिया गया. लगभग 1,900 मुसलमानों और रोहिंग्या शरणार्थियों को भी, अक्सर उचित प्रक्रिया के बिना, बांग्लादेश और म्यांमार निर्वासित कर दिया गया.
उन्होंने कहा, “इस तरह के निष्कासन गैर-प्रत्यावर्तन के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन करते हैं, जो उन व्यक्तियों को उन देशों में लौटाने से रोकता है जहां उन्हें उत्पीड़न, जीवन से मनमाने ढंग से वंचित होने, यातना, या अन्य गंभीर नुकसान का खतरा है.”
विशेषज्ञों ने जम्मू और कश्मीर में उल्लंघनों की लगातार प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिसमें इरफान मेहराज और खुर्रम परवेज़ सहित कई मानवाधिकार रक्षकों को दमनकारी सुरक्षा कानूनों के तहत वर्षों से मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है. “हम जम्मू और कश्मीर में मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को तत्काल बिना शर्त रिहा करने का आग्रह करते हैं.”
विशेषज्ञों ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह अपने आतंकवाद विरोधी कानूनों और प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप लाए और सभी कथित उल्लंघनों की स्वतंत्र रूप से जांच करे और अभियोजन सहित जवाबदेही सुनिश्चित करे.
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, “अत्यधिक आतंकवाद विरोधी उपाय न केवल मानव गरिमा, भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि प्रतिउत्पादक रूप से सामाजिक विभाजन और शिकायतों को बढ़ावा देते हैं जो आगे हिंसा में बदल सकते हैं.”
बयान में कहा गया है, “हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों से जम्मू और कश्मीर पर लंबे समय से चल रहे संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का आग्रह करते हैं, जिसने मानवाधिकारों के उल्लंघन और सीमा पार हिंसा के विनाशकारी चक्र को बढ़ावा दिया है.”
भारत के प्राकृतिक वन गायब हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का यह प्रश्न पूछा नहीं जा रहा
भारत के वनों पर “कार्बन कॉपी” की शृंखला के तहत एम. राजशेखर ने 5वीं रिपोर्ट में कई चिंताओं और बुनियादी सवालों को उजागर किया है. अंग्रेजी में राजशेखर की इस लंबी रिपोर्ट का हिंदी में सारांश प्रस्तुत है. वह लिखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है. आधिकारिक तौर पर, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की रिपोर्टों के अनुसार, देश का वन आवरण 1987 में 642,401 वर्ग किमी से बढ़कर 2023 में 715,342.61 वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%) हो गया है.
आंकड़ों का विरोधाभास और वास्तविक स्थिति
हालांकि, अन्य डेटासेट एफएसआई के दावों से असहमत हैं: राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) का अनुमान एफएसआई से लगभग 75,000 वर्ग किमी कम है, और यह दिखाता है कि देश वन आवरण खो रहा है, बढ़ नहीं रहा है. ग्लोबल फ़ॉरेस्ट वॉच 2020 में भारत के वन आवरण को एफएसआई के आंकड़ों से काफी कम, लगभग 15% (440,000 वर्ग किमी) बताता है. 2010 के एक शोध पत्र ने निष्कर्ष निकाला कि भारत के प्राकृतिक वन 1995 और 2005 के बीच 514,137 वर्ग किमी से घटकर 389,970 वर्ग किमी रह गए.
वन बहाली पर काम करने वाले जीवविज्ञानी बताते हैं कि एफएसआई की कार्यप्रणाली के कारण उसके आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाते हैं. आकार मायने रखता है: यदि क्रियाशील होने के लिए पर्याप्त बड़े वन क्षेत्रों (जैसे 1,000 वर्ग किमी से बड़े) की तलाश की जाए, तो भारत का वास्तविक वन आवरण देश के 1-10% तक गिर जाता है.
वनों की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का कारण
ऐतिहासिक विरोध: 1980 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने जब सघन वनों को केवल 10.7% बताया था, तब वन विभाग ने आपत्ति जताई थी, संभावित रूप से वनों की कटाई वाली भूमि को राजस्व प्रशासन को सौंपने से बचने और विफलताएं छिपाने के लिए.
वनीकरण प्रोत्साहन: कैम्पा (सीएएमपीए) एनएपी जैसे कार्यक्रमों से फंड तभी आता है जब वनीकरण कार्यक्रमों को सफल दिखाया जाता है, जिसके लिए वन आवरण में वृद्धि दिखाना आवश्यक है.
जलवायु परिवर्तन का प्रतिनिधित्व : हाल के दशकों में, भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक लड़ाकू के रूप में चित्रित करने की इच्छा, देश के वन आवरण अनुमानों को कम न होने देने का एक और कारण है. यह मुख्य रूप से कार्बन स्टॉक के बारे में है. 2021 में, एफएसआई के अनुमानों के अनुसार, 713,789 वर्ग किमी पर, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक 7.2 बिलियन टन है. देश ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड (CO2) समतुल्य का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की भी प्रतिबद्धता जताई है, जिसके लिए देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वनों के अधीन दिखाना आवश्यक है.
इन कारकों के कारण, एक दोहरा आंदोलन आकार ले चुका है: भारत मानवीय दबाव और परियोजनाओं के कारण प्राकृतिक वन खो रहा है, लेकिन वनों की एक ऐसी विस्तृत परिभाषा अपना रहा है, जिसमें वृक्षारोपण और चाय बागानों को भी वन माना जाता है, जिससे आधिकारिक संख्या बढ़ रही है. पूर्व महानिदेशक वीके बहुगुणा के अनुसार, वनों की स्थिति का आकलन कार्बन या पेड़ों की संख्या से नहीं, बल्कि आरक्षित और संरक्षित वनों की स्थिति से होना चाहिए, जो देश की 450 से अधिक नदियों का स्रोत हैं. उन्होंने अनुमान लगाया कि वास्तविक अच्छे वन भौगोलिक क्षेत्र का केवल 10 से 11 प्रतिशत हैं.
प्राकृतिक वनों के पतन के परिणाम
लगभग 10% या उससे कम वन आवरण देश के लिए गंभीर परिणाम लाता है. जल चक्र कमजोर हो रहा है. प्राकृतिक वनों के सिकुड़ने से उनकी पारिस्थितिक कार्यक्षमता गिर रही है. उदाहरण के लिए, अप्रैल 2024 में कावेरी नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र सूख गया.
आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है. गैर-इमारती वन उपज (एनटीएफपी) का संग्रह गिर रहा है, जिससे वनों में रहने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित हो रही है. पारिस्थितिक मोड़ बिंदु पर पहुंचने के साथ, वनों की विशेषताएं बदल रही हैं और मानव व गैर-मानव जीवन को सहारा देने की उनकी क्षमता कम हो रही है. उत्तरप्रदेश का सुहेलवा इसका उदाहरण है. रोगों का फैलाव हो रहा है. वनों के सिकुड़ने के साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हो रही है, और साथ ही क्यासानूर जैसे नई बीमारी के प्रकोप और मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है.
विकास परियोजनाओं और वन नुकसान की अनदेखी
वन विभाग की पुरानी कार्य योजनाएं और नौकरशाही की अस्वस्थता इस समस्या को बढ़ाती है. हम वन विखंडन, दशकों के बदलाव और जैव विविधता की स्थिति को नजरअंदाज करते हुए गैर-इमारती वन उपज संग्रह के लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वन भूमि का मार्ग बदल देते हैं.
कावेरी जलग्रहण क्षेत्र पर गौर किया जा सकता है. कोडागु (कावेरी का स्रोत) में रेल लाइनों, राजमार्गों और हाई टेंशन तारों के निर्माण के लिए 5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिससे कावेरी के 70% जलग्रहण क्षेत्र को नुकसान होगा. अन्य परियोजनाओं में ग्रेट निकोबार (130 वर्ग किमी वन नष्ट होगा), हसदेव अरण्ड, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, और केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना सहित कई बड़ी परियोजनाओं के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं.
आंकड़ों का प्रभाव: पर्यावरण मंत्रालय और एफएसआई द्वारा वन आवरण संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की यह सहवर्ती लागत है. जो देश मानता है कि वन उसकी भूमि का 21.76% कवर करते हैं, वह उनके प्रति उस देश की तुलना में अधिक लापरवाह होगा जिसका 10% वनों के अधीन है.
फिर भी भारत मौन है
ब्राजील की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (टीएफएफएफ) योजना, जो प्रति हेक्टेयर 4 डॉलर देती है, भारत में वनों की कटाई और वनीकरण के लिए मौजूद आर्थिक प्रोत्साहनों की तुलना में बहुत कम है (केवल ₹2,432 करोड़ वार्षिक भुगतान). वनीकरण योजना कैम्पा का आवंटन 2019-24 के बीच ₹38,516 करोड़ था, जो दर्शाता है कि वनों की कटाई और वनीकरण के आर्थिक प्रोत्साहन प्राकृतिक वनों की रक्षा के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक हैं. टीएफएफएफ भारत में काम नहीं करेगा.
वन विशेषज्ञ सुप्रभा सेशान के अनुसार, “एक बिंदु आएगा जिसके आगे चीजें बस हार मान लेंगी और तनाव के आगे झुक जाएंगी.” वनों के नुकसान और मौसम प्रणालियों पर उनके परिणामी प्रभावों के बीच संबंध भारत में विरले हैं.
राष्ट्रीय सुरक्षा में देश, उसके लोगों और उसकी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा शामिल है, फिर भी वनों के संबंध में भारत मौन है. एडुआर्डो गैलियानो की तरह, हम “मूर्खता से मिलती-जुलती चुप्पी बनाए रखे हुए हैं.” हमें याद रखना चाहिए कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पारिस्थितिकी के उपसमुच्चय हैं.
अपील :
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.