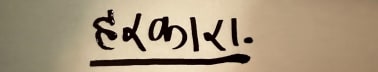27/07/2025: असंवेदनशील अदालतें! | केंचुआ का बिहारियों से धोखा | 66 लाख लोग हटे | चुनाव बायकॉट की दलील | बुलडोज़र काल में सियासी चुप्पी | शुक्ला जी के जलवे | गुरुदत्त का संगीत
‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.
निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल
आज की सुर्खियां :
गाज़ा की इस तस्वीर पर मुम्बई हाईकोर्ट के जज विचलित क्यों नहीं होते?
बिहार में नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया "मतदाताओं के साथ गंभीर धोखा" : एडीआर
66 लाख मतदाता बिहार SIR प्रक्रिया में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं
‘चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है, ऐसे में विपक्ष का चुनाव का बॉयकाट करना चाहिए’
बिहार में बढ़ते अपराधों पर बोले चिराग, मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करने का दुःख
विकास बराला की नियुक्ति पर पूर्व अधिकारियों का एतराज
ट्रम्प ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम फिर याद दिलाया
एनसीईआरटी स्कूलों में कराएगा ऑपरेशन सिंदूर की पढ़ाई
मध्य प्रदेश में कुपोषण की भयावह तस्वीर पर हाईकोर्ट सख्त, सभी कलेक्टर्स से रिपोर्ट तलब
बिहार में होमगार्ड की परीक्षा देने आई युवती के साथ एंबुलेंस में गैंग रेप
ओड़िशा में आदिवासी लड़कियों के सरकारी हॉस्टल में यौन शोषण के मामले
16-18 साल के किशोरों में सहमति से बने यौन संबंधों को 'शोषण' न माना जाए, इंदिरा जयसिंह का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष
सही समय पर सही जगह कैसे होना है, राजीव शुक्ला की तरक्की पर तरक्की का राज..
बंगाली मज़दूर को बंदूक की नोंक पर बांग्लादेश में धकेला गया
बुलडोज़र चलते रहेंगे और सियासी दल चुप रहेंगे!
पंकज राग: 'जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहां हैं' सामाजिक असमानता और मोहभंग को दर्शाते हैं
'द कॉल ऑफ म्यूजिक': हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया के अनकहे संघर्ष
गाज़ा की इस तस्वीर पर मुम्बई हाईकोर्ट के जज विचलित क्यों नहीं होते?
हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के 25 जुलाई को आए एक फैसले ने देशभर में एक नई बहस को जन्म दिया और वो क्या राष्ट की समस्याओं कों केन्द्र में रख ही नागरिक का वैश्विक नजरिया होना चाहिए? असल में कोर्ट ने माकपा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा गाजा पर एक रैली की अनुमति देने से इनकार को चुनौती दी गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को “देशभक्त बनने” और “भारत की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने” की सलाह दी. ये उस वक्त हो रहा था, जब दुनियाभर के बुद्धिजीवी, आर्टिस्ट और संवेदनशील नागरिक गाजा के पक्ष में अपने-अपने स्तर पर प्रतिरोध का स्वर बुलंद कर रहे हैं. गाजा में भूखमरी चरम पर पहुंच चुकी है. दुनिया के लोग तत्काल युद्धविराम के लिए मोर्चा खोले हुए हैं.
'द वायर' में सरयू पानी ने लिखा है कि कोर्ट की यह टिप्पणी दर्शाती है कि अदालत को न तो नरसंहार की गंभीरता की समझ है और न ही इस बात की कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में नागरिक समाज कैसे काम करता है. पिछले महीने गाजा को लेकर वैश्विक राय में बड़ा बदलाव आया है. कई संगठन जिन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी, अब खुलकर बोलने लगे हैं और इज़रायल के कृत्यों को नरसंहार की संज्ञा देने लगे हैं. 100 से अधिक मानवीय संस्थाओं ने मिलकर गाजा में सामूहिक भूखमरी की चेतावनी दी है. BBC, AFP, AP और Reuters जैसी एजेंसियों ने बयान जारी कर बताया कि उनके पत्रकार और उनके परिवार खुद भूखे मरने की कगार पर हैं. AFP ने पहली बार बयान देकर कहा कि उनके पत्रकारों की जान भूख से खतरे में है.
इस बीच, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे इज़रायल के समर्थक देशों ने भी तत्काल युद्धविराम की मांग की है. भारत ने भी, जो अभी हाल तक संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्धविराम प्रस्ताव पर अनुपस्थित था, अब स्थायी युद्धविराम और मानवीय सहायता की तत्काल आपूर्ति की मांग की है. हाई कोर्ट की टिप्पणी आश्चर्यजनक नहीं है. यह भारत में पिछले एक दशक में उभरी एक विशिष्ट 'एलीट सोच' को दर्शाती है. इसे तीन प्रमुख प्रवृत्तियों के संदर्भ में समझा जा सकता है: भारत में विदेश नीति को मीडिया और अदालतों द्वारा एक ऐसा विषय मान लिया गया है, जिस पर बहस या न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. सरकार की विदेश नीति की आलोचना को 'राष्ट्रविरोधी' कहा जाता है.
हाई कोर्ट ने माकपा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनकी फिलिस्तीन पर राय केंद्र सरकार से मेल नहीं खाती और वे “नहीं समझते कि यह देश की विदेश नीति को कितना नुकसान पहुंचा सकता है.” यह कोई पहली घटना नहीं है. सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी थी जिसमें भारत द्वारा इज़रायल को हथियार निर्यात रोकने की मांग की गई थी, यह कहते हुए कि अदालत विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
2006 मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 मुस्लिम पुरुषों को बरी कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने दोषी ठहराया था. अदालत ने कहा कि सबूत अपर्याप्त और गवाहों की गवाही विरोधाभासी है. यही बात अन्य मामलों - 2006 मालेगांव धमाके, 2002 अक्षरधाम हमले के दौरान भी देखी गई, जहां मुस्लिम अभियुक्तों को अंततः बरी किया गया. पत्रकार जोसी जोसेफ की किताब ‘द साइलेंट कू’ बताती है कि मीडिया ने कैसे खुफिया एजेंसियों से बिना पुष्टि के सूचना लेकर मुस्लिम आरोपियों को तुरंत 'आतंकवादी' घोषित कर दिया. दूसरी ओर, हिंदुत्व संगठनों से जुड़े मामलों को अलग नजर से देखा गया - उदाहरण के लिए प्रज्ञा ठाकुर, जो अब सांसद हैं.
इस सोच का नतीजा यह हुआ है कि फिलिस्तीन जैसे मुद्दों को, जो ऐतिहासिक रूप से उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के रूप में देखे जाते थे, अब ‘आतंकवाद’ के नजरिए से देखा जाने लगा है. मोदी शासन के दौरान नागरिक समाज को खास निशाना बनाया गया है. विदेशी फंडिंग पर रोक, एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी और कानून जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल इसके उदाहरण हैं. प्रधानमंत्री द्वारा 'आंदोलनजीवी' और 'अर्बन नक्सल' जैसे शब्दों के उपयोग ने सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को बदनाम करने और नागरिक सहयोग को खतरे में डालने का काम किया है. इसने संवेदनहीनता को बढ़ावा दिया है, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति.
इसका असर न्यायपालिका पर भी पड़ा है. मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारत सरकार पर रोहिंग्या शरणार्थियों को अंडमान सागर में छोड़ने का आरोप था. कोर्ट ने इसे “कल्पनाशील” और “सुंदर कहानी” बताया, जबकि यूएन ने इस पर चिंता जताई थी.
अंतरराष्ट्रीय कानून में जनसंहार की रोकथाम एक ‘jus cogens’ (अत्यावश्यक) सिद्धांत है, जिसे कोई भी समझौता या संधि दरकिनार नहीं कर सकती. सभी देशों पर यह बाध्यकारी होता है. इसका मतलब यह है कि कोई देश यह नहीं कह सकता कि क्योंकि यह नरसंहार उससे दूर हो रहा है, इसलिए यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है. यह हर देश और हर व्यक्ति की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है.
बिहार में नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया "मतदाताओं के साथ गंभीर धोखा" : एडीआर
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया "मतदाताओं के साथ गंभीर धोखा" है और यह सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों का उल्लंघन करती है.
अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में, एडीआर ने चुनाव आयोग द्वारा 21 जुलाई को दायर जवाब का जवाब दिया, जिसमें आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का बचाव किया था. आयोग ने कहा था कि यह पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए किया जा रहा है. बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 28 जुलाई को सुनवाई है. राज्य विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं.
सुचित्रा कल्याण मोहंती ने बताया है कि एडीआर ने अपनी प्रतिक्रिया में आयोग द्वारा आधार कार्ड, वोटर आईडी (एपिक) और राशन कार्ड को अकेले पहचान पत्र के रूप में स्वीकार न करने पर सवाल उठाया और इसे "स्पष्ट रूप से निरर्थक" बताया.
एडीआर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत बाकी 11 दस्तावेज भी जाली बनाए जा सकते हैं, ऐसे में उसकी यह दलील मनमानी और असंगत है कि आधार, एपिक और राशन कार्ड जालसाजी की दृष्टि से असुरक्षित हैं. एडीआर ने कहा, "यह स्थिति पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनावी धांधली की गंभीर आशंकाएं खड़ी करती है. कई मतदाताओं को बिना उनकी जानकारी या भागीदारी के उनके दस्तावेज अपलोड किए जाने की जानकारी मिली है."
एडीआर ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में जमीनी हकीकत चुनाव आयोग के दावों से अलग है. "कई कस्बों और गांवों से खबरें हैं कि एसआईआर प्रक्रिया मनमाने ढंग से, अवैध रूप से और आयोग की 24 जून की खुद की गाइडलाइन के खिलाफ चल रही है.
वरिष्ठ पत्रकारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एडीआर ने कहा, "बहुत जगह मतदाताओं की गैर-मौजूदगी में फार्म भरे जा रहे हैं. मतदाताओं को मैसेज मिल रहे हैं कि उनके दस्तावेज जमा हो गए हैं, जबकि उन्होंने कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की. कुछ मामलों में मृत व्यक्ति भी दस्तावेज जमा करने वाले दिखाए जा रहे हैं."
प्रत्युत्तर में यह भी कहा गया कि दस्तावेजों के जांच की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है. एसआईआर आदेश में दस्तावेज सत्यापन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जिससे निर्वाचन अधिकारियों (ईआरओ) को असीमित और अनियंत्रित अधिकार मिल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर वोटरों को बाहर किए जाने की आशंका है. एडीआर ने चुनाव आयोग के आकड़ों को भी भ्रामक बताया और कहा कि ड्राफ्ट रोल में नाम जुड़ना तब तक बेमतलब है, जब तक वैध दस्तावेज जमा न किए जाएं.
एडीआर के साथ इस याचिका में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, राजद सांसद मनोज झा, कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल और मुजाहिद आलम शामिल हैं.
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग का 24 जून 2025 का एसआईआर आदेश निरस्त करने की मांग की है. एडीआर की याचिका में कहा गया है कि "अगर इसे रद्द नहीं किया गया तो “एसआईआर’ आदेश लाखों वैध मतदाताओं को मनमाने ढंग से बाहर कर सकता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक बुनियाद कमजोर होगी.
66 लाख मतदाता बिहार SIR प्रक्रिया में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं
'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट है कि बिहार में चल रही विशेष तीव्र पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के अंतर्गत जारी चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 66 लाख मतदाता 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे. 2025 की मतदाता सूची के अनुसार, राज्य में कुल 7.89 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे. इनमें से 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त कर डिजिटल रूप से दर्ज किए जा चुके हैं, और ये नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होंगे. ECI ने बताया कि बाकी बचे मतदाताओं के फॉर्म की डिटाइजेशन प्रक्रिया भी 1 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी, साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की रिपोर्ट भी संलग्न की जाएगी. BLO रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 22 लाख मृतक मतदाताओं, 7 लाख ऐसे जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है और 35 लाख ऐसे मतदाता जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या जिनका पता नहीं चल सका — इन सभी को सूची से हटाया गया है. इसके अलावा, लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं.
विश्लेषण
‘चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली है, ऐसे में विपक्ष का चुनाव का बॉयकाट करना चाहिए’
भारतीय राजनीति में यह बहस लगातार तेज होती जा रही है कि क्या देश का चुनाव आयोग (EC) अपनी निष्पक्षता खो चुका है. विपक्ष बार-बार यह आरोप लगाता है कि चुनाव प्रक्रिया से छेड़छाड़ की जा रही है और संस्थाएं सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रही हैं. हाल ही में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर यह चिंता और भी गहरी हो गई है, जिसे विपक्ष मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की एक सुनियोजित साजिश के तौर पर देख रहा है. इन गंभीर आरोपों के बीच, एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष के पास इन चुनौतियों का कोई ठोस और प्रभावी जवाब है. पत्रकार और लेखक देबाशीष रॉय चौधरी का मानना है कि विपक्ष की मौजूदा रणनीति इन समस्याओं से निपटने के लिए अपर्याप्त है. अपनी पुस्तक 'टू किल ए डेमोक्रेसी: इंडिया'स पैसेज टू डेस्पोटिज्म' के लिए जाने जाने वाले देबाशीष ने हाल ही में फ्रंटलाइन पत्रिका के लिए एक लेख में यह तर्क दिया है कि अब विपक्ष के लिए चुनावों का बहिष्कार करना ही एकमात्र तार्किक और नैतिक रास्ता बचा है. उनका मानना है कि यह एक ऐसा कदम होगा जो भारतीय जनता को इन मुद्दों पर एक निर्णायक स्टैंड लेने के लिए मजबूर करेगा, जैसा कि अब तक नहीं हुआ है.
'द वायर' के कार्यक्रम "द इंटरव्यू विद करन थापर' में देबाशीष रॉय चौधरी अपने तर्क की शुरुआत इस बुनियादी सवाल से करते हैं कि यदि खेल पहले से ही धांधली भरा (rigged) है, तो उसमें हिस्सा लेने का क्या मतलब है. उनका कहना है कि जब विपक्षी दल यह दावा करते हैं कि चुनाव चोरी हो रहे हैं और फिर भी वे उन चुनावों में भाग लेते हैं, तो वे अनजाने में उस चोरी को ही वैधता प्रदान कर रहे होते हैं. इस प्रक्रिया को समझाने के लिए उन्होंने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का उदाहरण दिया, जिसकी प्रक्रिया खतरनाक रूप से असम के एनआरसी (NRC) जैसी दिखती है. असम में एनआरसी के कारण 19 लाख लोग मताधिकार से वंचित हो गए थे, जबकि बिहार में यह प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में पूरी की जा रही है, जिससे लाखों लोगों के नाम कटने का खतरा है. देबाशीष केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहते. वे महाराष्ट्र के पिछले चुनावों का भी उल्लेख करते हैं, जहां विपक्ष ने चुनाव आयोग पर "औद्योगिक पैमाने पर धांधली" और "मैच फिक्सिंग" का खुला आरोप लगाया था.
उनका मूल तर्क यह है कि चुनाव किसी भी लोकतंत्र का दिल और आत्मा होते हैं. यह जनता की इच्छा को जानने और यह तय करने का माध्यम है कि उन पर शासन कौन करेगा. यदि आपको यह विश्वास हो जाए कि यह पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है, तो लोकतांत्रिक राजनीति का कोई अर्थ नहीं रह जाता. ऐसी स्थिति में चुनाव में भाग लेना रणनीतिक और सामरिक रूप से एक गलत कदम है. यह ऐसा है जैसे आप यह जानते हुए भी मैच खेलने उतरें कि अंपायर बिका हुआ है और मैच पहले से ही फिक्स है. समझदारी इसी में है कि आप खेल से बाहर निकलें और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करें.
देबाशीष एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, जिसे वे "नैतिक भ्रम" (moral confusion) कहते हैं. जब विपक्ष एक तरफ कहता है कि चुनाव धांधली वाले हैं और लोकतंत्र मर चुका है, और दूसरी तरफ मतदाताओं से कहता है कि "आओ और हमें वोट दो", तो यह एक विरोधाभासी संदेश देता है. एक मतदाता के लिए यह स्थिति बहुत भ्रामक है. यदि व्यवस्था वास्तव में भ्रष्ट है और विपक्ष यह जानते हुए भी चुनाव लड़ रहा है कि वह हार जाएगा, तो यह एक तरह का पागलपन लगता है. मतदाता सोचेगा कि जब नतीजा पहले से तय है तो वह अपना वोट बर्बाद क्यों करे. यह संदेश न तो मतदाता को यह विश्वास दिलाता है कि व्यवस्था भ्रष्ट है, और न ही यह कि विपक्ष वोट देने लायक है. देबाशीष जोर देकर कहते हैं कि आप एक ही समय में चुनाव को धांधली भरा बताकर उसमें हिस्सा नहीं ले सकते. यह तार्किक रूप से असंगत और एक बहुत खराब राजनीतिक संदेश है.
इसके अलावा, देबाशीष विपक्ष की मौजूदा विरोध की रणनीति को "उलझा हुआ" (muddled) बताते हैं. वे कहते हैं कि चुनाव आयोग को लंबे-लंबे पत्र लिखना या उसके साथ अंतहीन बैठकें करना व्यर्थ है. यदि चुनाव आयोग वास्तव में भाजपा की कठपुतली है और चुनाव चोरी करने में मदद कर रहा है, तो उससे ही शिकायत करने का क्या औचित्य है. यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर में हुई चोरी की शिकायत चोर से ही करने जाएं. इन बैठकों और पत्रों से विरोध का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाने के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और यह रिकॉर्ड भी कोई ठोस बदलाव लाने में विफल रहा है.
इन समस्याओं के समाधान के रूप में, देबाशीष एक सीधा लेकिन नाटकीय रास्ता सुझाते हैं: चुनावों का बहिष्कार. वे कहते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम अदालत जनता होती है, इसलिए इस मुद्दे को जनता के पास ले जाना चाहिए. जब विपक्ष एकजुट होकर चुनावों का बहिष्कार करेगा, तो यह केवल एक राजनीतिक कदम नहीं होगा, बल्कि एक शक्तिशाली नैतिक बयान होगा. यह कदम चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगा. जब यह तर्क दिया जाता है कि बहिष्कार तो नरेंद्र मोदी और भाजपा को एकतरफा जीत सौंपने जैसा होगा, तो देबाशीष इसे खारिज कर देते हैं. वे कहते हैं कि ऐसी जीत एक "खोखली जीत" होगी. एक ऐसे चुनाव का परिणाम, जिसमें मुख्य विपक्ष ने भाग ही न लिया हो, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी. उन्होंने रवांडा का उदाहरण दिया, जहां राष्ट्रपति को 99% वोट मिलते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि इसका कोई मतलब नहीं है.
देबाशीष इस बात पर जोर देते हैं कि भारत की स्थिति बांग्लादेश जैसे देशों से बहुत अलग है, जहां विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद सरकार लंबे समय तक चलती रही. भारत का एक मजबूत लोकतांत्रिक इतिहास रहा है. यहां के लोगों ने 75 वर्षों से अधिक समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और उन्हें इस पर गर्व है. भारत की वैश्विक छवि एक जीवंत लोकतंत्र की है. यदि यहां विपक्ष के बिना चुनाव होते हैं, तो यह न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करेगा, बल्कि देश के भीतर भी एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संकट पैदा कर देगा. लाखों विपक्षी कार्यकर्ता, जिन्हें सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिलेगा, उनका गुस्सा और हताशा सार्वजनिक अशांति का कारण बन सकती है.
अंत में, देबाशीष का मानना है कि यह एक राजनीतिक लड़ाई है जिसे राजनीतिक रूप से सड़कों पर लड़ा जाना चाहिए, न कि चुनाव आयोग के दफ्तरों या अदालतों में. जब तक संस्थागत भ्रष्टाचार के आरोपों को जमीनी राजनीतिक कार्रवाई का समर्थन नहीं मिलता, वे खोखले लगते हैं. बहिष्कार एक ऐसा कदम है जो विपक्ष के जमीनी कार्यकर्ताओं को अभूतपूर्व रूप से सक्रिय कर देगा और जनता को यह समझने के लिए मजबूर करेगा कि दांव पर क्या लगा है. तेजस्वी यादव द्वारा बिहार चुनावों के बहिष्कार पर विचार करने की खबर पर, देबाशीष की सलाह स्पष्ट है: जल्दी फैसला करें. इस निर्णय में जितनी देर होगी, विपक्ष का पक्ष उतना ही कमजोर होता जाएगा. उनके अनुसार, देर-सवेर विपक्ष को चुनाव का बहिष्कार करना ही होगा, और यह आश्चर्य की बात है कि उन्हें यह समझने में इतना समय क्यों लग रहा है.
चौधरी ने कहा, “जब आपको पता है कि खेल तय हो चुका है, कि अंपायर भी उनके साथ है, तो आप क्यों खेल रहे हैं? इससे तो आप बस उनकी लोकतंत्र की नकल को वैधता दे रहे हैं.” उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक 'डेमोक्रेसी की झूठी छवि' बन चुका है, जहां संस्थाएं तो हैं, लेकिन उनमें आत्मा नहीं बची. उनका मानना है कि विपक्ष सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादा का अभिनय कर रहा है, जबकि हकीकत में जनता के साथ धोखा कर रहा है.
चौधरी ने अपने फ्रंटलाइन में लिखे लेख का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष अगर वास्तव में जनता के साथ है, तो उसे सड़क पर उतरना होगा, जनांदोलन खड़ा करना होगा, न कि ऐसी चुनावी प्रक्रियाओं को वैधता देना जो पहले से ही ‘किडनैप्ड डेमोक्रेसी’ का हिस्सा बन चुकी हैं.
बिहार में बढ़ते अपराधों पर बोले चिराग, मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करने का दुःख
बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन "एनडीए" में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है, जबकि राज्य विधानसभा का चुनाव सिर पर आ गया है. इसका कारण बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराध हैं, जो बीते कुछ समय से काफी बढ़ गए हैं. नतीजतन, नीतीश कुमार सरकार को गठबंधन के भीतर से ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले में पहले से ही नीतीश सरकार पर हमलावर रहे केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को एक बार फिर निशाना साधा. कहा - “मुझे दुख है कि मैं यहां ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, जहां अपराध पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है. इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा जिस तरह से बिहार और बिहारियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बिहार एक बहुत ही बुरे परिणाम की ओर बढ़ जाएगा.”
दरअसल, पासवान की यह टिप्पणी उस दिन आई जब राज्य एक महिला के साथ बलात्कार के एक और संगीन अपराध से हिल गया. पीड़िता होम गार्ड की परीक्षा देते समय बेहोश हो गई थी. उसके साथ एक एंबुलेंस के अंदर ड्राइवर और टेक्नीशियन ने मिलकर बलात्कार किया.
गया दौरे से पहले, पासवान ने मीडिया से कहा, “देखिए, एक के बाद एक, बिहार में आपराधिक घटनाओं की शृंखला चल रही है और प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों के आगे नतमस्तक दिख रहा है. यह सच है कि जो कुछ हुआ वो जितना निंदनीय और शर्मनाक हो सकता है, उतना ही है; कार्रवाई भी की गई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं. लेकिन पहला सवाल यह है कि आखिर ऐसे मामले बार-बार होते क्यों हैं? जिस तरह लगातार बिहार में हत्या, अपहरण, डकैती, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, यह अब ऐसी घटनाओं की एक सीरीज बन चुकी है और अब लगता है कि प्रशासन इन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रहा है.”
विकास बराला की नियुक्ति पर पूर्व अधिकारियों का एतराज
'द वायर' की रिपोर्ट है कि हरियाणा सरकार द्वारा विकास बराला को सहायक एडवोकेट जनरल नियुक्त किए जाने के खिलाफ देशभर के 45 से अधिक पूर्व IAS अधिकारियों ने विरोध जताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक खुला पत्र लिखकर इस फैसले को ‘बेटी बचाओ’ अभियान के खिलाफ बताया और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है.
विकास, भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे हैं. 2017 में उन्होंने एक युवती का पीछा करने (स्टॉकिंग) और यौन उत्पीड़न करने का आरोप झेला था. यह मामला उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था और भारी जन आक्रोश पैदा हुआ था. फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं और मुकदमा अभी लंबित है.
पूर्व IAS अफसरों की चिट्ठी में कहा गया है कि “एक गंभीर अपराध के आरोपी व्यक्ति को राज्य का कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करना, न्याय की मूल भावना के खिलाफ है.” 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रष्टाचार के एक मामले में P.J. थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. उसी मिसाल पर विकास बराला की नियुक्ति भी अमान्य होनी चाहिए. इस फैसले से न केवल पीड़िता को न्याय मिलने में बाधा आएगी, बल्कि यह हरियाणा की अस्मिता और महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है. पत्र में कहा है— “हम आग्रह करते हैं कि इस नियुक्ति को तत्काल रद्द किया जाए और इस केस का फास्ट-ट्रैक ट्रायल कराया जाए क्योंकि घटना को 7 साल से ज्यादा समय हो गया है.”
इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कई वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी शामिल हैं. इस नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारी विरोध हो रहा है. विपक्षी दलों और महिला संगठनों ने इसे “न्याय का मज़ाक” बताया है. वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
ट्रम्प ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम फिर याद दिलाया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तीन दिन से चल रहे भीषण संघर्ष को लेकर युद्धविराम की अपील की. ट्रम्प ने इसकी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष से भी तुलना की. उन्होंने कहा, "इस युद्ध में कई लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन यह मुझे भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष की याद दिलाता है, जिसे सफलतापूर्वक रोका गया था." ट्रम्प ने खुलासा किया कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बात की है और उनसे तुरंत युद्धविराम पर सहमति बनाने का आग्रह किया है. ट्रम्प ने यह भी कहा कि जब तक संघर्ष नहीं रुकेगा, वह इन दोनों देशों के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने इस स्थिति को भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के समान जटिल बताया, जिसे कूटनीति से सुलझाया गया था.
एनसीईआरटी स्कूलों में कराएगा ऑपरेशन सिंदूर की पढ़ाई
एनसीआरटी कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष मॉड्यूल तैयार कर रहा है. यह मॉड्यूल दो हिस्सों में होगा. पहला- कक्षा 3 से 8 के लिए और दूसरा- कक्षा 9 से 12 के लिए. इस मॉड्यूल में भारतीय सेना की वीरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य अभियान की गाथा शामिल की जाएगी. इसका उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रवाद, सेना के प्रति सम्मान और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है. अमृता मधुकल्या के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, चंद्रयान मिशन और इसरो की उपलब्धियों पर मॉड्यूल्स लाने जा रहा है. ये मॉड्यूल्स निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त होंगे और आने वाले शैक्षणिक सत्र में लागू किए जाएंगे. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को इन मॉड्यूल्स को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जो प्रत्येक विषय पर 8-10 पृष्ठों के होंगे. इनमें से एक मॉड्यूल पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर होगा, जबकि दूसरा चंद्रयान मिशन पर केंद्रित होगा. मॉड्यूल के माध्यम से छात्रों को रक्षा, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिलेगी. शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो व क्विज़ आदि सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छात्रों की समझ और विश्लेषण क्षमता भी विकसित हो सके. यह पहला अवसर है जब किसी सैन्य ऑपरेशन को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है.
वैकल्पिक मीडिया
मध्य प्रदेश में कुपोषण की भयावह तस्वीर पर हाईकोर्ट सख्त, सभी कलेक्टर्स से रिपोर्ट तलब
'द मूूकनायक' की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण और कुपोषणजनित बीमारियों की गंभीर स्थिति को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कैग (CAG) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं. इनमें से 1.36 लाख बच्चे गंभीर रूप से अतिकुपोषित हैं. वहीं, प्रदेश की महिलाओं में 57 प्रतिशत एनीमिया (रक्त की कमी) से पीड़ित हैं. इस पर हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए सभी जिलों के कलेक्टर्स से कुपोषण की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने राज्य शासन, मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता दिपांकर सिंह की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह सेंगर, अतुल जैन, अनूप सिंह सेंगर व कोविदा त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई. याचिका में पोषण ट्रेकर 2.0 और हालिया स्वास्थ्य सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए बताया गया है कि कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आ गया है. प्रोटीन और विटामिन की भारी कमी के कारण बच्चों की वृद्धि रुक रही है. वे औसत कद-काठी से छोटे (ठिगने) और बेहद दुर्बल हो रहे हैं. अंडरवेट यानी कम वजन वाले बच्चों के मामले में भी राज्य का स्थान दूसरे नंबर पर है.
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि गर्भवती महिलाओं, किशोरियों, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों के लिए वितरित किए जाने वाले पोषण आहार में भारी अनियमितताएं हैं. कैग रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पोषण आहार की गुणवत्ता और परिवहन व्यवस्था में करीब ₹858 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है.
बिहार में होमगार्ड की परीक्षा देने आई युवती के साथ एंबुलेंस में गैंग रेप
बिहार के गया जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 19 वर्षीय युवती को कथित रूप से दो एंबुलेंस कर्मचारियों ने उस समय बलात्कार का शिकार बनाया, जब वह बेहोश हालत में अस्पताल ले जाई जा रही थी. पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता, जो गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है, बिहार मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) की तीसरी बटालियन के बोद्धगया कैंपस में चल रही होम गार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान बेहोश हो गई थी.
अस्पताल में होश में आने के बाद युवती ने पुलिस को बताया कि एंबुलेंस कर्मचारियों ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. उसने पेट और निजी अंगों में तेज दर्द की शिकायत भी की, जिससे चलती एंबुलेंस में यौन उत्पीड़न की ओर इशारा मिला. पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह एंबुलेंस में हुई घटना के दौरान पूरी तरह सतर्क नहीं थी, क्योंकि वह बेहोश थी.
"तीन-चार लोग जो एंबुलेंस में मौजूद थे, उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया जब मैं बेहोश थी," युवती ने पुलिस को बताया. जांच अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी की समयावधि और रास्ते की पुष्टि भी हुई है.
ओड़िशा में आदिवासी लड़कियों के सरकारी हॉस्टल में यौन शोषण के मामले
“द टेलीग्राफ” में खबर है कि ओड़िशा में आदिवासी लड़कियों के सरकारी हॉस्टल में यौन शोषण के आरोपों ने राज्य सरकार के समक्ष खासी परेशानी पैदा कर दी है और उस पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है.
शनिवार को, बीजू जनता दल ने न्यायिक निगरानी में एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की, ताकि “सिस्टम की विफलता” और “गंभीर प्रशासनिक लापरवाही” की जांच हो सके. यह मांग तब आई जब कंधमाल जिले के दो अलग-अलग सरकारी आवासीय विद्यालयों की दो लड़कियों के गर्भवती होने की खबर सामने आई, जो राज्य भर में ऐसे मामलों की बढ़ती सूची में शामिल है.
पार्टी ने रायगढ़ा, मयूरभंज और कंधमाल के हॉस्टलों में रहने वाली आदिवासी लड़कियों के कम से कम चार गर्भधारण मामलों का हवाला दिया. बीजेडी ने आरोप लगाया, “ऐसे बहुत ही परेशान करने वाले घटनाक्रम सामने आए हैं, जिनमें आदिवासी लड़कियों का यौन शोषण और गर्भावस्था शामिल है, जो राज्य के देखरेख वाले हॉस्टलों में हैं."
शनिवार को ही एक और मामला सामने आया, जब केंद्रपाड़ा के डांगमाल गांव के नाग नारायण हाई स्कूल के एक शिक्षक को कक्षा-7 की लड़कियों के एक समूह के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में हिरासत में लिया गया. स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा सूचित किए जाने पर मरीन पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है.
16-18 साल के किशोरों में सहमति से बने यौन संबंधों को 'शोषण' न माना जाए, इंदिरा जयसिंह का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष
यह दलील 2012 में दायर एक याचिका के तहत दी गई है, जिसे अधिवक्ता निपुण सक्सेना ने दायर किया था. इसमें पॉक्सो (POCSO) कानून की उस धारणा को चुनौती दी गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु को स्वीकृत यौन संबंध के लिए न्यूनतम उम्र माना गया है. जयसिंह ने कहा, "16 से 18 साल की उम्र के किशोरों के बीच सहमति से बना यौन संबंध एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, जिसे अपराध के तौर पर देखना अनुचित है. इसे ‘शोषण’ नहीं माना जाना चाहिए.”
उनकी लिखित दलीलें किशोरों की यौन स्वायत्तता और आपसी सहमति के अधिकार के पक्ष में हैं, और वे कहती हैं कि कानून को व्यवहारिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है.
प्रोफाइल
सही समय पर सही जगह कैसे होना है, राजीव शुक्ला की तरक्की पर तरक्की का राज..
शुक्ला के पास सभी राजनीतिक दलों, कॉरपोरेट बोर्डरूम्स और ड्रेसिंग रूम्स में दोस्त हैं. सही समय पर फोटो खिंचवाने की उनकी अद्भुत क्षमता ऐसी है कि यह कांग्रेसी अब लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं.
'द प्रिंट' के लिए प्रशांत श्रीवास्तव ने राजीव शुक्ला का प्रोफाइल किया है. वर्ष 2000 में हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान, एक राजनीतिक दांव ने सभी का ध्यान खींचा. कांग्रेस की एक टूटी हुई शाखा, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के एक दिल्ली-आधारित पत्रकार को उम्मीदवार बनाया और ये थे राजीव शुक्ला.
केवल 22 विधायकों के समर्थन के साथ, उनके लिए जीत की संभावनाएं कम थीं; उन्हें सीट हासिल करने के लिए कम से कम 36 वोट चाहिए थे. राजनीतिक हलकों में संशय का माहौल था, लेकिन जब परिणाम घोषित हुए, तो शुक्ला ने 51 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया.
उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने बाद में स्वीकार किया कि क्या हुआ था. कई दलों के विधायकों ने शुक्ला के पक्ष में मतदान करने के लिए अपनी पार्टी लाइन को पार किया था.
वह चुनाव एक निर्णायक क्षण था जिसने शुक्ला की असाधारण क्षमता को उजागर किया—राजनीतिक विभाजनों के बीच पुल बनाने और प्रभाव डालने की. यह भारत के सबसे बहुमुखी शक्ति खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत थी, जो राजनीतिक हलकों, क्रिकेट स्टेडियमों, मीडिया सम्मेलनों या कॉरपोरेट सम्मेलनों में समान रूप से सहज हैं.
अब, 65 वर्ष की आयु में, वह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अंतरिम अध्यक्ष बनने की संभावना में हैं, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. शुक्ला वर्तमान में बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं.
‘द प्रिंट’ से बात करते हुए, उन्होंने याद किया कि अपने करियर के शुरुआती वर्षों में, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन राजनीति में प्रवेश करेंगे, लेकिन “किसी तरह, यह हो गया.”
“मैंने अपने पूरे करियर में (अच्छे) संबंध बनाए रखे हैं. मैं अभी भी अपने गृहनगर कानपुर और अपने राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हूं, जहां से मैंने पत्रकारिता, क्रिकेट प्रशासन और राजनीति में अपनी यात्रा शुरू की थी,” शुक्ला ने कहा.
पर्दे के पीछे के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के मामलों में केंद्रीय व्यक्ति तक, राजीव शुक्ला की यात्रा राजनीतिक समय, नरम शक्ति और रणनीतिक नेटवर्किंग की है—राजनीति, क्रिकेट और उससे परे. सही क्षणों पर फोटो खिंचवाने की उनकी अनोखी क्षमता ऐसी है कि यह कांग्रेसी अब लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं. ग्लैमर, शक्ति और खेल की दुनिया के बड़े नामों के साथ उनकी मुलाकातें अक्सर मीम फेस्ट को जन्म देती हैं.
बीसीसीआई में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मुखर आवाजों में से एक, सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने एक बार शुक्ला की भूमिका को “टमाटर” के रूप में परिभाषित किया था.
“मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बार शुक्ला को टमाटर कहा था. मुझे लगता है कि वह टमाटर की तरह हैं; सब्जी में भी हैं, सलाद में भी हैं,” कीर्ति आजाद ने द प्रिंट को बताया. “मैं उस व्यक्ति की सराहना करता हूं कि वह टमाटर है. अब मैं उसे जादूगर भी कहूंगा. चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, वह हमेशा मौजूद रहता है. वह कांग्रेस सांसद हैं लेकिन अमित शाह के बेटे के युग में बीसीसीआई प्रमुख बन रहे हैं.”
राजीव शुक्ला का जन्म कानपुर जिले के दर्शन पुरवा क्षेत्र में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उनके पिता, राम कुमार शुक्ला, एक वकील थे, और उनके नक्शेकदम पर चलते हुए, राजीव ने भी कानपुर के वीएस सनातन धर्म कॉलेज में कानून की पढ़ाई की. बाद में उन्होंने कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया. उनके बड़े भाई, दिलीप शुक्ला, भी कानपुर में रहने वाले पत्रकार हैं.
कानपुर के दर्शन पुरवा में मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे शुक्ला ने वीएस सनातन धर्म कॉलेज से कानून और क्राइस्ट चर्च कॉलेज से अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया. 1977 में सत्य संवाद में 200 रुपये मासिक वेतन के साथ पत्रकारिता शुरू की, फिर नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और दैनिक जागरण में काम किया. दिल्ली में 1980 के दशक में आए, जहां उनकी उल्कापात वृद्धि हुई.
कानपुर में कुछ लोग दावा करते हैं कि शुक्ला कॉलेज में एबीवीपी के सक्रिय सदस्य थे, लेकिन वह इससे इनकार करते हैं. मेरठ में जनसत्ता और फिर इंडियन एक्सप्रेस में काम के दौरान उन्होंने द्विभाषी पत्रकार के रूप में पहचान बनाई. रविवार पत्रिका में उनकी कवर स्टोरी ‘बेईमान राजा’ ने वी.पी. सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर तहलका मचाया, जिससे वह राजीव गांधी के करीब आए. “मैं 1990 तक स्कूटर से रिपोर्टिंग करता था,” वह हंसकर बताते हैं.
शुक्ला राजनीति, व्यवसाय, क्रिकेट और मनोरंजन की दुनिया को सहजता से जोड़ते हैं. 2004 में उन्होंने सोनिया गांधी के लिए शाहरुख खान की फिल्म स्क्रीनिंग आयोजित की. उनकी पत्नी अनुराधा प्रसाद बीएजी ग्रुप चलाती हैं, और उनके साले रविशंकर प्रसाद बीजेपी के दिग्गज हैं. शाहरुख, मुकेश अंबानी जैसे दिग्गजों से उनकी दोस्ती और फोटोज मीम फेस्ट का हिस्सा बनती हैं. “वह जानते हैं कि सही समय पर सही जगह कैसे होना है,” एक कांग्रेसी नेता कहते हैं.
1997 में नरेश अग्रवाल की लोकतांत्रिक कांग्रेस के जरिए राज्यसभा पहुंचे. 2003 में वह और सिराज मेहंदी कांग्रेस की ओर बढ़े. अहमद पटेल और प्रियंका गांधी के समर्थन से वह पार्टी के भरोसेमंद नेता बने. 2020 में हिमाचल प्रदेश प्रभारी बनाए गए, जहां उन्होंने तीन गुटों को संतुलित किया. “मैंने कहा, ‘महल बनाओ, सबको कमरे मिलेंगे; खंडहर रहा, तो कुछ नहीं,’” वह बताते हैं. 2022 में छत्तीसगढ़ से फिर राज्यसभा पहुंचे और 2025 में सीडब्ल्यूसी में शामिल हुए.
1989 में यूपीसीए के जरिए बीसीसीआई में आए. 2002 में भारतीय टीम के मीडिया मैनेजर बने, 2011 में आईपीएल अध्यक्ष. 2020 से बीसीसीआई उपाध्यक्ष हैं. “वह बोर्ड और क्रिकेटरों के बीच पुल हैं,” प्रशासक अमृत माथुर कहते हैं.
“वह सबके सबसे अच्छे दोस्त हैं,” राजदीप सरदेसाई कहते हैं. एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में शुक्ला ने हारने वाली सांसदों XI से जीतने वाली पत्रकारों XI की ओर पक्ष बदल लिया. “मैंने कहा, ‘आप सांसदों की तरफ थे.’ उन्होंने हंसकर कहा, ‘तो क्या? मैं भी पत्रकार हूं,’” सरदेसाई याद करते हैं. कानपुर के लेखक संजीव मिश्रा उन्हें “मस्त मौला कानपुरिया” कहते हैं. “वह अपनी जड़ें नहीं भूलते. हर कानपुरिया उनके दिल्ली घर में स्वागत पाता है.”
बंगाली मज़दूर को बंदूक की नोंक पर बांग्लादेश में धकेला गया
पश्चिम बंगाल के एक 19 वर्षीय प्रवासी मज़दूर के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे राजस्थान में दो महीने तक हिरासत में रखने के बाद सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा बंदूक की नोक पर जबरन बांग्लादेश में धकेल दिया गया. स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार, अमीर शेख नाम के इस युवक का एक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद यह मामला सामने आया, जिसमें वह बांग्लादेश के निवासियों को अपनी आपबीती सुना रहा है. इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
वीडियो में अमीर शेख को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह पश्चिम बंगाल के मालदा का निवासी है और काम के सिलसिले में राजस्थान गया था, जहां राज्य पुलिस ने उसे बांग्लादेशी होने के संदेह में पकड़ लिया. शेख का दावा है कि उसने पुलिस को अपना आधार कार्ड और माता-पिता के दस्तावेज़ दिखाए, लेकिन वे नहीं माने. उसके चाचा, मोहम्मद अजमौल शेख ने स्क्रॉल को बताया कि अमीर को रिहा करने के लिए राजस्थान पुलिस ने 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसे परिवार दे नहीं सका, और उसे दो महीने हिरासत केंद्र में बिताने पड़े. परिवार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जब तक कि यह वीडियो सामने नहीं आया. परिवार ने पश्चिम बंगाल में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनके पास 1950 के दशक से भारत में रहने के दस्तावेज़ मौजूद हैं.
यह घटना उन रिपोर्टों के बीच आई है, जहां तृणमूल कांग्रेस लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में बंगाली भाषी प्रवासी मज़दूरों को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिए जाने पर चिंता जता रही है. खासकर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद, कई भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम हैं, को हिरासत में लेकर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है. हाल ही में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी भारत से बिना उचित प्रक्रिया के लोगों को अवैध रूप से बांग्लादेश निर्वासित करना बंद करने का आग्रह किया है.
बुलडोज़र चलते रहेंगे और सियासी दल चुप रहेंगे!
भारत में बुलडोजर अब केवल एक निर्माण मशीन नहीं रह गया है. यह राज्य की ताकत का एक प्रतीक बन गया है, जिसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाने और ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है. स्क्रॉल में प्रकाशित विस्तृत लेख में, शोधकर्ता इस्माइल सलाउद्दीन तर्क देते हैं कि इन विध्वंस कार्रवाइयों को सबसे अधिक बल राजनीतिक दलों की गहरी चुप्पी से मिल रहा है. वे इस खतरनाक प्रवृत्ति को मुस्लिम समुदाय के दर्द को एक संवैधानिक संकट के बजाय एक राजनीतिक बोझ मानने की मानसिकता से जोड़ते हैं.
सलाउद्दीन असम के गोलपाड़ा में 600 से अधिक मुस्लिम घरों को "अवैध अतिक्रमण" बताकर गिराने, दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद विध्वंस जारी रखने और अहमदाबाद में "अवैध बांग्लादेशियों" के नाम पर हजारों घरों को उजाड़ने जैसी घटनाओं का उदाहरण देते हैं. वे इसे इतालवी दार्शनिक जियोर्जियो एगाम्बेन के "अपवाद की स्थिति" (state of exception) के सिद्धांत से जोड़ते हैं, जहां राष्ट्रहित के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है और कानून खुद सजा का एक हथियार बन जाता है. गोलपाड़ा की एक पीड़िता फातिमा बेगम कहती हैं, "हमने एक दिन में सब कुछ खो दिया. अब मेरे बच्चे गर्मी और बारिश में पीड़ित हैं. हम केवल सम्मान और सुरक्षा चाहते हैं.".
लेख का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों की भूमिका पर सवाल उठाना है. सलाउद्दीन कहते हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों की ओर से इस मुद्दे पर कोई गंभीर राजनीतिक विरोध या निरंतर आक्रोश नहीं दिखा है. इन दलों की चुप्पी के पीछे एक खतरनाक राजनीतिक गणित काम कर रहा है: मुसलमानों को भाजपा का विरोधी मानकर यह सोच लिया गया है कि वे वैसे भी विपक्ष को ही वोट देंगे, तो फिर हिंदू वोटों को नाराज करने का जोखिम क्यों उठाया जाए. इस चुप्पी ने भाजपा द्वारा शुरू किए गए इस खतरनाक रास्ते को और चौड़ा कर दिया है. सलाउद्दीन चेतावनी देते हैं कि यह केवल एक 'मुस्लिम मुद्दा' नहीं है. जब एक समुदाय की नागरिकता सौदेबाजी का विषय बन जाती है, तो देश के सभी नागरिक कमजोर हो जाते हैं. वे कहते हैं कि टूटते हुए घरों की आवाज और मशीनों की लगातार गूंज के बीच हम एक गणराज्य के गायब होने की ध्वनि सुन रहे हैं.
पंकज राग: 'जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहां हैं' सामाजिक असमानता और मोहभंग को दर्शाते हैं
'हरकारा डीपडाइव' के इस खास एपिसोड में निधीश त्यागी ने मशहूर संगीत इतिहासकार, कवि और पूर्व नौकरशाह पंकज राग से गुरुदत्त के संगीत और उनकी फिल्मों की विरासत पर बात की. पंकज राग की कई किताबें, जैसे धुनों के सहारे और कैफे सिने संगीत, बॉलीवुड संगीत के गहन अध्ययन को दर्शाती हैं.
पंकज राग के अनुसार, गुरुदत्त को संगीत की गहरी समझ थी, और उनकी फिल्मों में गीतों का फिल्मांकन (पिक्चराइजेशन) बेजोड़ था. ट्रॉली शॉट्स, लाइट और शेड का इस्तेमाल, और 75-100 एमएम फोकल लेंस का उपयोग उनके गीतों को विशाल और आकर्षक बनाता था. गुरुदत्त शुरू में फिल्मों में गीतों के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि गीत कथानक को बाधित करते हैं. फिर भी, विडंबना यह है कि उनकी फिल्मों के गीत आज भी सदाबहार हैं.
गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी (1951) एक रोमांटिक थ्रिलर थी, जिसमें साहिर लुधियानवी के गजलनुमा गीत 'तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले' और क्लब सॉन्ग्स जैसे 'शर्माए काहे' ने आधुनिकता का रंग भरा. ओपी नय्यर और एसडी बर्मन जैसे संगीतकारों के साथ गुरुदत्त ने हल्के-फुल्के और संजीदा दोनों तरह के गीतों को बखूबी पेश किया. आरपार (1954) के 'बाबूजी धीरे चलना' और मिस्टर एंड मिसेज 55 के 'उधर तुम हंसी हो' जैसे गीतों ने उस दौर के उभरते मध्यम वर्ग की नब्ज पकड़ी. उन्होंने यह भी कहा कि साहिब बीबी और ग़ुलाम जैसी फ़िल्में केवल स्त्री-विमर्श नहीं थीं, बल्कि भारतीय समाज की संरचनाओं और भावनात्मक असंतुलनों का दस्तावेज़ भी थीं.
प्यासा (1957) और कागज के फूल (1959) में गुरुदत्त ने संजीदा संगीत को अपनाया. प्यासा का ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है और 'जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहां हैं' जैसे गीत सामाजिक असमानता और मोहभंग को दर्शाते हैं. कागज के फूल में 'वक्त ने किया क्या हंसी सितम' और 'देखी जमाने की यारी' जैसे गीतों का फिल्मांकन कैफी आज़मी की लेखनी और वीके मूर्ति की सिनेमैटोग्राफी के साथ बेमिसाल था. साहब बीवी और गुलाम (1962) को पंकज राग गुरुदत्त का सर्वश्रेष्ठ साउंडट्रैक मानते हैं, जिसमें 'पिया ऐसो जिया में समाए गयो' और 'कोई दूर से आवाज दे' जैसे गीत सामंतवाद के अंत को दर्शाते हैं.
गुरुदत्त की पत्नी और मशहूर गायिका गीता दत्त उनकी फिल्मों की प्रमुख आवाज थीं. आज सजन मोहे अंग लगा लो जैसे गीतों में उनकी शालीन गायकी ने मध्यम वर्गीय दर्शकों को भी आकर्षित किया. हालांकि बाद में आशा भोसले ने भी कुछ गीत गाए, लेकिन गीता दत्त की शोख और संजीदा गायकी गुरुदत्त के संगीत की आत्मा रही.
गुरुदत्त का संगीत उनके डांस और ड्रामा के अनुभव से प्रभावित था। उदय शंकर के साथ उनके शुरुआती दिन और प्रभात स्टूडियो में कोरियोग्राफी का अनुभव उनके गीतों के फिल्मांकन में साफ झलकता है. उनके गीत, चाहे हल्के-फुल्के हों या उदास, हर मूड को छूते हैं और आज भी गुनगुनाए जाते हैं. पंकज राग कहते हैं कि गुरुदत्त का संगीत राज कपूर और आरडी बर्मन की तरह सदाबहार है, जो हर पीढ़ी को प्रेरित करता है.
चलते-चलते
'द कॉल ऑफ म्यूजिक': हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया के अनकहे संघर्ष
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया बाहर से जितनी राजसी और आकर्षक दिखती है, उसके भीतर कलाकारों के संघर्ष, लिंग भेद और सामाजिक पूर्वाग्रहों की उतनी ही गहरी और अनकही कहानियां छिपी हैं. प्रिया पुरुषोत्तम की नई किताब 'द कॉल ऑफ म्यूजिक' इन्हीं अनसुनी आवाजों और संघर्षों को सामने लाती है. स्क्रॉल में प्रकाशित एक समीक्षा में, संस्कृति समीक्षक मालिनी नायर बताती हैं कि यह किताब सिर्फ संगीत के महान दिग्गजों की महिमा का बखान नहीं करती, बल्कि आज के उन संगीतकारों के जीवन की पड़ताल करती है जो इस परंपरा के भीतर अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रहे हैं.
प्रिया पुरुषोत्तम, जो स्वयं आगरा घराने की एक स्थापित गायिका हैं, ने आठ संगीतकारों की जीवन यात्रा के माध्यम से इस दुनिया की जटिलताओं को उजागर किया है. किताब उन साहसिक सवालों को उठाती है जिनसे संगीत जगत अक्सर बचता है. उदाहरण के लिए, वायलिन वादक कला रामनाथ अपने अनुभव साझा करती हैं कि कैसे एक ही स्तर के पुरुष कलाकार की तुलना में उन्हें सम्मान और उचित फीस पाने के लिए दोगुना संघर्ष करना पड़ता है. वे कहती हैं, "लोग महिलाओं को गंभीरता से नहीं लेते... आज भी संगीतकारों द्वारा आयोजित समारोहों में मेरे साथ बुरी तरह से बर्ताव किया जाता है..".
इसी तरह, आगरा घराने की गायिका शुभादा पराडकर को उनकी दमदार और खुली आवाज में गायकी के लिए "मर्दाना" और "आक्रामक" कहकर आलोचना झेलनी पड़ी. उन्होंने इस लैंगिक पूर्वाग्रह पर सवाल उठाते हुए कहा, "हमें इसमें लिंग लाने की आवश्यकता क्यों है. एक कलाकार को कलाकार के रूप में समझें, महिला या पुरुष के रूप में नहीं.". किताब सारंगी वादक सुहैल यूसुफ खान के माध्यम से मिरासी जैसे वंशानुगत मुस्लिम संगीतकार समुदायों के खिलाफ जातिगत पूर्वाग्रह के मुद्दे को भी छूती है. 'द कॉल ऑफ म्यूजिक' कलाकारों के अथक रियाज, गुरु-शिष्य परंपरा की जटिलताओं और कला के आदर्शों तथा बाजार की वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों को भी गहराई से दर्शाती है. मालिनी नायर के अनुसार, यह पुस्तक संगीतकारों के जबरदस्त लचीलेपन का जश्न तो मनाती ही है, साथ ही उन असहज सच्चाइयों का सामना करने का साहस भी दिखाती है जो इस महान परंपरा का हिस्सा हैं.
वैसे प्रिया पुरुषोत्तमन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एक बेहतरीन युवा गायिका है. उनका एक हालिया गायन यहां सुनिये. आपका इतवार थोड़ा उजास हो जाएगा.
पाठकों से अपील :
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.